संस्कृतिः पहली चौथाई के अंधेरे
पैसा पिस्तौल है, उसका घोड़ा कब दबाना है, यह जानना राजनीति है।’’ मारियो पूजो के प्रसिद्ध उपन्यास गॉडफादर पर बनी फिल्मत्रयी का यह महान डायलॉग डॉन लुकेसी ने 1990 में कहा था। क्या ही इत्तेफाक है कि बिलकुल उसी साल भारत के माथे पर पूंजी की पिस्तौल एकदम तन चुकी थी, बस गोली चलने की देरी थी। यानी, बस राज्यादेश का इंतजार था और ठांय! आइएमएफ के कर्ज तले नई आर्थिक नीति 1989 में भी आ सकती थी, लेकिन राजनीति ने उसे दो साल रोके रखा। 1991 की जुलाई में जब पूंजी की गोली चली, तो हिंदुस्तान के समाज में पसरा बरसों का सौहार्दपूर्ण सन्नाटा एक झटके में शहीद हो गया।
तब से लेकर आज तक, हमने कभी नहीं पूछा कि नई आर्थिक नीतियों की बंदूक के छर्रे किस-किस को लगे। फिल्म में भी डॉन से विन्सेन्ट ने कभी नहीं पूछा था कि पूंजी की गोली चलेगी, तो लगेगी किसको। राजनीति और पूंजी के इस खूनी खेल में शायद मरने वाले की परवाह न की जाती हो, लेकिन विडंबना देखिए कि आज जब हम बदली हुई दुनिया में इक्कीसवीं सदी की पहली चौथाई की मुंडेर पर खड़े होकर एक अगाध गर्त में झांक रहे हैं, तो हमें यहां तक पहुंचाने वाले को चौतरफा श्रद्धा के फूल अर्पित किए जा रहे हैं।

एक शतकः कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस (दाएं) के 2025 में एक साथ सौ वर्ष हो रहे हैं

बीते दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिवंगत हुए डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लाई गई नई आर्थिक नीति ने भारत के समाज, संस्कृति और मनुष्य को जिस कदर बदला वह अभूतपूर्व तो है ही, उदारीकरण के पैरोकारों के आकलन के हिसाब से अप्रत्याशित भी है। भारत के समाज में जितना दो सौ साल में नहीं बदला था, पूंजी और राजनीति की जुगलबंदी ने महज ढाई दशक में उससे कहीं ज्यादा बदल डाला। इस बदलाव की जड़ें जिन लोगों और ताकतों तक जाती हैं, वे खुद आज अपनी बनाई दुनिया को पहचान पा रहे होंगे, इसमें शक है। उनके बरअक्स जिन ताकतों ने पूंजी की राजनीति के खिलाफ दुनिया को मनुष्यता के हक में बदलने के उद्यम किए वे भी बदल चुकी दुनिया को देखकर हतप्रभ हैं और पार्श्व में जा चुके हैं।
कोई भी समाज अपने आप नहीं बदलता। संस्कृति तो बहुत धीरे-धीरे बदलती है। इस बदलाव के पीछे राजनीतिक-आर्थिक ताकतें काम करती हैं। राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम के दबावों से सांस्कृतिक घटनाक्रम उपजते हैं। आजादी का आंदोलन इसका गवाह है। राजनीति के हित में अर्थ का जब हमला होता है, तो गोली समाज के सीने पर लगती है, संस्कृति के माथे पर लगती है, इतिहास की आंख पर लगती है।
नब्बे के दशक में अपने यहां यही हुआ। नई आर्थिक नीतियों और परिणामस्वरूप बदली घरेलू और वैश्विक राजनीति के दबाव में समाज की संवेदना गुणात्मक रूप से बदलने लगी थी। सांस्कृतिक विवेक चोटिल हो गया था। इतिहासबोध घायल हुआ था। जैसे किसी ने शांत तालाब में पत्थर की एक सिल्ली गिरा दी हो। सांस्कृतिक रूप से बरसों से तकरीबन ठहरे हुए समाज की सतह दरकी, तो स्मृतियों की निरंतरता टूट गई। इससे इतिहासबोध विकृत हो गया। विवेक चरने चला गया।
इक्कीसवीं सदी की दूसरी चौथाई का आरंभ एक ऐसा मौका है जब हमें थोड़ा ठहर कर कुछ जरूरी सवाल पूछने चाहिए। डॉ. मनमोहन सिंह का निधन बेशक इसका एक अहम और मौजू बहाना है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि 2025 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सौ साल पूरे हो रहे हैं, जिसने लगातार इस देश को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चाशनी में पागने की अथक मेहनत की है और नतीजतन आज केंद्रीय सत्ता में है। इसी के समानांतर, बीते 26 दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी अपनी स्थापना के सौवें साल में लग गई है, जो दक्षिणपंथ के खिलाफ प्रगतिशील संस्कृति की निरंतर वाहक रही है लेकिन आज ऐतिहासिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति में है। इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 2025 भारतीय गणतंत्र के लिए सांस्कृतिक रूप से बहुत अहम वर्ष है। दक्षिणपंथी संघ से लेकर वामपंथ और मध्यमार्गी कांग्रेस ने इस समाज पर जितनी गोलियां दागी हैं, उनके जख्मों का जायजा लेने का यही सही वक्त है।
राष्ट्रीय संस्कृति के दो सिरे
किसी भी समाज की संस्कृति एक दिन में नहीं बनती। उसे बनने में बरसों लगते हैं। जब हम कहते हैं कि भारत गंगा-जमुनी तहजीब का देश है, तो यह भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिकता को बताता है। जब हम कहते हैं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है, तो यह इस संस्कृति की भौगोलिकता को बताता है। जब हम कहते हैं कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, तो यह इस देश की बुनावट को बतलाता है। संस्कृति के ये तीन आयाम- ऐतिहासिकता, भौगोलिकता और बुनावट जब तक अक्षुण्ण रहे, तब तक राजनीति भी कमोबेश लोकतांत्रिक बनी रही। इस संस्कृति पर पूंजी और बहुसंख्यकवाद के समानांतर हमले से तीव्र बदलाव आया। बाबरी विध्वंस, मंडल आंदोलन, रूस के विघटन और नवउदारवाद से परिभाषित 1991-92 का दौर इसलिए ढाई दशक के बदलावों को समझने में निर्णायक है।
उस दौर की संसद की बहसों को देखा जाना चाहिए। अजब इत्तेफाक है कि नवउदारवाद का विरोध कम्युनिस्ट पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समान रूप से कर रही थीं। दोनों के विरोध के पीछे तर्क पद्धति और राजनीति भले अलग-अलग हो। संसदीय कम्युनिस्टों के सामने हालांकि सांप्रदायिकता की दूसरी चुनौती भी थी। उन्हें चुनना था कि नवउदारवाद प्राथमिक शत्रु है या हिंदू सांप्रदायिकता। वामपंथी दलों ने सांप्रदायिकता को प्राथमिक शत्रु माना और कांग्रेसनीत नवउदारवाद को आने दिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि न तो बाबरी बचेगी, न ही कालान्तर में भाजपा को सत्ता में आने से कांग्रेस रोक पाएगी। उस समय हिंदू सांप्रदायिकता को प्राथमिक शत्रु मानने में दिक्कत नहीं थी, बशर्ते कांग्रेस और वाम इस समाज को उसका विकल्प दे पाते।
बाबरी विध्वंस के महज छह साल बाद 1998 में पहली बार सत्ता में आए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने पहला हमला संस्कृति पर बोला। पाठ्यक्रमों से लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं तक उसने संघ का वैचारिक एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। इसमें उसे खास दिक्कत नहीं हुई क्योंकि घर-घर तक राम को पहुंचाने का काम दूरदर्शन के माध्यम से कांग्रेस बरसों पहले कर चुकी थी। इस संदर्भ में यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस गाय को लेकर 2014 के बाद पूरा देश जला, वह गाय कभी अपने बछड़े के साथ इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस (आर) का चुनाव चिह्न थी।
इस देश में हिंदुओं की पार्टी शुरू से कांग्रेस ही थी, लेकिन उसने धर्म को राजनीति से मोटे तौर पर दूर रखा था। भाजपा ने अपने मातृ संगठन आरएसएस के एजेंडे पर चलते हुए धर्म को ही राजनीति का खूंटा बना लिया और अभय मुद्रा वाले राम-हनुमान तथा औघड़ मुद्रा वाले शिव को आक्रामक दंडदाताओं में तब्दील कर डाला। कांग्रेस के पास इसकी कोई काट नहीं थी। वाम ने तो कभी माना ही नहीं कि धर्म की राजनीति को वर्ग-संघर्ष के अलावा किसी और चीज से टक्कर दी जा सकती है। बाकी समाजवादी, लोहियावादी और दूसरे किस्म के सामाजिक न्यायवादी सत्ता में हिस्सेदारी की परिवारवादी राजनीति तक सिमट कर अपनी विश्वसनीयता गंवा बैठे। इस तरह संघ का विचार इस देश का सांस्कृतिक नैरेटिव बन गया। सह-अस्तित्व, बहुलतावाद और समावेश की जो संस्कृति सामाजिक ताने-बाने को सदियों से बचाए हुए थी, वह खतरे में पड़ गई।
संस्कृति के मोर्चे पर यह बदलाव धर्म के रास्ते आया है, इस बात को याद रखना जरूरी है। संघ एकै चालकानुवर्तिता के मंत्र पर चलता है। इस विचार में संचालक केवल एक है, बाकी सब अनुयायी। जैसे एक चरवाहा और बाकी भेड़ें। जब चरवाहा एक होता है, तो धर्म एकाश्म हो जाता है- एक आदमी चराएगा, बाकी चरेंगे। ऐसे ही नहीं संघ एक कुआं, एक श्मशान, एक टैक्स, एक चुनाव, एक देश की बात करता है। एकल पर यह जोर विविधता और बहुलता का सीधा दुश्मन है। धर्म की एकाश्मता संस्कृति को एकरंगा बना देती है, गंगा-जमुनी प्रवृत्ति को नष्ट कर देती है। यह संघ के विद्वानों के सोचे-समझे राजनीतिक दर्शन की उपज है।
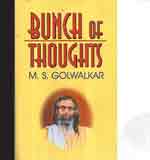
गुरु गोलवलकर की पुस्तक
गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में दुश्मन के रूप में तीन 'म' गिनवाए हैं- मुसलमान, मार्क्सवादी और मैकाले यानी ईसाई। भाजपा की समकालीन राजनीति का यही आधारपत्र है। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान का धर्म-आधारित राष्ट्र बनना जबकि भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य बनना संघ की छाती में गड़ा ऐसा शूल है जिसके लिए वह सौ साल से कलप रहा है। उसके पास एक अधूरा प्रोजेक्ट है, जिसे अपने सौवें साल यानी 2025 में उसे अंजाम पर पहुंचाना है। उसकी डेडलाइन तय है और एजेंडा भी। बाकी के पास क्या है?
कांग्रेस के पास आजादी के बाद राष्ट्र-निर्माण का प्रोजेक्ट था। नेहरू की मौत के बाद ही यह सपना खटाई में पड़ गया। फिर उसने कोई सपना न पाला, न जनता को दिखलाया, बल्कि अपने गढ़े बूढ़े, बौने, विकलांग लोकतंत्र में दंगों से लेकर इमरजेंसी, बाबरी विध्वंस, शाहबानो और उदारीकरण के अमिट धब्बे लगा दिए। वामपंथियों का प्रोजेक्ट साम्यवाद शुरू से ही टैक्टिक्स के नाम पर संसदीय गड्ढे में फंस गया था, अब वह वहीं कई टुकड़े में दम तोड़ रहा है। लोहियावादी, सर्वोदयी और तमाम दूसरे किस्म के समाजवादियों का विचार इनके नेताओं के सशक्तीकरण और अवसान के साथ ही खत्म हो गया। ऐसे में जो काम दूसरी राजनीतिक पार्टियों को करना था, वह काम सिविल सोसायटी और एनजीओ सतही तौर पर कर रहे हैं- वे 'आइडिया ऑफ इंडिया' की याद दिलाते हुए प्रतिरोधी जलसों में जुटे हुए हैं। उनके पास संस्कृति की कोई ठोस राजनीति नहीं है, तो घूम-फिर के उनका किया-धरा कांग्रेस की चुनावी झोली में जा गिरता है।

राम मंदिर से बहुत पहलेः दूरदर्शन पर रामायण के जरिये घर-घर पहुंचे थे राम
इस तरह संस्कृति के दो मोटे अध्याय- एक, आजादी के आंदोलन से निकला भारतीय राष्ट्रवाद और दूसरा, संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद- इस देश में सौ साल के दौरान चली राजनीति के साये में विकसित या विकृत होकर अपने-अपने मौजूदा अंजाम तक पहुंचे हैं। इस व्यापक विरोधाभासी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समाज की अपनी रोजमर्रा की देसी-स्थानिक संस्कृति ने जो बदलाव महसूस किए, वहां हम पूंजी की भूमिका की शिनाख्त कर सकते हैं। पूंजी अपने साथ तकनीक और प्रौद्योगिकी लेकर आई थी। तकनीक-प्रौद्योगिकी ने राज्य और नागरिक के बीच मध्यस्थता कर के व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया और पहले से मौजूद विभाजनों को और तीखा कर दिया। इसकी शुरुआत हम अस्सी के दशक की शुरुआत में टीवी के आने से मान सकते हैं, जब पहली बार पूरे देश ने सरकारी प्रसारक दूरदर्शन पर भगवान राम के दर्शन किए थे और विज्ञापनों को देखकर यह जाना कि दो मिनट में पेट कैसे भरा जा सकता है, पड़ोसी का सामान देखकर जलना चाहिए और अपनी कमीज दूसरे की कमीज से सफेद होनी चाहिए। सामूहिकता और सहकारिता पर जीते आ रहे उदारमना समाज को टीवी सबसे पहला झटका था।
देसी संस्कृति
पीछे मुड़कर देखने पर हमें सतही तौर से यही लगता है कि बीते कुछ दशक का इतिहास अनिवार्यतः तकनीकी और प्रौद्योगिकी का इतिहास रहा है। ऐसा वास्तव में नहीं है। तकनीक, प्रौद्योगिकी, उपकरणों और मीडिया की आमद पूंजी की चेरी है। उसे पूंजी के हित में आना ही था। नब्बे के दशक में जिस किस्म के ढांचागत समायोजन और कथित सुधारों की शर्तें भारत पर थोपी गईं, वे बिना प्रौद्योगिकीय विकास और उपकरणों के संभव हो ही नहीं सकती थीं। इन उपकरणों ने हमारी सामान्य जिंदगी और श्रम से खाली बचने वाले समय के साथ जो खिलवाड़ किया, उसने हमारी रोजमर्रा की स्थानिक संस्कृतियों को हमेशा के लिए बदल डाला।
हाल ही में गुजरे फिल्मकार श्याम बेनेगल ने 1992 में धर्मवीर भारती की कहानी पर सूरज का सातवां घोड़ा नाम की फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में नायक और नायिका सवाल की शक्ल में एक गीत गाते दिखे थे, ‘ये शामें / सब की सब शामें / क्या इनका कोई अर्थ नहीं...?’ यह सवाल मामूली नहीं था। यह इंसानी सभ्यता से जुड़ा एक बुनियादी सवाल था। कथाकार काशीनाथ सिंह के मशहूर उपन्यास ‘काशी का अस्सी’ में जम्बूद्वीप की शामों का जिक्र है, जिससे अंग्रेजों को दिक्कत थी। उन्हें दिक्कत शामों में छुपी उस संस्कृति से थी जिसके साथ जनता की राजनीति नत्थी थी। सो, उन्होंने चौबीस घंटे के दिन-रात में से शाम को खत्म कर दिया। इसी तर्ज पर नई आर्थिक नीति ने पहले संस्कृति से राजनीति को बाहर निकालकर उसे खोखले मनोरंजन में बदला, फिर शामों को ही धीरे-धीरे खा गई।
जहां कहीं शामें राजनीतिक या अराजनीतिक हुआ करती थीं, हर उस जगह अब शामों का एक रंग-रूप देखने को मिलता है। इसकी शक्ल बीते तीन दशकों में हुई तकनीकी तरक्की ने तय की है और अलग-अलग किस्म की सत्ताओं ने अपने पक्ष में शामों का इस्तेमाल मुकम्मल कर लिया है। अब दिल्ली के कॉफी हाउस से बगावत की चिंगारी नहीं उठती, मार्केटिंग के फॉर्मूले निकलते हैं। अब शाम उत्तेजक बौद्धिक चर्चाओं वाली पार्टी (गोविंद निहलाणी, 1984) के नाम नहीं होती, टीवी के परदे पर राष्ट्रवादी बुलेटिनों में उबलती है। बीते ढाई दशक में हमारे खाली समय का बुनियादी चरित्र बदल डाला गया है। शामें बदलने लगीं, तो सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत पसंद, नापसंद, साझा संघर्ष और साझे सपने भी बदले।
यह उपभोक्तावाद का दौर था, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां इंसानों को खरीदारों में बदल रही थीं। हमें बताया जा रहा था कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं, और क्या चाहना चाहिए। ड्राईंग रूम में हमें कैद कर के हमारी कामनाओं की नकली सूची बनवाई जा रही थी। इन्हीं निजी कामनाओं के इर्द-गिर्द लोकप्रिय विमर्श भी टीवी से संचालित होने लगा। केबल नेटवर्क के आने से चुनने के विकल्प बढ़े, तो प्रसारण में सरकारी शाकाहार का अंत हुआ। यह शाकाहार भारतीयों के जीवन से भी जाता रहा। खानपान और सामाजिक आदतों से शाकाहार का विसर्जन नब्बे के दशक के अंत में इंटरनेट के आगमन के साथ इंसानी मूल्यों से समझौते तक चला आया। टीवी के बाद मनुष्य को समाज, समूह, समुदाय और घर-परिवार से अलग करने का अगला चरण इंटरनेट ने चलाया। टीवी ने नकली कामनाएं जगाई थीं, इंटरनेट दो कदम आगे बढ़कर हमारी कामनाओं की जासूसी करने लगा।
आज जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं, उसका पूर्ववर्ती संस्करण आर्पानेट था जिसे 1989 में खत्म कर दिया गया क्योंकि सत्तर के दशक में अमेरिका में हुए सेना की फाइलों से जुड़े एक घोटाले में यह बात सामने आ गई थी कि इंटरनेट का इस्तेमाल लोगों की जानकारियों को चुराने के लिए सरकारी रक्षा एजेंसियां करती हैं। इसका नाम बदलकर नब्बे के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब (डब्लूडब्लूडब्लू) कर दिया गया। इंटरनेट आने के बाद भारत का नागरिक वैश्विक नागरिक हो गया, लेकिन उसकी निजता वैश्विक ताकतों के हवाले हो चुकी थी। दिलचस्प यह है कि कोई डेढ़ दशक तक हम इंटरनेट को अनजाने में यह सिखाते रहे कि भविष्य में हमें ही कैसे बेदखल किया जाना है। अपनी मेधा हमने इंटरनेट को दी, अब वह हमें बेरोजगार करने की ताकत पा चुका है।
इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में इंटरनेट वाला मोबाइल जब घर-घर पहुंच गया, तो लोग खुद अपनी निजता को बाजार में दांव पर लगाने लगे। सदियों से ठहरा हुआ एक समाज खुद को अभिव्यक्त करने का सस्ता साधन तो पा चुका था, लेकिन लोकतंत्र के एक नागरिक के बतौर अभिव्यक्ति का शऊर और उसे बचाने की सलाहियत उसमें कभी नहीं भरी गई थी। लिहाजा इस समाज में अभिव्यक्तियों की फसल बिना जड़ के लहलहाने लगी। अभिव्यक्ति अब सस्ता शौक बन चुकी थी। पहले टीवी आया, फिर टेप, वॉकमैन, डीवीडी, पेजर, ब्लूटूथ, मोबाइल। हर नया साधन पिछले को खत्म करता गया और इसके साथ मनुष्य के चौबीसों घंटे पर तकनीक का कब्जा होता गया। बीतेक दसेक साल में पैदा हुई मोबाइल अभिव्यक्तियों ने मनुष्य को आत्मरतिग्रस्त बनाकर हादसों को जन्म देना शुरू कर दिया। सेल्फी लेते वक्त हुई मौतें इसका शुरुआती उदाहरण बनीं। अब मामला हनीट्रैप और डिजिटल अरेस्ट तक आ पहुंचा है।
निजी अभिव्यक्ति के लोकतांत्रीकरण का दूसरा प्रभाव यह हुआ है कि विशेषज्ञता के पेशे खतरे में पड़ गए हैं। अब हर कोई हर चीज का विशेषज्ञ है। इसलिए संस्कृति के अहम घटक, जैसे इतिहास, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान, भाषा, आदि सब कुछ इंटरनेट का मोहताज है। समाज का अर्जित सामूहिक ज्ञान और अनुभव आज कठघरे में है। इसने साझेपन को बट्टा लगा दिया है। सामूहिकता को ‘वर्चुअल’ बना दिया। 2020 के मार्च में आई कोरोना महामारी ने बची-खुची कसर पूरी कर दी।
अतिवाद की महामारी
टीवी ने सबसे पहले बताया कि क्या काम्य है, मोबाइल ने नकली कामनाओं की लत लगवा दी। जब कामनाएं बाहरी साधनों पर निर्भर हो गईं, तभी महामारी आ गई। कामनाग्रस्त आदमी अकेला पड़ गया। चूंकि जीवन नैतिक रूप से निर्बंध था क्योंकि सामूहिकता तो बहुत पहले जा चुकी थी, इसलिए घर में बंद अकेले मनुष्य को अतिवाद ने खींचा; अंधराष्ट्रवाद, कट्टरता, विभाजन, पहचान आधारित विमर्श ने आकर्षित किया। अब उसका काम केवल उत्पादों से नहीं चलने वाला था, उसे उकसाने वाली कुविचारों की नियमित खुराक भी चाहिए थी ताकि सामूहिकता का आभास बना रह सके।

पूंजी और तकनीक ने अपने तीन-चार दशक के सफर में समाज को इस तरह से बदल डाला है कि अब मनुष्य को बड़ी आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता है
इसका परिणाम यह हुआ है कि लगातार बंटी हुई दुनिया से आ रही विध्वंसक ऊर्जाओं के प्रभाव में आदमी दुनिया को और बांट देना चाह रहा है। वह अपने घर में ही अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान रहा है। पहचान के लिए खुराक उसे टीवी चैनल, वॉट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह से मिल रही है- उन सूचनाओं की मार्फत जिनका कोई पुष्ट स्रोत नहीं है। चूंकि उसका अपना जीवन किसी नैतिक स्रोत और सामूहिकता से कट चुका है, तो उसके दोस्त और दुश्मन की पहचान का पैमाना आयातित है। वह इतना अकेला, उत्तेजित और उद्वेलित है कि किसी क्षण किसी का भी गला काट सकता है।
बीते वर्षों के दौरान बनी ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों में घूमते-फिरते, आजाद, हमलावर और जर्राह कंकालों को विषय बनाया गया है। इन्हें जॉम्बी कहते हैं। ये मरते नहीं हैं, केवल मारते हैं, गोकि ये वास्तव में मरे हुए हैं। पॉपुलर संस्कृति-माध्यमों में जॉम्बी सौ साल से ज्यादा वक्त से मौजूद हैं या कहें, आधुनिकता की जितनी उम्र है उतनी ही उम्र जॉम्बी की भी है। हमारे समाज में जॉम्बी बीते दो-ढाई दशक में पूंजी के पैदा किए अलगाव और अनैतिकता की पैदाइश हैं। महामारी की त्रासदी से निकला मनुष्य अपने आचार, व्यवहार, संवाद और प्रतिक्रियाओं में जॉम्बी जैसा ही दिखता है।
सांस्कृतिक नियंत्रण
पूंजी और उससे आई तकनीक ने अपने तीन-चार दशक के सफर में समाज को इस तरह से बदल डाला है कि अब आदमी को बड़ी आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके माध्यम से हमारे मत, निर्णय और विचार प्रक्रिया को किसी खास हित में मोड़ दिया जा सकता है और इच्छित परिणाम निकाले जा सकते हैं।
टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और महामारी से चली सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया का अगला चरण जनरल इंटेलिजेंस है। वह ऐसा बिंदु होगा जब प्रौद्योगिकीय विकास अनियंत्रित हो जाएगा। यह एक ऐसी अवस्था होगी जब मनुष्य के दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित करने की तकनीक कामयाब हो जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी मेधा से भी तीक्ष्ण हो जाएगा। संस्कृति पर इसका प्रभाव यह होगा कि सारा ज्ञान सतही जानकारियों और सूचनाओं तक सीमित हो जाएगा। सर्वव्यापी सत्ता को नापसंद तमाम विचार हाशिये पर जाकर अप्रासंगिक हो जाएंगे। फिर सत्ता का विचार ही समकालीन समाज का स्वीकृत विचार बन जाएगा।
भारत जैसा देश, जो अब भी सांस्कृतिक रूप से एकाश्म नहीं है, यहां सांस्कृतिक नियंत्रण सबसे बड़ा और सबसे महीन खतरा है। इस संदर्भ में ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा इकलौता दल है जिसके नारे राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक होते हैं। इन सांस्कृतिक नारों में भरकर प्रच्छन्न व संक्षिप्त संदेश फैलाए जाते हैं। हारा हुआ पक्ष हमेशा मानता है कि जीते हुए के पास एक मजबूत नैरेटिव था। यह कभी नहीं पूछा जाता कि विजेता के नैरेटिव के घटक क्या-क्या थे; आखिर उन घटकों को आपस में मिलाकर उसने एक ठोस नैरेटिव कैसे गढ़ा; सारे वाद्य मिलकर एक ऑर्केस्ट्रा में कैसे तब्दील हो गए? दुर्भाग्य से, भारत की किसी भी विपक्षी राजनीतिक पार्टी के पास अपना सांस्कृतिक एजेंडा नहीं है। रणनीति तो दूर की बात रही। कुछ हद तक अस्मिताओं को ये दल समझते हैं, लेकिन सारा मामला सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण तक जाकर सिमट जाता है। भाजपा के सांस्कृतिक नारे और संदेशों पर बाकी दलों ने अब तक केवल प्रतिक्रिया दी है। अपना सांस्कृतिक विमर्श नहीं गढ़ा या सामने रखा। लिहाजा, वे जनता में जो संदेश पहुंचाते हैं उसका कोई सांस्कृतिक तर्क नहीं होता। कोई मुलम्मा नहीं होता। वे भाजपा की तरह प्रच्छन्न मैसेजिंग नहीं कर पाते।
समाज, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का आह्वान करने वालों के पास जब सांस्कृतिक संदेश ही नहीं हैं, तो कोई भी माध्यम क्या कर लेगा? यही वह संकट है जहां मनुष्य के दिल-दिमाग पर नियंत्रण की तकनीक-प्रौद्योगिकी संघ के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ एकमेक हो कर कारगर बन जाती है।
भविष्य का सवाल
जनरल इंटेलिजेंस की कगार पर खड़े भारत जैसे एक सामंती मानसिकता वाले समाज के लिए दो बातें आज की तारीख में उम्मीद बंधा सकती हैं। पहली, कि तकनीक किसी की बपौती नहीं है, सारा मामला नैरेटिव का है। इसी से जुड़ी दूसरी बात यह है कि आदमी के दिमाग को नियंत्रित करने की राह में उसका दिमाग ही सबसे रोड़ा है। इसलिए बहुलतावादी संस्कृति में भरोसा रखने वाली ताकतें यदि बचे-खुचे दिमाग का प्रयोग कर के अपने सांस्कृतिक संदेश हिंदुस्तान की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हिसाब से गढ़ सकें, तो तकनीक की तानाशाही धरी की धरी रह जाएगी।
देश की सत्ता, आर्थिकी, राजनीति, संस्थाओं पर कब्जा ठोस रूप में हमें दिखाई देता है, लेकिन संस्कृति पर नियंत्रण को देख पाना कठिन है। लंबे दौर में बनी संस्कृतियां इतनी जल्दी बेशक खत्म नहीं होती हैं, लेकिन एक बार हो चुके बदलाव को पलट पाना असंभव होता है। आप सरकार बदल सकते हैं, अर्थव्यवस्था बदल सकते हैं लेकिन समाज के बदल चुके मानस को लौटा नहीं सकते। इसलिए, बीते दशकों में हुए सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव हमें आगे के लिए आगाह करते हैं।
2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही कुछ विद्वान चुनावी राजनीति के ऊपर सामाजिक संस्कृति और संस्कृति की राजनीति के सवाल को तरजीह देने की बात कर रहे हैं। 2025 में प्रवेश करते समय यह मसला और गंभीर हो चला है क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति अपने इतिहास के अहम पड़ाव पर पहुंचने को है। अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी क्या सत्ता की राजनीति की जगह संस्कृति की राजनीति की उम्मीद प्रतिरोधी शक्तियों से की जा सकती है?