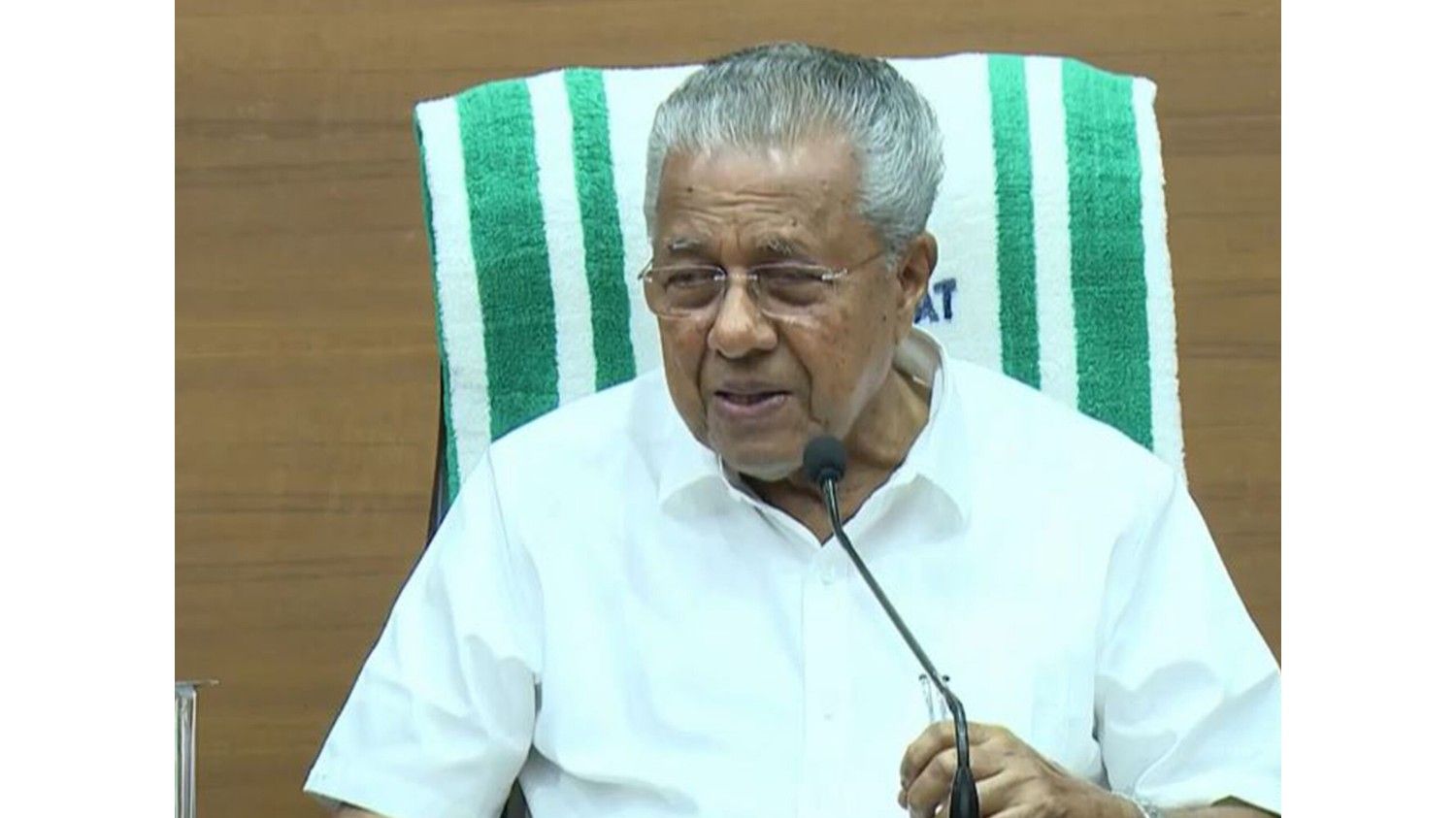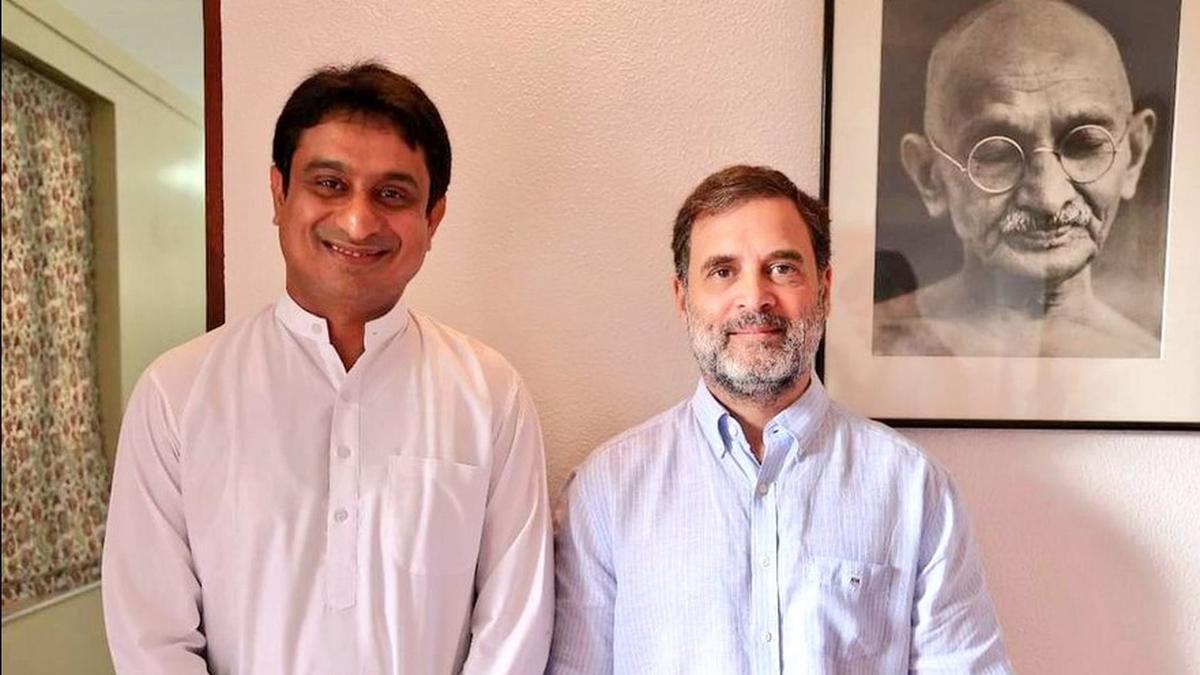बॉलीवुड की पटकथा में आजकल नए ‘खलनायक’ के तौर पर उभर रहा डिमेंशिया बीमारी आंसू बहाता है और फिल्में हिट भी करता है, मगर सच्चाई से है कोसों दूर
बीमारियां हमेशा से सिनेमा वालों को खींचती रही हैं। कभी कलात्मक तरीके से टीबी के कारण खांसते हुए नायिकाओं को मौत आती थी। बाद में, कैंसर सिनेमा की पटकथा में, तुरुप के पत्ते की तरह आया। बालों का झड़ना, कीमोथेरेपी के दृश्य, अंतिम विदाई। फिर इसकी भी ताजगी खत्म हो गई। उसके बाद फिल्म निर्माताओं ने एक और भयंकर बीमारी ढूंढ निकाली, डिमेंशिया और अल्जाइमर। इस बीमारी में सिनेमा की हर जरूरत मौजूद है। याद, पहचान, प्यार और दिल टूटना।

सब कुछ रूमानी नहींः थ्री ऑफ अस में अहलावत के साथ शैफाली
अल्जाइमर को बॉलीवुड अक्सर केवल कहानी कहने की सुविधा तक सीमित कर देता है। हालांकि यह बीमारी जोरदार क्लाइमेक्स दे सकती है, लेकिन यह डिमेंशिया की जीती-जागती हकीकत के साथ न्याय नहीं कर पाती। हाल ही में आई मोहित सूरी के निर्देशन वाली फिल्म सैयारा (2025) अल्जाइमर पर आधारित दुखद प्रेमकथा है। नायिका मुश्किल से बीस साल की है, जिसे अल्जाइमर हो जाता है। चिकित्सकीय दृष्टि से देखें, तो यदि अल्जाइमर की शुरुआत जल्दी हो जाए, तो 65 साल से कम उम्र के रोगियों में उसका इलाज हो जाता है। जल्दी शुरुआत का मतलब भी 40 से 50 साल के बीच है। बीस तो बिलकुल नहीं।
सैयारा पहली फिल्म नहीं है। 2008 में आई यू मी और हम में काजोल ने भी एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था, जिसके लिए अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था उसकी शादी के लिए खतरा बन जाती है। फिल्मों को अब खलनायक के रूप में रूढ़िवादी माता-पिता, जाति व्यवस्था या पुराने बॉलीवुड मेलोड्रामा के षडयंत्रकारी ससुराल वालों की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बीमारी ही काफी है। शहरी, उदार, आर्थिक रूप से संपन्न मल्टीप्लेक्स के दर्शकों के संघर्ष अब पहले जैसे नहीं रहे। इसलिए अल्जाइमर अब नई बाधा के रूप में उभर रहा है।
इन फिल्मों में मरीज के वास्तविक जीवन को बमुश्किल दिखाया जाता है। इसकी बजाय दर्शकों को देखभाल करने वाले की पीड़ा ज्यादा दिखाई देती है। दर्शक प्रेमी की साथी ‘खोने’ पर तड़प देखते हैं। कैमरा शायद ही कभी प्रेमिका के उस एहसास पर टिक पाता है, जिसमें भ्रम, अस्पष्टता हो। कहानी मरीज के साथ नहीं, बल्कि उसके इर्द-गिर्द कही जाती है।
इस मायने में ब्लैक (2005) अलग राह पर चलती है। निर्देशक संजय लीला भंसाली ने डिमेंशिया को विकलांगता और अंधकार के ओपेरानुमा दृश्य में बदल दिया था। शिक्षक बने अमिताभ बच्चन के लिए अल्जाइमर दूसरा अंधकार बन जाता है, आत्म-विनाश का रूपक। सौंदर्यवादी भंसाली इस बीमारी को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह देखने में भव्य, मार्मिक और प्रभावशाली दिखता है। लेकिन सटीक नहीं! क्योंकि अल्जाइमर के इलाज की वास्तविकता कुछ अलग ही है। इस बीमारी में भटकन होती है, दूसरे नुकसान पहुंचा देंगें यह भ्रम होता है, संयम खो जाता है, काम करने गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन फिल्मों में यह सब गायब रहता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि सिनेमा में रूपक की कोई जगह नहीं है। लेकिन रूपक जब विस्तार की जगह लेता है, तो नतीजा कुछ अलग होता है। जैसे पीड़ा थोड़ी ग्लैमरस हो जाती है। देखने में यह नाटकीयता आकर्षक होती है, लेकिन बीमारी की रोजमर्रा की चुनौतियों से मीलों दूर होती है।
सुधीश शंकर की तमिल फिल्म मारीसन (2025) में, अल्जाइमर को कहानी आगे बढ़ाने के लिए एकदम सतही बना दिया गया है। इसमें वडिवेलु ने वेलन का किरदार निभाया था। उसे यह बीमारी तब होती है, जब वह पहली बार एक चोर (फहाद फासिल) से मिलता है। लेकिन कहानी में एक ‘मोड़’ आता है और पता चलता है कि वेलन बीमारी के बारे में झूठ बोल रहा था। इस फिल्म में अल्जाइमर हकीकत के रूप में नहीं, सस्ते हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह लोगों को हैरान करने के लिए धोखे की तरह है। इससे भी बुरी बात यह है कि वेलन धोखेबाज और हत्यारा निकलता है, जिससे यह खतरनाक धारणा और मजबूत हो जाती है कि मनोभ्रम से जुड़े लोग खतरनाक होते हैं। लेकिन जब तक फिल्म में यह पता चलता है कि वास्तव में वेलन की पत्नी को अल्जाइमर है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। एक गंभीर न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार को केवल कहानी आगे बढ़ाने के टूल तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें संवेदनशीलता या अंतर्दृष्टि नहीं है।

गोल्डफिश में दीप्ति नवल
दुनिया भर की फिल्मों में स्टिल ऐलिस (2014) ने अलग तरह की नायिका दी। जूलियन मूर की भाषा विज्ञान की प्रोफेसर अपनी ही उलझनों को बयान करती है। फिल्म में नायिका की उलझन, उसके डर और उसे नियंत्रित करने की उसकी कोशिश दिखाई पड़ती है। फिल्म का फोकस परिवार का दुख नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिगत अनुभव हैं। नतीजतन यह ऐसी फिल्म है, जो हेरफेर से नहीं, बल्कि आत्मीयता से सहानुभूति पैदा करती है।
अविनाश अरुण की थ्री ऑफ अस (2023) ऐसी ही फिल्म है। यह मेलोड्रामा में नहीं जाती या अल्जाइमर को दुख भरी बाधा के रूप में सरल नहीं बनाती। यह शैलजा (शेफाली शाह) के अनुभव को अव्यवस्थित अनुभव के रूप में प्रस्तुत करती है। वह कभी-कभी संघर्ष करती है, अपनी पुरानी यादें भूल जाती है, अपराधबोध और लालसा महसूस करती है और अपनी क्षीण होती हुई स्मृति का एहसास करती है।
सैयारा या यू मी और हम के उलट, थ्री ऑफ अस डिमेंशिया को किसी ऐसे ‘खलनायक’ में नहीं बदलती, जिसे प्यार से हराया जा सके। उसके बदले, यह बीमारी चिंतनशील यात्रा का हिस्सा बन जाती है, जिसमें नुकसान तो शामिल है ही, साथ ही स्वीकारोक्ति, पुरानी यादें और कोमलता से सहा गया दुख भी शामिल है।
पुशन कृपलानी की गोल्डफिश (2023) डिमेंशिया पर आधारित एक और ईमानदार भारतीय फिल्म है। दीप्ति नवल इस बीमारी से ग्रस्त एक मां और कल्कि कोचलिन उनकी बेटी की भूमिका में हैं। गोल्डफिश को सिर्फ नवल का संवेदनशील चित्रण ही नहीं, बल्कि उसके आसपास का समुदाय भी उल्लेखनीय बनाता है। यह फिल्म डिमेंशिया को किसी एक परिवार तक सीमित निजी त्रासदी के रूप में नहीं, बल्कि सामूहिक वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करती है। लंदन के दक्षिण एशियाई इलाके में रहने वाले अाप्रवासी दया के साथ मदद को आगे आते हैं। यह अव्यवस्थित लगता है, कभी-कभी हास्यास्पद और अक्सर निराशाजनक। लेकिन दूसरे शब्दों में कहें, तो यह वास्तविक लगता है।

स्टिल एलिस
डिमेंशिया और अल्जाइमर के मरीजों का इलाज करने वाले मुंबई के मनोचिकित्सक डॉ. हरीश शेट्टी जोर देते हैं कि डिमेंशिया की देखभाल में समुदाय बेहद अहम है। मरीज तब बेहतर महसूस करते हैं जब उन्हें सहारा देने वाले कई लोग हों, न कि सिर्फ एक बोझिल जीवनसाथी। यू मी और हम या सैयारा जैसी फिल्मों में मरीज को एक ही ‘‘बेहद प्यार करने वाला’’ साथी मिलता है। यह आदर्श स्थिति है लेकिन अलग-थलग करने वाला परिदृश्य है। गोल्डफिश इस ढर्रे को तोड़ती है। यह फिल्म दिखाती है कि बीमारी हमेशा अकेले व्यक्ति को ही नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि देखभाल के नेटवर्क के जरिए भी उसका इलाज किया जा सकता है।
असल जिंदगी में डिमेंशिया शायद ही कभी सिनेमा में दिखाए गए एकांत, रूमानी सफर जैसा होता है। असल में उसके बोझ तले परिवार बिखर जाते हैं। वसीयत और देखभाल की जिम्मेदारियों को लेकर बच्चों के संघर्ष में कड़वाहट आ जाती है। मां या पिता की देखभाल की लगातार मांग के चलते पति-पत्नी के बीच नाराजगी बढ़ जाती है। डॉ. शेट्टी अपने यहां आने वाले मरीजों के जरिये रोज की जिंदगी की इन हकीकतों का सामना करते हैं। सैयारा में मरीज के माता-पिता अपनी बेटी को अजनबी के पास छोड़कर, उसे ऐसे सुनसान घर में ले जाते हैं, जिससे वह अनजान है। यह डॉक्टरों की सलाह के बिल्कुल उलट है। डॉ. शेट्टी जोर देते हैं कि डिमेंशिया की देखभाल, परिचित जगहों और मदद के नेटवर्क से आसान बनती है न कि किसी एकांत में आत्म-त्यागी व्यक्ति की कल्पना पर।
सैयारा में ही, चिकित्सकीय रूप से एक ही बात सही लगती है। पड्डा का किरदार अपने पिछले प्रेमी को अपने वर्तमान साथी से कहीं ज्यादा स्पष्टता से याद करता है। न्यूरोलॉजिस्ट इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह आम बात है, डिमेंशिया में सबसे ताजा यादें सबसे पहले मिटती हैं, जबकि पुरानी यादें अक्सर ज्यादा समय तक बरकरार रहती हैं। फिल्म में यह सटीकता दुर्लभ क्षण है, वरना पूरी फिल्म काल्पनिकता से प्रभावित है।
बॉलीवुड भले ही अभी भी डिमेंशिया से निपटना सीख रहा हो, मगर थिएटर कई बार इससे बेहतर कर पा रहे हैं। भारत में मंचित फ्लोरियन जेलर का नाटक द फादर में नसीरुद्दीन शाह के साथ दर्शक डिमेंशिया के भटकाव को भीतर से महसूस कर पाते हैं। इसके बदले गए सेट, धुंधली हो गई समयरेखा नायक के टूटे मन को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित कर पाए। डॉ. शेट्टी का कहना है कि फिल्म के मुकाबले शाह का अभिनय गहन अध्ययन और बारीकियों पर ध्यान देने वाला था।
इसका एक पक्ष यह भी है कि सिनेमा ने जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। जैसे पुरानी फिल्मों में टीबी या बाद में कैंसर ने दर्शकों को ऐसी बीमारियों से परिचित कराया, जिनके बारे में वे शायद पहले कभी बात नहीं करते थे, वैसे ही पर्दे पर डिमेंशिया सार्वजनिक चर्चा का विषय बना है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन जागरूकता बढ़ाना और समझ बढ़ाने में अंतर है।

मारीसन फिल्म का दृश्य
इसका खतरा बस इतना है कि अल्जाइमर, त्रासदी का संक्षिप्त रूप बन जाता है और उसकी जटिलताएं समाप्त हो जाती हैं। इस स्थिति को केवल गिरावट की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इस बात पर कम ध्यान दिया जाता है कि मरीज कितने साल अपनी गरिमा, हास्य और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। फिल्मों में यह दिखाई ही नहीं पड़ता कि परिवारों कैसे खुद को ढालते हैं, समुदायों कैसे मदद के लिए आगे आता है, कैसे देखभाल का ढांचा विकसित होता है। फिल्मों में बस रोते हुए विदाई ही दिखाई पड़ती है।
मुख्यधारा का सिनेमा चमक-दमक पसंद है। पीड़ा में भी उसे ग्लैमर चाहिए। लेकिन डिमेंशिया ग्लैमरस नहीं है। यह अव्यवस्थित, अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण है। अगर फिल्म निर्माता सचमुच ऐसी कहानियां सुनाना चाहते हैं, तो उन्हें नाटकीयता से आगे बढ़कर न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, देखभाल करने वालों से सलाह लेनी होगी, जो जानते हैं कि बीमारी क्या है। उन्हें मरीजों को उनकी व्यक्तिपरकता वापस देनी होगी, बजाय इसके कि उन्हें देखभाल करने वालों के दर्द के इर्द-गिर्द घूमने वाले उपग्रह बना दें।
अल्जाइमर सिर्फ जाति-विरोध या माता-पिता की अस्वीकृति जैसे पुराने ढर्रे के बदलने कुछ नया विरोध दिखाने का तरीका नहीं है। यह ऐसी बीमारी है, जो लाखों परिवारों को प्रभावित करती है।
अगर फिल्म निर्माता कहानी की बैसाखियों के बजाय सहानुभूति चुनें, तो वे न सिर्फ यह समझा पाएंगे कि भूलना क्या होता है, बल्कि यह भी बता पाएंगे कि परवाह करने का क्या मतलब होता है। आखिरकार, जैसा कि एलिजाबेथ बिशप हमें याद दिलाती हैं, हारने की कला में महारत हासिल करना मुश्किल नहीं है।
(पटकथा लेखिका और विज्ञापन फिल्म निर्माता रह चुकी हैं। मुंबई में रहती हैं।)