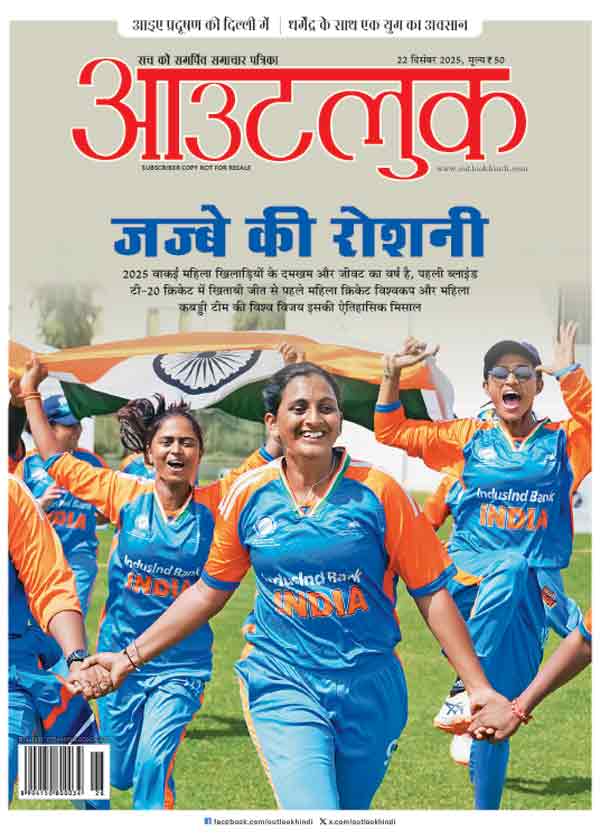भारत को अमेरिका के साथ हो रहे नुकसान को कम करते हुए चीन से सौदेबाजी की राह अपनानी चाहिए
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया भर के देशों पर बीते 2 अप्रैल को टैरिफ लगाने के अपने कदम को अमेरिका के लिए ‘मुक्ति दिवस’ करार दिया। इन शुल्कों के असर का विश्लेषण दुनिया भर में किया जा रहा है। इन शुल्कों का पैमाना और इनकी प्रकृति बेहद विघटनकारी है, लेकिन इनसे जैसी अनिश्चितता पैदा हुई है वह तर्कसंगत आर्थिक और कारोबारी निर्णय लेने को लगभग असंभव बना रही है।
ट्रम्प का कहना है कि टैरिफ राजस्व बढ़ाने वाला साधन है जो महत्वपूर्ण कर कटौती की संभावनाएं पैदा करेगा। सवाल है कि व्यापारिक साझीदारों को अमेरिकी निर्यात पर टैरिफ कम करने और अधिक बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए मजबूर करने के घोषित उद्देश्य के साथ इस कदम को कैसे जोड़ा जा सकता है? यदि व्यापारिक साझीदारों के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप टैरिफ कम भी हो जाते हैं, तो उस राजस्व का क्या होगा, जिसके बढ़ने की बात की गई है? उच्च टैरिफ की आड़ में अमेरिका का फिर से औद्योगिकीकरण करने के तीसरे उद्देश्य के लिए टैरिफ को कई वर्षों तक अनुमानित स्तर पर रखने की आवश्यकता होगी ताकि निवेशकों को अमेरिका में उद्योग स्थापित करने के लिए राजी किया जा सके।
यदि टैरिफ को अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऊपर या नीचे किया जा सकता है, तो किसी भी निवेशक को लंबी अवधि के लिए अमेरिका में निवेश करने का जोखिम क्यों लेना चाहिए? इस प्रकार के विरोधाभासों और नीतिगत असंगति के परिणामस्वरूप अनिश्चितता पैदा हो रही है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती आएगी, शायद मंदी भी। यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से भू-राजनैतिक समीकरणों में फेरबदल करेगी। सत्ता समीकरण बदल जाएंगे। कुछ देश हारेंगे, कुछ जीतेंगे।
यह शुल्कों का खेल वैचारिक और राजनैतिक परिवर्तनों के उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में हो रहा है जिसका ट्रम्प ने पहले ही आगाज कर दिया है। इनमें कार्यपालिका पर संवैधानिक बंदिशों की थोक भाव में अस्वीकृति, शासन की तेजी से आकार लेती मनमर्जी और यहां तक कि सनकी शैली और संघीय सरकार की संस्थागत प्रणाली का व्यवस्थित और सचेत तरीकों से खोखला होते जाना शामिल है। यह घटनाक्रम अनिवार्य रूप से अमेरिका की विश्वसनीयता और नई-पुरानी वचनबद्धताओं के पालन में उसके प्रति विश्वास को प्रभावित करेंगे। यहां तक कि अगर उसके व्यापारिक भागीदार अपने ऊपर लगाए गए टैरिफ में छूट प्राप्त करने के लिए उसे रियायतें देते हैं, तब भी वे कभी आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह समझौता कायम रहेगा।
आखिरकार, ट्रम्प द्वारा अपने पहले कार्यकाल में किया अमेरिका-कनाडा और अमेरिका-मैक्सिको मुक्त व्यापार समझौता अब कागज का एक पुलिंदा भर रह गया है। अपने बाहरी संबंधों में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चोट विश्वसनीयता का नुकसान है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य महाशक्ति है, लेकिन यह अब वह अनिवार्य शक्ति नहीं है जो कभी थी। बाकी दुनिया ऐसे एक अविश्वसनीय अमेरिका से खुद को दूर करके आसानी से अब आगे बढ़ सकती है।
वर्तमान अराजकता से उभरने वाले प्रमुख भू-राजनैतिक परिवर्तन क्या हैं?
एक, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार अब ‘पश्चिम’ नाम की कोई इकाई नहीं रह गई है। ट्रम्प ने वैचारिक आत्मीयता, ‘साझा मूल्यों’ और यहां तक कि साझा सुरक्षा परिप्रेक्ष्य को नष्ट कर दिया है जिसने एक शक्तिशाली और प्रभावशाली ट्रांस-अटलांटिक क्षेत्र का गठन किया था। अमेरिका पिछले दो दशकों से अपना रणनीतिक ध्यान अटलांटिक पार से हटाकर हिंद-प्रशांत पर केंद्रित किए हुए है क्योंकि उभरते हुए चीन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा ज्यादा प्रमुख और जरूरी हो गई है। यह बदलाव जारी है इसलिए यूरोप को अब अपना बचाव खुद करना चाहिए। यूरोप इस अस्तित्वगत चुनौती का जवाब कैसे देता है, इसका उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था के आकार पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
दूसरा, ट्रम्प ने चीन की हथेली पर रणनीतिक विजय को सजाकर रख दिया है। याद किया जाना चाहिए कि मार्च 2023 में मास्को की यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टीवी पर अपने मेजबान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था, ‘‘अभी कुछ बदलाव होने हैं- जैसे हमने 100 वर्षों में भी नहीं देखे- और इन परिवर्तनों को लाने वाले हम हैं।’’ पुतिन ने जवाब दिया था, ‘‘मैं सहमत हूं।’’
उदारवाद अपने आप में किसी देश के नागरिकों के बीच समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को प्रेरित करने के बजाय राजनैतिक दुरुपयोग का शब्द बन गया है। पीछे मुड़कर देखें, तो जिनपिंग और पुतिन के बीच हुआ संवाद उल्लेखनीय रूप से पूर्वदर्शी प्रतीत होता है। ट्रम्प ने अमेरिका के प्रभुत्व वाले तत्कालीन भू-राजनैतिक क्षेत्र में एक जगह खाली छोड़ दी है। चीन कम से कम एशिया में एकमात्र शक्ति है जिसके पास इस स्थान पर कब्जा करने का प्रयास करने के लिए समग्र आर्थिक, सैन्य और तकनीकी क्षमताएं हैं। उदाहरण के लिए, यूएसएड को नष्ट करने और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को समर्थन कम करने से चीन को अब दक्षिण के देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। यदि उसने कोई कूटनीतिक चूक नहीं की तो नई भू-राजनैतिक परिस्थिति का चीन सबसे बड़ा लाभार्थी रहेगा। ट्रम्प द्वारा उस पर लगाए गए ताजा टैरिफ का त्वरित प्रतिशोध इशारा करता है कि चीन आश्वस्त है। यह इस वास्तविकता को दर्शाता है कि भले ही अमेरिका अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वैश्विक व्यापार में उसकी हिस्सेदारी अब 12.5 प्रतिशत है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक राष्ट्र है। चीन वैश्विक व्यापार के 15.2 प्रतिशत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन चुका है। लिहाजा ट्रम्प के पहले कार्यकाल की तुलना में अमेरिका के साथ सौदेबाजी की ताकत चीन के पास अधिक होगी।
‘द वेस्टलैंड: ए वर्ल्ड इन परमानेंट क्राइसिस’ के लेखक रिचर्ड कपलान जैसे विश्लेषकों द्वारा एक विचार रखा गया है कि सभी तीन प्रमुख शक्तियां-अमेरिका, रूस और चीन-गिरावट की ओर हैं। चीन के बारे में उनका तर्क है कि चीन अब जनसंख्या के लिहाज से गिरावट के दौर में प्रवेश कर चुका है, कि मध्यम वर्ग के निर्माण में उसकी सफलता ने अत्यधिक दमनकारी और सर्वसत्तावादी सरकार को बनाए रखना मुश्किल कर दिया है और वह जल्द ही लगभग 2-3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर तक पहुंच जाएगा।
भले ही यह प्रशंसनीय हो, तीन प्रमुख शक्तियों की सापेक्ष स्थिति वर्तमान में चीन के पक्ष में ही है। चीनी नेतृत्व भविष्य के लिए अपने आर्थिक दृष्टिकोण में इन मंद कारकों को पहचानता है, लेकिन अपनी वृद्धि में प्रौद्योगिकीय विकास के सबसे महत्वपूर्ण चालक होने के नाते चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित उन्नत तकनीक में भारी और स्थायी रूप से निवेश कर रहा है। अन्य उन्नत राष्ट्र जहां जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को छोड़ रहे हैं, चीन स्वच्छ-तकनीकी में निवेश के साथ आगे बढ़ रहा है।
तीसरा, हम उदार लोकतांत्रिक राज्य के क्षरण और दुर्बलता को देख रहे हैं, जिसे निकट भविष्य में पुर्नजीवित करना मुश्किल हो सकता है। सोवियत संघ के पतन के बाद 1992 में फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा घोषित इतिहास के अंत और अंतिम आदमी वाली घोषणाओं से हालांकि अभी हम बहुत दूर हैं।
फुकुयामा ने तर्क दिया था कि उदार लोकतंत्र और पूंजीवादी बाजार वाला अर्थशास्त्र अंततः बेजोड़ राजनैतिक और वैचारिक प्रणालियों के रूप में उभरेगा, जिसका भविष्य में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। बावजूद इसके सहस्राब्दी के मोड़ पर इतिहास एक धमाके के साथ वापस आया। 11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित ट्विन टावर्स पर अल-कायदा के हमले के बाद शुरू हुए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध ने अमेरिका और अन्य लोकतांत्रिक देशों में सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगा दिया।
इसके बाद अन्य झटके भी लगे- 2008-09 का वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट, 2015-16 में आर्थिक मंदी और 2020-23 की कोविड महामारी, जिसने दुनिया भर में कम आय, उच्च बेरोजगारी, सशक्त राज्य और व्यक्तिगत ऋणग्रस्तता को पैदा किया। लोगों के जीवन में राज्य की भूमिका की काफी वृद्धि हुई, जबकि आर्थिक संभावनाओं में गिरावट ने शासी अभिजात वर्ग के प्रति व्यापक आक्रोश और क्रोध को जन्म दिया। उसी समय, तकनीकी प्रगति ने वैश्वीकरण को मजबूत किया, लेकिन उसके लाभ ज्यादातर महानगरीय अभिजात वर्ग को ही मिले जिनका अपने ही देशों में पीछे छूट चुकी आबादी के साथ रिश्ता टूट चुका था।

दोस्तीः 2024 में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग रूस यात्रा के दौरान पुतिन के साथ (दाएं)
वैश्वीकरण अपने आप में एक सकारात्मक प्रवृत्ति है क्योंकि यह अधिक धन पैदा करती है, लेकिन असमान वितरण, बढ़ती आय और धन की असमानता ने उसे बदनाम कर दिया है। उसी के चलते एक के बाद एक देशों में लोकलुभावनवाद और संकीर्ण राष्ट्रवाद का उदय होता गया। यह वैश्वीकरण का अपरिहार्य परिणाम नहीं है, बल्कि सार्वजनिक नीति की विफलता है। कई देशों में राजनीतिक नेतृत्व को या तो धनी वर्ग ने अपने पाले में खींच लिया है या वैश्वीकरण की लहर से पीछे छूट गए लोगों को आवाज देने में उदारवादी वामपंथ विफल रहा है। इस चक्कर में उदारवाद अपने आप में किसी देश के नागरिकों के बीच समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को प्रेरित करने के बजाय राजनीतिक दुरुपयोग का शब्द बन गया है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में अमेरिका ने उदार लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य किया, भले ही उसका अपना आचरण प्राय: विपरीत आवेगों से प्रेरित था। अब हम अमेरिका में ही इसकी विकृति देख रहे हैं और दुनिया भर में इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्तर पर दक्षिणपंथ के प्रति और भी अधिक झुकाव दिखने की संभावना है। बदलते हुए भू-राजनैतिक परिदृश्य में निहित जोखिमों से निपटने के लिए भारत अच्छी तरह से तैयार है और बढ़ी हुई रणनीतिक स्वायत्तता के साथ खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है।
चौथा, ठीक ऐसे समय में जब मानवता के सामने आने वाली अधिकांश चुनौतियां देशों की सरहदों को पार कर चुकी हैं, अब बहुपक्षवाद अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की भावना और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता के बिना काम नहीं कर सकता। युद्ध का खतरा हाल के इतिहास में किसी भी समय की तुलना में आज अधिक है।
इस भू-राजनैतिक मंथन में भारत को खुद को कहां स्थापित करना चाहिए? वह चीन के साथ एक सौदा कर सकता है जो इस क्षेत्र में चीन की श्रेष्ठता को स्वीकार करे। भारत को अपना सिर नीचे रखना चाहिए और ट्रम्प के अमेरिका के तहत उसके हितों को होने वाले अपरिहार्य नुकसान को कम करने के लिए काम करना चाहिए। रक्षा और उच्च तकनीक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के अवसर हो सकते हैं जो भारत के लिए फायदेमंद हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 27 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से बचना समझदारी थी।
इन सामरिक चालों के समानांतर, भारत को अपने बाहरी आर्थिक संबंधों में विविधता लाने की आवश्यकता है। हमें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी से बाहर रहने के पहले वाले निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और निर्भीक होकर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप सीपीटीपीपीपी में सदस्यता के लिये आवेदन करना चाहिए। एशिया प्रशांत आर्थिक सम्मेलन (एपेक) में शामिल होने के लिए भारत के आवेदन को पुनर्जीवित करना भी सार्थक हो सकता है। आर्थिक विविधीकरण यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ चल रहे मुक्त व्यापार समझौतों के शीघ्र समापन की मांग करता है। और अंत में, भारत को अपने दक्षिण एशियाई पड़ोस में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यह चीन के हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों के प्रति देश को कम संवेदनशील बनाएगा।
(श्याम सरन पूर्व विदेश सचिव हैं, लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)