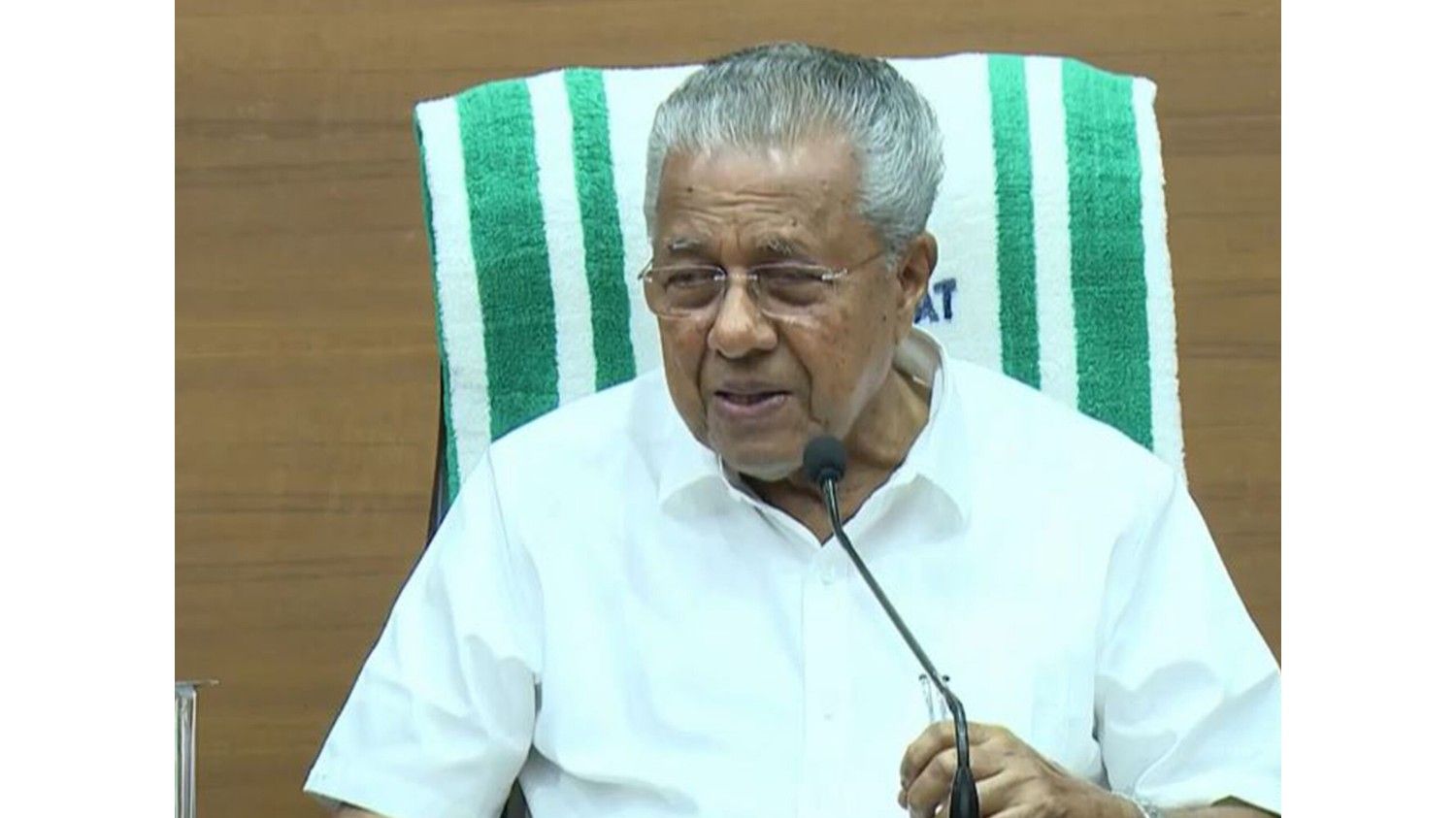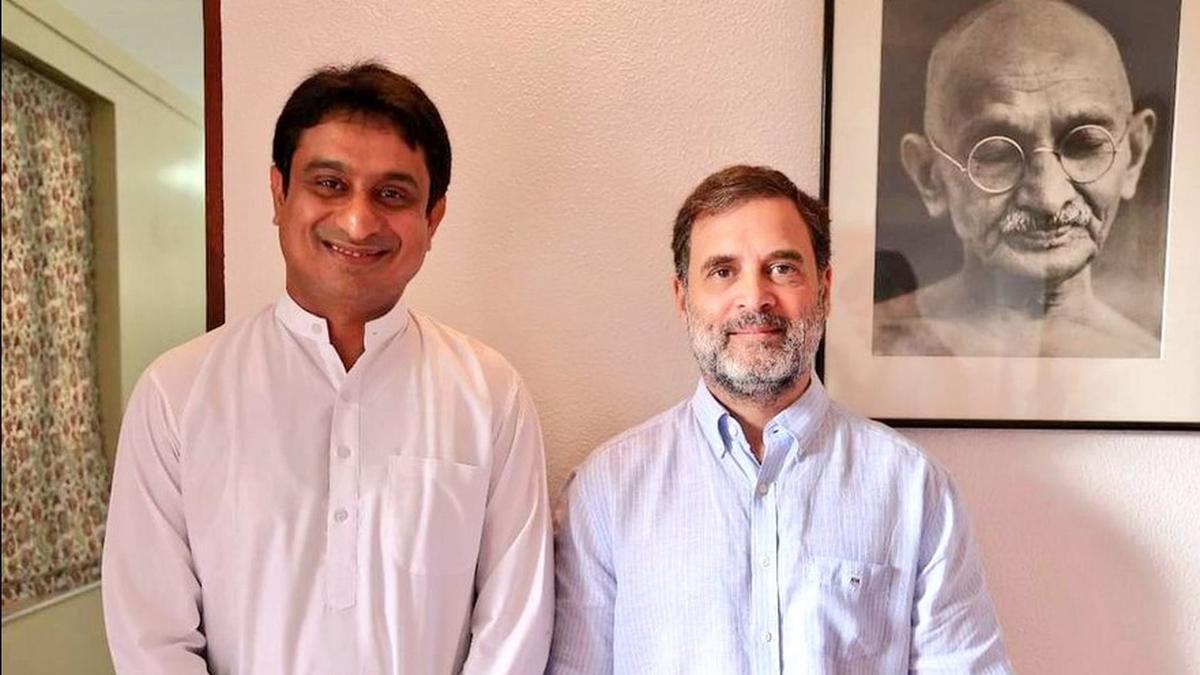आम धारणा के विपरीत बंधुआ मजदूरी अभी भी प्रचलित है। यह बेगारी, बाल श्रम, ऋण बंधन, मानव तस्करी जैसे रूपों में मौजूद है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स (जीएसआई) 2013 के मुताबिक, दुनिया भर में 29 लाख से अधिक लोग गुलामी की जकड़न में हैं। जीएसआई सूचकांक का आकलन है कि भारत में तकरीबन 1.33 करोड़ से 1.47 करोड़ के बीच बंधुआ मजदूर हैं। हालांकि, भारत के पास इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लेबर फाइल में जे. जॉन के अनुमान के मुताबिक, भारत के 472,900,000 श्रमिकों में से 5 प्रतिशत से अधिक ईंट भट्टों में काम करते हैं (एनएसएसओ 2011-12)। अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 50,000 से 1,00,000 ईंट भट्टे कार्यरत हैं (लेबर फाइल, 2014) और यह क्षेत्र अपने संचालन के तौर-तरीकों से बंधुआ मजदूरी और ऋण मजदूरी को बढ़ावा देता है।
भट्टों में काम करने वाले श्रमिकों को मासिक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है बल्कि उन्हे प्रति ईंट उत्पादन पर भुगतान मिलता है। पीस-रेट मजदूरी (पीआरडब्ल्यू) विधि श्रम लागत के मूल्य के अनुरूप नहीं है और यह बमुश्किल ही गुजारे के लिए पर्याप्त है। कम मजदूरी और गरीबी के कारण अधिकांश श्रमिक काम के शुरुआत में नियोक्ताओं/मालिकों से स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, दैनिक जरूरतों के तहत या विशिष्ट घटनाओं (जैसे शादी और अंतिम संस्कार) के लिए ऋण लेकर बंधुआ मजदूरी के जाल में फंस जाते हैं। एक बार जब कर्ज ले लिया जाता है तो मजदूर काम के लिए अपनी शर्तों पर से नियंत्रण खो देते हैं और आम तौर पर उन्हें सीजन के खत्म होने तक कोई अंदाजा ही नहीं रहता कि वो कितना प्राप्त करने के हकदार हैं या क्या वह अब भी कर्जदार हैं और अपने कर्ज का भुगतान कर रहे हैं। दिए गए ऋण पर भारी ब्याज भी लिया जाता है जो ऋण के दरों को बढ़ा देता है। अग्रिम अनुबंध, मजदूरों के आवाजाही को प्रतिबंधित कर भट्ठे में ही काम जारी रखने के लिए मजबूर करते हुए भट्टा मालिकों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं।
पीआरडब्ल्यू के तहत श्रम प्रबंधन की इस प्रकार से संरचना की गई है कि सतत रहने के बावजूद उत्पादन मौसमी है और अग्रिम और मजदूरी के स्थगन की संरचना मजदूरों की आर्थिक गतिशीलता को क्षीण करती है। कई अन्य कारणों की वजह से भी पीआरडब्ल्यू अपनी प्रकृति में शोषक और भेदभावपूर्ण है। खराब मौसम की स्थिति के कारण काम रुकने और ईंटों का उत्पादन नहीं होने पर कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। बीमारी या छुट्टी के दौरान किसी तरह की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। ईंटों की ढलाई से पहले की मजदूरी जैसे मिट्टी ढोना, मिलाना, सानना आदि पीआरडब्ल्यू विधि में नहीं गिना जाता है।
ईंट भट्टों में काम के घंटे बेहद कठिन और लंबे होते हैं क्योंकि यह प्रति दिन अधिकतम ईंटों का उत्पादन करने के लिए ईंट भट्ठा मालिकों के हित में है। प्रतिदिन 8 घंटा और सप्ताह में 48 घंटे के नियम का पालन नहीं किया जाता है। ईंट भट्ठा क्षेत्र मौसमी श्रम पर आधारित है, इसलिए गैर उत्पादन महीनों के दौरान किसी तरह की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है। महिलाओं को श्रमिकों के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और उन्हे अलग से मजदूरी नहीं दी जाती है। ईंट भट्टों के मालिक आम तौर पर पति, पत्नी और दो बच्चों सहित पारिवारिक मजदूरी करवाते हैं और चार या उससे अधिक के समूह के सामूहिक उत्पादन पर परिवार के मुखिया, आम तौर पर पुरुष को भुगतान करते हैं। यह क्षेत्र बाल श्रम से पीड़ित है, अधिक ईंटों का उत्पादन करने के लिए मजदूर माता-पिता बच्चों की सहायता लेने को आवश्यक समझते हैं।
ऋण बंधन या बंधुआ मजदूरी की पहचान गुलामी की एक संस्था या ऐसे ही काम के रूप में की गई है (लेबर फाइल 2014)। फोर्स्ड लेबर कंवेन्शन 1930, यूएन स्लेवरी कंवेन्शन 1926 और यूएन सप्लीमेंटरी कंवेन्शन 1926 के जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपकरण (आईएलओ) जबरिया मजदूरी या बंधुआ मजदूरी को गुलामी एक रूप मानते हैं।
श्रमिकों को ऋण बंधन से मुक्त करने के लिए 1976 में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) (बीएलएसए) अधिनियम भारत में प्रख्यापित की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 26 से बीएलएसए अधिनियम में बहुत कुछ लिया गया था। हालांकि, इस अधिनियम का कार्यान्वयन अप्रभावी साबित हुआ और बीएलएसए अधिनियम में दंड के प्रावधान लगभग नहीं के बराबर थे। भट्ठा नियोक्ताओं/ मालिकों पर शायद ही कभी मुकदमा चलाया जाता है, अगर मुकदमा चलता भी है तो आरोप 1976 के अधिनियम के तहत नहीं होता बल्कि दुर्व्यवहार या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने का आरोप होता है। ज्यादातर मालिक आर्थिक दंड का भुगतान कर बच जाते हैं और इसमें कारावास की सजा अत्यंत दुर्लभ है।
ईंट भट्टे मिनीमम वेजेस एक्ट 1948 में अनुसूचित हैं और विभिन्न राज्य सरकारें ईंट-भट्ठा मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रकाशित करती हैं। हालांकि, पंजाब में सेंटर फोर एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन की ओर से किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि सरकार द्वारा घोषित पीस रेट वेज रेट (पीआरडब्ल्यू), मजदूरों को वास्तव में मिलने वाली मजदूरी के साथ मेल नहीं खाता। यह सर्वेक्षण पीस रेट वेज रेट (पीडब्ल्यूआर) और घोषित मिनीमम वेज रेट (एमडब्ल्यूआर) के बीच के स्पष्ट अंतर को भी उजागर करता है, जहां काम की सभी श्रेणियों, अकुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल और उच्च कुशल श्रेण में पीडब्ल्यूआर और एमडब्ल्यूआर के बीच आय भिन्नता पर्याप्त है।
ईंट भट्टों का संचालन न सिर्फ 1976 के बीएलएसए अधिनियम और 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उल्लंघन करता है बल्कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 और अन्य दूकरे कानूनों के साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 का भी उल्लंघन करता है। इनके संचालन में उल्लेखनीय तौर पर बंधुआ मजदूरी पर आईएलओ कन्वेंशन संख्या 29 और 105, जिसे भारत ने अनुमोदित किया था और यूनिवर्सल डिक्लेअरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (यूडीएचआर) 1948 के जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी पालन नहीं किया जाता है। यूडीएचआर का अनुच्छेद 7 कहता है कि किसी को भी गुलामी या दासता में नहीं रखा जाएगा, दासता और दास व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा। यूडीएचआर का अनुच्छेद 23 काम की अनुकूल परिस्थितियों, गैर भेदभाव, समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार और अनुकूल पारिश्रमिक पर जोर देता है। भारत आईसीईएससीआर में एक पक्ष भी है जिसका अनुच्छेद 7 काम के लिए अनुकूल स्थितियों, उचित मजदूरी, काम की स्वस्थ और सुरक्षित स्थितियों को मान्यता देता है।
यह देखने की बात है कि भट्टों से बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए पीस-रेट वेज की अपमानजनक प्रकृति को देखते हुए इसकी जगह पर मासिक वेतन पद्धति लागू कर सरकार इसे खत्म करती है या नहीं।
(उर्मिला राव सेंटर फोर एजुकेशन एंड कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली में रिसर्च एंड कम्यूनिकेशन मैनेजर हैं)