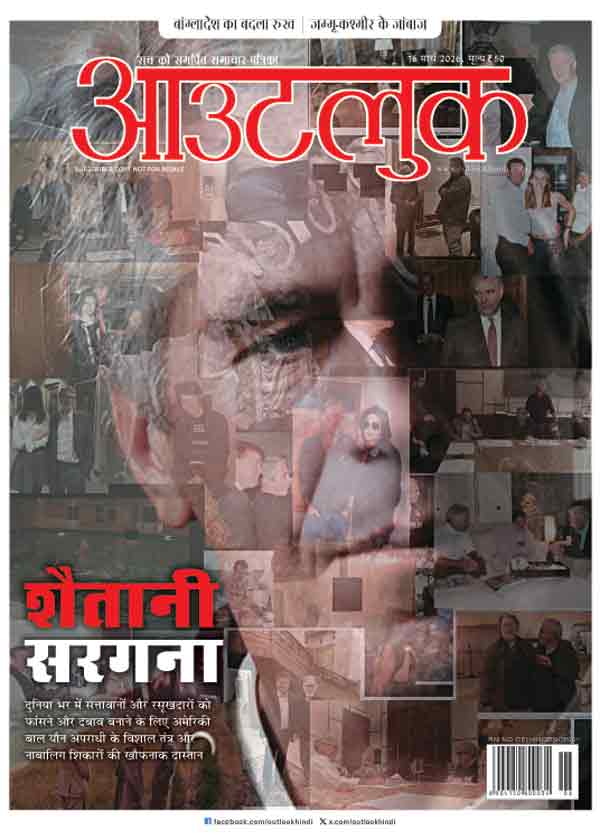आमतौर पर जब भी लोग बाढ़ से हुए नुकसान की गुणा-गणित करते हैं, तो इसमें केवल बड़े नुकसान ही जोड़े जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई छोटे नुकसान हैं, जिन्हें अखबारों के पन्नों में प्रमुखता से जगह नहीं मिलती। मिलती भी है तो अखबारों के कोने में दबकर रह जाती हैं। कितने लोग जानते हैं कि इस अगस्त, दिल्ली के हरी नगर में भारी बारिश के बाद एक दीवार गिर गई, जिसमें आठ लोग मारे गए, जिनमें दो बच्चे भी शामिल थे। कुछ ही दिनों बाद, दरियागंज में तीन मजदूर मारे गए जब निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। अत्यधिक बारिश से न केवल पहाड़ टूटते हैं और सड़कों पर पानी भरता है, बल्कि पुराने और कच्चे मकान भी जर्जर हो जाते हैं। अक्सर ये मकान ढह जाते हैं और कई मौतें हो जाती हैं। इन घटनाओं का शायद बारिश से हुई मौत के आंकड़ों में कोई हिसाब नहीं रखा जाता, लेकिन ये मायने रखते हैं।
जलवायु परिवर्तन से मानसून का पैटर्न बदल चुका है। अत्यधिक बारिश का असर हाशिए पर जी रहे लोगों पर सबसे ज्यादा होता है। एक रात में किसान अपनी पूरी फसल खो सकते हैं। दिहाड़ी मजदूर और बटाईदार किसानों की कमाई पलभर में खत्म हो जाती है। जिनके पास बचत, बीमा या कर्ज लेने की सुविधा नहीं होती, उनके लिए बाढ़ कर्ज, भुखमरी या जबरन पलायन में बदल सकती है।
आवास सबसे बड़े खतरे में है। मिट्टी, फूस या अस्थायी सामग्री से बने कच्चे घर आसानी से ढह जाते हैं और उनके साथ किताबें, खाना और जरूरी सामान भी चला जाता है। ओडिशा, असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ इन्हें बार-बार उजाड़ देती है।
बाढ़ के बाद शिक्षा और आश्रय दोनों प्रभावित होते हैं। डूबे हुए स्कूल राहत शिविर बन जाते हैं। पढ़ाई में आई यह रुकावट उन्हें पीढ़ियों तक गरीबी और हाशिए पर धकेल देती है।
पर्यावरण के लिहाज से सबसे संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र सबसे ज्यादा इसकी मार झेल रहा है। भूस्खलन और बादल फटना आम हो चुका है। वहां के अधिकतर जगह जर्जर हो गए हैं। जोशीमठ का हालिया उदहारण सबके सामने है। अब हादसा "कब होगा" का नहीं, बल्कि "कब तक टाला जा सकता है" का सवाल रह गया है। फिर भी, प्रकृति के प्रकोप से बचा नहीं जा सकता, लेकिन नुकसान कम हो, इसका ध्यान रखा जा सकता है।
शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, बाढ़ से बचने का सबसे बुनियादी उपाय नालों की सफाई है। जिन इलाकों में बाढ़ आने की सबसे ज्यादा संभावना है, वहां रहने वाले परिवारों के पास सिक्योरिटी कवर नहीं है। बीमा बहुत कम है और ज्यादातर लोगों के पास जमीन के कानूनी अधिकार नहीं हैं, इसलिए वे हर साल अस्थायी टेंट में फंसे रहते हैं। छत पर पैबंद लगाना, नाला साफ करना या दीवार मजबूत करना—ये छोटे-छोटे कदम कई जिंदगियां बचा सकते हैं और नुकसान रोक सकते हैं।
हर बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित कमजोर तबका होता है। बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, परिवार बेघर होते हैं और समुदाय बार-बार उजड़ते हैं। जब कारोबार ठप हो जाते हैं और सड़कें डूब जाती हैं तो आर्थिक नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। आपदा से पहले तैयारी करना, उसके बाद नुकसान संभालना से कहीं सस्ता, सुरक्षित और मानवीय है।
भारत अब बाढ़ को "हर साल की आम बात" मानकर नहीं चल सकता। सवाल यह है कि क्या जिंदगियां, रोजगार और शहर सुरक्षित होंगे या हम हर बार छोटी-छोटी लापरवाहियों की भारी कीमत चुकाते रहेंगे। बाढ़ का पूर्वानुमान भले कठिन हो, लेकिन यह तय है कि वह आएगी। अगली बारिश से पहले तैयारी, समावेशिता और दूरदृष्टि सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।
लेखक: डॉ. एलिया जाफर
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट