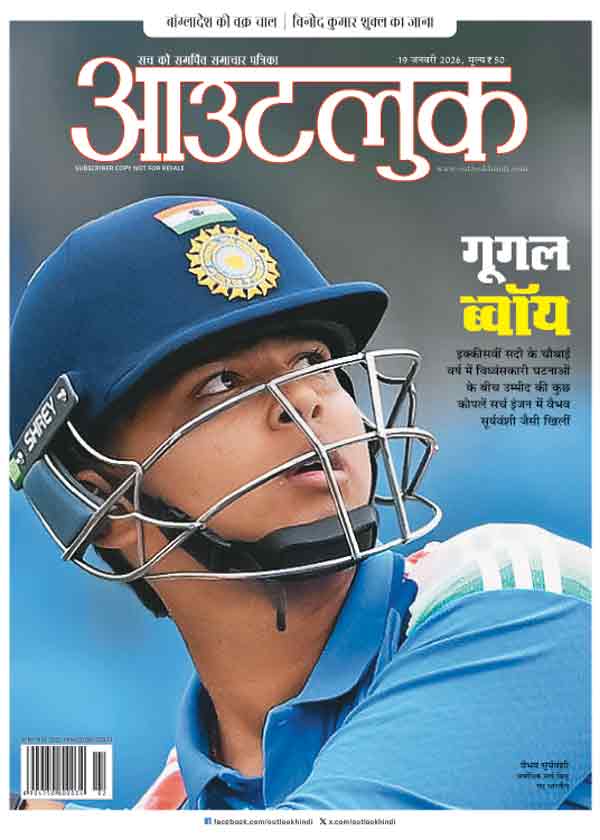1999 में कारगिल की हिमालयी चोटियों पर बहने वाली ठंडी हवाएं सिर्फ सर्दियों की ठंडक से कहीं ज़्यादा कुछ लेकर आईं। वे दक्षिण एशियाई इतिहास के सबसे साहसी सैन्य दांवों में से एक और भारत के उस निर्णायक जवाब का दृश्य थीं, जिसने उपमहाद्वीप में डेटरेंस के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। यह समझने के लिए कि ऑपरेशन विजय कैसे एक रक्षात्मक रुख से ऑपरेशन सिंदूर के सक्रिय डेटरेंस में बदल गया, पहले कारगिल को सिर्फ एक सैन्य लड़ाई से कहीं ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भारत की रणनीतिक कमजोरियों और उस लचीलेपन को दिखाया जिसने इसके भविष्य के सिद्धांत को आकार दिया।
कारगिल संघर्ष मनमानी आक्रामकता से शुरू नहीं हुआ; यह योजनाबद्ध रणनीतिक धोखे से शुरू हुआ। ऑपरेशन बद्र, जिसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1998 के अंत में ही योजनाबद्ध कर लिया था, यह समझने में एक बड़ी गलती थी कि भारत कैसे संयम और संकल्प दोनों का प्रदर्शन कर सकता है। यह योजना अपनी सादगी में आश्चर्यजनक थी: पाकिस्तानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन कश्मीरी आतंकवादी होने का नाटक करते हुए कारगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के साथ खाली सर्दियों की चौकियों पर कब्जा कर लेगी। इससे उन्हें श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली मुख्य सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर नियंत्रण मिल जाता।
इस दांव के समय और निष्पादन ने इसे विशेष रूप से कपटपूर्ण बना दिया। मुशर्रफ ने यह ऑपरेशन तब शुरू किया जब लाहौर शिखर सम्मेलन चल रहा था, जहाँ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को शांति की पेशकश की थी। उन्होंने पाकिस्तान की सेना की संरचना को बदल दिया था ताकि अपने भरोसेमंद लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठा सकें। ऑपरेशन बद्र की रणनीति से पता चला कि पाकिस्तान बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नहीं समझ पाया। मुशर्रफ ने सोचा कि परमाणु समानता पाकिस्तान को एक विश्वसनीय डेटरेंस देगी जो आक्रामकता के दौरान भी प्रभावी होगी। यह विचार, कि परमाणु हथियारों को एक प्रभावी निवारक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत गलत साबित हुआ।
भारत द्वारा आरंभ किया गया ऑपरेशन विजय, जो 26 मई 1999 को प्रारंभ हुआ, इस संघर्ष का निर्णायक उत्तर था। इसकी रणनीति एक संतुलित एवं चरणबद्ध सैन्य प्रतिक्रिया पर आधारित थी, जो सीमित संसाधनों के बावजूद भारत की सैन्य योजना की परिपक्वता को दर्शाता है। अत्यधिक दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में भारत ने दो पूर्ण सैन्य डिवीजनों की तैनाती की, जिनमें से लगभग तीस हजार सैनिक प्रत्यक्ष युद्ध में संलग्न थे। पैदल सेना और तोपखाने के बीच तालमेल, लक्ष्यान्वेषण की संयुक्त योजना और सटीक समन्वय ने एक ऐसा सैन्य लय निर्मित किया जिसका पाकिस्तानी सेनाएँ जवाब नहीं दे सकीं।
परमाणु आयाम ने इस संघर्ष को और अधिक जटिल बना दिया। पाकिस्तान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी—विशेषतः विदेश सचिव शमशाद अहमद द्वारा यह कथन कि पाकिस्तान अपनी ‘सम्पूर्ण सैन्य क्षमताओं’ का उपयोग करेगा, दक्षिण एशिया के इतिहास में प्रथम स्पष्ट परमाणु संकेत था। भारत ने इस खतरे का उत्तर संयम और रणनीतिक स्पष्टता से दिया। भारत अपनी ‘No First Use’ नीति पर अडिग रहा और यह स्पष्ट किया कि परमाणु अस्त्र पारंपरिक युद्ध की प्रतिक्रिया को अवरुद्ध नहीं कर सकते।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, विशेषतः अमेरिका और चीन की, ने भी पाकिस्तान की आक्रामकता को अस्वीकार कर भारत की कूटनीतिक स्थिति को मज़बूत किया। चीन की तटस्थता और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान से बिना शर्त वापसी की माँग इस बात का संकेत थी कि वैश्विक ताकतें इस संघर्ष के प्रति अधिक जिम्मेदार और संतुलित दृष्टिकोण अपना रही थीं।
कारगिल युद्ध भारत के लिए पहला मीडिया-प्रसारित युद्ध भी था। भारत के उदारीकरण के पश्चात उभरते मध्यम वर्ग ने पहली बार युद्ध को सीधे प्रसारण में देखा। यह युद्ध केवल सैन्य पराक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय मानस के पुनर्जागरण का क्षण था। कैप्टन विक्रम बत्रा का प्रसिद्ध उद्घोष—"यह दिल माँगे मोर", न केवल युद्ध विजय का प्रतीक था, बल्कि उस नव-उदित आत्मविश्वास का भी सूचक था जो भारत अपने सामरिक व्यवहार में प्रदर्शित कर रहा था।
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप भारतीय प्रतिरोध नीति में एक doctrinal बदलाव आया, जो 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के रूप में अपने चरम पर पहुँचा। कारगिल से प्राप्त सबक—जैसे चरणबद्ध प्रतिक्रिया की उपयोगिता, अंतरराष्ट्रीय वैधता की आवश्यकता, तकनीकी श्रेष्ठता का महत्त्व, और राजनीतिक-सैन्य समन्वय की अनिवार्यता, ने भविष्य की सैन्य रणनीतियों की नींव रखी। सिंदूर में लक्षित हमलों की सटीकता, न्यूनतम collateral damage, और हताहतों की कम संख्या कारगिल के बाद विकसित हुई टेक्नोलॉजी और सामरिक सोच का प्रमाण थीं। उस समय की आवश्यकताओं ने भारत को सटीक हथियार प्रणालियों और बेहतर निगरानी क्षमताओं के विकास की दिशा में प्रेरित किया।
कारगिल ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया, कि परमाणु अस्त्र पारंपरिक युद्धों में सुरक्षा की गारंटी नहीं बन सकते। दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरणों में इस अनुभव ने भारत को अपने रणनीतिक दृष्टिकोण को अधिक दृढ़ और सक्रिय बनाने की प्रेरणा दी। पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध की नीति के उत्तर में भारत ने जो रणनीतिक परिपक्वता दिखाई, उसका आधार कारगिल में अनुभव की गई चुनौतियाँ थीं।
हर्ष पांडे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में पीएचडी शोधार्थी हैं।