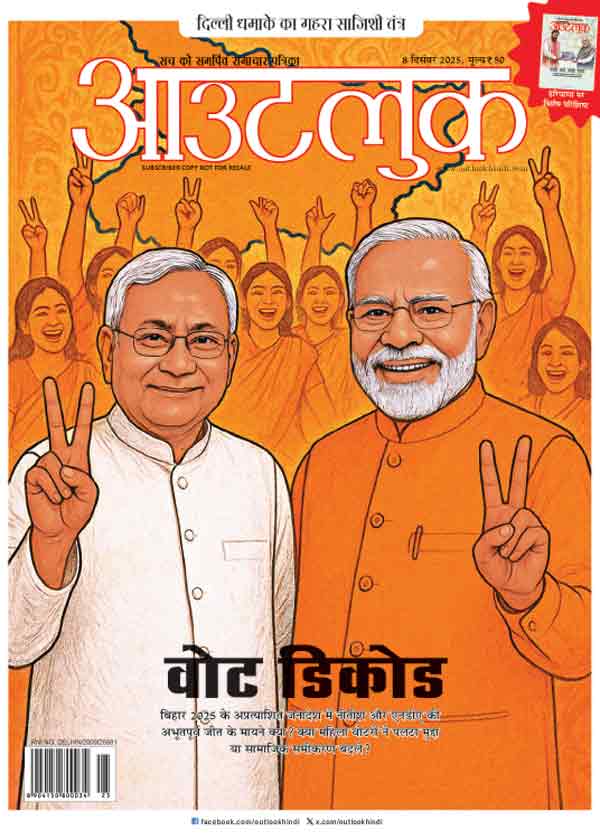कुछ दिनों पहले किसी ने खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, क्योंकि लाने वाला मुसलमान था, और अपने इस फैसले की घोषणा सोशल मीडिया पर भी कर दी। मौका देखकर खाना सप्लाई करने वाली कंपनी ने समावेशी भारतीयता में अपनी अटूट आस्था व्यक्त की, और घटनाक्रम को अपने पीआर का माध्यम बना लिया। दूसरी तरफ, मुसलमान का लाया खाना लेने से इनकार करने वाले ग्राहक के समर्थन में ट्विटर वीर उतर पड़े, कंपनी के बहिष्कार की अपीलें हो गईं। उस ग्राहक को पचास हजार रिट्वीट और समर्थन मिल गए। दावे किए गए कि बहिष्कार अभियान सफल हुआ, कंपनी की बिक्री घट गई।
इस सिलसिले में एक बहुत दिलचस्प और मानीखेज शब्दावली सामने आई- ‘चुनाव की स्वाधीनता’। बहुत-से “सुशिक्षित” लोगों ने तर्क दिया कि यह तो हर आदमी की स्वाधीनता है कि वह किसका लाया खाना खाएगा या नहीं खाएगा। किसी मुसलमान का लाया खाना लेने से इनकार करना उस ग्राहक का व्यक्तिगत अधिकार और चुनाव की स्वाधीनता है।
मतलब यह कि भारत की स्वाधीनता के 72 साल पूरे होने पर, आप ऐसे समाज में हैं जहां चुनाव की स्वाधीनता जैसे पदबंध का उपयोग मानसिक रुग्णता पर परदा डालने और नफरत को जायज ठहराने के लिए किया जा सकता है। चुनाव की ऐसी स्वाधीनता का अगला कदम यही हो सकता है कि कोई किसी जाति के व्यक्ति का लाया खाना लेने से इनकार कर दे, रेस्तरां, ट्रेन या हवाई जहाज में भोजन परोसने वाले की जाति या धर्म पूछ ले। हमारा देश ही नहीं, सारी दुनिया जिस तरह के “ज्ञान” की जकड़ में है, उसे देखते हुए तय मानिए कि ऐसी मांग का समर्थन करने वाले भी हजारों की तादाद में निकल आएंगे। यह कोई नहीं सोचेगा कि आपकी चुनाव की स्वाधीनता किसी मनुष्य की गरिमा को नकारने पर आधारित नहीं हो सकती।
शब्दों और धारणाओं का दुरुपयोग इसी एक मामले तक सीमित नहीं। समाज में विवेक और तर्कबुद्धि की हैसियत कितनी कम होती जा रही है, इसके उदाहरण आजकल खोजने नहीं पड़ते। मूर्खता का अभूतपूर्व उत्सव मनाते इस समय में वे रोज-ब-रोज बिन बुलाए आपसे आ टकराते हैं।
एक उदाहरण याद करेंः कोई स्वामी जी दावा करते हैं कि उन्होंने सूर्य को आदेश दिया कि वह 40 मिनट बाद उदित हो। भला सूर्य की क्या मजाल कि स्वामी जी का आदेश टाले! उनके श्रोतागण बेहद खुशी और तारीफ के साथ तालियां बजाते हैं, सोशल मीडिया पर इस निहायत बेतुकी बात को रद्द करने वालों को विज्ञान-भैरव तंत्र और योगवाशिष्ठ का ज्ञान बांटते हैं। आस्था को ठेस पहुंचाने वालों को ‘ठीक’ करते हैं। और ये लोग कोई गैर पढ़े-लिखे, साधारण लोग नहीं, ऊंचे दर्जे और हैसियत वाले प्रोफेशनल लोग हैं, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के ज्ञानी हैं। असल में, अंग्रेजी जाने बिना आप स्वामी जी के प्रशंसक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह प्रवचन अंग्रेजी में ही करते हैं। ऐसा भी नहीं कि स्वामी जी मिथक और किंवदंती के मुहावरे में बोल रहे हैं। वह तो उतनी ही यथार्थपरकता के साथ अपनी ताकत का, सूरज पर अपने रौब का बयान कर रहे हैं जितनी यथार्थपरकता के साथ भाषा का प्रयोग अखबार में किया जाता है। आस्था और चमत्कार का यों तो चोली-दामन का साथ है, लेकिन साधारण लोग जिन चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, वे बहुत ही सीमित संदर्भ में प्रकृति के नियमों के परे या विपरीत जाते दिखते हैं। ऐसे चमत्कारों में से सबसे ऊंचे दर्जे का चमत्कार किसी मृत व्यक्ति को फिर से जिला देना ही तो हो सकता है, लेकिन इस चमत्कार में भी एक मृतक के फिर से जी उठने से दूसरे मृतकों पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
स्वामी जी के दावे पर गदगद होने वाले अंग्रेजीदां, उच्च कोटि प्रोफेशनल क्या यह भी भूल गए हैं कि सूरज का उगना और डूबना भाषा का रूपक भर है। सूरज न उगता है, न डूबता है। अपने आसपास चक्कर लगाती पृथ्वी की गति और स्थिति के आधार पर कहीं उगता दिखता है, तो कहीं डूबता। क्या ये इतना भी नहीं सोच पाते कि किसी जगह सूर्योदय को चालीस मिनट रोक दिया- इस दावे का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी की गति को चालीस मिनट के लिए रोक दिया। दूसरे शब्दों में सौरमंडल की गति का स्थगन, यानी महाप्रलय, इसके बावजूद स्वामी जी बोल रहे हैं, भक्तगण तालियां ठोक रहे हैं। संयोग नहीं कि ये उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्हें बुद्धिजीवी शब्द तक से चिढ़ है, तर्क, विवेक और बुद्धि की बात सोचने तक से जिन लोगों की कोमल भावनाएं आहत हो जाती हैं।
यह बुद्धि-विरोध के अद्भुत विस्तार का समय है। यह सत्यातीत समय है, पोस्ट ट्रुथ वक्त। जैसे कुछ बातें कालातीत होती हैं, वक्त से परे, वैसे ही इस समय में हम सत्य के परे जा चुके हैं; और जब सत्य का ही अर्थ नहीं रहा, तो सत्य तक पहुंचने के माध्यम यानी तर्क और विवेक की क्या जरूरत? बस बनी-बनाई धारणा और भावना ही सब कुछ है। टेक्नोलॉजी पढ़ लें या मैनेजमेंट; इस सत्यातीत समय में कोई जरूरी नहीं कि आपकी पढ़ाई आपके सोच-विचार का भी विस्तार करे। आप नितांत बेतुकी बातों पर मुग्ध ही नहीं हो सकते, उन्हें जायज ठहराने के लिए तर्क के दांवपेच भी खेल सकते हैं। सोच-विचार की जरूरत ही क्या है, विवेक का काम ही क्या है? इस वक्त में चुनाव की स्वाधीनता के नाम पर घोर मनुष्य-विरोधी आक्रामकता और आस्था के नाम पर शुद्ध विवेकहीनता को जायज ठहराया जा सकता है।
ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं, स्वाधीनता की, बिना विवेक के जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्वाधीनता पराधीनता का विलोम है। दूसरों पर निर्भर या उनके अधीन किन्हें रहना पड़ता है? कब तक रहना पड़ता है? उन्हें जिनका अपना “स्व” अपनी जिम्मेदारी लेने लायक न हुआ हो। तब तक जब तक कि वे अपना आप संभालने लायक न हो जाएं। बच्चे पूरी तरह स्वाधीन नहीं होते, उनके लिए फैसले मां-बाप लेते हैं। बीमार और कमजोर लोग स्वाधीन नहीं होते, उनके लिए फैसले तीमारदार और चिकित्सक लेते हैं। रोजमर्रा के इसी अनुभव का विस्तार राजनीति और समाज में करें तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों औरतें अपने फैसले आप लेने के लिए संघर्ष करती हैं, और हर समाज में कौन लोग उनका विरोध करते हैं, और क्यों? आपको यह भी समझ आ जाएगा कि अंग्रेजी राज और भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के बीच मूल विरोध इसी बात को लेकर था कि अंग्रेज दावा करते थे कि हम कोई अत्याचारी किस्म का राज थोड़े ही चला रहे हैं, हम तो बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से असमर्थ लोगों को सभ्य बनाने के बोझ (वाइट मेंस बर्डेन) का वहन कर रहे हैं। चर्चिल को तो पक्का विश्वास था कि दस साल के भीतर-भीतर भारतीय खुद ही गिड़गिड़ाएंगे कि अंग्रेज वापस आएं और राज-काज संभालें।
हमारा राष्ट्रीय आंदोलन केवल अंग्रेजी राज खत्म कर देने का आंदोलन नहीं था। राजनैतिक स्वाधीनता के लक्ष्य जितना ही महत्व इस आंदोलन ने समाज में विवेक के विस्तार को दिया था। मनुष्य मात्र की गरिमा का स्वीकार इस विवेक का प्रस्थान-बिंदु था। विभिन्न स्तरों पर समाज-सुधार की कोशिशों और राजनैतिक स्वाधीनता हासिल करने की कोशिशों के परस्पर संबंध को ध्यान में रखे बिना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के चरित्र, महत्व और आत्मविश्वास को समझा ही नहीं जा सकता। इस आत्मविश्वास का ही फल है कि चर्चिल भारतीयों द्वारा वापस बुलाए जाने की राह देखते-देखते ही इस दुनिया से निकल लिए।
यह आत्मविश्वास स्वाधीनता की जिस परिकल्पना पर आधारित था, उसे सबसे सुंदर शब्द गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की उस मशहूर कविता में दिए गए हैं, जिसमें कवि अपने देश के लिए ऐसी स्वाधीनता की प्रार्थना करता है जिसमें हर नागरिक का “मन भयरहित हो, माथा ऊंचा हो, और जहां विवेक की सरिता को अविवेक और अंधविश्वास के रेगिस्तान ने सोख न लिया हो।”
स्वाधीनता का 73वां साल शुरू होते समय हम ऐसे समय में हैं, जिसमें तथाकथित सुशिक्षित जन लोकतंत्र से ऊब गए लगते हैं। यह ऐसा समय है, जिसमें भय को हवा में घोला जा रहा है। यह ऐसा समय है जिसमें विवेक की सरिता को जानबूझ कर सुखाया जा रहा है। बुद्धिजीवी मात्र के प्रति घृणा का संचार किया जा रहा है। यह ऐसा समय है जिसमें बहुत सारे लोग स्वेच्छा से अपने विवेक और स्वाधीनता को ‘अच्छे दिनों’ के लालच में महानायक के चरणों में अर्पित करने को बेताब हैं। बात केवल अपने देश की नहीं, कई और देशों की भी है। ऐसी स्थिति में, मुझे तो अपने उपन्यास ‘नाकोहस’ के एक पात्र की टीस ही याद आती है, “किस दुनिया के सपने देखे, किस दुनिया तक पहुंचे!”
(लेखक वरिष्ठ आलोचक, टिप्पणीकार, जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं)