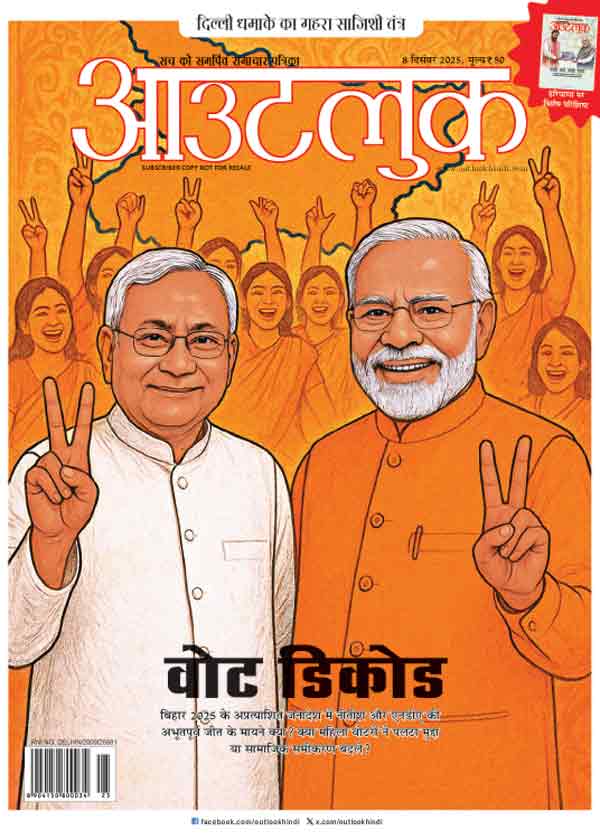जून के महीने में पश्चिमी विक्षोभ इस तरह के संक्षिप्त अंधड़ हर साल लाता है, पर यह भाषाई अंधड़ लंबे समय बाद आया है। कोठारी आयोग (1964-66) ने त्रिभाषा फार्मूले की विस्तृत चर्चा की थी। आयोग ने बताया था कि यह फार्मूला 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केस) ने सुझाया था और पांच वर्ष बाद मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस सुझाव को मंजूरी दी गई थी। नेहरू युग में भाषा-नीति एक बड़ा राजनैतिक मुद्दा थी, जिसे संविधान सभा पूरी तरह सुलझाए बगैर छोड़ गई थी। आजादी मिलने के बाद राष्ट्र-निर्माण का काम एकीकरण से जोड़कर देखा जाता था। यह एक गंभीर प्रशासनिक जिम्मेदारी मानी जाती थी। उस समय तक बाजार के जरिए आर्थिक एकीकरण का विमर्श अभी भविष्य के गर्भ में छिपा था।
यह एक अनोखी बात है कि कोठारी आयोग में त्रिभाषा फार्मूले की चर्चा शिक्षा नीति के नए प्रारूप के मुकाबले ज्यादा स्पष्ट और ताजगी लिए हुए दिखती है। आयोग की रिपोर्ट ने साफ कहा था कि त्रिभाषा फार्मूले के पीछे शैक्षिक सोच से कहीं ज्यादा ‘राजनैतिक और सामाजिक विवशताएं थीं।’ कोठारी आयोग ने फार्मूले को लागू करने में आई दिक्कतों का जिक्र करते हुए लिखा था कि यह प्रयास सफल नहीं हुआ है। विफलता के कारणों में, आयोग के अनुसार, पाठ्यचर्या में भाषा का भारी बोझ, हिंदी क्षेत्रों में एक अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ने के लिए उत्साह का अभाव, गैर-हिंदी क्षेत्रों में हिंदी की पढ़ाई को लेकर प्रतिरोध, और पांच-छह साल (कक्षा छह से 10 या 11 तक) द्वितीय और तृतीय भाषा पढ़ाने का खर्च शामिल था। तृतीय भाषा को लेकर आयोग ने लिखा था कि कई इलाकों में छात्रों को बहुत कम लाभ इस वजह से मिला है क्योंकि परिस्थिति व्यावहारिक नहीं थी, यानी वे एक ऐसी भाषा सीख रहे थे, जो उनके माहौल में नहीं थी।
कोठारी आयोग की रिपोर्ट का आलेख जे.पी. नाइक ने तैयार किया था, जो समूचे देश के शैक्षिक यथार्थ को भलीभांति समझते थे। त्रिभाषा फार्मूले की चर्चा का आलेख दिखाता है कि शैक्षिक जरूरतों और राजनैतिक दबावों के बीच संतुलन बिठाने में आयोग को कितनी परेशानी हुई। सारे विकल्पों और एक सदस्य की असहमति पर विचार करने के बाद आयोग ने लिखा था, “हम गंभीरता से महसूस करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में तीन भाषाओं की पढ़ाई मातृभाषा पर बच्चे की पकड़ में व्यवधान डालेगी और उसके बौद्धिक विकास को प्रभावित करेगी।”
दौलत सिंह कोठारी और जे.पी. नाइक अगर आज जीवित होते तो प्रारंभिक शिक्षा की दशा और नीति पर चकित और दुखी होते। साठ के दशक में वे यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि स्कूली शिक्षा का बड़े पैमाने पर निजीकरण हो जाएगा और शासन स्वयं शिक्षा को बाजार के हवाले करने में लगा होगा। दूसरी तरफ वे इस बात से भी चौंकते कि हिंदी क्षेत्र ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में सरकारी स्कूल पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इस निर्णय का घोषित कारण यह बताया जाता है कि माता-पिता अंग्रेजी के आकर्षणवश बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं। नई शिक्षा नीति का प्रारूप इस प्रवृत्ति पर चिंता जताता है और इसे अंग्रेजी-प्रेमी अभिजनों के वर्चस्व का प्रभाव मानता है।
जहां तक हिंदी का सवाल है, वह अब राजनैतिक दूध देने वाली गाय नहीं रही। देश का एकीकरण अब राजनीति के उस दौर से बहुत दूर जा चुका है, जो आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू हुआ था और जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी। जिस नव-राष्ट्रवाद की छाया संसद के ताजा चुनावों पर पड़ी है, वह भाषा और शिक्षा का मोहताज नहीं है। हिंदी पट्टी का जनमानस अब हिंदी के राजनैतिक प्रश्रय का यथार्थ देख चुका। उसकी भावनाएं अब मातृभाषा में शिक्षा के विचार और वादे से स्पंदित नहीं होतीं। शहरी मध्यम वर्ग का मानस बाजार की जरूरतों को सर्वोपरि मानकर अपनी संतान को जल्दी से जल्दी अंग्रेजी के प्रयोग में दक्षता देने के प्रति उत्साहित है।
जहां तक इस वर्ग की संतान के मानस का प्रश्न है, उसमें भाषा और राष्ट्रीय भावना का एक नया समीकरण देखा जा सकता है। भाषाविद और समाजशास्त्री चेज़ लडूसा ने बनारस के प्राइवेट स्कूलों का लंबे समय तक अध्ययन किया है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों का दृष्टिकोण समझाते हुए वे लिखते हैं कि हिंदी अब मातृभूमि की तरह पवित्र स्मृति और भक्तिभाव जगाने की भाषा रह गई है जबकि अंग्रेजी आकांक्षाओं के आकाश जैसी है, उत्साह और कहीं भी जा पहुंचने की स्वतंत्रता देने वाली। यह विश्लेषण कुछ नाटकीय लग सकता है, पर हिंदी प्रदेशों के शहरी मध्यम वर्ग का मनोविज्ञान सचमुच कुछ ऐसा ही है। राष्ट्रभाषा बनने का सपना दिखाते-दिखाते हिंदी अपने ही क्षेत्र में बेगानी और कमजोर पड़ गई है। आजादी के आंदोलन में हिंदी जिस राष्ट्र के निर्माण का प्रतीक और माध्यम बन गई थी, वह अपनी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था और उससे उपजे अरमानों के लिए अंग्रेजी को ज्यादा उपयुक्त पाता है।
जिन सरकारी स्कूलों में हिंदी शिक्षण का माध्यम है, उनकी हालत अच्छी नहीं है। अध्यापकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते ये स्कूल नौकरशाही के नियंत्रण और राजनैतिक दखलंदाजी की मार भी लगातार सहते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रतियोगिता में पिछड़ जाने का एहसास और उससे उपजने वाली हताशा और थकान भी बच्चों तक लगातार संप्रेषित होती रहती है। अन्य विषयों की बात क्या की जाए, स्वयं हिंदी की पढ़ाई भी दकियानूसी ढर्रे से मुक्त नहीं हो सकी है। साहित्य, आलोचना और भाषा विज्ञान के क्षेत्रों में हिंदी की ऊंचाइयां अध्यापकों के प्रशिक्षण में दूर-दूर तक नहीं झलकतीं, स्कूलों में कैसे प्रतिबिंबित होंगी। अन्य विषयों की पढ़ाई में इस्तेमाल हो रही हिंदी भी प्रायः बेजान बनी हुई है। इस स्थिति को सुधारने का काम जिन संस्थानों के जिम्मे डाला जा सकता था, वे स्वयं बदहाली और कोताही के शिकार हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हिंदी कोई सपना नहीं, सिर्फ पूजा भाव जगाती है।
भाषा की शिक्षा वाले हिस्से में नई शिक्षा नीति का प्रारूप एक तरह की शाब्दिक बहार पेश करता है। तीन वर्ष की आयु से बहुभाषिकता की बहार के बीच बच्चों की मातृभाषा या घर की भाषा ज्ञान और विचार का माध्यम ठीक-ठीक कैसे बनाई जाएगी, इस प्रश्न का कोई विश्वसनीय उत्तर नीति का दस्तावेज नहीं देता। बोलियों और मानक भाषा के बीच के रिश्ते बच्चों की समझ को पुष्ट करने के काम आएं, इसकी कोई युक्ति भी नीति का मसविदा नहीं सुझाता। आदिवासी भाषाओं को शिक्षा के दायरे में लाना काफी समय से एक नीतिगत प्राथमिकता बनाए जाने का इंतजार कर रहा है। इस तरह के तमाम सूक्ष्म सवालों की तह में अध्यापकों के भाषाई प्रशिक्षण को उपजाऊ बनाने की पहल का इंतजार छिपा है। लगता है, यह इंतजार अभी जारी रहेगा।
(लेखक प्रखर शिक्षाविद और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)