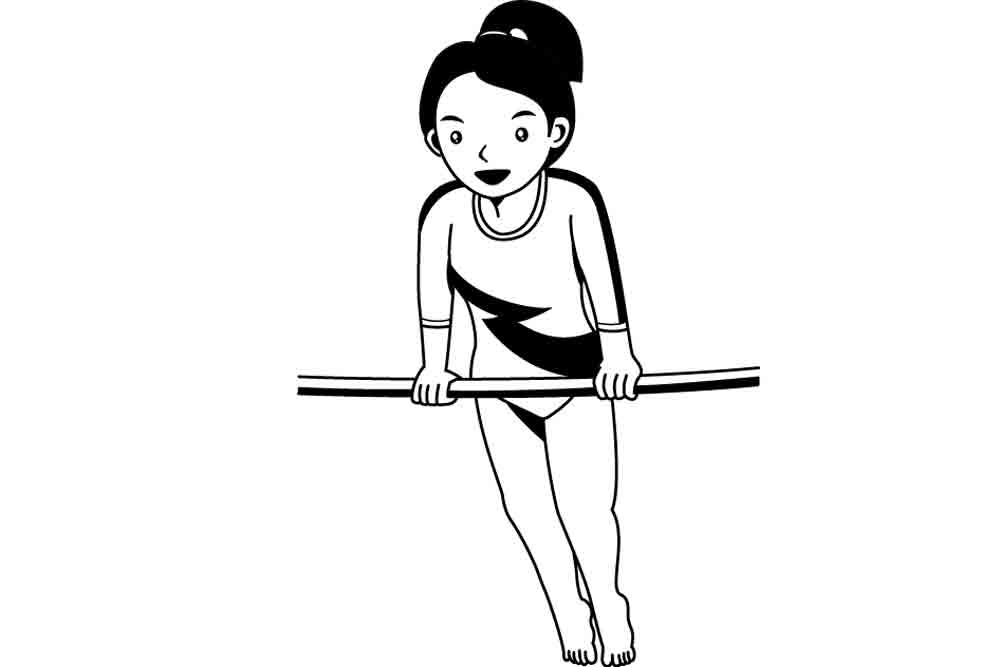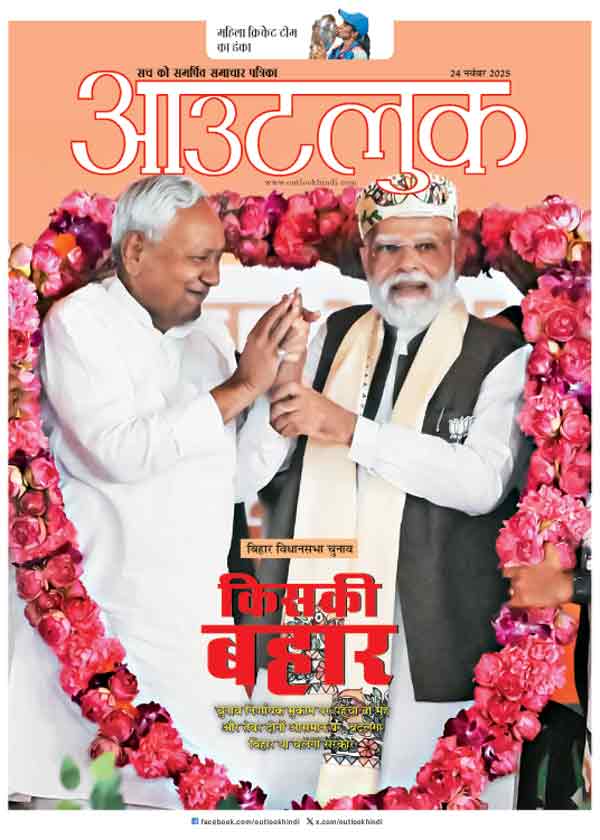आउटलुक अपने पाठको के लिए अब हर रविवार एक कहानी लेकर आ रहा है। इस कड़ी में आज पढ़िए दीपक शर्मा की कहानी। पिता की दूसरी शादी और मां-बेटी के रिश्तों की सघनता दर्शाती यह खूबसूरत कहानी।
“वॉल्ट” (फलांग भरो) मां अपनी सीटी बजाती है।
स्कूल का लाट मेरे सामने है।
लगभग पैंतालीस मीटर की दूरी पर।
“कैरी” (थाम लो), अपनी दूसरी सीटी के साथ लाट के बुर्ज पर खड़ी मां मेरी दिशा में वॉल्ट की पोल लहराती हैं।
मेरे हाथ पोल संभालते हैं और मैं उसके संग दौड़ पड़ती हूं।
तेज़, बहुत तेज़!
“शिफ्ट” (खिसक जाओ), मां तीसरी सीटी देती हैं।
वॉल्ट से पहले के मेरे डग पूरे हो चुके हैं।
पोल का बकस लाट के ऐन नीचे है।
पोल को उसमें बिठलाते समय मेरा निचला हाथ सरककर मेरे ऊपरी हाथ तक जा पहुंचता है।
इधर पोल अपने बकस में मजबूती से बैठती है, उधर अपने दोनों हाथों को मैं अपने सिर से खूब ऊपर उठा लेती हूं।
एक गुलेल की तरह पोल तेजी से मुझे ऊपर उछालती है और मेरी टांगें ऊपर की दिशा में घूम पड़ती हैं।
पोल की बगल-बगल।
मां की सीटी की झूम की लय में बहती हुई।
आगे बढ़कर मां मुझे झपट लेती हैं।
समूची की समूची।
हम दोनों अब एक साथ हैं।
एक-दूसरे की बांहों में।
लाट के बुर्ज के पीछे।
“ज्योग्रफी मिस ने अपना क्वार्टर छोड़ दिया है।” मैं अपनी शिकायत पेटी खोल लेती हूं, “अब वह अब हमारे क्वार्टर में आ गई हैं…।”
स्कूल के परिसर में अध्यापकों के लिए क्वार्टर बने हैं।
“मैं यही चाहती थी।” मां हंस पड़ती हैं।
“ज्योग्रफी मिस ने पापा के साथ शादी कर ली है…।”
“मैं यही चाहती थी। मुझसे छिड़ी तेरे पापा की जंग उसकी तरफ उलट ले…।”
“लेकिन पापा उसके साथ बहुत खुश हैं…” मैं हैरान हूं। पूरे स्कूल में प्यार बांटने वाली मां बस इन्हीं ज्योग्रफी मिस से ही तो नफरत करती रहीं, “पापा उसके साथ कभी झगड़ा नहीं करते। चौबीसों घंटे मधुर-मधुर पुकारा करते हैं। सारा झगड़ा अब मेरे साथ होता है। उसका भी। पापा का भी। मैं ही कष्ट में हूं…”
“तुम कब कष्ट में नहीं थीं।” मां मुझे अपनी बाहों से अलग कर देती हैं।
“जब तुम मेरे पास थीं।” मैं रो पड़ती हूं।
“मैं अब तुम्हारे ज्यादा पास हूं।” अपने हाथ मां मेरे कंधों पर टिका देती हैं। “सिंड्रेला की कहानी याद है? उसे रात की डांस पार्टी में जाने के लिए सवारी किसने भेजी थी?”
“उसकी मां ने…”
“उसे पार्टी की बढ़िया पोशाक किसने पहनाई थी?”
“उसकी मां ने…”
“उसे राजकुमार के सामने कौन लाया था?”
“उसकी मां…”
“राजकुमार के कान में कौन फुसफुसाई थी, डांस करते समय सिंड्रैला का एक स्लीपर चुरा लो?”
“उसकी मां…”
“उस मां के पास इतनी ताकत कहां से आई?” मां मेरे गाल थपथपाती हैं।
“मैं नहीं जानती कैसे।”
“नहीं जानती?” मां हंसती हैं।
“वह ताकत उसे उसकी मौत ने दी थी। जब तक वह जिंदा थी, अपनी सिंड्रैला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मरने के बाद उसने सिंड्रैला को राजकुमार के महल में जा पहुंचाया…”
“मुझे राजकुमार नहीं चाहिए।” मैं मां के सीने के साथ जा चिपकती हूं, “मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे पास रहना चाहिए। तुम्हारे साथ रहना चाहिए…”
“ठीक है।” मां झट मान जाती हैं, “मैं तुम्हें रोज इधर बुला लूंगी। आज की तरह। सीटी बजा कर। तुम रोज आओगी?”
“मैं आऊंगी। रोज आऊंगी…”
“अब नीचे चलें?” मां मेरे गाल चूमती हैं।
“यहां से कूदेंगे?” मैं पूछती हूं, “नीचे?”
लोप होने से पहले मां इसी बुर्ज से नीचे कूदी थीं।
“नहीं, हम सीढ़ियों से नीचे जाएंगे…”
मां मुझे लाट के अंदर ले आती हैं। गोल दीवारों के बीच कई सीढ़ियां नीचे उतर रही हैं।
बिना टेक के।
बिना जंगले के।
“चलें?” अपनी टेक देकर मां मुझे पहली सीढ़ी पर ले आती हैं।
“इन्हें गिनोगी?” वे पूछती हैं।
सीढ़ियों की संख्या जब भी ज्यादा होती, मां और मैं सीढ़ियों की गिनती जरूर करते।
“हां” मैं गिनना शुरू करती हूं।
नौ की गिनती पूरी होती है तो सीढ़ियों का पहला घुमाव आन प्रकट होता है।
“इसमें ऐसे नौ घुमाव हैं।” जंगले की तरह मां मुझे अपनी बाहों की ओट में ले रही हैं, “अब बताओ इसमें कितनी सीढ़ियां होंगी?”
“निन्यानवे।” उत्तर देने में मुझे तनिक देर नहीं लगती है, जैसे पहला घुमाव नौ सीढ़ियों के बाद आता है, आखिरी घुमाव के बाद भी नौ सीढ़ियां होंगी ही होंगी…”
“मेरी नन्ही जादूगरनी।” मां झुककर मेरे बाल चूम लेती हैं।
“पापा कहते हैं, अर्थमैटिक में कोई जादू नहीं है। बस दिमाग को फुर्ती दिखलानी चाहिए…”
सारा स्कूल पापा को मैथ्स-विजर्ड, गणित-जादूगर के नाम से जानता है।
“जैसे मेरे ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट में शरीर का फुर्ती में आना और फुर्ती में रहना जरूरी है?” मां अपने अनुभव से बोल रही हैं। चक्रपट्टी और मैदान वाले खेलकूद में मां बेजोड़ रही हैं। हमारी नई खेल टीचर मां जैसा एक भी करतब-क्रिया नहीं कर पातीं। उनके पास पोल वॉल्टिंग में मां जैसा टेक-ऑफ नहीं, हाईजंप में मां जैसी सिजर्स नहीं, ईस्टर्न कट-ऑफ नहीं, वेस्टर्न रोल नहीं, स्ट्रैडल नहीं, ट्रिपल जंप में मां जैसा हॉप नहीं, स्टैप नहीं, जंप नहीं।
हम निन्यानवे सीढ़ी तक आ पहुंचे हैं।
“तुम घर जाओ।” मां मुझसे विदा लेना चाहती हैं।
“तुम कहां जाओगी?” मैं पूछती हूं।
“अपने लोक में। वहां कई ग्रह हैं। कई तारे। कुछ नीचे, कुछ बुलंद। कुछ चमकीले कुछ मंद। लेकिन कोई किसी को इशारा नहीं देता। किसी से इशारा नहीं लेता। अपने अपने दायरे में, अपने अपने इशारे पर वह अपना-अपना घूमते हैं। अपनी-अपनी मौज में, अपनी अपनी मर्जी से…”
“मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।” मैं मां की टांगों से चिपक के लेती हूं। पौने छह फुट की मां के आगे दस साल के मेरे पौने चार फुट बौने हैं।
“नहीं!” अपनी मजबूत बांहों से मां मुझे विलग कर देती हैं, “नहीं। तुम यहीं रहो। उधर हम एक-दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगी। उधर सभी को अकेले रहना पड़ता है। तुम यहां रहोगी तो मैं तुम्हें इधर बुला सकूंगी…”
“मुझे तुम्हारी सिटी का इंतजार रहेगा।”
लबडब लबडब लबडब मेरा दिल जोर से धड़कता है। डोलता है।
मां से मैं अभी बिछुड़ना नहीं चाहती। कभी बिछुड़ना नहीं चाहती।
“यह सीटी तुम पहन क्यों नहीं लेती?” मां फुर्ती से अपना हाथ घुमाती हैं और अपनी गर्दन खाली कर देती हैं।
“लो!”
सीटी अब मेरी गर्दन में है।
सरूर से भरकर सिटी के ऊपरी सिरे पर बने मुंहवाले छेद में मैं अपनी पूरी ताकत के साथ सांस छोड़ती हूं। सिटी की बंद दीवार से वह टकराती है और छेदवाली दूसरी दीवार से गूंज बनकर बाहर आ लपकती है।
लाट से क्वार्टर तक मैं सीटी बजाती जाती हूं। धीमी-धीमी, मीठी-मीठी।
मां को अपने साथ रखती हुई।
वहां पहुंचने पर दरवाजे की घंटी की बजाय सीटी देती हूं। मां के अंदाज में। अंदर वालों को चौंकाने के वास्ते, चिढ़ाने के वास्ते। मां की सीटी से दोनों की दुश्मनी पुरानी भी है और कड़ी भी।
“कौन?” मेरा अंदाजा सही साबित हुआ है। दोनों एक साथ दरवाजे पर लपक लिए हैं।
चौंके- चौंके।
चिढ़े-चिढ़े।
जवाब में मैं सीटी बजा देती हूं खूब जोर से।
“कहां मिली?” पापा पूछते हैं।
“लाट पर।” मैं कहती हूं। उन्हें नहीं बताती सिटी के साथ मां को भी इधर लिवा लाई हूं।
“आज? कमाल है इतने दिन सबकी नजर से बची रह गई?”
आज ही के दिन पांच शुक्रवार पहले मां घर से लोप हुई थीं।
“वही है क्या?” ज्योग्रफी मिस उत्तेजना से भर उठती है।
“देखता हूं।” सीटी को पापा मेरी गर्दन से अलग कर देते हैं।
“क्या निशानी है?” ज्योग्रफी मिस अधीर हो रही है।
“इसकी डोरी वाली ठैठी पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए…”
“आपका नाम?”
“वह ऐसी ही थी। घर के लिए बर्तन भी खरीदती तो मेरा नाम उन पर लिखवा दिया करती…”
“यहां भी लिखा है।” ज्योग्रफी मिस कहती है, “और इसकी डोरी के मनके तो देखिए। मामूली तांबे के नहीं लगते।”
“कीमती लगते हैं…”
“मेरी सीटी है।” सीटी के लिए उसका लालच मुझसे देखे नहीं बनता। झपटकर उसके हाथों से मैं सीटी अपने हाथों में ले लेती हूं। अपनी गर्दन पर लौटाने।
“यह सीटी तुझे देनी पड़ेगी।” ज्योग्रफी मिस मेरी गर्दन की ओर बढ़ती है।
“सीटी हम ले लेंगे।” बीच ही में पापा उसे रोक देते हैं, “लेकिन ऐसे नहीं। आज नहीं। अभी नहीं…।”
“क्यों नहीं?” ज्योग्रफी मिस तमकती है, “जब मैं कह रही हूं इसे आज ही लेना है, अभी ही लेना है। इसकी आवाज मैं सह नहीं सकती, इतनी तीखी, इतनी तेज…”
“क्यों?” पापा अपना हाथ उठाते हैं और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर छोड़ देते हैं… “मेरा कहा कोई कहा नहीं? मेरा कहा नहीं सुनोगी? अपनी ही कहती जाओगी? मनवाती जाओगी?”
“मैंने क्या कहा?” एक झटके के साथ ज्योग्रफी मिस दरवाजा लांघती है। अंदर अपने कमरे की तरफ मुड़ती है और लोप हो जाती है।
“यह सीटी मैं कभी नहीं दूंगी।” मैंने दोनों हाथों से उसे ढांप लिया है।
“मत देना!” पापा मेरे गाल थपथपाते हैं।
इस नई जंग में वे मेरे साथ हैं।
दीपक शर्मा
30 नवंबर 1946 को अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मी दीपक शर्मा की कहानियां एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। उनकी भाषा और कहानी के अंत हमेशा पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लखनऊ क्रिश्चियन कालेज के स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग से अध्यक्षा, रीडर पद से सेवानिवृत्त हुईं दीपक शर्मा की पहली कहानी 1979 में धर्मयुग में ‘कोलम्बस अलविदा’ नाम से छपी थी। तब से अब तक उनके 18 कहानी संग्रह आ चुके हैं।