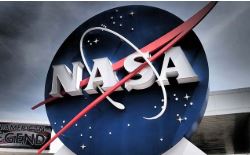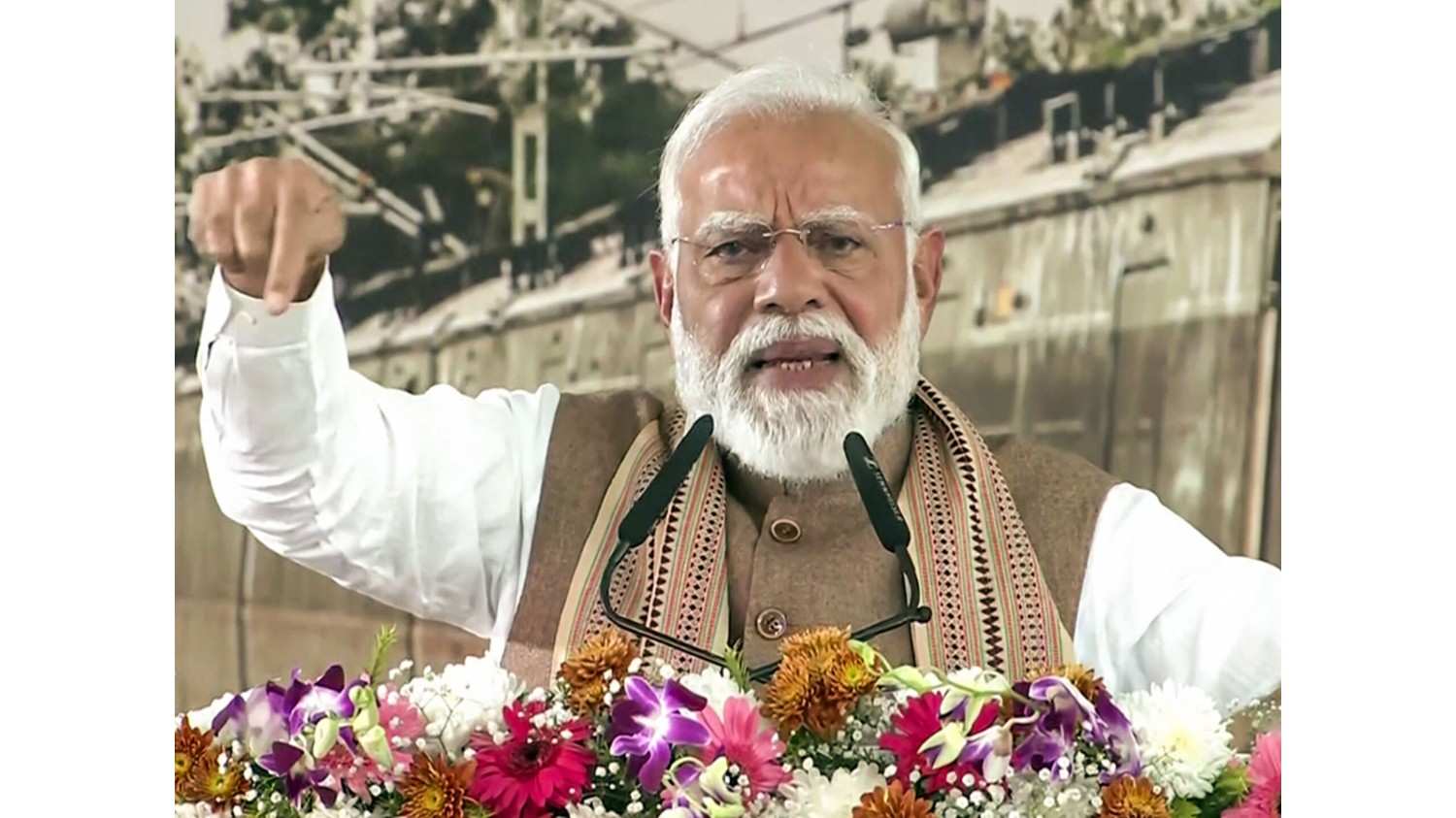चंद्रमा पर उतरना, वहां ध्वज फहराना, वहां की मिट्टी अनुसंधान के लिए लाना अब पुरानी बात है। अब नई अंतरिक्ष दौड़ पृथ्वी के इस इकलौते उपग्रह पर स्थायी निर्माण और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर शुरू हो गई है, जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र अहम भूमिका निभा सकते हैं।
खबरों की मानें तो अप्रैल 2025 में चीन ने वर्ष 2035 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना पेश की थी, जो उसके प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को ऊर्जा देगा। इसके जवाब में अगस्त में अमेरिका के कार्यवाहक नासा प्रशासक सीन डफी ने कहा कि अमेरिका वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर अपना परमाणु रिएक्टर चालू कर सकता है।
यह नया भले ही लगे लेकिन यह चौंकाने वाली खबर कतई नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह अचानक शुरू हुई होड़ नहीं है। नासा और अमेरिकी ऊर्जा विभाग लंबे समय से छोटी परमाणु ऊर्जा प्रणालियों पर काम कर रहे हैं, जो चंद्रमा पर अड्डों, खनन कार्यों और दीर्घकालिक निवास के लिए बिजली उपलब्ध करा सकें। अंतरिक्ष कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हथियारों की होड़ नहीं बल्कि रणनीतिक बुनियादी ढांचे की दौड़ है।
कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं
परमाणु ऊर्जा का अंतरिक्ष में इस्तेमाल नया विचार नहीं है। 1960 के दशक से अमेरिका और सोवियत संघ ने रेडियोआइसोटोप जनरेटर का उपयोग किया है, जो छोटे स्तर के रेडियोधर्मी ईंधन से उपग्रहों, मंगल रोवर्स और वॉयजर मिशनों को शक्ति प्रदान करते हैं।
संयुक्त राष्ट्र की 1992 का ‘‘बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से संबंधित सिद्धांत’’ नामक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव यह रेखांकित करता है कि सौर ऊर्जा अपर्याप्त होने पर परमाणु ऊर्जा आवश्यक हो सकती है। यह प्रस्ताव सुरक्षा, पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय परामर्श के दिशा-निर्देश तय करता है।
अंतरराष्ट्रीय कानून में कहीं भी चंद्रमा पर शांतिपूर्ण उद्देश्यों से परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर रोक नहीं है। लेकिन पहला सफल देश भविष्य के आचरण और कानूनी व्याख्याओं के लिए मानक तय कर सकता है।
पहला होने का महत्व
अमेरिका, चीन और रूस समेत प्रमुख देशों ने 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यह तय करती है कि सभी देश एक-दूसरे के हितों का “उचित ध्यान” रखें। इसका अर्थ है कि यदि कोई देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाता है, तो अन्य देशों को उसके आसपास काम करने के लिए कानूनी और भौतिक रूप से सीमाएं होंगी।
संधि के अन्य अनुच्छेद भी इसी तरह के आचरण की सीमाएं तय करते हैं, हालांकि वे सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। सभी देशों को चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर स्वतंत्र रूप से पहुंचने का अधिकार है, लेकिन वे संप्रभुता का दावा नहीं कर सकते। फिर भी, देश वहां ठिकाने और सुविधाएं बना सकते हैं, जिन तक उनकी पहुंच नियंत्रित की जा सकती है।
बुनियादी ढांचा प्रभावी है
किसी क्षेत्र में रिएक्टर लगाना वहां स्थायी उपस्थिति का संकेत है, खासकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जैसे संसाधन-समृद्ध इलाकों में, जहां क्रेटरों में बर्फ मौजूद है। यह बर्फ रॉकेट ईंधन और चंद्र अड्डों के लिए जल स्रोत बन सकती है। इन संवेदनशील और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बनाने से कोई देश संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित कर सकता है और व्यवहारिक रूप से दूसरों को रोक भी सकता है।
सौर ऊर्जा की सीमाएं और परमाणु विकल्प
चंद्रमा पर वायुमंडल न के बराबर है और वहां 14 दिन तक अंधेरा रहता है। कुछ क्रेटरों में सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ऐसे में सौर ऊर्जा कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुपयोगी हो जाती है। एक छोटा चंद्र रिएक्टर लगातार 10 वर्ष से अधिक समय तक बिजली दे सकता है, जिससे आवास, रोवर्स, 3डी प्रिंटर और जीवन-समर्थन प्रणालियां संचालित हो सकती हैं। यही तकनीक मंगल मिशनों के लिए भी जरूरी मानी जा रही है।
पारदर्शी शासन की जरूरत
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास तकनीक के साथ-साथ शासन में भी नेतृत्व करने का अवसर है। अगर वह अपने कार्यक्रमों को सार्वजनिक रखे, अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करे और शांतिपूर्ण उपयोग का वादा करे, तो यह अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। भविष्य में चंद्रमा पर प्रभाव का निर्धारण झंडों से नहीं बल्कि वहां बनाए गए ढांचे और उनके उपयोग के तरीके से होगा। परमाणु ऊर्जा इस भविष्य का अहम हिस्सा बन सकती है, बशर्ते इसे जिम्मेदारी और अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप लागू किया जाए।