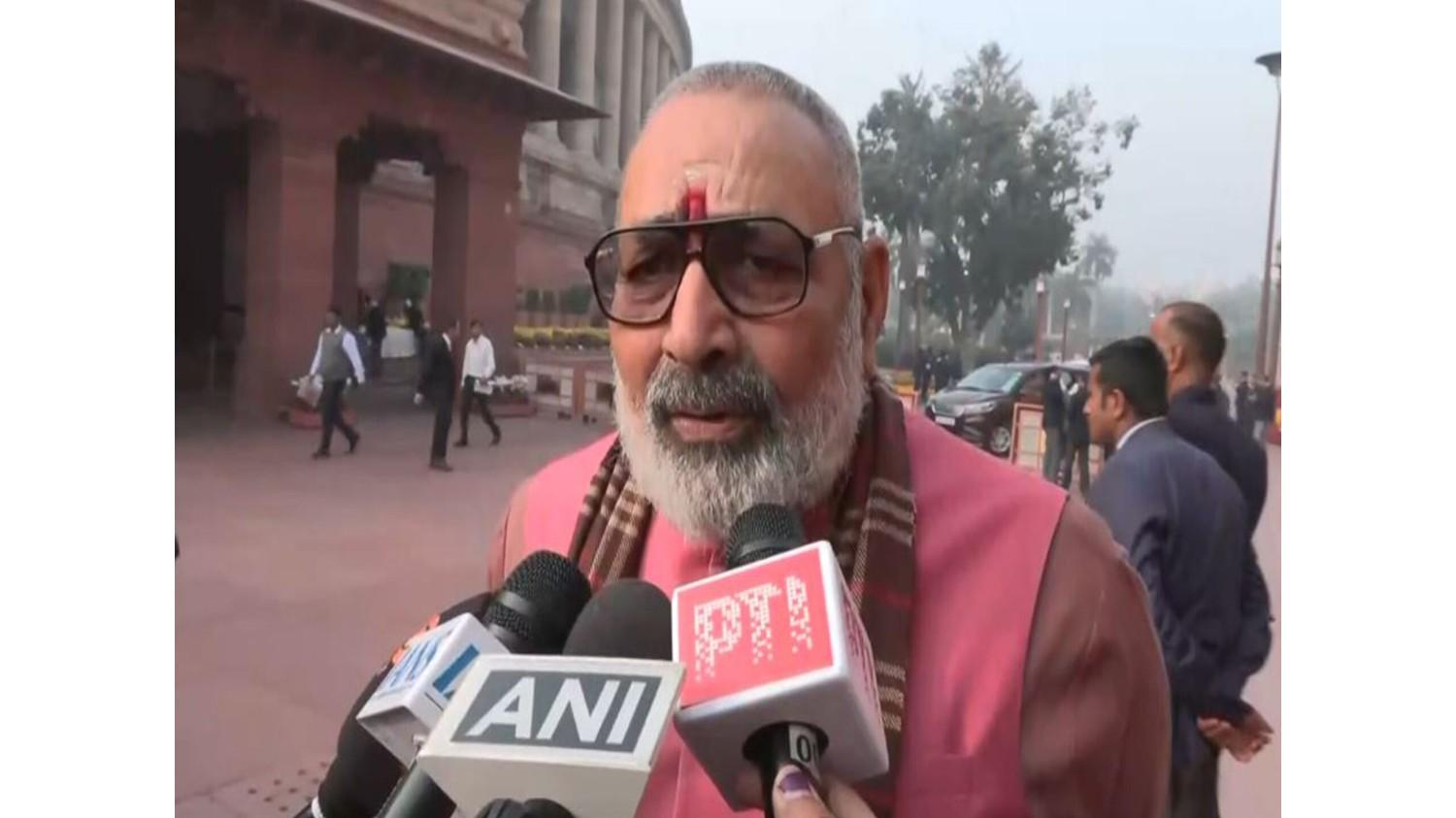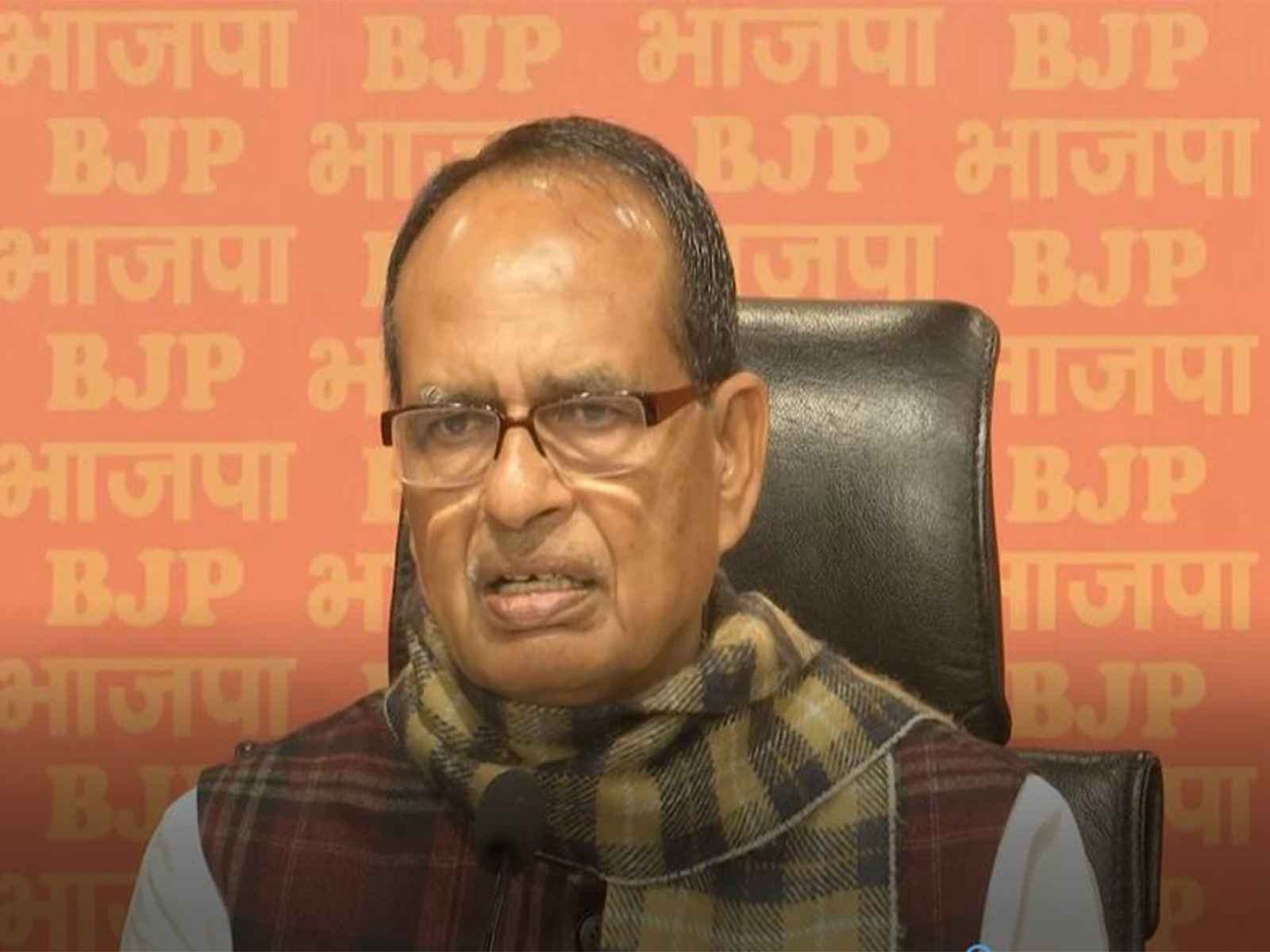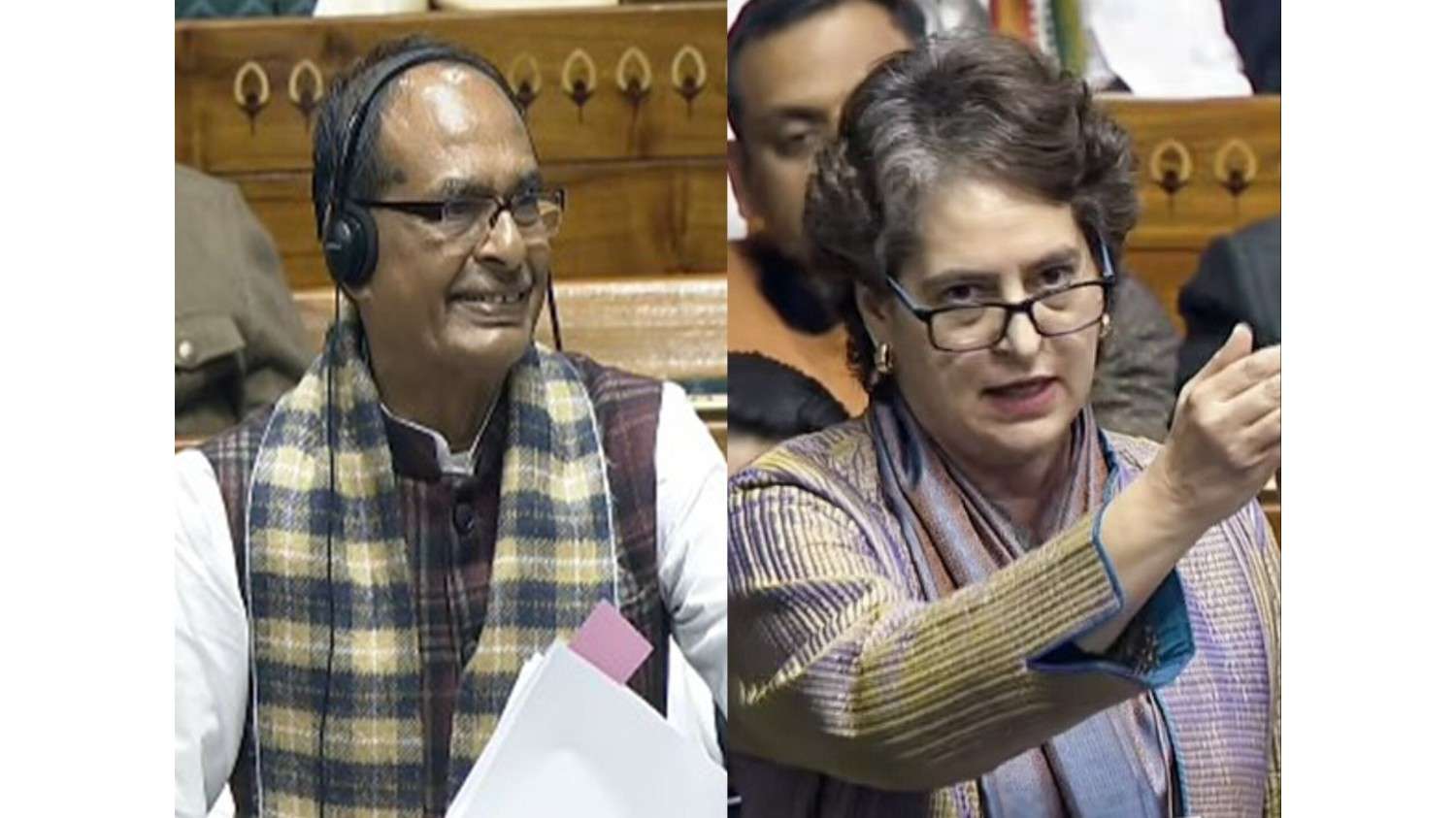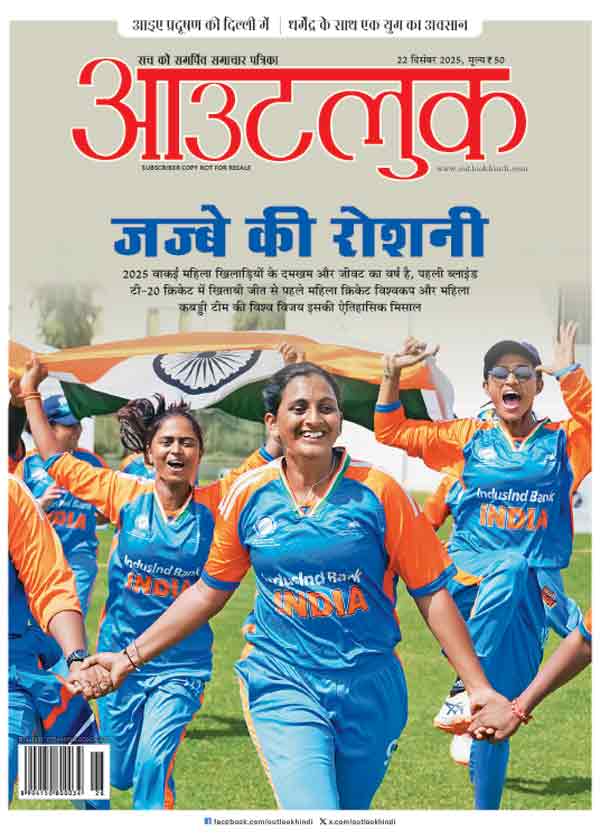एसआइआर के जरिए लोकतंत्र में हिस्सेदारी सीमित करने की चुनाव आयोग की प्रक्रिया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के मूल सिद्धांत के साथ विश्वासघात
हाल में मैंने देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के उद्धरण के साथ मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा। उसमें मैंने 1951-52 के पहले आम चुनाव के लिए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने आई चुनौतियों का हवाला दिया। उस समय गणतंत्र नवजात अवस्था में था, बंटवारे से त्रस्त था, निरक्षरता थी और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार दूर की कौड़ी था। फिर भी, देश के लोगों ने चुनाव प्रक्रिया में पूरा भरोसा दिखाया क्योंकि उनका मानना था कि चुनाव कराने वाली संस्था निष्पक्ष, स्वतंत्र और तब की कार्यपालिका या सरकार से पूरी तरह अप्रभावित है।
चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के तहत हुई और उसे लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संरक्षक माना जाता है, जिसकी संवैधानिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों में केंद्रीय भूमिका है। चुनाव आयोग महज प्रशासनिक प्राधिकरण नहीं है। संविधान निर्माताओं ने उसे भारतीय लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में देखा था, ऐसी संस्था जो राजनीति से ऊपर उठे और जनादेश की पवित्रता की रक्षा करे। उसे वैधता सरकार से नहीं, बल्कि संविधान और करोड़ों देशवासियों से मिलती है, जिन्हें विश्वास है कि उनके वोट की गिनती बिना किसी भय या पक्षपात के की जाएगी। मतदान का अधिकार लोगों को सरकार का उपहार नहीं, बल्कि यह संविधान के तहत सुरक्षित लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी संस्था, चुनाव आयोग को भी, इसे कम करने का अधिकार नहीं है।
हालांकि, चुनाव आयोग ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) जैसे उपायों से ऐसी प्रक्रिया शुरू करता लग रहा है, जो पक्षपातपूर्ण, अपारदर्शी या लोगों को बाहर करने वाला है। इस तरह यह उस बुनियाद को ही कमजोर कर रहा है, जिसकी रक्षा के लिए उसे बनाया गया था। इसके अलावा, बड़ा नुकसान यह भी है कि उस संस्था में मतदाताओं का भरोसा डिग रहा है, जिसकी स्थापना लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए की गई थी।
यह विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, लेकिन बिहार से जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से जुड़ी हालिया खबरें बेहद चिंताजनक हैं। जमीनी स्तर पर सक्रिय लोग बता रहे हैं कि करोड़ों लोगों के मताधिकार छिनने का डर सता रहा है। एसआइआर कहने को, तो मतदाता सूची को अद्यतन करने का उपाय है, लेकिन यह ऐसा औजार बन गया है, जिससे गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों के वोटरों का लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है या उन पर सवाल उठा रहे हैं। यह लोकतांत्रिक आधार को व्यापक बनाने के बजाय उसे संकुचित करता है, जिससे सशक्तीकरण के बजाय मताधिकार से वंचित होने की ओर अग्रसर होता है।

हम राज्य भर से गरीबों, भूमिहीनों, आदिवासियों, प्रवासी मजदूरों, अल्पसंख्यकों और विपक्षी दलों के क्षेत्रों से मतदाता सूची से संदिग्ध रूप से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की खबरें सुन रहे हैं। दशकों से मतदान करते आ रहे लोगों को मतदान के दिन अचानक पता चलता है कि उनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं। परिवारों को पता चलता है कि कुछ सदस्यों को बरकरार रखा गया है, जबकि अन्य के नाम काट दिए गए हैं। मतदान का अधिकार सबसे बुनियादी संवैधानिक गारंटी है, वह बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो जाता है। यह नौकरशाही की मूक हिंसा है जिसे सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हथियार बनाकर निर्देशित करते हैं। यह ऐसे राज्य में आयोग के ‘चुनिंदा कागजात’ की मांग से भी जाहिर होता है, जहां संबंधित कागजात देश में सबसे कम उपलब्ध हैं।
जहां लोगों को सिर्फ मतदाता सूची में बने रहने के लिए हाथ-पैर मारना पड़े, वह पतनशील लोकतंत्र है। बिना उचित प्रक्रिया के वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाना सामान्य त्रुटि नहीं, बल्कि जनता की संप्रभुता की चोरी है। हर संदिग्ध पुनरीक्षण लोगों और राज्य-सत्ता के बीच संवैधानिक समझौते पर चोट है। जब आयोग कठिन सवालों के जवाब देने से मुंह चुराता है, तो इससे चुनावों में भरोसा ही डिगेगा।
आज वह भरोसा डगमगा गया है। संविधान के संरक्षक के रूप में गठित आयोग अब उसे नष्ट करने में जुटा है। अपने कामकाज को सत्ताधारियों के हितों के साथ जोड़कर, वह अपनी ही स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है। लोकतांत्रिक भागीदारी को सीमित करने वाली प्रक्रियाओं के जरिए वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के मूल विचार के साथ विश्वासघात करता है, जो संविधान के सबसे क्रांतिकारी वादों में एक है।
इस संस्थागत पतन की वास्तविकता जितनी स्पष्ट है, उतनी ही निर्विवाद भी। पांच राज्यों के ताजा लोकनीति-सीएसडीएस सर्वेक्षण से पता चलता है कि एक-तिहाई से भी कम मतदाता अब चुनाव आयोग में विश्वास व्यक्त करते हैं, जबकि इस संस्था पर ‘अविश्वास’ करने वालों का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। आयोग में ‘अत्यधिक विश्वास’ व्यक्त करने वालों का अनुपात भी घट रहा है। संस्थागत साख में यह तीव्र गिरावट वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी (वी-डेम) परियोजना की भारतीय लोकतंत्र के मूल्यांकन में भी प्रतिध्वनित होती है। 2024 की लोकतंत्र रिपोर्ट भारत के ‘चुनावी निरंकुशता’ के पतन का खुलासा करती है। इसके मुताबिक, 2023 में देश निरंकुशता के मामले में शीर्ष 10 है।
चुनावी निष्पक्षता की रक्षा करने वाली संस्था ही उसकी गिरावट में भागीदार और अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र सूचकांक में भारत चुनावी निरंकुशता की ढलान की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस तरह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का संकट सिर्फ कोई धारणा नहीं, बल्कि संवैधानिक संकट है, जो लोकतांत्रिक वैधता के मूल पर ही प्रहार करता है।
सवाल यह नहीं है कि बिहार के अगले चुनाव में कौन जीतता या हारता है, बल्कि यह है कि क्या चुनाव आयोग में अभी भी वह नैतिक साहस है, जिससे वह संविधान के अनुसार स्वतंत्र संस्था बनी रहे। चेतावनी साफ है, अगर आयोग इसी राह पर चलता रहा, तो उसे भारतीय लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में नहीं, बल्कि सत्तावादी दबावों के आगे झुकने वाले सहयोगी के रूप में याद किया जाएगा।
लोगों को जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, क्योंकि अगर मताधिकार खोखला हो गया है। तो उस पर टिकी बाकी सभी बातें, जैसे संसद, प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र भी चरमरा जाएगा। तो क्या हम खोखला और घुटना टेकू लोकतंत्र चाहते हैं?
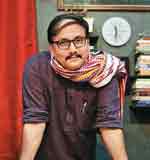
(लेखक राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य हैं। उनकी चर्चित किताब ‘इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स ऐंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी’ है। विचार निजी हैं)