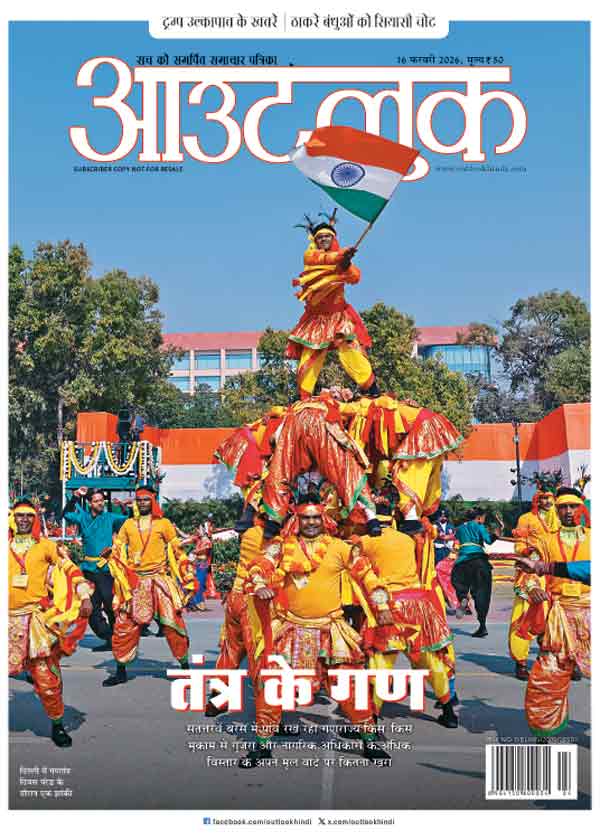वाकई अभूतपूर्व! हमारे गणतंत्र या ‘‘लोकतंत्र की जननी’’ में ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिला था। न्याय के शिखर और सरकार पहले भी टकराए हैं, हदें लांघने के आरोप पहले भी उठे हैं, लेकिन सिर्फ संविधान के दायरे के हवाले से ही। शायद ही कभी सवाल उठा कि कौन सर्वोच्च है राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या ऐसे आरोप उछले कि देश के प्रधान न्याायाधीश ‘‘धर्म युद्ध, गृह युद्ध’’ के जिम्मेदार हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ‘‘सुपर संसद’’ बन गई है। हालात इस मुकाम पर पहुंच गए कि केंद्र सरकार को निर्देश देने की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कह दिया कि हम कौन हैं निर्देश देने वाले, हम पर दखलंदाजी के आरोप हैं, आप वहीं आवेदन लेकर जाइए। गौरतलब है कि उस पीठ की अगुआई न्यायाधीश बी.आर. गवई कर रहे थे, जो अगले ही महीने के मध्य में अगले प्रधान न्यायाधीश बनने वाले हैं। आरोप केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों-नेताओं की ओर से ही नहीं उछले (अलबत्ता बाद में पार्टी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने उसे उनकी निजी टिप्पणी करार दिया), उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 को ही सुप्रीम कोर्ट के पास “नाभिकीय मिसाइल’’ बता दिया, जिसमें उसे विशेष अधिकार हासिल है।
इसकी फौरी वजह तो सुप्रीम कोर्ट के तीन हालिया फैसले हैं, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल को नागवार गुजरे। हाल में तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि राज्यपाल की ओर से 10 विधेयकों को दूसरे दौर में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना अवैध और कानूनी रूप से गलत है और इसलिए उसे रद्द किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि ये विधेयक राज्यपाल के पास अनावश्यक रूप से लंबे समय से लंबित हैं, तथा राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को भेजने में भी कोई साफगोई नहीं दिखाई, इसलिए उन्हें उस तारीख को स्वीकृत माना जाएगा, जब उन्हें पुनर्विचार के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था।
अदालत ने विधेयकों की मंजूरी के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर अधिकतम तीन महीने की अवधि की भी व्यवस्था तय कर दी। उसके कुछेक दिन पहले अदालत की एक अन्य पीठ ने ऊर्दू को भारतीय भाषा बताया और कहा कि उसका मजहब से कोई लेनादेना नहीं है इसलिए उसके उन्नयन, विकास तथा पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद ही वक्फ संशोधन कानून, 2025 पर प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुआई वाली पीठ ने अगली सुनवाई तक उसके तीन प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी। ये मामले भाजपा और संघ परिवार के लिए विशेष अहमियत रखते हैं, यह तो जाहिर है।
कार्यपालिका या विधायिका बनाम न्यायपालिका का विवाद वैसे तो नया नहीं है। आजादी के बाद अनेक ऐसे विवाद याद किए जा सकते हैं। अमूमन तमाम सरकारें अप्रिय अदालती फैसलों पर न्यायपालिका पर सवाल उठाती रही हैं। हर संस्था अपनी स्वायत्तता पर जोर देती रही है, लेकिन कभी भी मामला इस सीमा तक या भाषा की मर्यादाएं नहीं लांघती थीं। इसी मामले में यह विवाद आश्चर्यजनक-सा लगता है। तो, क्या विशेष सियासी मजबूरियां आन पड़ी हैं या मौजूदा दौर में क्या पहली बार सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ ज्यादा प्रतिकूल लग रहा है? वैसे तो, राज्यपालों की भूमिका भी उस सियासत से जुड़ी लगती है, जिसके जरिए केंद्र सरकार अपनी तरह से राज्यों में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। वक्फ के मामले में भाजपा और उसकी विचारधारा के संगठन-संस्थाओं के एजेंडे में रहा है। जो भी हो, मामले को इस हद तक ले जाने की वजहें किसी खास सियासी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती हैं और मजबूरी का भी।
विवाद की शुरुआत उपराष्ट्रपति, जो संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, के राज्यसभा प्रशिक्षुओं के एक कार्यक्रम में भाषण से हुई। उन्होंने कहा, “हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद को भी निर्देश दिया जा रहा है। कामकाज की समय-सीमा तय की जा रही है। यह कैसे संभव है? सुप्रीम कोर्ट के पास चौबीसों घंटे अनुच्छेद 142 न्यूक्लीयर मिसाइल है। इससे तो लोकतंत्र में चुनाव का अर्थ ही नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बन गया है।” लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि धनखड़ साहब को मालूम होना चाहिए कि हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में कोई पद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने ही ताकत दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ की राय भी तकरीबन यही है। उनका सवाल है, “पद कैसे सर्वोच्च हो सकता है? प्रधान न्यायाधीश या किसी न्यायाधीश का पद भी बड़ा नहीं, बल्कि उसका संवैधानिक दायित्व बड़ा है। और तमिलनाडु वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो तीन महीने की समय-सीमा की बात की है, वह तो गृह मंत्रालय के मानक प्रक्रिया के ज्ञापन के मुताबिक ही है।” विपक्ष तथा इंडिया ब्लॉक की राजनैतिक पार्टियों ने तो धनखड़ के बयान की कड़ी निंदा की ही।
लेकिन, उसके बाद तो जैसे बर्र का छत्ता ही छेड़ दिया गया। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने तो यहां तक कह दिया कि “सीजेआइ (प्रधान न्यायाधीश) संजीव खन्ना की वजह से जगह-जगह गृह युद्घ जैसी स्थिति है।” वे यहीं नहीं रुके, कहते गए, “सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं की क्या दरकार है।” वे यह भी बोले कि “संसद के अगले सत्र में एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी विधेयक फिर लाया जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभी तो न्यायपालिका में कोई एससी-एसटी, पिछड़ा जज नहीं है, सिर्फ भाई-भतीजावाद चल रहा है।” इस संदर्भ में यहां यह जिक्र करना शायद गैर-मुनासिब न हो कि 13 मई को मौजूदा प्रधान न्यायाधीश के रिटायर होने पर उस पद आने वाले अगले न्यायाधीश्ा गवई एससी वर्ग से ही आते हैं।
दुबे ही नहीं, उसके बाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा, एक अन्य नेता राजीव चंद्रशेखर ने भी राष्ट्रपति पर समय-सीमा के निर्देश पर आपत्ति उठाई। इन सबकी दलील है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु वाले फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत कामकाज के निष्पादन में राष्ट्रपति के पास कोई ‘पॉकेट वीटो’ या ‘पूर्ण वीटो’ उपलब्ध नहीं है। संवैधानिक योजना किसी भी तरह से यह प्रावधान नहीं करती है कि कोई संवैधानिक प्राधिकारी संविधान के तहत अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अदालत अनुच्छेद 201 की मूल भावना और सरकारिया तथा पंछी आयोगों की रिपोर्टों के साथ-साथ गृह मंत्रालय के 04 फरवरी 2016 के मानक प्रक्रिया ज्ञापन के मुताबिक निर्धारित करती है कि राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना जरूरी है। इस अवधि से अधिक किसी भी देरी के मामले में, उचित कारण दर्ज करने होंगे और संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। अदालत इन्हीं प्रवधानों के तहत राज्यपाल के लिए एक महीने से तीन महीने की अधिकतम अवधि तय की (देखें बॉक्स, तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल)।
तमिलनाडु राज्य विधानसभा से पारित 12 विधेयक 13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2023 के बीच राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजे गए थे। मौजूदा राज्यपाल आर.एन. रवि ने 18 नवंबर 2021 को कार्यभार संभाला, लेकिन उन्होंने अक्टूबर 2023 तक किसी भी विधेयक पर जरूरी कार्रवाई नहीं की। राज्यपाल की इस निष्क्रियता के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने रिट याचिका दायर की। अदालत ने 10 नवंबर 2023 को नोटिस जारी किया तो राज्यपाल ने 13 नवंबर को 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए रोक लिया। राज्यपाल की दलील थी कि विधानसभा से दोबारा पास हुए ये विधेयक संघीय सूची के मामलों के विपरीत हैं।
गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों के रवैयों और प्रतिकूल विधोयकों को रोके रखने की शिकायतें 2014 के बाद से ही आम रही हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र से इसकी शिकायतें लगातार आती रही हैं। महाराष्ट्र में उद्घव ठाकरे सरकार को विश्वास मत प्रकट करने के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारी के आदेश को तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी.के. चंद्रचूड़ की अगुआई वाले खंडपीठ ने गैर-संवैधानिक ही बताया था। बंगाल में मौजूदा उपराष्ट्रपति धनखड़ जब राज्यपाल थे तो ममता बनर्जी सरकार के साथ लगातार उनके टकराव की खबरें आम थीं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि “धनखड़ की टिप्पणियां बेहद आपत्तिजनक और अवमानना की सीमा पर हैं। संवैधानिक पद पर होने के नाते उनसे अन्य संवैधानिक संस्थानों और पदों को बनाए रखने और उनका सम्मान करने की उम्मीद की जाती है। उपराष्ट्रपति ने बार-बार सुप्रीम कोर्ट के प्रति उपेक्षा दिखाई है, जो बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति है।” द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने भी धनखड़ की टिप्पणियों को अनैतिक और “अवमानना” बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्थापित कर दिया है कि विधानसभा से पारित विधेयकों को कोई भी अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकता है।”
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा कि “यह सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज करने और संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश है, जिसे हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। धनखड़ साहब और निशिकांत दुबे के बयानों से हमारी आशंका सही साबित होती है कि इनकी मंशा संविधान बदलने की है। इसके खिलाफ इंडिया ब्लॉक एकजुट है।”
दरअसल राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय-सीमा बांधने से भी ज्यादा भाजपा नेताओं और संघ परिवार को वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तीन बिंदुओं पर अंतरिम रोक से परेशानी हो सकती है (देखें बॉक्स, अंतरिम आदेश)। गौरतलब है कि इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ साल पूरे हो रहे हैं। सो, केंद्र सरकार की कोशिश उसके मूल एजेंडों में एक और मामले को पूरा करने की हो सकती है। संघ और भाजपा के भी घोषणा-पत्रों में तीन मूल एजेंड़ा में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा तो पूरा हो चुका है, उसमें सिर्फ समान नागरिक संहिता का मामला बचा है। उसके लिए संविधान संशोधन की दरकार है, जो संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई संख्या की दरकार है, जो अभी एनडीए के पास नहीं है। लेकिन उसमें भी तीन तलाक पर रोक के जरिए एक हद तक वादा पूरा किया जा सका है।
इसीसे जुड़ा वक्फ का भी मामला है। वक्फ संपत्तियों की जमीन को लेकर लंबे समय से संघ परिवार के हलकों में काफी चर्चाएं हैं। सरकार की ओर से भी यही कहा गया है कि रेलवे और रक्षा क्षेत्र के अलावा वक्फ के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है और उसमें कई विवाद भी हैं। कुछ विपक्षी नेताओं की मानें तो वक्फ का मसला संघ परिवार के लिए इसलिए भी अहम है कि पुरानी मस्जिदों-मजारों वगैरह को विवादास्पद घोषित किया जा सके तो शायद इस तरीके से भी 1993 के उपासना स्थल अधिनियम के तहत रोक से भी निजात पाई जा सकती है। असल में उपासना स्थल कानून को भी संघ परिवार से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। ये कयास हैं लेकिन सरकार का कहना है कि वक्फ का प्रबंधन अगर ठीक ढंग से हो तो गरीब पासमांदा मुसलमानों को, प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, “पंक्चर लगाने जैसे छोटे-मोटे काम से आगे विकास का रास्ता खुल सकेगा।” सरकार का दावा है कि इससे मुस्लिम औरतों को भी राहत मिल सकेगी।
दावे तो ठीक हैं लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पर सुनवाई के पहले दिन ही प्रधान न्यायाधीश ने सवाल किए कि 12वीं, 13वीं, 14वीं सदी की वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज भला कहां से मिलेंगे या वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति का क्या मतलब है। ऐसे ही कई सवालों पर अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता कोई ठोस जवाब नहीं दे सके थे। उन्होंने कहा कि लाखों शिकायतों के आधार पर यह संशोधन लाया गया है तो अदालत ने पूछ लिया कि वे दस्तावेज कहां है। इस पर मेहता हफ्ते भर की मोहलत मांगने लगे। अगले दिन भी मेहता कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए तो अदालत ने तीन बिंदुओं पर रोक लगाकर या यथास्थिति कायम रखने का उनसे वादा लेकर अगली सुनवाई की तारीख 5 मई को मुकर्रर कर दी।
यही नहीं, वक्फ संशोधन कानून में एक और मामले को गैर-संवैधानिक या संविधान की मूल भावना के विरुद्घ बताया जा रहा है। और वह यह है कि वक्फ करने का अधिकार पांच साल तक इस्लाम का पालन करने वाले को ही हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका इसी मामले में है। वे पूछती हैं, “अगर मैं अपनी संपत्ति किसी इस्लामी संस्था को दान देना चाहूं तो कोई कानून मेरे इस मौलिक अधिकार को कैसे रोक सकता है। फिर कौन तय करेगा कि पांच साल तक इस्लाम का पालन कोई कैसे करे।” यही नहीं, आपत्ति जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों पर फैसला करने के अधिकार पर भी है। सरकार कहती है कि इस कानून का मजहब से कोई लेनादेना नहीं है, जबकि वक्फ तो अल्लाह के नाम से ही किया जाता है। जो ऐसी अनेक याचिकाएं, शायद पचासेक, अदालत में हैं, इसीलिए अदालत ने पांच मुद्दे तय किए हैं, जिस पर बहस और सुनवाई होनी है।
इस विवाद का असर बेशक सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ा दिखता है। 21 अप्रैल को कम से कम दो मामलों की सुनवाई कर रही अलग-अलग पीठों ने टिप्पणियां कीं कि केंद्र सरकार को निर्देश देने की याचिकाओं की प्रति सरकार को भी सौंपे, क्योंकि हम पर कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं। मुर्शीदाबाद हिंसा से संबंधित याचिका लेकर पहुंचने वाले वकील विष्णु शंकर जैन से तो न्यायाधीश गवई ने कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि “आपके नाम में तो विष्णु और शंकर दोनों लगा है, तीसरा नेत्र खोलिए आपको सब दिख जाएगा।” मुर्शीदाबाद हिंसा को लेकर भी अलग-अलग आरोप उछल रहे हैं (देखें बॉक्स, मुर्शीदाबाद की लपटें)।
बहरहाल, यह विवाद वाकई देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है। संविधान विशेषज्ञ इस राय के हैं कि सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार की व्यवस्था इसी मकसद से है कि कार्यपलिका या विधायिका बहुमत के दम पर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला कोई कानून या नीति न बना पाए। वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े का कहना है, “शीर्ष अदालत अनेक बार अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकार का प्रयोग करके फैसले सुना चुका है। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला भी तो विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके दिया था। अगर अनुकूल फैसले आए तो ठीक लेकिन प्रतिकूल हो जाए तो विरोध का क्या मतलब है। इससे तो मंशा वाकई संवैधानिक दायरे से बाहर जाने की लगती है।’’ अब देखना है आगे यह टकराव क्या शक्ल लेता है।
वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम आदेश

शीर्ष अदालत ने वक्फ (संशोधन) कानून 2025 पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई, मगर तीन बिंदुओं पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया और सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन और विरोधी याचिकाकर्ताओं को पांच दिन की मोहलत दी। अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। तब तक:
. किसी वक्फ संपत्ति में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा, सभी वक्फ संपत्तियों में यथास्थिति कायम रहेगी, चाहे वे जिस रूप में वर्गीकृत हों
. ‘वक्फ बाइ यूजर’ की प्रथा के तहत पंजीकृत या घोषित संपत्ति भी यथावत रहेगी
. राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, उनकी स्थिति भी यथावत रहेगी
तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामला

मुख्यमंत्री स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के इसी फैसले पर सबसे ज्यादा विवाद भड़का
. अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास कोई 'पॉकेट वीटो' या 'पूर्ण वीटो' उपलब्ध नहीं है
. सरकारिया तथा पंछी आयोगों की रिपोर्टों और गृह मंत्रालय के 4 फरवरी 2016 के मानक ज्ञापन के मुताबिक राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे विधेयकों पर तीन महीने के भीतर फैसला करना आवश्यक है
. राज्यपाल किसी विधेयक पर मंजूरी देने में गुरेज या राष्ट्रपति के विचार के लिए रोकता है तो राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से अधिकतम एक महीने के भीतर लौटाए
. राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत मंजूरी न देने की स्थिति में राज्यपाल को अधिकतम तीन महीने के भीतर विधेयक को अपनी आपत्ति के साथ वापस करना होगा
. राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को रोक लेने की स्थिति में राज्यपाल को अधिकतम तीन महीने के भीतर ऐसा करना होगा
. विधानसभा में पुनर्विचार के बाद विधेयक प्रस्तुत करने की स्थिति में राज्यपाल को अधिकतम एक महीने में मंजूरी देना होगा
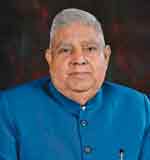
“सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 न्यूक्लीयर मिसाइल है। सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बन गया है”
जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति

“सीजेआइ की वजह से गृह युद्घ जैसी स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाए तो संसद की क्या दरकार है”
निशिकांत दुबे, भाजपा सांसद
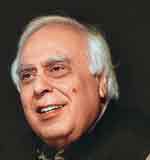
“हमारे लोकतंत्र में कोई पद नहीं, संविधान सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने ताकत दी है”
कपिल सिब्बल, वरिष्ठ वकील, राज्यसभा सदस्य

“पद नहीं, संवैधानिक दायित्व बड़ा है। राज्यपाल के मामले में गृह मंत्रालय का ज्ञापन समय तय करता है”
कुरियन जोसफ, पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट

“यह सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज करने की कोशिश है। साफ है कि इनकी मंशा संविधान बदलने की है”
मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष