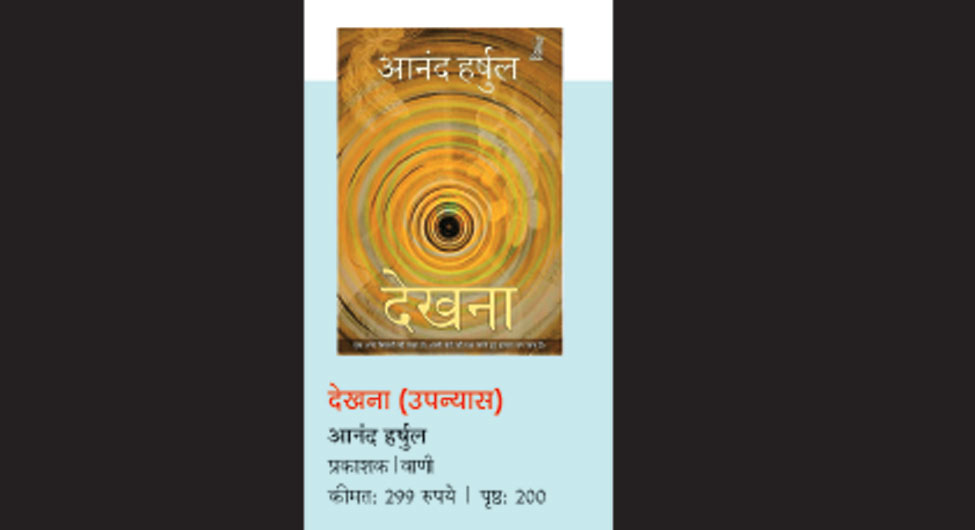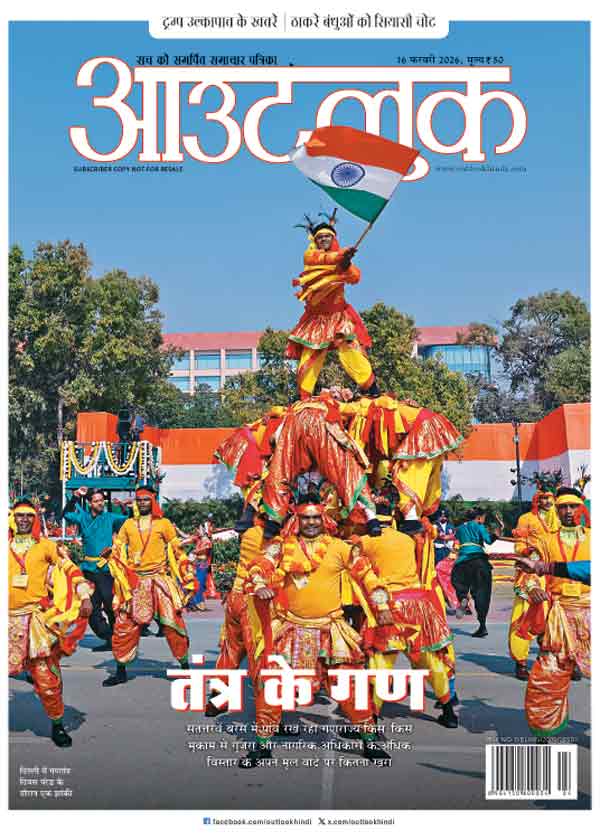रेलवे स्टेशन पर जीवन यापन करने वाले भिखारियों के जीवन पर आधारित इस उपन्यास का मुख्य पात्र एक अंधा व्यक्ति है। यहां अंधे बच्चे के अंधे होने की विडंबना का विवरण है, अंधेरे का रोशनी से संघर्ष है। अंधे बच्चे का यह पूछना है कि सूरज क्या होता है और अंत में यह पहचानने लगना कि कौन से पक्षी के उड़ने की आवाज कैसी होती है।
आनंद हर्षुल की कहानियां पढ़ते हुए देखा जा सकता है कि वह गरीबों को अपनी रचनाओं में प्रमुख स्थान देते हैं। यह किताब भी गरीबी को भीतरी तह तक जाकर देखती है। लेखक ने बड़ी कुशलता से गरीबी, रेल और भीख की जुगलबंदी को लिखा है। इसे इन पंक्तियों से समझा जा सकता है, ‘‘कई बार जनरल डिब्बे की भीड़ को देखकर लगता था कि यह पूरी भीड़ भी कहीं भीख मांगने जा रही है। यह भीड़ भिखारियों से बस थोड़ी ही ऊपर थी। बस इतनी कि भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि मेहनत-मजदूरी कर कमा-धमा रही थी। मजदूरी न मिले और भूख इतनी जग जाए कि असहनीय हो जाए तो यह भीड़ कभी भी भीख की ओर फिसल सकती थी।’’
बाल मनोविज्ञान का विश्लेषण भी इस पुस्तक में बहुत बारीकी से किया गया है। मुख्य पात्र के अतिरिक्त गंजेड़ी गोविंद का किरदार और बचपन से वृद्धावस्था तक की उसकी यात्रा भी बहुत रोचक है। इसके अलावा इस किताब में एक प्रेमकथा है, एक काली लड़की और एक अंधे भिखारी के प्रेम विवाह और साहचर्य की कथा। उनके बीच प्रथम प्रणय की घटना को बहुत सुंदरता से लिखा गया है जिसके फलस्वरूप यह केवल एक अक्षम व्यक्ति का प्रणय नहीं रह गया है।
यह कितनी मार्मिक बात है कि भिखारियों को भीख में मिलने वाला भोजन, उस भोजन से अच्छा होता है, जो स्कूल में दोपहर को सरकार की योजना से मुहैया होता है। उपन्यास की यह एक पंक्ति सरकारी योजनाओं की पोल खोल देती है।
कोरोना काल का बड़ा सजीव चित्रण लेखक ने किया है। उस समय जब समर्थ व्यक्ति भी सीमाओं में बंधे हुए थे, नौकरीशुदा लोग अपने रोजगार खो रहे थे; ऐसे में भिखारियों पर क्या गुजरी होगी? इस प्रश्न का विस्तृत जवाब इस पुस्तक में मिलता है। यहां पुस्तक के परिवेश को देखते हुए यह बात रेखांकित करने योग्य है कि शहर और रेलवे स्टेशन के भिखारी अलग-अलग होते हैं और अलग-अलग होती हैं उनकी रिरियाहटें। लेकिन एक जैसी होती है अपने बच्चों को पढ़ा सकने की उनकी आकांक्षा, उन्हें सुरक्षित रख पाने की जद्दोजहद।
यह उपन्यास कोरोना काल में सरकार की थाली बजवाने, टार्च जलवाने जैसी घोषणा पर भी उंगली उठता है कि कैसे इस तरह की घोषणाएं लोगों की तकलीफ का मजाक बना देती हैं और सरकार की व्यवस्थागत उन कमियों को छुपा लेती हैं, जिसका परिणाम हजारों लोगों की मौत के रूप में सामने आता है। पुस्तक के आवरण पर ही यह पता चल जाता है कि यह एक अंधे भिखारी की कथा है जो अपनी बेटी की रक्षा करते हुए हत्यारा बन जाता है। इस घटना से आगे यह जेल की कथा बन जाती है। जेल में भी कैदियों और कर्मचारियों में कुछ मानवता बची रह गई है जो अंधे कैदी से अच्छा व्यवहार करते हैं।
स्टेशन पर भिखारी और जेल में कैदी दोनों ही अंधेरों में जीते हुए जीव हैं। जीवन की मुख्यधारा से कटे हुए सड़ांध और अनिश्चय में जीते हुए मनुष्य, भले ही उनकी आंखें देख पाती हों या नहीं। उनके जीवन और परिस्थितियों को वैचारिक और तार्किक कसौटियों पर यह पुस्तक परखती है। इस पुस्तक को पढ़ना भारत के सबसे गरीब और तथाकथित अभागे लोगों के जीवन दर्शन से रूबरू होना है।
देखना (उपन्यास)
आनंद हर्षुल
प्रकाशक|वाणी
कीमतः 299 रुपये | पृष्ठः 200