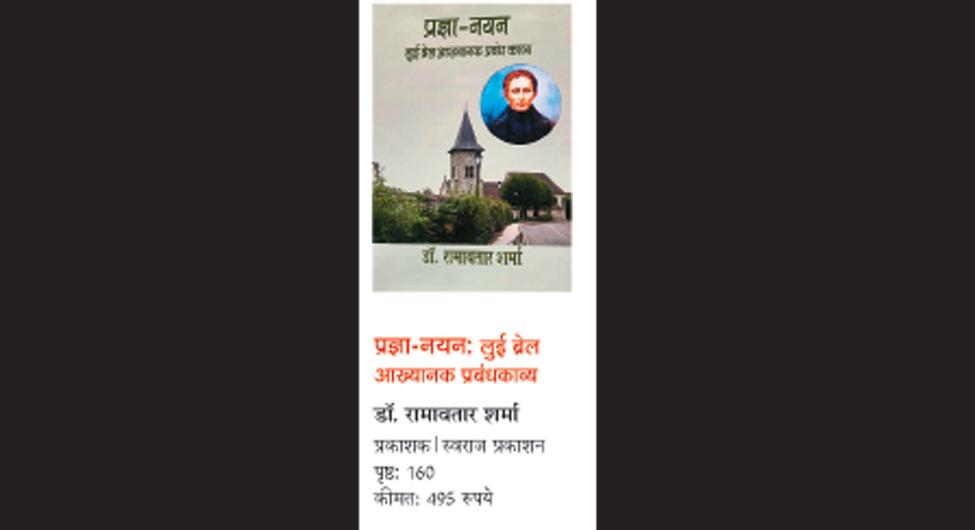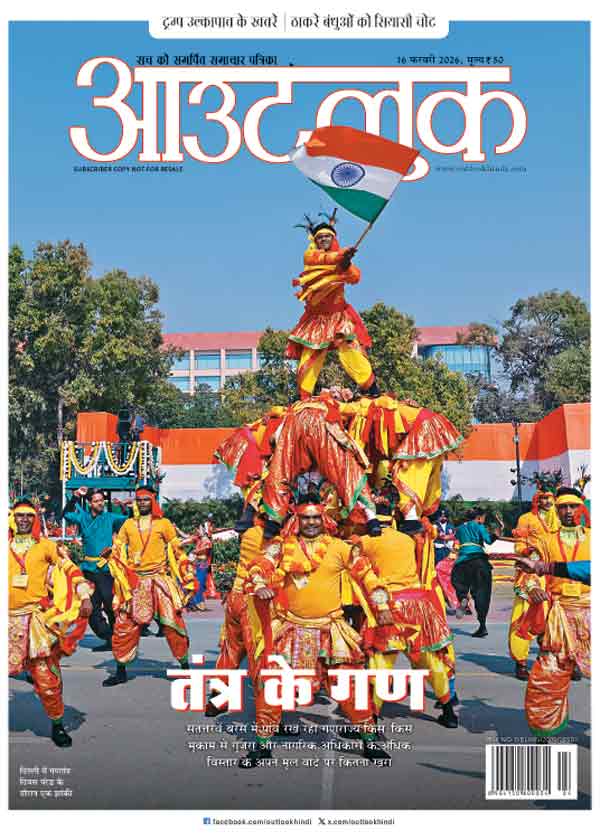शायद यह पहली बार है कि विश्व की किसी भाषा में ब्रेल-लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल के जीवन और महान अवदान पर आख्यानात्मक प्रबंध-काव्य की रचना की गई है। ‘प्रज्ञा-नयन: लुई ब्रेल आख्यानक प्रबंध काव्य’ की रचना एक घटना कही जा सकती है। यह काव्य-कृति एक नेत्रहीन लेखक की दुनिया के समस्त नेत्रहीनों के मसीहा, जो स्वयं नेत्रहीन थे, के प्रति कृतज्ञतापूर्ण भावांजलि है। इस काव्य-कृति को इसी रूप में पढ़ा जाना मुनासिब है।
इसके रचयिता रामावतार शर्मा ने लुई ब्रेल को ‘समर्पण’ में लिखा है, “दृष्टिहीन जग के अवतार,/हे मनुज लुई तुम अति उदार।/सदियों से बंद ज्ञान के द्वार/उगा तर्जनी पर अक्षर संसार/ दे ऊसर भू को जलधार,/भिगोया दृष्टिहीन संसार/नाव तो अब भी है मझधार/चलाओ खुद अपनी पतवार/समर्पण यह लघु सेवा-सार/काव्यजल की सीकर सुकुमार/सहज शिशु भोला मन का प्यार/इसे कर लो लुई अंगीकार।” यह समर्पण बताता है कि दुनिया के नेत्रहीनों के लिए लुई ब्रेल परम श्रद्धेय ही नहीं, उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, जिसे सनेत्र मनुष्य देख नहीं पाते हैं।
भाषा और शैली द्विवेदी युग और छायावाद युग के संधि-स्थल की है। पूरी काव्य-कृति इसी भाषा और शैली में लिखी गई है। आधुनिक हिंदी साहित्य की विकास-यात्रा में छायावाद के बाद सर्ग-बद्ध प्रबंध-काव्य (महाकाव्य-खंडकाव्य) लिखने की परंपरा समाप्त हो जाती है। आधुनिक भाव-बोध अभिव्यक्ति की नई भाषा और शिल्प-विधान खोज लेता है। लेकिन रामावतार शर्मा अभी पुराने अंदाज में ही अपनी कविताएं, गीत और गजल लिखते हैं। ‘प्रज्ञा-नयन’ आठ सर्गों में विभक्त है – ‘प्रथम प्रकाश किरण’, ‘उर्वर बीज’, ‘अंकुर एवं पल्लवन’, ‘क्यारी’, ‘वाटिका’, ‘फुलवारी’, ‘उपवन’, और ‘बसंत और पतझड़’। प्रत्येक सर्ग का छंद-विधान अलग है। गेयता रामावतार शर्मा के काव्य-कर्म का विशिष्ट गुण रहा है जो ‘प्रज्ञा-नयन’ में भी है। आधुनिक काव्य-आस्वाद के पाठकों को भी आनंद आएगा।
कवि ने माना है कि 40 साल पहले उनके मन में लुई ब्रेल महान पर काव्य-रचना की बात आई थी। लेकिन बड़े कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए समुचित कथानक उनके पास नहीं था। डॉ. वेदप्रकाश वर्मा की पुस्तक ‘लुई ब्रेल का जीवन तथा क्रांतिकारी आविष्कार’ से उन्हें कथानक-रचना का आधार मिल गया। यह काव्य-कृति केवल लुई ब्रेल के जीवन और जीवन-संघर्ष से ही पाठकों का परिचय नहीं कराती, इसमें ब्रेल-लिपि के आविष्कार की महान घटना के पहले के इतिहास-पथ का भी वर्णन किया गया है। इसमें उन शख्सियतों के महत्वपूर्ण प्रयासों का भी स्मरण किया गया है, जिससे यह सफर मुकाम पर पहुंचा। मसलन, डैनिस दिदरो, जिन्होंने 21 साल के कठिन तप से 35 खंडों का विश्वकोश तैयार किया था, और वालोंतन ओए, जिन्होंने पेरिस में अपने घर को ही पहला अंध-विद्यालय बनाया, वियना से फ्रांस आने वाली संगीतज्ञ मारी थैरेसिया वो पाराधी, जो सामान्य लिपि के उभरे अक्षरों से बखूबी पढ़ना-लिखना जानती थीं और जिनके पास उनके एक यंत्रकार मित्र द्वारा बनाया गया यंत्र था जिसमें लगी सुइयों से मोटे कागज पर पूरी वर्णमाला उभारी जा सकती थी। साथ ही, उस दौर के यूरोपीय, खासकर फ्रांस के महान चिंतकों और वैज्ञानिकों का भी स्मरण किया गया है जिन्होंने मानववाद की स्थापना की दिशा में महती भूमिका निभाई। इस तरह से कवि ने लुई ब्रेल के युग को भी आत्मसात करने की कोशिश की है। कहने का आशय यह है कि इस काव्य-कृति ने लुई ब्रेल और उनके आविष्कार को चमत्कार के रूप में नहीं, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा है।
बचपन में ही आंखों की ज्योति गंवा बैठे लुई ब्रेल की जीवन-यात्रा पैतृक गांव कूरे से लेकर पेरिस तक कठिनाइयों से भरी रही, जहां उन्होंने अध्ययन, अध्यापन और आविष्कार किया। उन्हें उम्र (4 जनवरी 1809 - 6 जनवरी 1852) भी कम मिली। उन्होंने लंबे प्रयत्न के बाद ब्रेल-लिपि का आविष्कार किया। हालांकि, उनके अपने विद्यालय में ही ब्रेल-लिपि का प्रयोग रोक दिया गया। इस बीच उन्हें क्षय रोग हो चुका था। इन समस्त बाधाओं के बावजूद वे जीवन के हर पड़ाव पर अपने कर्म-पथ पर अडिग रहे और कभी निराशावादी नहीं हुए। अनीश्वरवादी चिंतकों—वैज्ञानिकों के उस दौर में लुई अंत तक ईश्वरवादी बने रहे। जीवन के अंतिम दिनों में वे जैसे एक शांत दार्शनिक हो गए थे।
रामावतार शर्मा ने लुई की इस जीवन-यात्रा को उनके जीवन में आए कई अंतरंग पात्रों और प्रसंगों के साथ कविता में गूंथा है। साहित्यिक गुणवत्ता की चर्चा अलग है, कृति के कथ्य यानी लुई ब्रेल की साधना और मानवता को दिए अवदान के प्रति कवि की निष्ठा में कोई कमी नहीं है। यह पुस्तक ब्रेल-लिपि में यथाशीघ्र प्रकाशित होगी तो लुई के प्रति श्रद्धा रखने वाले अनेक नेत्रहीन पाठकों तक पहुंच पाएगी। यह भारत और विश्व की अन्य भाषाओं में भी अनूदित होकर ब्रेल-लिपि में प्रकाशित हो सके तो आगे कई रचनात्मक कृतियां संभव हो सकती हैं। यहां यह उल्लेख करना अवांतर नही कहलाएगा कि रामावतार शर्मा की पत्नी विदुषी कुसुमलता मलिक ने लुई ब्रेल के जीवन-संघर्ष पर आधारित ‘लुई की सुई’ शीर्षक नाटक लिखा है। दोनों कृतियां आगे-पीछे आई हैं।
प्रज्ञा-नयन: लुई ब्रेल आख्यानक प्रबंधकाव्य
डॉ. रामावतार शर्मा
प्रकाशक|स्वराज
पृष्ठ: 160
कीमतः 495 रुपये