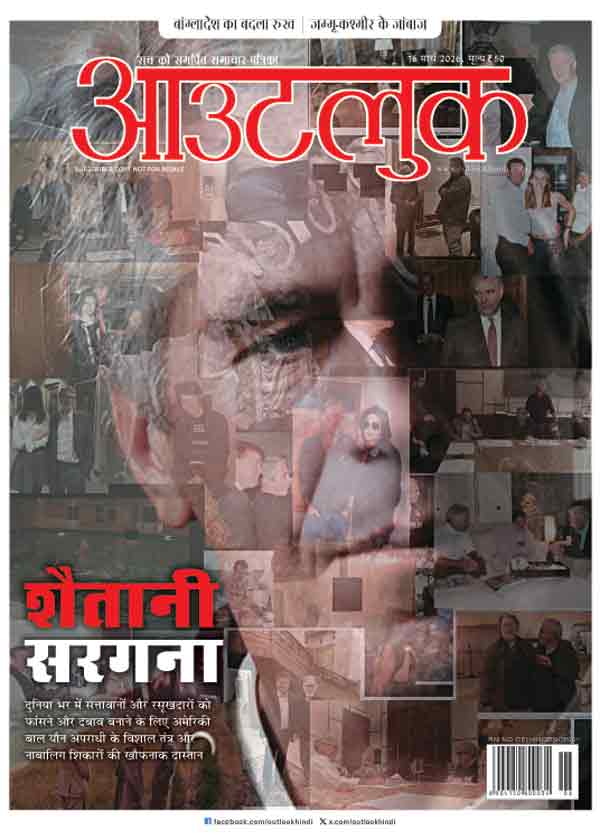30 लाख रुपये की रॉयल्टी की खबर को कैसे देखते हैं?
पूरा प्रसंग हिंदी प्रकाशन जगत के लिए उत्साहजनक है, भले ही लोगों को इसमें थोड़ा नाटकीयता का तत्व दिखे। एक समय था जब हिंदी किताबों की लाखों प्रतियां महीने भर में बिक जाया करती थीं। कई पुस्तकों के पहले संस्करण ही दो लाख प्रतियों के होते थे। वह भी उस दौर में, जब प्रचार-प्रसार के साधन आज जितने व्यापक और तेज नहीं थे। उस समय अग्रिम भुगतान और रॉयल्टी की राशि भी उतनी ही आश्चर्यजनक हुआ करती थी। लेकिन पिछले दो-तीन दशकों में किसी किताब ने अपने छपने के वर्षों बाद एकाएक ऐसा प्रदर्शन नहीं किया। इसके पीछे विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य का श्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना तो है ही, प्रकाशक की भूमिका भी महत्वपूर्ण जरूर होगी।
हिंदी प्रकाशन में पारदर्शिता की दिशा में नया मोड़ साबित हो सकता है?
मुझे यह प्रसंग पारदर्शिता का नहीं, बल्कि प्रदर्शन का लगता है। मुझे नहीं लगता कि अधिकांश लेखक अपनी रॉयल्टी का इस तरह सार्वजनिक प्रदर्शन पसंद करेंगे। छिटपुट विवादों को छोड़कर रॉयल्टी का परिदृश्य पारदर्शी ही है। पहले जब सामग्री डिजिटल नहीं थी, तो संदेह और गलतफहमी की गुंजाइश ज्यादा थी। आज हर प्रक्रिया- प्रिंटर को मेल करने, भुगतान करने, जीएसटी चुकाने, स्टॉक दर्ज करने से लेकर बिलिंग तक सब कुछ डिजिटल है। ऐसे में किसी भी तरह की गलती या गड़बड़ी पूरे डेटा और अकाउंट को उलझा सकती है। छोटे प्रकाशक शायद कर भी लें पर सैकड़ों किताबों वाले प्रकाशक यह नहीं कर सकते।
कई लेखक आरोप लगाते हैं कि प्रकाशक उनकी किताबें री-प्रिंट या पेपरबैक के नाम पर बिना जानकारी दिए छापते रहते हैं?
यह आरोप नहीं, बल्कि जरूरी बहस है। इससे अंततः प्रकाशन और लेखन जगत का ही भला होगा। आम तौर पर अनुबंध में स्पष्ट लिखा होता है कि किसी किताब के री-प्रिंट या नए संस्करण के अधिकार किस तरह से होंगे। कुछ अनुबंधों में प्रकाशक एक्सक्लूसिव राइट ले लेते हैं, तो कुछ में ‘री-प्रिंट क्लॉज’ अलग से दर्ज होता है। सामान्यतः अनुबंध में री-प्रिंट के लिए लेखक की सहमति आवश्यक होती है। ऐसे में प्रकाशक बिना सूचना दिए री-प्रिंट नहीं कर सकता। अनुबंध को लेखक और प्रकाशक-दोनों के लिए गंभीरता से लेना जरूरी है।
हिंदी में रॉयल्टी का कोई मानक क्यों नहीं है, जबकि अंग्रेजी में यह काफी स्पष्ट है?
मुझे ऐसा नहीं लगता। हिंदी के प्रतिष्ठित प्रकाशक भी अब अंग्रेजी प्रकाशन जगत के समान मानकों का पालन करते हैं। आम तौर पर रॉयल्टी का बैंड 8-10 फीसदी के बीच होता है। अंग्रेजी प्रकाशन जगत में यह इसलिए अधिक स्पष्ट दिखते हैं क्योंकि उसका बाजार वैश्विक है, नेटवर्क और डेटा-एक्सेस वहां बहुत पहले से स्थापित है। वहीं भारतीय भाषाओं का मार्केट अपेक्षाकृत छोटा, बिखरा हुआ और अव्यवस्थित रहा है, लेकिन अब यह तेजी से बदल रहा है।
क्या ई-बुक्स और ऑडियो-बुक्स की बिक्री का हिस्सा भी रॉयल्टी में शामिल होता है? यदि हां, तो किस अनुपात में?
हां, ई-बुक्स और ऑडियो बुक दोनों का रेवेन्यू रॉयल्टी में शामिल होता है, पर प्रतिशत और कैलकुलेशन प्लेटफॉर्म-विशेष के अनुबंध पर निर्भर करता है। हम जब रॉयल्टी स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसमें ई-बुक और ऑडियो बुक जैसे डिजिटल फॉर्मेट से होने वाली आय को समझने में आसानी के लिए अलग दिखाते हैं। यानी लेखकों को यह स्पष्ट तौर पर बताया जाता है कि किताब के डिजिटल फॉर्मेट से कितनी आय हुई और उस पर रॉयल्टी किस आधार पर लागू हुई। सामान्यतः ई-बुक में प्लेटफॉर्म के हिसाब से 25 प्रतिशत तक और ऑडियो में यह प्लेटफॉर्म और डिस्ट्रिब्यूशन के तौर-तरीके से 25 से 50 प्रतिशत के दायरे में होता है। यह हर अनुबंध में स्पष्ट तौर पर लिखा होता है। हम इस फॉर्मेट पर भी जोर देते हैं इसलिए पहले से ही सभी डिजिटल पॉइंट क्लियर रखते हैं।
हिंदी-अंग्रेजी लेखकों के बीच असमानता के क्या कारण देखते हैं?
अंग्रेजी किताबों का बाजार वैश्विक है। इसलिए बड़े प्रकाशक और रिटेलर वैश्विक स्तर पर निवेश करते हैं, जिससे अग्रिम भुगतान और बड़ी रॉयल्टी संभव हो पाते हैं। अंग्रेजी किताबों को वैश्विक वितरण, संस्थागत बाजार और कॉरपोरेट खरीदारों तक पहुंच मिलती है। इससे किताबों पर जोखिम कम और संभावित लाभ अधिक हो जाता है। इसके विपरीत, हिंदी का बाजार क्षेत्रीय है और बिक्री के विकल्प अपेक्षाकृत सीमित रहते हैं। इस मामले में दोनों भाषाओं और उनके मार्केट की तुलना शायद सही नहीं होगा।
हिंदी साहित्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रकाशकों और लेखकों को किन नीतिगत बदलावों की जरूरत है?
साहित्य और भाषा की आर्थिक स्थिति तब मजबूत होती है जब उसे बोलने वाला समाज मजबूत हो। दुनिया भर की नजरें तब उस तरफ होती हैं जब उस भाषा का बाजार बढ़ता है। इस तरह यह सिर्फ लेखकों-प्रकाशकों का मामला नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ा नीतिगत प्रश्न है। मसलन, पिछले दिनों जीएसटी में बदलाव हुआ तो कागज पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। अब सोचिए, इससे किताबें महंगी होंगी। प्रकाशक तथा लेखक इससे कैसे निबटेंगे?
साहित्य में भरोसे और ईमानदारी के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं?
हम लेखकों के लिए एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, जहां वे कभी भी अपनी किताबों का प्रामाणिक डेटा देख सकेंगे। शुरुआत में हम एक महीने पर अपडेट करेंगे, फिर धीरे-धीरे रियल-टाइम अपडेट पर ले आएंगे। हमें लगता है यह कारगर शुरुआत है।