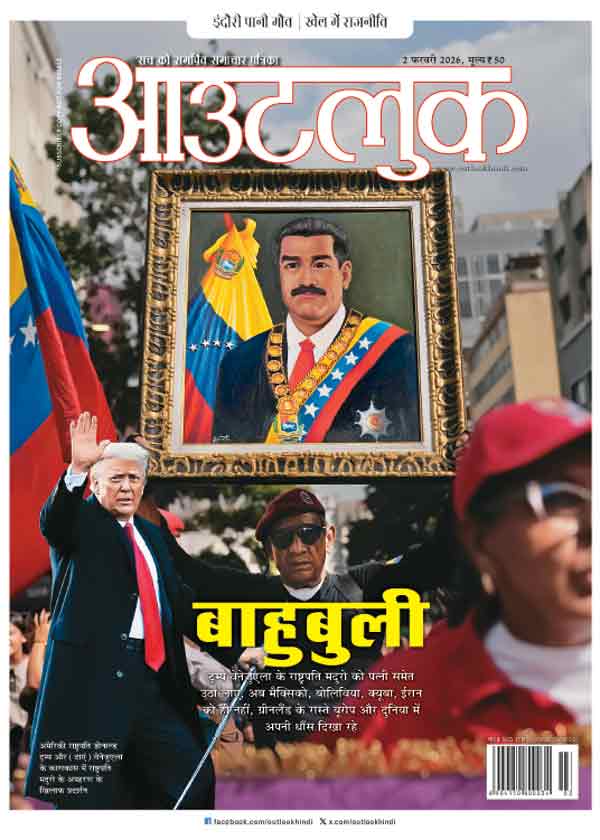हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए कुछ साल पहले मुझे किसी ने सलाह दी थी कि मैं श्रीलाल शुक्ल के जासूसी नॉवेल पर फिल्म बनाऊं। राग दरबारी की लोकप्रियता से पहले उन्होंने पल्प फिक्शन में हाथ आजमाया था। मैंने उनका नॉवेल आदमी का जहर पढ़ा, तो मुझे लगा कि यह एक बाकमाल सस्पेंस थ्रिलर हो सकता है। लेकिन समस्या यह आई कि दौर बदल चुका है और जासूसी के टूल्स भी बदल गए हैं। यह तब की कथा है, जब सीसीटीवी कैमरों का कोई अस्तित्व नहीं था। समय के साथ नई तकनीकें आती हैं और उन तकनीकों के साथ समाज बदलता है। इसलिए सिनेमा भी अगर अपने समय की कहानी कह रहा हो, तो वह बदलेगा। आजादी के पहले का सिनेमा आजादी के बाद के सिनेमा से अलग था। पचास और साठ के दशक का सिनेमा सत्तर और अस्सी के दशक से अलग था। नब्बे के दशक और 2000 के बाद हिंदुस्तानी सिनेमा ने जो लीक बदली, वह पहले के तमाम दशकों के मुकाबले एक अलग ही लीक है।
बहुत पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि मैं हर दशक का एक सिनेमा चुन लूं और सिनेमा के इर्द-गिर्द भारतीय समाज की सामाजिक-राजनैतिक कथा कहूं। जाहिर है, यह केवल आइडिया भर ही रह गया और इस पर मैं काम नहीं कर पाया। बहरहाल, जब कोई भी बाजार विकसित होता है, तो एक मिथक भी उसके साथ जोर पकड़ता है। जैसे अगर मैं कहानी लेकर प्रोड्यूसरों के पास घूम जाऊं, तो ज्यादातर प्रोड्यूसरों की पहली शंका होती है कि यह विषय चलेगा या नहीं, लोग पसंद करते हैं या नहीं, इस तरह की फिल्म हिट होती है या नहीं। ऐसी तमाम ऊहापोह के बीच पीपली लाइव जैसी फिल्म आती है और हिट हो जाती है। प्रोड्यूसर पीपली लाइव की गली में घुस जाना चाहते हैं जबकि उन्हें इस पर यकीन करना चाहिए कि विषय एकदम नया और मनोरंजक हो, तभी उसके लोकप्रिय होने की संभावना होती है। और हर फिल्म रिलीज से पहले एक संभावना भर होती है।
मेरा अपना अनुभव है, जब मैं अनारकली... की स्क्रिप्ट लेकर घूम रहा था, तब ज्यादातर कहते थे कि वीमेन सेंट्रिक फिल्में नहीं चलतीं। लेकिन हकीकत यह है कि अपने जमाने में सुजाता भी हिट हुई थी और मदर इंडिया भी, सीता और गीता भी हिट हुई थी और पाकीजा भी। उमराव जान को तो बेशुमार सराहना मिली थी। लेकिन ऐसी तमाम फिल्मों ने भी आज तक फिल्म निर्माताओं को महिलाओं के नायकत्व के मामले में मुतमईन नहीं किया है। पता नहीं, पिछले साल 2017 में कैसी हवा चली कि महिला मुद्दों पर एक के बाद एक फिल्में आईं और ज्यादातर फिल्मों ने हिंदी सिनेमा का झंडा बुलंद किया, जैसे सीक्रेट सुपरस्टार, तुम्हारी सुलु, मॉम, सिमरन, लिप्सटिक अंडर माई बुर्का, अनारकली ऑफ आरा, नाम शबाना, फिल्लौरी, नूर, बेगम जान, हसीना पार्कर, पार्च्ड, मातृ। हम कह सकते हैं कि इन फिल्मों ने यह मिथ तो तोड़ ही दिया कि महिला मुद्दों पर आधारित फिल्मों पर कारोबार के मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि, कारोबार का गणित भी अब पहले की तरह उलझा हुआ नहीं रह गया है। डिजिटल सहित बाकी प्लेटफॉर्म के चलते फिल्में अब विविधरंगी हो रही हैं और पॉपुलरिटी के तमाम पुराने फंडे नाकाम हो रहे हैं।

हमारे समय में फिल्मों में बदलाव की यह शुरुआत अनुराग कश्यप से होती है, जिन्होंने सिनेमा में सामाजिक यथार्थ को मनोरंजक तरीके से एक्सप्लोर किया। उन्होंने छोटे शहर के किरदारों को रजत परदे पर बारीकी से बुना। उनके साथ ही सुभाष कपूर (फंस गए रे ओबामा), दिबाकर बनर्जी (खोसला का घोंसला, ओए लकी लकी ओए), आनंद एल. राय (तनु वेड्स मनु), तिग्मांशु धूलिया (पानसिंह तोमर) जैसे निर्देशकों ने बॉलीवुड सिनेमा की मुख्यधारा पर पुरानी लीक से हटने का दबाव डाला। इन तमाम निर्देशकों की फिल्मों ने अपना नया भूगोल खोजा, जिसमें छोटे शहर-कस्बों के अलावा मुंबई और दिल्ली आई जरूर लेकिन इन महानगरों का वह हिस्सा आया, जिसे हम चमकदार नहीं कह सकते। यही वजह है कि करण जौहर जैसे पारंपरिक दिमाग भी अब नये प्रयोगों को लेकर उत्साहित हो रहे हैं।
मुझे इसकी जो सबसे बड़ी वजह लगती है, वह है दुनिया भर की सूचनाओं और दुनिया भर के सिनेमा तक पहुंच का आसान होना। एक वक्त था, जब पहली दुनिया के देशों के फैशन को तीसरी दुनिया के देशों तक पहुंचने में कई साल लग जाते थे। हमारे यहां ही किसी सुदूर कस्बे में घटी घटनाओं को राजधानी से प्रकाशित होने वाले अखबार तक पहुंचने में एक दो दिन का वक्त लग जाता है। बॉलीवुड में भी बाहर की फिल्मों को कॉपी करने का चलन लंबे अरसे तक रहा। इसके बावजूद हमारा अपना सिनेमा खड़ा हुआ। वी. शांताराम से लेकर गुरुदत्त, कमाल अमरोही, के. आसिफ, राज कपूर, विजय आनंद, बिमल रॉय जैसे निर्देशकों ने भारतीय सिनेमा की जमीन मजबूत की। आज का दर्शक ज्यादा सचेत है और डिजिटल क्रांति ने दुनिया भर के सिनेमा से बॉलीवुड सिनेमा की तुलना दर्शकों के लिए आसान कर दी है। इसलिए फिल्मकार जोखिम उठा रहे हैं और बॉलीवुड की पारंपरिक सरहदें तोड़ रहे हैं।
एक बात की कमी फिर भी रह जाती है। एक फिल्मकार जो दायरा अपने लिए निर्धारित करता है और उसमें उसे सफलता मिल जाती है, तो फिर वह नए दायरे बनाने में संकोच करता है। मैं अक्सर हैरान होता हूं कि जिस स्टीवन स्पीलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई, उसी स्टीवन स्पिलबर्ग ने इंडियाना जोन्स की सीरीज भी बनाई, जुरासिक पार्क भी बनाई। लेकिन हमारे यहां अपने जॉनर (दायरे) से बाहर जाने का साहस फिल्मकारों में क्यों नहीं होता? हालांकि शेखर कपूर जैसे अपवाद भी हैं, जिन्होंने मासूम और मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन जैसी अलग-अलग क्राफ्ट की फिल्म बनाई। लेकिन ज्यादातर लोग अपने को खोलने से बचते हैं। हमारे यहां साइंस फिक्शन को लेकर गहरी उदासीनता है और रामसे ब्रदर्स की टुच्ची हॉरर फिल्मों के बाद डर के साथ खेलना बंद कर दिया गया है। अच्छी बात है कि इधर स्त्री और तुंबाड़ जैसी कुछ अच्छी कोशिशें हुई हैं।
असल बात है, हमारा सिनेमा अपने समाज को अच्छी तरह समझने लगा है। इसकी वजह राज्यों की फिल्म नीतियां भी हैं। विकेंद्रीकरण किसी भी विधा को समृद्ध ही करता है। नई मेधाओं को जब मुख्यधारा से जुड़ने में आसानी होने लगती है, तो मुख्यधारा भी लचीली होने लगती है। कहने को भले बॉलीवुड का सिनेमा हिंदी का सिनेमा था, लेकिन उसने हिंदी भाषी समाज को समझने के मामले में उदारता बरतने में ज्यादा रुचि आज से पहले नहीं दिखाई थी। मेरा साया फिल्म में गाना था, 'बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे'। 1966 में आई इस फिल्म में यूपी के बरेली शहर का जिक्र भर था, लेकिन उस पूरे शहर की कथा को फिल्म तक पहुंचने में पचास साल लग गए। पिछले साल आई थी बरेली की बर्फी। मेरी अपनी फिल्म में बिहार का आरा शहर है, जिसने आजादी से लेकर मजदूर-किसान आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थोड़े दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म पटाखा में राजस्थान का सबसे मौलिक रंग सामने आया है। कुल मिलाकर यह कि जैसे-जैसे हिंदी सिनेमा अपनी जमीन बढ़ाता जाएगा, उसकी चमक भी बढ़ती जाएगी।
(लेखक चर्चित फिल्म अनारकली ऑफ आरा के निर्देशक हैं)