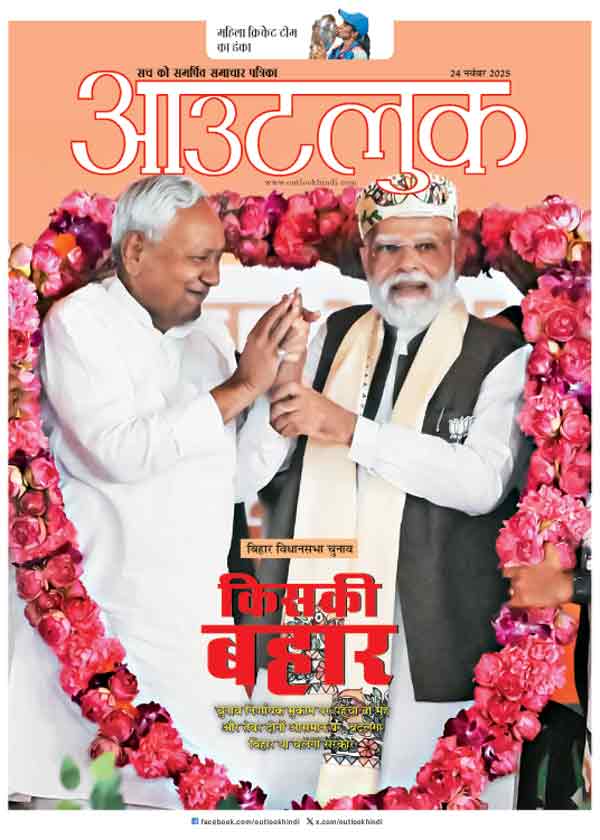कर्नाटक का जनादेश यकीनन इस दौर में अप्रत्याशित और एक मायने में ऐतिहासिक है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नतीजों के दिन देर शाम भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा। वैसे, उनके “अप्रत्याशित” में कुछ और अर्थ-व्यंजना छिपी हो सकती है। दरअसल, इन चुनावों ने शायद 2014 के बाद मुकम्मल तरीके से किसी दल या गठबंधन को एकतरफा जीत देने के जन-रुझान को बदल दिया है। 2014 को विखंडित जनादेश से मुक्ति के लिए ऐतिहासिक कहा जा रहा था। उसके बाद हुए कई विधानसभा चुनावों में भी यही रुझान दिखा था, सिर्फ भाजपा के मायने में ही नहीं, बल्कि बिहार और दिल्ली, पंजाब में दूसरी पार्टियों और गठबंधनों को भी इतनी जीत हासिल हुई कि विपक्ष के कोई मायने ही नहीं रह गए। लेकिन कर्नाटक की जनता ने हर किसी को तवज्जो दी, न किसी को बहुत ज्यादा, न किसी को बहुत कम। यही नहीं, इसमें एक खास कायदा भी दिखा। हर जगह स्थापित पार्टियों और राजनैतिक धाराओं को ही जीत मिली। दो निर्दलीय भी जीते तो वे खास राजनैतिक पार्टियों या धाराओं से ही जुड़े हुए हैं। यानी कर्नाटक के लोगों ने एकतरफा जीत के चलन को बदलकर राजनीति को फिर पुराने या कहें अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थापित कर दिया। इसी मायने में यह ऐतिहासिक है, और कई मामलों में बेहद चौंकाऊ भी।
चौंकाऊ इतना कि इसकी कुछ पहेलियों को सुलझाना राजनैतिक पंडितों और चुनाव विश्लेषकों के लिए भी आसान नहीं रहा। एक पहेली तो यही है कि 38 प्रतिशत वोट हिस्सेदारी पाकर कांग्रेस 78 सीटों पर अटक गई, जबकि 36.2 प्रतिशत वोट लेकर भाजपा 104 सीटों पर पहुंच गई, जो कांग्रेस के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा हैं। सीएसडीएस के निदेशक, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं, “हर पार्टी को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ज्यादा वोट मिले, जो उसके कुल वोट प्रतिशत में दिखता है लेकिन प्रतिकूल प्रभाव वाले या कड़ी टक्कर वाले क्षेत्रों में उसकी हिस्सेदारी घटने से सीटों की संख्या में इतना अंतर दिख सकता है।” मतलब यह हुआ कि प्रदेश के हर क्षेत्र में वोटों का रुझान एक जैसा नहीं रहा। यह भी कि खास समुदायों के इलाकेवार रुझान में भी बदलाव दिख सकता है।
हालांकि, मोटे तौर पर लगता है कि राज्य में 11 प्रतिशत आबादी वाले वोक्कालिगा समुदाय ने अपने बुजुर्ग नेता, जनता दल (सेकुलर) के प्रमुख, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह दूसरे बड़े तबके 12 प्रतिशत आबादी वाले लिंगायत ने भी अपने नेता बी.एस. येदियुरप्पा पर ही भरोसा जताया, जो भाजपा में लौटकर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की तरह लड़े। लिंगायतों की ग्रामीण आबादी ने अपने कुछ पढ़े-लिखे लोगों की उस पहल को शायद खास तवज्जो नहीं दी कि उन्हें अलग अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा देकर आरक्षण मुहैया कराया जाए। इसी वजह से पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में लिंगायतों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाकर वोट हासिल करने की रणनीति शायद काम नहीं आई। इसके अलावा सिद्धरमैया के ओबीसी, दलित और मुस्लिम गठजोड़ का मंत्र अहिंदा भी बड़े पैमाने पर कारगर नहीं हो पाया, वरना उन्हें पुराने मैसूर के अपने क्षेत्र चामुंडेश्वरी में जेडीएस के हाथों करीब 35,000 वोटों से करारी हार नहीं झेलनी पड़ती। वे दूसरी सीट बादामी से भी महज 1600 वोटों से ही जीत पाए। राजनैतिक पंडितों की मानें तो अहिंदा फार्मूला अगर ठोस ढंग से कांग्रेस के लिए काम करता तो उसे भाजपा को गद्दी से दूर रखने के लिए इस कदर जोड़-जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
इसी वजह से यह कयास भी लगाया जा रहा है कि दलित वोटों में भी बंटवारा हुआ है। मायावती की बसपा को 0.3 प्रतिशत वोट और एक सीट मिली। यही नहीं, तटीय और मुंबई कर्नाटक जैसे इलाकों में दलितों के वोट भाजपा की ओर जाने के भी कयास हैं। यानी कर्नाटक ने किसी को न खारिज करके राजनीति को पुराने दौर में पहुंचा दिया है, जिसमें कोई भी एकतरफा सिपहसालार बनने की ताकत नहीं रखता।
इसके अक्स भी नतीजों के बाद सरकार बनाने की जद्दोजहद और अभूतपूर्व नाटकीय घटनाक्रमों के रूप में दिखे, जो फौरन 1996 के आम चुनावों और उसके बाद के दौर की याद ताजा कर गए। यूं तो गठबंधनों की राजनीति का दौर 1967 की गैर-कांग्रेसी राजनीति और साझा सरकारों के गठन से ही शुरू हुआ और फिर 1977 तथा 1989 में जनता पार्टी और जनता दल के प्रयोगों में गठजोड़ की राजनीति कायम हुई, लेकिन 1996 के बाद ऐसा माना जाने लगा था कि गठबंधनों की राजनीति का अब कोई विकल्प नहीं है।
कर्नाटक के इन चुनावों में कूल 222 (दो सीटों पर चुनाव नहीं हुए, विधानसभा में कुल संख्या 224) में भाजपा 104 सीटें हासिल करके सरकार बनाने से वंचित नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उसे सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस पहले ही तैयारी कर चुकी थी। 12 मई के मतदान के अगले दिन कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने जेडीएस के महासचिव के. दानिश अली से बात की। 15 मई को नतीजे के दिन दोपहर बाद जैसे ही यह साफ हुआ कि भाजपा बहुमत से दूर है और कांग्रेस (78), जेडीएस-बसपा (38) को मिलाकर बहुमत हासिल हो रहा है तो कांग्रेस ने फौरन जेडीएस के राज्य अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी। उधर, देवेगौड़ा को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बसपा प्रमुख मायावती और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी जैसे नेताओं के भी फोन गए और इन सबने भाजपा को सत्ता से दूर रखने की अपील की। कुमारस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन जाकर सरकार बनाने के दावे का ऐलान किया।
इससे भाजपा खेमा भी सक्रिय हुआ। भाजपा नेता अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा के साथ राज्यपाल वजुभाई वाला के पास पहुंच गए। शाम को दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम कर्नाटक को विकास के रास्ते से भटकने नहीं देंगे।” अगले दिन 16 मई को जेडीएस और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके विधायकों के खरीद-फरोख्त में जुट गई है। कुमारस्वामी ने कहा, “हरेक विधायक को 100 करोड़ रुपये और मंत्री पद की पेशकश की जा रही है।” फिर कांग्रेस और जेडीएस ने विधायकों को किसी रिसॉर्ट में भेज दिया।
इस बीच कुमारस्वामी ने कांग्रेस और जेडीएस विधायकों के दस्तखत समेत 117 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी राज्यपाल को सौंप दी। जेडीएस के महासचिव दानिश अली कहते हैं, “अगर राज्यपाल हमें नहीं बुलाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।” यानी दोनों तरफ से तैयारी पूरी थी। टीवी चैनलों में कानूनी विशेषज्ञों की राय सुर्खियां बन रही थीं कि राज्यपाल को क्या करना चाहिए। कुछ सबसे बड़ी पार्टी को बुलाने के पक्ष में थे तो कुछ के मुताबिक चुनाव बाद बने गठजोड़ को तरजीह देना जायज है। असल में दोनों तरह की परंपराएं रही हैं। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने की सबसे चर्चित मिसाल 1996 में 13 दिनों की भाजपा की अटलबिहारी वाजपेयी सरकार थी, जिसे किसी से समर्थन हासिल नहीं हुआ तो हटना पड़ा था। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की सरकार में कांग्रेस के समर्थन से देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे।
देवेगौड़ा फिनामिना
अब देवेगौड़ा लगभग 92 साल की उम्र में एक बार फिर प्रासंगिक हो उठे हैं। घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया कि देवेगौड़ा उसी तरह एक फिनामिना बनकर उभरे, जैसे 2014 में मोदी उभरे थे। फर्क सिर्फ यह है कि मोदी फिनामिना से देश के बड़े हिस्से में एक ही निर्णायक नेता सबको बौना बना रहा था, जबकि कर्नाटक से निकला देवेगौड़ा फिनामिना सभी तरह की आवाजों को उभरने और एकजुट होने का वायस बन सकता है। मोदी फिनामिना में विपक्ष ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के बाकी नेताओं और सहयोगी दलों की पहचान खोती जा रही है। शायद इसी से शिवसेना और तेलुगूदेशम को कुछ अलग राह पकड़नी पड़ी।
इसके विपरीत देवेगौड़ा फिनामिना ने सभी पार्टियों को एक मंच पर आने और मोदी फिनामिना के सामने खड़े होने का मौका जुटा दिया है। यहीं से 2019 के समीकरण खुल रहे हैं।
2019 के समीकरण
इन चुनावों ने यह तो साबित कर दिया कि कांग्रेस एकला चलो की रणनीति पर नहीं चल सकती। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अगले आम चुनावों में नेता पद पाना है तो उन्हें साबित करना होगा कि वे सभी गैर-भाजपा पार्टियों और उनके बीच के तमाम विरोधाभासों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। कर्नाटक के नतीजों से भी जाहिर है और जैसा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि अगर वहां कांग्रेस जेडीएस वगैरह से चुनाव पूर्व तालमेल कर लेती तो भाजपा पिछले विधानसभा चुनावों से 16 प्रतिशत वोट और 64 सीटें ज्यादा नहीं हासिल कर पाती। अगर कांग्रेस और जेडीएस का यह गठजोड़ 2019 के चुनावों तक कायम रहता है तो मौजूदा विधानसभा नतीजों से भाजपा को सिर्फ 6 संसदीय सीटों पर ही बढ़त मिल सकती है जबकि 2014 में उसे राज्य की कुल 28 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें मिल गई थीं।
हालांकि, हर चुनाव अपना अलग गणित लेकर आता है लेकिन यह फार्मूला अगर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष अपनाता है तो 2019 में आंकड़ों के हिसाब से भाजपा की राह में रोड़े खड़ा करना मुश्किल नहीं होगा। इसकी तैयारी एक मायने में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा तथा रालोद के गठबंधन के रूप में दिख भी रही है। फिर जिस पैमाने पर भाजपा विरोधी गोलबंदी तैयार करने में माकपा के सीताराम येचुरी, जदयू के असंतुष्ट शरद यादव विपक्षी नेताओं और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ जुटे हैं, उससे इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता।
कर्नाटक में भाजपा अगर जोड़तोड़ कर सरकार बनाने की अपनी कोशिशों में सफल हो जाती है तो यकीनन विपक्ष को अपना वजूद कायम रखने के लिए इस गोलबंदी की कोशिशें और तेज करनी पड़ सकती हैं। यही भाजपा के लिए भी चुनौती है कि वह इस गोलबंदी को किस पैमाने पर रोकने में सफल हो पाती है क्योंकि आर्थिक मोर्चे से लेकर किसी भी मामले में केंद्र सरकार के पास उपलब्धियां दिखाने को कुछ खास नहीं है। हां, भावनात्मक मुद्दे जरूर उसके पास हो सकते हैं लेकिन उन्हें भी 2014 के पैमाने पर हवा देना शायद संभव न हो। तब मोदी इन भावनात्मक मुद्दों के अलावा बढ़ती आकांक्षाओं के भी प्रतीक थे।
बहरहाल, 2019 के महासंग्राम का मैदान कर्नाटक चुनावों ने सबके लिए खोल दिया है। हालांकि, उसके पहले इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनावों से गुजरना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि देश की सियासत में एक बड़े मंथन का दौर शुरू हो गया है।