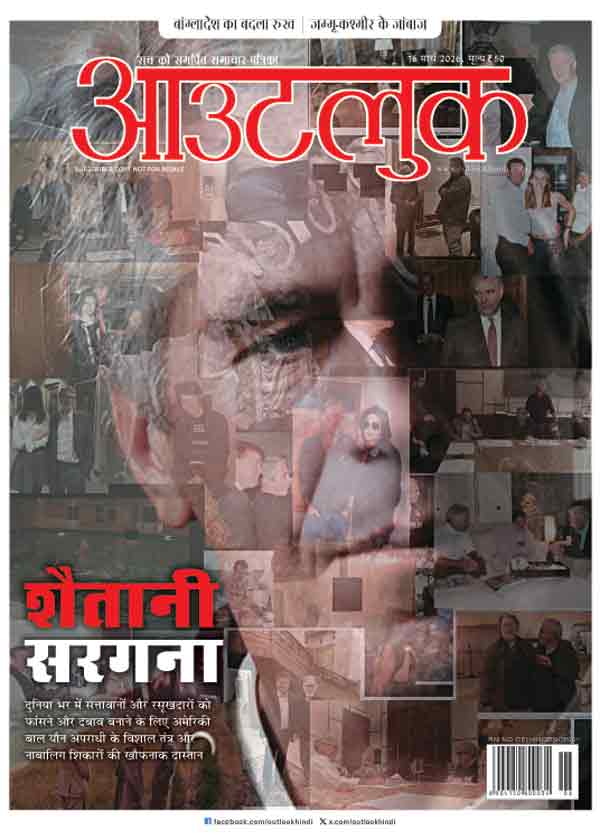प्रतिबंध विद्रोह पैदा करते हैं, इसका इतिहास तो सदियों पुराना है, और बड़े आंदोलनों तथा उससे सत्ता-परिवर्तन की मिसालें भी अनेकानेक हैं। लेकिन सोशल मीडिया के प्रसार, उसकी पहुंच, उसकी विविधता इतनी व्यापक है कि उसके कुछ प्लेटफॉर्म पर बंदिश लगाइए तो दूसरे मंच भी उतनी ही तेजी से प्रभावी हो जाते हैं और उसकी पिंग (रफ्तार या उछाल) इतनी जबरदस्त है कि फटाफट जुटान और बगावत की चिंगारी को आग में बदलने में बिजली की रफ्तार भी छोटी पड़ जाए। इसी मायने में नेपाल की कहानी एक नई मिसाल पेश करती है और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नवाचार से चौंकाती है।
सोशल मीडिया हाल के वर्षों में बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान और उसके पहले ‘अरब वसंत’ में अरब जगत के देशों में बड़े तख्तापलट या सरकारों की चूलें हिलाने में भरपूर इस्तेमाल हुआ था। लेकिन मोटे तौर पर इन सबमें एसएमएस (जैसे अन्ना आंदोलन) या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सएप या इसी तरह के पारंपरिक या ज्यादा प्रचलित-प्रसारित प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल हुआ था। सो, नेपाल की के.पी. शर्मा ओली की सरकार को शायद लगा कि इन प्लेटफॉर्म पर बंदिश लगाकर वह नौजवानों में पनप रहे असंतोष को कुछ हद तक दबा लेगी। सो, 5 सितंबर को “राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव बिगड़ने” का हवाला देकर 26 लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब सब रुक गए। लेकिन युवा सरकार से ज्यादा स्मार्ट निकले। सोशल मीडिया ने उन्हें फौरन विकल्प मुहैया करा दिया। वे गेमर्स के वर्चुअल कम्युनिटी हब डिस्कॉर्ड पर जुटे और विरोध की रूपरेखा तय की। यही सोशल मीडिया की ताकत और व्यापकता है, जिसका असर नेपाल की 15-30 वर्ष की युवा पीढ़ी ने दिखाया और यही नेपात की कहानी को अनोखा बनाता है।
इस तरह जिन रणनीतियों को धरातल पर उतारने में कभी बरसों, महीनों या हफ्तों लगते थे, जनरेशन जी ने कुछ घंटों में यह कर दिखाया। देखते ही देखते ‘नो बैन इन नेपाल’, ‘वॉइस ऑफ जेन जी, इंटरनेट राइट’ जैसे हैशटैग पूरे देश और दुनिया में ट्रेंड करने लगे। हजारों युवा सरकारी इमारतों पर पथराव करने लगे और राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत की खबरें आने लगीं। काठमांडू की सड़कें युद्घक्षेत्र में बदल गईं। ओली और तमाम मुख्यधारा की पार्टियों के नेताओं को सुरक्षित ठिकाने तलाशने पड़े।

बवाल के बादः काठमांडू में विद्रोही युवाओं के थाने को जला देने के बाद सफाई करते लोग
नेपाल का यह विद्रोह अकेला नहीं है। हाल के वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश युवाओं के डिजिटल इस्तेमाल वाले विरोधों से हिल चुके हैं। 2024 में बांग्लादेश में आरक्षण नीति और बेरोजगारी को लेकर विश्वविद्यालय छात्रों ने आंदोलन छेड़ा। ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुई यह लहर कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं को जोड़ लाई। ‘नो कोटा, जॉब फॉर यूथ’ जैसे हैशटैग ने आंदोलन को दिशा दी। केवल ढाका यूनिवर्सिटी से लगभग 50 हजार छात्र सड़क पर उतर गए। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
श्रीलंका में भी 2022 का आर्थिक संकट युवाओं और छात्रों के डिजिटल आह्वान से सियासी विस्फोट में तब्दील हो गया। ‘गोटा गो होम’ जैसे हैशटैग ट्रेंड ने पूरे देश के गुस्से को एक नारा दे दिया। वॉट्सऐप और टेलीग्राम के ग्रुपों ने मिनटों में हजारों लोगों को संगठित कर दिया। विरोध इतना व्यापक हुआ कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को भी देश छोड़ना पड़ा। पिछले चार साल में भारत के तीन पड़ोसी देशों में युवाओं के विरोध को सोशल मीडिया ने अंजाम तक पहुंचाया है। इन सभी देशों में आंदोलन को धार देने का काम सोशल मीडिया ने किया।
वर्ल्ड वैल्यू सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘पिछले दो दशकों में आम नागरिक बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे हैं, जिनमें सबसे आगे छात्र और युवा रहे हैं। युवाओं में प्रदर्शनों में भाग लेने की इच्छा 1990 के दशक के बाद से अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है और इस दौरान विरोध प्रदर्शनों की संख्या भी बढ़ी है।’’
काठमांडू यूनिवर्सिटी के मास मीडिया डिपार्टमेंट के हेड निर्मल मणि अधिकारी आउटलुक से कहते हैं, ‘‘नेपाल में पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जैसे- जनआंदोलन या मधेस आंदोलन। लेकिन उसमें पुराने तौर-तरीकों को अपनाया गया। उसकी गति धीमी थी। सूचना का प्रसार अखबारों, टीवी चैनलों या मुंह जबानी होता था, जिसमें हफ्तों लग जाते थे। इस बार स्थिति अलग थी। सिर्फ 24 से 48 घंटों के भीतर आंदोलन चरम पर पहुंच गया, क्योंकि सोशल मीडिया ने तुरंत सूचना दी। जब सरकार ने युवाओं पर दमन किया, तो खबर पलक झपकते वायरल हो गई, जिससे प्रदर्शनकारियों की संख्या तेजी से बढ़ी।”
हालिया वर्षों में भारत में भी डिजिटल असहमति की शक्ति बार-बार देखी गई है। 2020-21 का किसान आंदोलन इसका उदाहरण रहा। दिल्ली की सीमा पर हो रही घेराव और पुलिस टकराव को प्रदर्शनकारियों ने लाइवस्ट्रीम किया, तस्वीरें और वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर वायरल हुए और देखते ही देखते हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड बन गया। पॉप सिंगर रिहाना जैसी अभिनेत्रियों ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया।
इसी तरह, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुआ एंटी-सीएए आंदोलन सिर्फ शाहीन बाग के धरने पर निर्भर नहीं रहा। ट्विटर अभियानों, वायरल इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पोस्ट ने ऐसा माहौल गढ़ा कि यह सीधे संविधान बचाने की लड़ाई की तरह दिखने लगा। हैशटैग ‘मी टू इंडिया’ आंदोलन ने असहमति को बिल्कुल नए रूप में सामने रखा। यह किसी शहर की सड़क या मैदान में नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह ऑनलाइन था, जिसमें हजारों महिलाओं ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के अनुभव साझा किए। उसने राजनैतिक दलों, विश्वविद्यालयों और कंपनियों को कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर दिया।
वैश्विक स्तर पर भी यही पैटर्न दिखाई देता है। दस साल पहले अरब स्प्रिंग ने साबित किया था कि फेसबुक पेज और ट्विटर थ्रेड्स तख्तापलट भी करा सकते हैं। 2019 के हांगकांग विरोध प्रदर्शनों में युवाओं ने तकनीक को हथियार बना लिया। टेलीग्राम ग्रुप्स और एन्क्रिप्टेड चैट का इस्तेमाल करके उन्होंने पुलिस की रणनीतियों को चकमा दिया। लाखों की संख्या में भीड़ सड़क पर उतर आई। यह आंदोलन चीन समर्थित हांगकांग सरकार के एक्सट्राडिशन बिल के खिलाफ था, जिसके तहत हांगकांग के लोगों को मुख्यभूमि चीन में मुकदमों का सामना करने के लिए भेजा जा सकता था। बाद में, सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। अमेरिका में भी ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन पुलिस बर्बरता और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ शुरू हुआ था। लाखों ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट के चलते यह अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनों में एक बना।
अमेरिका स्थित यूएसआइपी की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 2015 से 2019 के बीच हुए प्रदर्शनों में युवाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं को अपने आंदोलनों में सफलता भी मिल रही है, क्योंकि युवा मुख्यधारा की राजनीति की बजाय अनौपचारिक राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। युवा प्रदर्शनकारियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकों का इस्तेमाल कर विरोध के तरीकों को बदल दिया है। इससे जुलूस-जलसे का खर्च कम हुआ, भागीदारी बढ़ी और आंदोलन ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ।
डिजिटल मंचों की असली ताकत रफ्तार और पहुंच है। आज हर जगह इंटरनेट है और सभी के हाथों में स्मार्टफोन है। स्टेटिस्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 1.2 अरब लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन और करीब 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। पीयू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व स्तर पर, 15-24 वर्ष की आयु-वर्ग के लगभग 80 फीसदी से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं जबकि उच्च-आय वाले देशों में यह लगभग 95-99 प्रतिशत है।
स्मार्टफोन और इंटरनेट ने आंदोलन की बाधाओं को लगभग खत्म कर दिया है। कोई भी किसी पोस्ट को शेयर करके या अपना हैशटैग बना कर आंदोलन का हिस्सा बन सकता है। भारत-नेपाल संबंधों के विशेषज्ञ और राजनैतिक समाजशास्त्री उद्धव प्याकुरेल आउटलुक से कहते हैं, ‘‘पहले विरोध के अगुआ आम तौर पर कुछ लोग होते थे। लेकिन अब नेतृत्व विकेंद्रित हो चुका है; कोई एक करिश्माई नेता आंदोलन का चेहरा नहीं होता, बल्कि हजारों छोटे आयोजक अपने-अपने ग्रुप, चैट और नेटवर्क में इसे आगे बढ़ा रहे होते हैं।’’ वे आगे कहते हैं, ‘‘पहले पुलिस पोस्टर फाड़ सकती थी या गिरफ्तार कर सकती थी, पर आज कोई वीडियो इतनी बार रीशेयर हो जाता है कि किसी एक की जवाबदेही तय करना मुश्किल होता है।’’
हालांकि डिजिटल आंदोलनों में अफवाह का खतरा भी लगातार बना रहता है। बांग्लादेश में एक झूठी अफवाहों ने अनावश्यक हिंसा भड़का दी थी। वहीं, 2021 में वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल पर हुआ हमला भी सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं के कारण भड़का था। डिजिटल मंच एक ओर लोकतांत्रिक असहमति और नागरिक भागीदारी को मजबूत करने की क्षमता रखता है, तो वहीं दूसरी ओर उतनी ही ताकत से उन्हें अस्थिर भी कर सकता है।
सोशल मीडिया के साथ एक और बात है, जो उसके नकारात्मक पक्ष को दिखाती है। कई बार जितनी तेजी से कोई हैशटैग चलता है, वह उतनी ही तेजी से ठंडा भी पड़ जाता है। इसे “स्लैक्टिविज्म” भी कहा जाता है, जहां लोग सिर्फ अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर या एक नारा पोस्ट करके समझ लेते हैं कि उन्होंने संघर्ष में योगदान दिया।
इसका एक और पहलू है। यूनिसेफ के मुताबिक, ‘‘डिजिटल असहमति की उपलब्धियां अक्सर लंबे समय तक ठोस बदलाव में नहीं बदल पातीं। प्रदर्शन तत्काल सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्त्री-पुरुष समानता या सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ठोस सुधार अक्सर लंबित रहते हैं।’’
सूडान का आंदोलन इसका उदाहरण है। सूडान में 2019 में मूल रूप से लोकतंत्र की बहाली, सैन्य शासन की समाप्ति और नागरिक सरकार की स्थापना की मांग पर केंद्रित आंदोलन हुआ। लंबे संघर्ष के बाद राष्ट्रपति उमर अल-बशीर को हटाया गया और अस्थायी नागरिक-सैन्य साझा सरकार बनी। लेकिन युवाओं की सबसे अहम मांगें- स्थायी लोकतांत्रिक ढांचा, रोजगार, शिक्षा और स्त्री-पुरुष समानता-समग्रता में पूरी ही नहीं हुईं। नई सत्ता संरचनाओं में युवाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया और 2021 में सैन्य तख्तापलट ने इन उम्मीदों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलनों की मुख्य मांगें, सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति का सुधार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना था। लेकिन इनमें किसी भी पर कोई ठोस बदलाव नहीं किया गया।
भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के लिए यह परिघटना अवसर और खतरे दोनों लेकर आती है। एक तरफ स्मार्टफोन से लैस युवा आबादी किसी भी मसले को राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना सकती है। जलवायु संकट, दलित अधिकार या स्त्री-पुरुष न्याय जैसे आंदोलन अब स्थानीय अखबारों या टीवी डिबेट पर निर्भर नहीं हैं, एक्स और इंस्टाग्राम सीधे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा देते हैं। महामारी के दौरान ऑक्सीजन और अस्पतालों के घोर अभाव को लिए बने स्वयंसेवी नेटवर्क ने दिखाया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से व्यवस्था विरोध और राहत कार्य दोनों में तेजी लाई जा सकती है।
नेपाल के हैशटैग अपने आप में कानून नहीं बदल सकते, मगर वही हैशटैग नेताओं को पीछे हटने, अदालतों का ध्यान आकर्षित करने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब असहमति केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि कौन सड़क पर मार्च कर रहा है, बल्कि इस पर भी करती है कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है, क्या शेयर कर रहा है असहमति और सत्ता के बीच की जंग डिजिटल स्पेस में भी उतनी ही है, जितनी जमीन पर।
यानी सोशल मीडिया ने विरोध प्रदर्शनों के लिए घर-घर जाकर पर्चे बांटने, छात्र हॉस्टलों के कमरों में बैठक कर जोखिम भरी गुप्त बैठकें करने की जरूरत तकरीबन खत्म कर दी है, न रात काली कर नारों से दीवारें रंगनी हैं। डिजिटल युग ने क्रांति की पूरी परिभाषा बदल कर रख दी। हालांकि डिजिटल मंचों ने राजनीति की धार को तेज भी किया और भोथरा भी। मसलन, नेताओं ने जिस माध्यम से अपनी छवि चमकाई, चुनाव जीते, मतदाताओं को रिझाया उसी माध्यम पर ही उनकी पोल खोली गईं और वहीं वे बे-आबरू हुए। समाज ने इसकी ताकत समझी और सत्ता की संरचना को पूरी तरह बदल दिया है। यह संरचना इतनी बदली कि कई देशों की सत्ता की नींव हिला दी।
सोशल मीडिया आंदोलन

. 2020-21 में भारत में भी किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया की भूमिका अहम रही
. नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ एंटी-सीएए आंदोलन में ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर चले अभियान ने भीड़ जुटाई
. श्रीलंका में भी 2022 का आर्थिक संकट युवाओं और छात्रों के डिजिटल आह्वान से सियासी विस्फोट में बदल गया
. 2024 में बांग्लादेश में विश्वविद्यालय छात्रों के आंदोलन में ‘नो कोटा’, ‘जॉब फॉर यूथ’ हैशटैग खूब चले
. सबसे पहले अरब स्प्रिंग ने साबित किया था कि फेसबुक पेज और एक्स थ्रेड्स सरकार का तख्तापलट करा सकते हैं