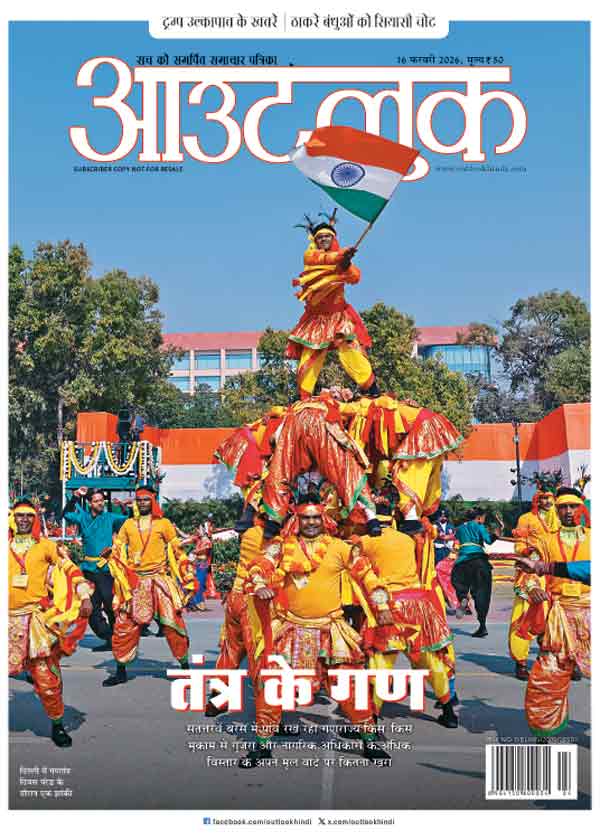ब्रिटिश शासकों, इतिहासकारों, अध्येताओं, लेखकों, लोक गीतकारों ने 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुए सिपाही विद्रोह को कई नामों से पुकारा है। नामकरण की यह विविधता विद्रोह के प्रति लोगों के अलग-अलग नजरिये को दर्शाती है। विद्रोह को अपमानजनक संबोधन ‘गदर’ से लेकर ‘भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम’ तक बताया गया है, हालांकि अंग्रेजों द्वारा अपमानजनक संबोधन के रूप में प्रयुक्त गदर शब्द आगे चल कर भारतीयों के लिए सम्मानजनक बना। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अमेरिका में 1913 में गठित संगठन का नाम ‘गदर’ रखा गया। अपने मुखपत्र का नाम भी उन्होंने ‘गदर’ रखा। 1857 के विद्रोह पर करीब 75 साल बाद लिखे गए पहले हिंदी उपन्यास का शीर्षक भी ‘गदर’ है। अमृतलाल नागर ने विद्रोह संबंधी ब्योरे एकत्रित किए, तो उस पुस्तक का नाम ‘गदर के फूल’ रखा।
नामकरण के अलावा विद्रोह के चरित्र को लेकर भी कई धारणाएं मिलती हैं। उसे ‘सामंती’ से लेकर ‘जनवादी’ तक कहा जाता है। विद्रोह में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में भी कई दावे हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड में मारे गए अंग्रेजों (बच्चों और महिलाओं समेत) का आंकड़ा 6,000 के करीब है। बाद में अंग्रेजों द्वारा की गई बदले की कार्रवाई में मारे जाने वाले भारतीयों की संख्या 8 लाख से 30 लाख तक बताई जाती है। इसमें विद्रोह से जुड़े अकाल और महामारी में मारे जाने वाले भारतीयों की संख्या को भी शामिल किया जाता है। विद्रोह के इतिहासकारों, विभिन्न घटनाओं और पात्रों पर आधारित संस्मरण तथा कथात्मक विवरण लेखन में सभ्य-असभ्य और क्रूर-क्रांतिकारी का परस्पर विरोधी विमर्श भी मिलता है।
1857 के विद्रोह के मूल में महज धार्मिक अस्मिता का प्रश्न था या यह मूलत: राष्ट्रीयता के विचार से परिचालित था, यह सवाल खासा विवादास्पद रहा है। कहने का आशय, कि 1857 के विद्रोह के विविध पहलुओं पर प्रस्तुत किए गए तर्कों-प्रतितर्कों की एक पूरी दुनिया हमारे सामने मौजूद है। दरअसल, जब हम इसे राष्ट्रवाद के साथ जोड़ कर देखते हैं, तब पता चलता है कि यह सीधा और सरल विचार कभी नहीं रहा है। युग-विशेष, युगीन परिस्थितियां, सामाजिक ताना-बाना आदि कारक राष्ट्रीयता के विचार को एक जटिल और कई बार अंतर्विरोधपूर्ण विचार बनाते हैं। 1857 के विद्रोह के मूल में स्थित राष्ट्रीयता के विचार को भी इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए।
‘झंडा सलामी गीत’ अथवा कौमी तराना 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख पात्र अजीमुल्ला खान यूसुफजई ने लिखा था। यह दिल्ली के ‘पयाम-ए-आजादी’ नामक दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था। फरवरी 1857 में शुरू किए गए इस उर्दू-हिंदी पत्र के प्रकाशक अजीमुल्ला खान और मुख्य संपादक बादशाह बहादुर शाह जफर के पोते मिर्जा बेदार बख्त थे (पत्र को नाना साहब का संरक्षण प्राप्त था क्योंकि उनके दीवान अजीमुल्ला खान फरवरी 1857 में यह प्रिंटिंग प्रेस भारत लेकर आए थे)। सितंबर 1857 से मराठी में भी यह पत्र झांसी से प्रकाशित हुआ। बादशाह जफर का प्रसिद्ध परचा ‘पयाम-ए-आजादी’ में ही प्रकाशित हुआ था। 29 मई 1857 को पत्र ने विद्रोह को अपना घोषित समर्थन दिया। ब्रिटिश सरकार ने “राजद्रोह” के आरोप में पत्र के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। बेदार बख्त को फांसी दे दी गई। माना जाता है कि अजीमुल्ला खान कानपुर की पराजय के बाद नाना साहब के साथ नेपाल की सीमा की ओर निकल गए थे जहां 28 वर्ष की आयु में बीमारी से उनकी मौत हो गई।
कानपुर निवासी अजीमुल्ला खान न सिपाही थे, न सामंत। वे अत्यंत साधारण सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से थे। उनके मिस्त्री पिता का निधन हो चुका था। 1837-38 के अकाल में माता के साथ वे संयोग से जीवित बच गए थे। बाद में माता का भी निधन हो गया। उन्होंने अनाथालय और एक अंग्रेज के घर में काम करते हुए शिक्षा प्राप्त की। वे पहले कई अंग्रेजों के सचिव बने फिर नाना साहब के दीवान का पद संभाला। नाना साहब ने बहुभाषाविद (उन्हें अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषा आती थी) और कुशाग्र-बुद्धि अजीमुल्ला खान को प्रधानमंत्री के पद पर पदोन्नति दी।
ऐसा माना जाता है कि अजीमुल्ला खान इंग्लैंड प्रवास के दौरान नाना साहब की पेंशन तो बहाल नहीं करा पाए, लेकिन ब्रिटिश आधिपत्य से भारत को मुक्त कराने का विचार और दृढ़ इरादा लेकर भारत लौटे। ब्रिटिश साम्राज्य अजेय है, यह मिथक उन्होंने अपनी आंखों से टूटता हुआ देखा। उन्होंने देखा कि क्रीमिया युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं को रूस की सेना ने पराजित कर दिया है। अजीमुल्ला खान नवजागरण की चेतना के दायरे के बाहर की गई देश की स्वाधीनता की चिंता और प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। 'झंडा सलामी गीत' इस प्रकार हैः
हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा,
पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा।
यह हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा,
इसकी रूहानियत से रौशन है जग सारा।
कितना कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा,
करती है जरखेज जिसे गंगो-जमुन की धारा।
ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा,
नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा।
इसकी खानें उगल रहीं सोना, हीरा, पारा,
इसकी शान-शौकत का दुनिया में जयकारा।
आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा,
लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा।
आज शहीदों ने है तुमको अहले-वतन ललकारा,
तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा।
हिंदू-मुसलमां-सिख हमारा भाई-भाई प्यारा,
यह है आजादी का झंडा इसे सलाम हमारा।।
इस गीत में ब्रिटिश आधिपत्य को भारत की राष्ट्रीय पराधीनता के रूप में चिन्हित किया गया है क्योंकि हिंदुस्तानी इस मुल्क के स्वभाविक मालिक हैं। यह सही है कि 1857 के विद्रोह का भौगोलिक विस्तार मुख्यत: उत्तर, पूर्व और मध्य भारत तक था, लेकिन क्रांतिकारियों का दावा हिमालय से समुद्र तक हिंदुस्तान का है। यह एक जरखेज धरती है जिसकी संपदा को अंग्रेज लूट रहे हैं। “ऐसा मंतर मारा” की ध्वनि है कि अंग्रेजियत का जादू महत्वपूर्ण माने जाने वाले भारतीयों के सिर चढ़ कर बोल रहा था। इस ध्वनि की गूंज गांधी के ‘हिंद स्वराज’ में मिलती है जहां वे कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, हमने खुद उनकी गुलामी कबूल की है।
यह सही है कि ज्यादातर राजे-रजवाड़ों और भारतीय ब्रिटिश आर्मी की बटालियनों ने विद्रोहियों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया अथवा तटस्थ रहे। नवशिक्षित भद्रलोक द्वारा प्रवर्तित नवजागरण की चेतना का संबंध भी 1857 के विद्रोह के साथ नहीं जुड़ता। इस गीत में उस समय के प्रामाणिक भारतीय की कसौटी प्रस्तुत की गई है कि वही सच्चा भारतीय है जो शहीदों की ललकार पर गुलामी की जंजीरें तोड़ने का उद्यम करता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 1857 के विद्रोह के बाद चले आजादी के संघर्ष के फलस्वरूप जो भारत की आजादी संभव हुई, उसके खिलाफ राजे-रजवाड़े, सांप्रदायिक संगठन और कितने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति खिलाफ थे। ऐसे अप्रामाणिक भारतीयों के चलते देश का बंटवारा भी हुआ।
यह सही है कि विद्रोह में कई बार धार्मिक, जातिवादी, जातीय, क्षेत्रीय आदि दरारें उभरती हैं। एक उपमहाद्वीप के आकार के देश में, जिसका अत्यंत प्राचीन समाज विविधताओं और साथ ही विषमताओं से भरा हो, विद्रोह के दौरान दरारों का उभरना स्वाभाविक था। गौरतलब है कि गीत में धार्मिक अस्मिता के सवाल पर देश की आजादी का आह्वान नहीं किया गया है। अलबत्ता, सभी धर्मावलंबियों के बीच एकता और प्यार का उल्लेख किया गया है। शायद अजीमुल्ला खान धार्मिक अस्मिता की पुकार को राष्ट्रीय अस्मिता की पुकार में बदलना चाहते थे। गीत में अगर भारत की नारियों का भी आह्वान होता तो गीत की सार्थकता दोगुनी हो जाती क्योंकि 1857 के विद्रोह में सामाजिक-आर्थिक हाशियों पर आबाद महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
कहने की जरूरत नहीं कि इस गीत को वर्तमान नव-साम्राज्यवादी संकट और सांप्रदायिक वैमनस्य के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की युवा पीढ़ियों को कम से कम यह जरूरी काम करना चाहिए।
(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पूर्व फेलो हैं)