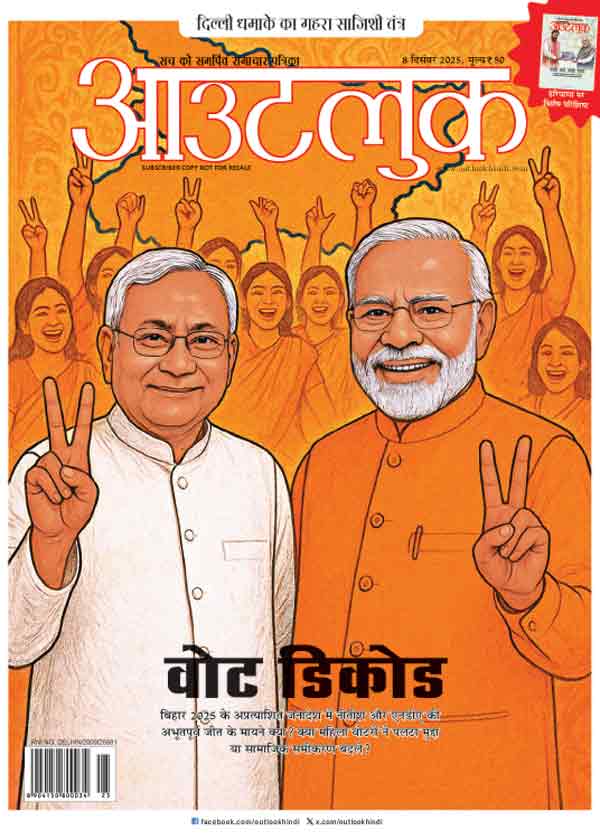फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक ज्यां लुक गोडार्ड का एक मशहूर कथन है, “एक कहानी की शुरूआत, मध्य और अंत होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो।” यानी हर कहानी जो शुरू होगी, उसका किसी मोड़ पर तो अंत होना ही होगा, फिर चाहे वह कहानी तीस साल तक क्यों न चलती रहे। 1990 के दशक में विकसित हुए बॉलीवुड में सफलता की नई परिभाषा लिखने वाली खान तिकड़ी- शाहरुख, सलमान और आमिर खान के स्टारडम को हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी और दशक के समक्ष रखकर नापा नहीं जा सकता। इन सितारों का उदय भारत के आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के जिस दौर में हुआ उससे मिलता-जुलता कोई उदाहरण नहीं है। अब चर्चा आम है कि क्या खान स्टारडम का अजीम-उल-शान दौर आखिरी लम्हों से गुजर रहा है। शाहरुख, सलमान और आमिर खान की लोकप्रियता उनके अभिनय के साथ-साथ इस बात पर भी टिकी रही कि उन्होंने लगातार बदलते मीडिया परिदृश्य में खुद को किस तरह प्रासंगिक बनाए रखा। लेकिन अब तीनों खान सितारों के करिअर पर सिलसिलेवार ढंग से नजर डालने पर वक्त की करवट के संकेत देखे जा सकते हैं।
स्टारडम के तीन चेहरे
नब्बे के दशक में परवान चढ़ने वाले बॉलीवुड को अगर एक शरीर माना जाए तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शाहरुख उस शरीर में प्यार और टीस से भरा दिल हैं, आमिर खान उलझन भरा दिमाग और सलमान खान उसके हाथ। वो हाथ जिन्हें उदारीकरण के बाद भारत में फिल्मी सेहतमंदी का ख्वाब बेचने वाले जिम्नेजियम ने तराशा लेकिन पहले बात दिल यानी शाहरुख खान की।
एनआरआइ सुपरस्टारडम
याद कीजिए दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे का क्लाइमैक्स। मद्धिम गति से भागती ट्रेन के डिब्बे से एक हाथ बाहर फैलाए, चोटिल मुस्कान के साथ राज पीछे छूटती सिमरन का हाथ थाम ही लेता है। उस लम्हे में शाहरुख खान ने दरअसल काजोल का ही नहीं बल्कि दुनिया की चकाचौंध भरी गलियों से गुजरकर सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे भारतीयों का हाथ थामा। शाहरुख का सफर दीवाना से शुरू हुआ लेकिन स्टारडम की जो उड़ान उन्होंने तीन साल बाद डीडीएलजे से भरी, वो तीस साल तक चलती रहेगी इसका अंदाजा उस वक्त कोई नहीं लगा सकता था। लंदन में पलने-बढ़ने के बावजूद हिंदुस्तानी पारिवारिक मूल्यों से लबरेज डीडीएलजे के राज ने हिंदी सिनेमा को वह किरदार दिया जिसने उपभोक्तावाद की नई और सपनीली दुनिया में भारतीय पहचान कायम रखने के तरीके सुझाए, जिसकी मर्दानगी गुस्से में भरे वंचित शहरी अमिताभ बच्चन के विकल्प के तौर पर उभरी। एक ऐसा ग्लोबल भारतीय पुरुष जिसमें नफासत थी, प्यार की गुंजाइश थी, सपने थे और समझौते करने की भारतीय परंपरा का निर्वहन भी था।

सरहदों को बेमानी करते भूमंडलीकरण में हिंदुस्तानी पहचान संभाले नए वक्त का नया मर्द जिसकी साधारण शक्ल-ओ-सूरत और ब्रॉन्डेड कपड़ों में शहरी युवा अपना अक्स देख सके, जिसके रोने का मतलब टूटना नहीं, भावनाओं के समंदर को आंखों से बयान करने की ताकत थी। आसान शब्दों में कहा जाए, तो भारत से बाहर निकलने वाला हर प्रवासी भारतीय राज हो सकता था और यही शाहरुख खान के स्टारडम का आधार बना। नब्बे और 2000 के दशक में शाहरुख ने लगातार ऐसे किरदार निभाए जिनका वजूद धर्म, जाति और भारत में रहने से परिभाषित नहीं था, लेकिन इन ग्लोबल हिंदू किरदारों में उनकी मुसलमान पहचान को पूरी तरह जब्त कर लिया गया। शाहरुख के करिअर में मुसलमान होने की दुविधा से जूझता माइ नेम इज खान बहुत देर से आया। दीगर है कि शाहरुख के बेहिसाब स्टारडम का दौर भारत में हिंदुत्ववादी ताकतों के उफान का दौर भी रहा। ऐसे में धर्म और समाज के संवेदनशील मसले से जूझने के बजाय, उनके स्टारडम को तराशा उस नए शहरी मर्द की संवेदनशील और पारिवारिक छवि की परिकल्पना ने जिसे करण जौहर ने भरपूर भुनाया।
धार्मिक पहचान और हिंसात्मक स्टारडम
सलमान खान ने इसके विपरीत जाते हुए कुछ हद तक अपनी धार्मिक पहचान को हालिया सालों में जिया है। मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन से पारिवारिक रोमांस में डूबे संस्कारी प्रेम के रूप में सलमान ने अपनी जगह बनाई लेकिन शाहरुख खान के आधुनिक एनआरआइ राज के सामने देसी प्रेम का ग्लैमर उन्नीस ही रहा। गौर करने लायक बात यह है कि 2002 में मुंबई में फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने और गैर-इरादतन हत्या के मामले के बाद मीडिया में उभरी सलमान खान की बैड बॉय इमेज ने उनके फिल्मी करिअर को एक खास दिशा देने की जमीन तैयार की। राधे भैया अवतार में सलमान तेरे नाम में क्या उतरे, इस किरदार का औरतों के लिए दकियानूसी नजरिया, शारीरिक हाव-भाव और हिंसा सलमान खान के सिनेमाई रसूख की पहचान बन गए, भले ही उन्होंने अपने करिअर में दर्जनों कॉमेडी और रोमांटिक रोल निभाए। वॉन्टेड फिल्म से गोलियां दागते और गालियां बरसाते सलमान खान के राधे अवतार ने हिंदी सिनेमा को एक नया एक्शन हीरो दिया। उदारीकरण के बाद भारतीय शहरों में पनपे मनोरंजन के केंद्र मल्टीप्लेक्स के ‘सभ्य’ नए मध्यवर्गीय दायरे से बाहर फेंक दिए गए दर्शक वर्ग का हीरो। उनके तराशे हुए जिस्म और हिंसात्मक किरदारों में जैसे भारतीय समाज के वंचित वर्ग ने अपनी ताकत खोज ली।
सलमान पर लिखे गए तमाम लेख इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके चाहने वालों में एक बड़ा वर्ग छोटे शहरों में रहने वाले मुसलमानों का है। हालांकि ये सोचना बेमानी है कि उनकी अपार लोकप्रियता की वजह यही दर्शक वर्ग है। खासकर दबंग के बाद सलमान की स्टारडम ने ‘मल्टीप्लेक्स’ मोड़ लिया लेकिन बिजनेस की संभावनाओं के मद्देनजर सलमान ने अपनी धार्मिक पहचान को ईद पर ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज की रवायत से जोड़ा। शाहरुख की तरह सलमान भी 1988 से शुरू हुए अपने फिल्मी सफर में ज्यादातर प्रेम, राजू, सूरज और अमन सरीखे हिंदू किरदारों में ही दिखाई दिए मगर तीनों खानों में वे पहले थे जो 1990 में ही सनम बेवफा में मुसलमान किरदार के तौर पर पर्दे पर उतरे और उसके बाद तुमको ना भूल पाएंगे में अली, सांवरिया में ईमान और कुछ बरस पहले आई सुल्तान में सुल्तान अली खान बने। भले ही इनमें धार्मिक पहचान का किरदार की जिंदगी पर कोई असर न रहा हो। उन्होंने तो धर्म और भारत-पाकिस्तान की ऐतिहासिक कड़वाहट के बीच खुद को सीधे स्थापित भी किया, भले ही वह ब्राह्मण बजरंगी भाईजान के तौर पर रहा हो लेकिन सलमान ‘भाई’ पहचान को उस किरदार से अलग करके देखना मुमकिन नहीं।
सरोकार वाली स्टारडम

शाहरुख के निभाए नाजुक मर्द और सलमान के शारीरिक अतिरेक के दो किनारों के बीच जगह तलाशी आमिर खान ने। हालांकि आमिर को किसी खास छवि में बांधकर देखना टेढ़ी खीर है। उन्होंने खुद को रोमांटिक और सड़कछाप टपोरी किरदारों से निकालते हुए सजग, संवेदनशील मध्यमवर्गीय शख्स के तौर पर स्थापित करने में कामयाबी पाई और इसमें सिनेमा का मल्टीप्लेक्स की चपेट में आना अहम रहा। शाहरुख जिस उपभोक्तावादी सिनेमा के पोस्टर बॉय बने, आमिर उसका हिस्सा होते हुए भी खुद को उसमें डूबे हुए सितारे की छवि से बचाते हुए चलते रहे। लगान के बाद दिल चाहता है, रंग दे बसंती, तारे जमीं पर और 3 इडियट्स ने जहां उन्हें शिक्षित मध्यवर्गीय दर्शकों से जोड़ा, वहीं टीवी सीरीज सत्यमेव जयते से उन्होंने अपनी सिनेमाई छवि को सफलतापूर्वक सामाजिक ब्रॉन्ड में बदल डाला।
नए चेहरों की चुनौती
अगर हम 2014 के बाद भारत में राजनीतिक माहौल के आइने में खान स्टारडम को रखकर देखें, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बदले सामाजिक माहौल में खान स्टारडम की चमक फीकी पड़ी है। तीनों खान पिछले कुछ सालों में कभी न कभी धार्मिक पहचान के कारण अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे तो कई मसलों पर चुप्पी बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार भी बने।
सिनेमाई सितारे केवल सिनेमा के किरदार या व्यावसायिक उत्पाद नहीं होते, वे स्वयं में वक्त और समाज के लक्षण समेटे होते हैं। इसलिए उनके पैरों तले की जमीन अगर दरकने लगे तो इसमें सामाजिक-राजनीतिक बदलावों के संकेत का छिपा होना लाजमी है। खान तिकड़ी की चमक अगर फीकी पड़ती दिख रही है तो क्या ये सिर्फ सिनेमा का सवाल है? कुछ और सामाजिक परिस्थितियों को भी देखना होगा जैसे मी टू के बाद बने माहौल में सिनेमा के पर्दे पर उतरने वाले पुरुष सितारे और पर्दे से इतर उनकी छवि। रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव चंद नाम हैं, जिनके किरदारों ने छोटे-बड़े शहरों के बदले हुए मर्द का स्वरूप पेश किया है। स्टाइल, अभिनय और सफलता की भूख लिए रणवीर सिंह की लोकप्रियता जहां खान स्टारडम को सीधी चुनौती देती नजर आती है, वहीं आयुष्मान खुराना कमजोरियों से जूझती एक ऐसी प्रोग्रेसिव मर्दानगी की कमान संभाले हैं, जो कहीं न कहीं आमिर खान के मध्यवर्गीय जागरूक मर्द के ढांचे में फिट बैठती है। अक्षय कुमार के राष्ट्रवादी सुर वाले सिनेमा की चुनौती तो है ही। यानी शाहरुख, सलमान और आमिर की सिनेमाई छवियों के विकल्प स्पष्ट तौर पर तैयार हैं और अब उन्हें अपने कामयाब लेकिन बासी ढांचों को तोड़े बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा।
ओटीटी और सोशल मीडिया का लोकतंत्र
तीनों खान ने अपनी स्टारडम की कहानी सिर्फ फिल्मी किरदारों के जरिए नहीं गढ़ी बल्कि इस सफलता के पीछे टेलीविजन नेटवर्क का फैला जाल और विज्ञापन की दुनिया के जरिए घर-घर तक पहुंचना भी शामिल है। नब्बे और 2000 के दशक में सैटेलाइट टीवी का भारत समेत दुनिया में जबरदस्त विस्तार और फिल्मी चैनलों की लाइसेंसिंग इस अपार स्टारडम के मजबूत खंभे बने। दुनियाभर में पहुंचने वाले फिल्मी चैनल, टीवी शो और फिल्म अवॉर्ड प्रसारण ने जहां शाहरुख और सलमान के स्टारडम को बेमिसाल मजबूती दी, वहीं आमिर ने टीवी जैसे करीबी माध्यम का इस्तेमाल अपनी जिम्मेदार अभिनेता-ऐक्टिविस्ट छवि गढ़ने और विस्तार देने में किया। टीवी की पहुंच और असर का वह दौर अब पुरानी बात है जिसमें कोई तड़का लगाया नहीं जा सकता। वक्त अब ओटीटी और सोशल मीडिया का है, जिसमें सितारा बनने के लिए सिने अभिनेता या अभिनेत्री होना जरूरी नहीं।
यूं तो भारत में ओटीटी भी टीवी और फिल्मों के पुराने चेहरों का ठिकाना बनता जा रहा हैं, लेकिन नए मंच ने विक्रांत मैसी जैसे कई चेहरों के फिल्मी करिअर को बढ़ने का मौका दिया है, जिनकी फिल्में सिनेमा हॉल में सीमित रिलीज या फिल्म फेस्टीवल पर निर्भर रहती थीं।
अगर समाज और मीडिया ध्रुवीकरण के इस वक्त की सच्चाई है, तो सोशल मीडिया की लोकतांत्रिक संभावनाएं भी हमारे मीडिया-माहौल को परिभाषित करती हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे डिजिटल चैनल दरअसल स्टारडम के विकेन्द्रीकरण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अपनी अपार सफलता के चलते खान तिकड़ी को भले ही इन माध्यमों पर भी करोड़ों फॉलोअर हासिल हों, लेकिन महामारी की मार से जूझ रहे सिनेमा में खान स्टारडम की यात्रा अब निर्णायक मोड़ पर है। तीनों के सामने मसला है नए भारत में अपनी नई भूमिका तलाशने का जिसका इंतजार उनके करोड़ों चाहने वालों को है।
(वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय, लंदन के मीडिया और संचार विभाग में हिन्दी सिनेमा पर शोध कर रही हैं। बीबीसी हिन्दी सेवा में पत्रकार रह चुकी हैं और सिनेमा और सम-सामयिक मुद्दों पर लिखती हैं)