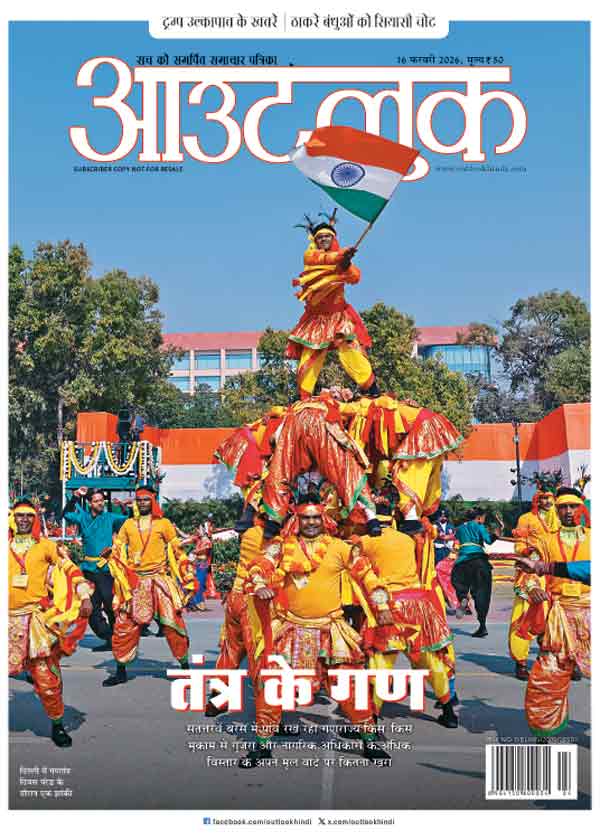मार्च के पहले हफ्ते में मैं अमेरिका में था। अपने मेजबान के घर उनकी किताबों की आलमारी से आदतन छेड़छाड़ के दौरान मेरी निगाह ग्राहम ग्रीन की किताब द क्वाउइट अमेरिकन पर पड़ी। बेहद बिगड़ैल और वाचाल डोनाल्ड ट्रम्प के राज वाले अमेरिका में 1955 के इस क्लासिक को फिर से पढ़ना बेचैन करने वाला एक तजुर्बा है। उसे पढ़ते हुए एक खयाल यह आता है कि अपने दूसरे कार्यकाल में बतौर राष्ट्रपति ट्रम्प ने आखिरकार अमेरिका को बीते सात दशक के उसके संस्थागत पाखंड से दूर हटाने का काम किया है।
ग्रीन की कहानी का सूत्रधार एक निराशावादी अफीमची ब्रिटिश पत्रकार थॉमस फाउलर है और कहानी का नायक एक सज्जन और आदर्शवादी अमेरिकी आल्डेन पाइल है (जिसके अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए का एजेंट होने की ओर इशारा किया गया है)। कथानक दक्षिण-पूर्वी एशिया का है जब कम्युनिस्टों की हिंसक बगावत तले फ्रेंच उपनिवेशवाद लड़खड़ा रहा था। वियतनाम को कम्युनिस्टों से दूर रखकर उसे लोकतंत्र के लिए महफूज बनाने का कार्यभार फ्रांस से अपने कंधे पर लेने वाले अमेरिका के बौद्धिक और वैचारिक पूर्वग्रह को ग्रीन ने अपनी रचनात्मक अफसानानिगारी से पूरी तरह तार-तार कर दिया है।
उपन्यास का नायक युवा अमेरिकी ‘‘अपनी मासूमियत और अज्ञानता में पूरी तरह आत्म विश्वस्त है।’’ यह अज्ञानता बड़ी खतरनाक है। ग्रीन लिखते हैं, ‘‘मासूमियत उस लाचार कोढ़ी के जैसा है, जिसकी घंटी गुम हो गई है और वह दुनिया भर में ऐसे घूम रहा है जैसे उससे किसी को कोई खतरा न हो।’’
दूसरी ओर अंग्रेजी पत्रकार एक घुटा हुआ किरदार है, जिसने उस इलाके में लंबा वक्त बिताया है, उस जगह को जानता है और वहां की सांस्कृतिक सूक्ष्मताओं तथा इंकलाबी राजनीति के विश्वासघाती पहलुओं से परिचित है। वह अमेरिकी नायक से कहता है, ‘‘तुम और तुम्हारे जैसे लोग ऐसे लोगों की मदद से जंग छेड़ने में लगे हुए हो जिनकी इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उन्हें साम्यवाद नहीं, भर पेट चावल चाहिए।’’ फिर वह मजाक उड़ाते हुए प्रसिद्ध अमेरिकी डॉमिनो थ्योरी का सूत्र पढ़ता है, ‘‘मैं पूरे रिकॉर्ड से वाकिफ हूं। थाईलैंड गया, तो मलेशिया जाएगा, फिर इंडोनेशिया भी जाएगा। ‘‘जाएगा’’ का मतलब?’’ पत्रकार की बात को नायक पाइल पकड़ नहीं पाता, जो स्वाभाविक रूप से अमेरिकी विचार का नुमाइंदा है। यही डॉमिनो थ्योरी अंतत: केनेडी के शासन में ‘सर्वश्रेष्ठ और सबसे चमकदार’ लोगों के वजूद का सहारा बन गई थी, जिसने एक के बाद एक अमेरिका को लड़ाइयों में झोंक डाला। तमाम देशों के करोड़ों लोगों ने साम्यवाद के फैलाव को रोकने पर लक्षित भ्रामक अमेरिकी नीतियों और विचारों का जबरदस्त प्रतिरोध किया था।
ब्रिटिश पत्रकार चाहता था कि युवा अमेरिकी वियतनामियों के राष्ट्रवाद की ताकत को समझे। तमाम औपनिवेशिक सत्ताओं की तरह फ्रेंच भी मानते थे कि उनकी भूमिका इतनी उदार और लाभदायी है जो राष्ट्रवादी आकांक्षाओं पर भारी पड़ जाएगी। अब अमेरिकी भी उसी दुष्चक्र में फंस गए थे। ऐसे में अंग्रेजी पत्रकार युवा अमेरिकी को याद दिलाता है कि वे सारे बाहरी लोग जो वियतनामियों की भलाई चाहते हैं उन्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कि ‘यह देश उनका है।’
उपन्यासकार ग्रीन अमेरिकी उद्दंडता और अज्ञानता को साफ पहचान पा रहे थे, जिसके चलते अमेरिकियों की पीढ़ी दर पीढ़ी वियतनाम में हताहत होती रही। बावजूद उसके, आगे आने वाले तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दुनिया भर में लोकतंत्र लाने और उसे महफूज करने की सनक चढ़ी रही- पहले वियतनाम, फिर अफगानिस्तान और इराक। ऐसे सारे उद्यम व्यर्थ गए। अमेरिकियों के सभ्यताबोध पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। अब जाकर एक ऐसा राष्ट्रपति आया है, जो लोकतंत्र को रत्ती भर भी भाव नहीं देता। दुनिया में लोकतंत्र को बचाने में ट्रम्प की कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह तो यूरोप और कनाडा के स्थापित लोकतंत्रों को उलटे कमजोर करने में ही जुटे हुए हैं। ट्रम्प की नजर में तो अमेरिकी लोकतंत्र ही अपने आप में अच्छाइयों और बुराइयों का कुल जमा घालमेल भर है (जिस रूप में अमेरिकी लोग बीती तीन सदियों के दौरान यहां लोकतंत्र को भोगते आए हैं)। ट्रम्प के भीतर कतई ऐसी कोई प्रेरणा नहीं है जो अमेरिकी ऊर्जाओं और कल्पनाओं को ‘लोकमंगल’ के लिए काम करने की ओर प्रवृत्त करती हो, जिसका जिक्र जॉन एफ. केनेडी ने अपने संक्षित राष्ट्रपतित्व काल में जाने कितनी ही बार किया था। अमेरिका के दोस्तों और दुश्मनों के भीतर अमेरिका-विरोध की जैसी भी भावना है, उसे कम करने या दूर करने में भी ट्रम्प की कोई रुचि नहीं है।
ग्रीन का नायक इतनी ईमानदारी से अमेरिकी मिशन में आस्था रखता है कि वह ब्रिटिश से कहता है कि एक बार यदि कम्युनिस्टों का राज आ गया तो वियतनाम के लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को गंवा देंगे। वह कहता है, ‘‘उन्हें वही मानना होगा, जो उन्हें बताया जाएगा, उन्हें खुद सोचने की कोई मोहलत नहीं दी जाएगी।’’ इस पर ब्रिटिश पत्रकार तिरस्कार से कहता है, ‘‘सोचना ऐय्याशी का काम है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जब कोई किसान रात को अपने झोंपड़े में लौटता है, तो वह ईश्वर और लोकतंत्र के बारे में सोचता होगा?’’
ट्रम्प, उनके ‘सह-राष्ट्रपति’ एलन मस्क और उप-राष्ट्रपति जे. डी. वान्स निश्चित रूप से उस ब्रिटिश किरदार के साथ खुद को सहमत पाते होंगे। अमेरिका का इससे कोई लेना-देना नहीं है कि ईरानी या चीनी या फिर रूसी लोगों को वही बात माननी पड़ रही है, जो उनके शासक उन्हें बता रहे हैं। ट्रम्प साफ तौर से मानते हैं कि अमेरिका को दूसरे शासकों और उनके लाचार नागरिकों के बीच के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए- वे शासक अच्छे हों, बुरे हों या घटिया। लोकतंत्र, सुराज, मानवाधिकार और उदार मूल्यों के विचारों से यह प्रस्थान शायद उतना ही अहम है जितना कुलीन अमेरिकी कारोबारियों की झोली भरने के लिए सैन्यबल और धनबल का इस्तेमाल करने की ट्रम्प की कथित धमकी।
इसलिए उनका 14 मार्च को लिया गया निर्णय कोई अचरज पैदा नहीं करता जब उन्होंने युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया के अनुदानों में कटौती करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिकी सरकार द्वारा अनुदानित समाचार प्रतिष्ठान, जैसे वॉयस ऑफ अमेरिका, रेडियो फ्री एशिया और रेडियो फ्री यूरोप अब कमजोर हो जाएंगे। ये वही प्रतिष्ठान है, जो ‘अमेरिकी मूल्यों’ के प्रसार का सबसे प्रत्यक्ष औजार हुआ करते थे। तीन पीढि़यों से अमेरिका के रणनीतिक जानकार उन ‘मूल्यों’ को शीतयुद्ध के दिनों वाले अमेरिकी ‘प्रभाव’ में अंतर्निहित मानते आए हैं। भारत भी शीतयुद्ध का एक मैदान था, जहां के ‘बुद्धिजीवियों’ को बहला फुसला कर अपने पाले में खींचने की अमेरिकी और रूसी कवायद में जाने कितनी ही जानें गईं, कितने ही लोग बेइज्जत हुए और जाने कितनों का करियर नष्ट हो गया। वह दौर दुनिया भर में ‘दिलो दिमाग’ पर कब्जे की महाशक्तियों की लड़ाई का था।
बहुत हाल तक वॉयस ऑफ अमेरिका को दूसरे देशों के ‘शासक’ अस्थिरता और विध्वंस पैदा करने वालों की आवाज के रूप में देखा करते थे। इसके उलट, तमाम ‘बागी’ और ‘असहमत’ ताकतें दुष्प्रचार के इस माध्यम पर उभरे समर्थन के स्वरों से अपने-अपने संघर्षों के लिए वैधता हासिल करती थीं। बीते वर्षों कई देशों में जो सत्ता-परिवर्तन हुए, जिन्हें अलग-अलग रंगों के नाम से क्रांतियां कहा गया, वे उसका उदाहरण हैं। मसलन, 2019-20 में हांगकांग में जो सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल मची थी, उसे हवा देने में वॉयस ऑफ अमेरिका की भूमिका को लेकर चीन अब भी बहुत नाराज है।
बहुत संभव है कि दुष्प्रचार के ऐसे माध्यमों को निपटाने के पीछे ट्रम्प प्रशासन का यह यकीन रहा हो कि इनमें लिबरल लोग भरे पड़े हैं। कारण चाहे जो हो, लेकिन दुनिया भर में तो यही संदेश गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अब प्रभाव जमाने की वैश्विक लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखता और वह लगातार इसकी मुनादी खुद कर रहा है। इसलिए मौजूदा निरंकुश शासकों तथा संभावित तानाशाहों की नजर में यह स्वागत योग्य कदम होना चाहिए।
सिर कटाकर ‘महानता’ हासिल करने की सनक में फंसे ट्रम्प के अमेरिका को समझने में ग्रीन के नायक आल्डेन पाइल जैसे लोग बेशक चकमा खा सकते हैं।
(वरिष्ट पत्रकार और स्तंभकार। विचार निजी हैं)