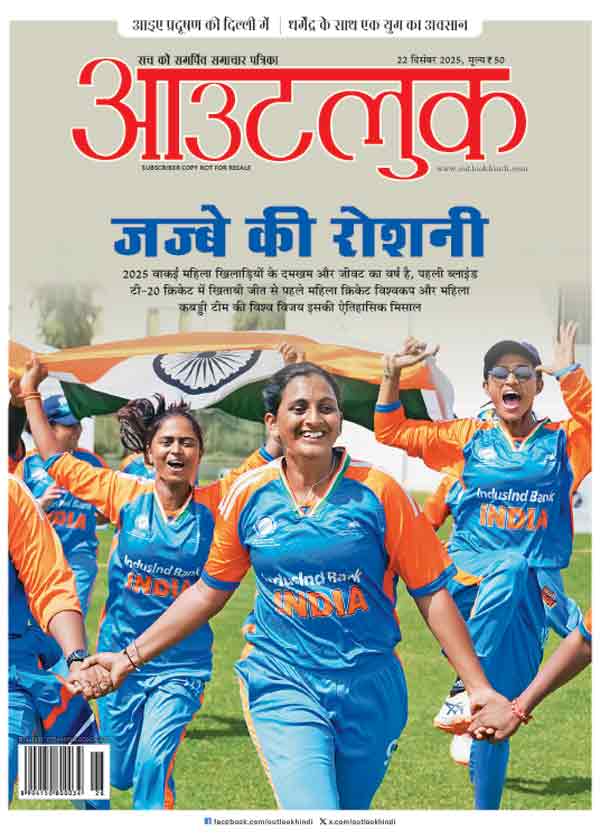अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान को ‘‘लड़ाई बंद करने" के लिए राजी करने का श्रेय लिया, न मानने पर दोनों देशों के साथ व्यापार बंद करने की धमकी दी। एक बार नहीं, बल्कि वाशिंगटन, रियाद और बाद में भी, नई दिल्ली सिर्फ दुस्साहस और बड़बोलेपन से ही नहीं चौंकी, बल्कि एक ही पलड़े पर तौले जाना सबसे हैरान करने वाला था। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने कहा, आओ, हम आप लोगों के साथ ढेर सारा व्यापार करने जा रहे हैं। इसे रोको, इसे रोको। रोकते हो, तो हम व्यापार करेंगे। नहीं रोकते, तो कोई व्यापार नहीं होगा।’’ फिर थोड़ा रुककर कहा, ‘‘और अचानक उन लोगों ने कहा, हम रोक रहे हैं।’’ ट्रम्प ने कबूल किया कि दूसरी वजहें भी थीं, ‘‘लेकिन व्यापार बड़ी वजह है।’’ पाकिस्तानी लीडरान ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिका की तारीफ की और ट्रम्प का खुलकर शुक्रिया अदा किया। लेकिन भारत इससे खुश नहीं हुआ।
फिर, भारत को पाकिस्तान के साथ नत्थी कर दिया गया, एक पलड़े पर ला खड़ा किया गया था। यह नई दिल्ली के लिए शर्मनाक था। उससे दूरी बढ़ाने के लिए दो दशकों से अधिक समय तक भारी कूटनीतिक जद्दोजहद की गई थी। ऐसा लग रहा था कि भारत के हक में स्थितियां माकूल हैं, तभी ट्रम्प ने उस पर पानी फेर दिया। भारतीय नीति-नियंताओं के लिए यह बयान कूटनीतिक भूल-चूक से कहीं बड़ा था, यह गहरी समस्या का लक्षण था।

रुख बदलाः अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
विशेषज्ञों और जानकारों की ओर से लगातार तीखे सवाल उठ रहे थे। भारतीय विदेश नीति में कहां गलती हुई? क्या भारत फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच गया है, और पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया है? अमेरिका के साथ भारत की बड़े पैमाने की वैश्विक साझेदारी के क्या मायने हैं? तनाव फौरन घटाने की अपील तो साझीदार यूरोपीय देशों, पश्चिम एशिया और धरती के दक्षिण देशों के नेताओं ने भी की। लेकिन दबाव आया तो कुछ भी काम नहीं आया।
जर्मनी में पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के रवैये के बारे में कहते हैं, ‘‘पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत के साथ हमदर्दी जताई गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे से जोड़कर देखा गया।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘हमें अपने नजरिए को मंजूर करवाने की कोशिश बढ़ानी होगी। हमें द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को यूएनएससी 1267 कमेटी के दायरे में रखने के लिए समर्थन की जरूरत है। हमें रणनीतिक साझेदारों के साथ अपने आतंकवाद विरोधी नजरिए को जोरदार ढंग से पेश करने की जरूरत है।’’

नए वर्ताकारः सुप्रिया सुले, कनिमोई, रविशंकर प्रसाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लगातार यात्राएं और वैश्विक नेताओं- ट्रम्प, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां से लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वगैरह से गलबहियां मौजूदा संकट में काम नहीं आए। सभी ने पहलगाम हमले की तो निंदा की, लेकिन पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाई। यह दौर उससे अलहदा है, जब मार्च 2000 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर कड़ा संदेश दिया था।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत अशोक मुखर्जी कहते हैं, ‘‘संकट आतंकवादी हमले का था, जिसमें निर्दोष आम लोग मारे गए। इसी मुद्दे पर कूटनीतिक प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर नहीं।’’ वे आगे कहते हैं, ‘‘अगर हम आतंकवाद से मुकाबले के लिए कार्रवाई करते हैं, तो हमारी उम्मीद यह होगी कि अमेरिका भारत के साथ एकजुटता दिखाए और पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को खत्म करने में मदद करे, जिसमें फंडिंग भी शामिल है। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए।’’ मुखर्जी की राय भारत में आम धारणा का ही आईना है।
देश में कई लोग अमेरिकी रवैए को विश्वासघात की तरह देखते हैं। आखिरकार, मोदी सरकार ने ट्रम्प को लुभाने के लिए क्या नहीं किया, हदें लांघ दीं। पहलगाम कत्लेआम के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लोगों की भावनाएं चरम पर हैं। कई भारतीय पर्यटक मौजूदा संकट के दौरान पाकिस्तान का साथ देने के कारण तुर्किए और अजरबैजान की अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। पुराने लोग पाकिस्तान के साथ अमेरिका की पिछली गहरी दोस्ती को याद करते हैं कि कैसे उसने बांग्लादेश युद्ध के दौरान खुलकर इस्लामाबाद का साथ दिया था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में फौज की ज्यादतियों की जानकारी देने के लिए वाशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों का दौरा किया था। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने रूस के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की मदद के लिए भारतीय सेना भेजने का फैसला किया। और अलग बांग्लादेश बन गया। हालांकि, यह दशकों पहले की बात है।

नए वर्ताकारः असुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, अभिषेक बैनर्जी
आज, रिश्तों में उतार-चढ़ाव के बावजूद ट्रम्प के बड़बोलेपन और हर बात का श्रेय लेने की फितरत की वजह से दिल्ली और वाशिंगटन रिश्तों को खराब नहीं होने देंगे। दोनों देशों की चीन को लेकर रणनीतिक चिंताएं साझा हैं। वाशिंगटन की भारत के साथ गर्मजोशी की वजह चीन की बढ़ती राजनैतिक और आर्थिक ताकत है, जिससे आने वाले वर्षों में अमेरिका की महाशक्ति की हैसियत को चुनौती मिल सकती है। भारत के लिए, अमेरिका के साथ दोस्ती एशिया में चीन के खिलाफ बीमा की तरह है। फिलहाल, भारत नाराज है, लेकिन कुछ हफ्तों में अमेरिकी प्रशासन की ओर से भारत को खुश करने की कोशिश हो सकती है। उसके बाद दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए काम करना होगा। व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में कुछ महीने लगेंगे। व्यापार की बातचीत से जुड़े लोगों के अनुसार, यह साल के अंत तक हो सकता है। अमेरिका की नजर भारत के विशाल बाजार पर भी है, जबकि भारत उच्च तकनीक में सहयोग के लिए अमेरिका की ओर देख रहा है, ये ऐसे मसले हैं जो संबंधों को बरकरार रखने में कारगर रहेंगे। भारत-अमेरिका संबंधों को मौजूदा संकट से पहले की स्थिति में आने में समय लगेगा।
वाशिंगटन के इलियट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की जोआना स्पीयर कहती हैं, ‘‘मुझे लगता है कि दोनों के संबंध मजबूत हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प बदलती घटनाओं से बहुत प्रभावित होते हैं और फौरन ऐसी नीतियों का ऐलान कर देते हैं जो संबंधों की मजबूती को झुठलाती हैं। भारत महत्वपूर्ण साझीदार है और अमेरिका चाहेगा कि वह चीन के खिलाफ संतुलन बनाए, इसलिए संबंधों को कमजोर करना अमेरिकी भू-रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा।’’
भारत का रवैया
भारत ने ट्रम्प को सीधे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, सरकार देश के लोगों से अमेरिका के बयान को दबाने की कोशिश में लगा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपने हवाई ठिकानों पर हमले और नुकसान के बाद संघर्ष विराम पर मजबूर हुआ। विदेश मंत्रालय ने यह तो कहा कि अमेरिकी अधिकारियों से फोन पर बात हुई, लेकिन इससे इनकार किया कि बातचीत के दौरान व्यापार को लेकर कोई बात हुई। भारत-पाकिस्तान के मुद्दों में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की गुंजाइश से भी इनकार किया गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने घोषणा की, “जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसके साथ हमारा बर्ताव द्विपक्षीय और पूरी तरह से द्विपक्षीय होगा। इस पर कई वर्षों से राष्ट्रीय सहमति है।” पाकिस्तान ने हमेशा भारत के साथ अपने विवाद को अंतरराष्ट्रीय बनाने और बीच में किसी तीसरे देश को लाने की कोशिश की है।

मेरी समझ में अगली विदेश नीति वास्तव में बड़ी सोच, लंबी सोच, लेकिन समझदारी से सोचने की होगी, एस. जयशंकर, विदेश मंत्री
प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आए, तो उन्होंने अपनी सरकार की ‘‘पड़ोस पहले’’ नीति की शुरुआत की। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित सभी दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलावा भेजा। 2015 में मोदी अफगानिस्तान की सरकारी यात्रा से वापस आ रहे थे तो क्रिसमस के दिन शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने अचानक लाहौर में उतर गए थे। लेकिन 2 जनवरी, 2016 को पठानकोट वायु सेना ठिकाने पर आतंकी हमले से शांति बहाली की कोशिशें टूट गईं। उसके बाद 2016 और 2019 में आतंकी हमलों से रिश्तों में कड़वाहट घुलती गई। मोदी का भरोसा पूरी तरह से टूट गया और भारत ने ‘‘आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते’’ की नई नीति बनाई। कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने से संबंध और खराब हो गए। अब खुलकर कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के किसी भी दुस्साहस का जोरदार जवाब दिया जाएगा।
लेकिन बाकी दुनिया इस मुद्दे को अलग नजरिए से देखती है। जॉर्ज मेसन युनिवर्सिटी के अली ममादोव कहते हैं, ‘‘कश्मीर दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट में एक बना हुआ है। वह सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती वाले क्षेत्रों में एक है और चीन से उसकी निकटता रणनीतिक जोखिम की एक और परत जोड़ती है। इसके अलावा, बगल का लद्दाख क्षेत्र स्थिति और जटिल बना देता है, जहां भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। वहां कुछ साल पहले हुईं झड़पें भी गवाह हैं कि तनाव कितनी तेजी से बढ़ सकता है।’’
संकट का दूसरा पहलू यह है कि भारत की पड़ोसी देशों से रिश्तों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। अगस्त 2014 में मोदी पहली बार नेपाल गए थे, तब वे वहां लोकप्रिय थे, लेकिन संवैधानिक संकट और भारत के नेपाल की नाकेबंदी के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। इसी तरह शेख हसीना के तख्तापलट के बाद भारत का सबसे करीबी सहयोगी बांग्लादेश अब लगभग दुश्मन देश बन गया है। मालदीव और श्रीलंका से भी द्विपक्षीय संबंधों में उतार आया है। चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति और भारत के पड़ोस में उसकी मौजूदगी ने छोटे देशों को ऐसा विकल्प दिया है, जो पहले उपलब्ध नहीं था।
भारत का रुख कैसे बदला
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने दुनिया के लिए अपने बाजार खोले, तबसे अमेरिका और पश्चिम के साथ नई दिल्ली के संबंधों में बदलाव आया। इस दौर में इजरायल के साथ संबंध बढ़ते गए हैं और फिलस्तीनी लोगों के लिए नई दिल्ली का समर्थन धीरे-धीरे कम होता गया। भारत फिलस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को फिलस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाले पहले गैर-अरब देशों में था। 1975 में दिल्ली में पीएलओ कार्यालय स्थापित किया गया था। पीएलओ प्रमुख यासर अराफात भारत के करीबी दोस्त थे। आज, इजरायल के साथ भारत की गलबहियों की वजह से फिलस्तीनी लोगों के लिए सहानुभूति घटती गई है।
अमेरिका में जो बाइडन के कार्यकाल में भारत को बहुत फायदा मिला। वह यूक्रेन युद्ध के दौरान अपने पुराने मित्र रूस के साथ खड़ा हो सका और मास्को पर वाशिंगटन के प्रतिबंधों के बावजूद कम दरों पर तेल खरीद सका। बाइडन प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ बेहद कम बातचीत की। लेकिन मनमौजी ट्रम्प के मामले में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। वे पता नहीं, कब गर्म, कब नरम रुख अपना लेंगे।
नई दिल्ली को मौजूदा संकट से कुछ सबक सीखने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति को नाराज करने की कीमत पर भी राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर लाल रेखाएं खींचना सबसे अच्छा है। ट्रम्प की टिप्पणियों पर चुप रहने या अनदेखा करने से बात नहीं बनेगी। विदेश नीति पर जयशंकर कहते हैं, ‘‘अगली विदेश नीति वास्तव में बड़ी सोच, लंबी सोच, लेकिन समझदारी से सोचने की होगी।’’ भारत को समझदारी से सोचने और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। बदलती दुनिया में आर्थिक ताकत सबसे अधिक मायने रखती है।