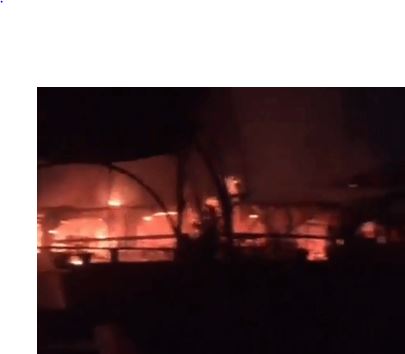रंगमंच के शिखर पुरुष इब्राहम अल्का जी ने 1967 में चेखव के प्रसिद्ध नाटक "थ्री सिस्टर्स" का मंचन किया था। वह एनएसडी मेंइस नाटक पहला प्रोडक्शन था। उससे 19 साल पहले आज़ादी के एक वर्ष बाद यह नाटक 1948 में दिल्ली में हुआ था। अल्का जी के 24 साल बाद मशहूर रंगकर्मी एम के रैना ने 1991 में इस नाटक को रोबिन दास और एस रघुनंदन ने भी एनएसडी में मंचित किया था, इसके करीब 23 साल बाद एनएसडी ने इसे फिर मंचित किया है। इस बार इसका निर्देशन जानी मानी रंगकर्मी एवम अभिनेत्री मीता वशिष्ठ ने किया।
वह रंगमंच फ़िल्म और टी वी के दर्शकों के बीच एक जाना पहचाना नाम हैं। इसलिए दर्शकों में उनक़ा यह नाटक देखने की काफी उत्सुकता था। वैसे तो यह नाटक एनएसडी के तृतीय वर्ष के छात्रों द्वारा मंचित किया गया था। यह रंगमंडल का नाटक नहीं था जहां अनुभवी और पेशेवर कलाकर हों लेकिन दर्शकों को उनके एक नाटक से उम्मीद तो थी पर क्या मीता जी उनकी उम्मीदों पर खरीं उतरीं क्योंकि कई लोगों को यह नाटक उतना पसंद नहीं आया जबकि कई लोगों को यह पसंद भी आया। यह कोई पहली घटना नहीं जब एक नाटक पर लोगों की राय अलग अलग न आई हो। वैसे मीता जी इस नाटक से काफी खुश हैं। उनकी मेहनत रंग लाई।
श्री रैना और प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक रवींद्र त्रिपाठी को यह नाटक बहुत पसंद आया लेकिन इस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रंगकर्मी आसिफ और चर्चित नाटककार राजेंश कुमार को यह नाटक कमजोर लगा। हिंदी के दो नाट्य समीक्षक तो मध्यांतर के बाद यह नाटक देख नहीं सके।इन पंक्तियों का लेखक भी यह पूरा नाटक देख नहीं सका क्योंकि यह नाटक मंच पर टेकऑफ नहीं कर पाया। इस नाटक की शुरुवात रूसी समाज के एक पार्टी नृत्य से होती है और वह एक प्रभाव शाली दृश्य था।
इसमें कोई शक नहीं कि इस नाटक का सेट बहुत सुंदर था कॉस्ट्यूम भी बेहतरीन था और संगीत तथा प्रकाश व्यवस्था भी ठीक थी लेकिन अधिकतर पुरुषकलाकारों का अभिनय और संवाद कमजोर था।
चेखव ने 1900 में यानी आज से 124 साल पहले यह नाटक लिखा था जो 1901 में मास्कों थिएटर में खेला गया था ।देखते देखते यह नाटक दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ और अब तक न जाने कितनी बार खेला गया। यह नाटक रूस की अक्टूबर क्रांति 1917 से पहले लिखा गया था जिसमें एक मध्यवर्गीय परिवार की तीन लड़कियों की कहांनी है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने जीवन में प्रेम और विवाह मेसुख की तलाश करती हैं लेकिन उन्हें यह सुख नहीं मिल पाता और उनके सपने टूट ते हैं।इस दृष्टि से यह एक ट्रैजिक कहांनी है। लेकिन क्या मीता जी इस ट्रेजेडी को उभार पायीं।उनक़ा यह नाटक बहुत ही मंथर गति का था और वह कथ्य को पूरी तरह उभारने में सफल नहीं हो पाया।दर्शकों को बांधने में कामयाब नहीं रहा। लेकिन एम के रैना इस राय से सहमत नहीं।वे कहते हैं आखिर मैँ एक दर्शक भी तो हूँ।मैंने कल यह नाटक देखा। मुझे बहुत पसन्द आया। यह छात्रों का नाटक था और उनक़ा अभिनय अच्छा था।एक दो जगह प्रकाश व्यवस्था अच्छी नहीं थी लेकिन कुल मिलाकर यह नाटक अच्छा था।
रवींद्र त्रिपाठी का कहना है कि यह एक वंडरफुल नाटक है। यह यथार्थवादी नाटक है। पहली बात यह है कि यह छात्रों का नाटक है इसलिए इसे उस रूप में देखा जाना चाहिए। एनएसडी के छात्र क्या सीख पाये यह महत्वपूर्ण बात है। मेरे हिसाब से सबका काम अच्छा है।मुझे तो दिनेश खन्ना द्वारा निर्देशित तीन बहनों से यह अच्छा लगा। पर एम एक रैना अपने द्वारा निर्देशित तीन बहनों से इस नाटक की तुलना नहीं करना चाहते हैं। वे कहते हैं यह तुलना ठीक नहीं। वसुधा के संपादक और इप्टा से जुड़े विनीत तिवारी का कहना है कि इसमें कसावट की कमी है।
सब कुछ बहुत साफ़-सुथरा। सेट, साउंड, लाइट, मंच पर मौजूद हर पात्र, उसके परिधान, उनकी ज़ुबान (हालाँकि स और श में और ज और ज़ में थोड़ी गलतियाँ रह गईं थीं, लेकिन श्रोताओं को भी कौन इतना पता है भला), उनके हाव-भाव, संगीत, अभिनय, सभी कुछ। लेकिन फिर भी कहीं कुछ था जो नाटक को दर्शंकों से नहीं जोड़ पा रहा था। मंच के अलावा नाटक में अगर किसी स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है तो वो एकाध बार ही किया जाता है और वो भी दर्शकों की दृष्टि तन्द्रा तोड़ने के साथ-साथ कुछ बहुत प्रभावी दिखने के लिए, मसलन दर्शकों के बीच से या पार्श्व से कलाकार की एंट्री। इस नाटक में एंट्री एग्जिट के लिए एक तीसरी जगह (मंच के सामने रैंप बनाकर) का इस्तेमाल किया गया और वो इतनी बार किया गया कि लगता था किरदार बेचारा बार-बार बाहर काहे जा रहा है, नीचे उतरकर सामने की सीट पर ही बैठ जाए।
नाटक मनुष्यों की प्रवृत्ति, बदलते हुए रिश्तों, नयी प्रगाढ़ताओं और पुराने मधुर संबंधों में आने वाले कसैलेपन आदि चीज़ों को व्यक्त करता है। लेकिन अनेक तरह के दोहराव नाटक को लम्बा खींच देते हैं, और चरित्रों से जुड़ने में अवरोध पैदा करते हैं। साथ ही जब आप एक विदेशी नाटक को हिंदी में कर रहे हैं तो कुछ जगह अनुवाद मूल की शुद्धता के आग्रह से भरा हो और कुछ जगह कोई चलताऊ शब्द अपना लिया जाए, ये मिलावट नहीं हो सकती। उससे दर्शक न ये मान पाता है कि ये उसे इस दृष्टि से देखना है कि ये विदेशी पृष्ठभूमि का है और न ही ये कि ये अपनी ही ज़मीन का है। इस वजह से संवादों से अजनबियत बन जाती है (जैसे बार-बार बीवी को लाजवाब कहना आमतौर पर हिंदी में नहीं होता, उसी तरह सुलटाना शब्द का प्रयोग बिलकुल ही मेल नहीं खाता बाकी संवादों से, ऐसे और भी प्रसंग हैं।)
थोड़ा-सा चरित्रों के बारे में - तीनों बहनों का अलग-अलग चरित्र और स्वाभाव तो उभरता है लेकिन एक चीज़ तीनों की समान है - तीनों जूते पहनकर ही सोतीं और उठती हैं। यह भी थोड़ा विचित्र लगता है। सवा तीन घंटे के इस नाटक में कसावट की कमी महसूस हुई। पर राजेश कुमार और आसिफ इस नाटक को लेकर अधिक आलोचनात्मक हैं। राजेंश का कहना है कि यह नाटक दर्शकों को बांधने में सफल नहीं रहा।नाटक हमेशा दर्शकों की कौटियों पर कसा जाना चाहिए। अगर यह केवल छात्रों के लिए है तो फिर क्यों टिकट का इंतज़ाम क्यों। जाहिर है यह दर्शकों के लिए भी है।उनक़ा कहना है कि इसमें कथ्य उभर नहीं पाया क्योंकि निर्देशन कमजोर है।मीता एक अच्छी अभिनेत्री हैं पर अच्छा अभिनेता अच्छा निर्देशक हो जरूरी नहीं।"
आसिफ का कहना है कि इस नाटक में निर्देशक रूसी समाज की संवेदना को समझ नहीं पाया। इसमें कथ्य उभर नहीं पाया। दरअसल यह नाटक बहुत लंबा और खींचा हुआ था।इसे कसा होना चाहिए।लेकिन मीता बशिष्ठ इस नाटक से बहुत खुश हैं और संतुष्ट भी हैं।
उनक़ा कहना है कि दिल्ली में रहने वाले रूसी समुदाय ने इसे बहुत पसंद किया वे पहले दिन आये थे।कल लोग साढ़े तीन घण्टे अंत तक इसे देखते रहे। जहां तक आम दर्शकों की बात है। वह तो लोकप्रिय फिल्में पसंद करता है। मैं 40 दिन तक इसके प्रोडक्शन में लगी रही।।सभी कलाकारों ने बढ़िया काम किया।"
वैसे उनक़ा कहना है कि उन्होंने पहले कभी तीन बहनों का मंचन नहीं देखा कभी और न ही उसमें काम किया। वैसे दिल्ली में इस नाटक का पहला शो 1948 में हुआ था। एल टी जी की स्थापना जब हुई थी तो इसी नाटक के प्रदर्शन से हुई थी। दुर्भाग्य से उस दौर के वीडियो नहीं कि पता चले वह कैसा था। एक ही नाटक की कई प्रस्तुतियां होती हैं ,इसलिए इसे इस रूप में भी देखा जाना चाहिए।