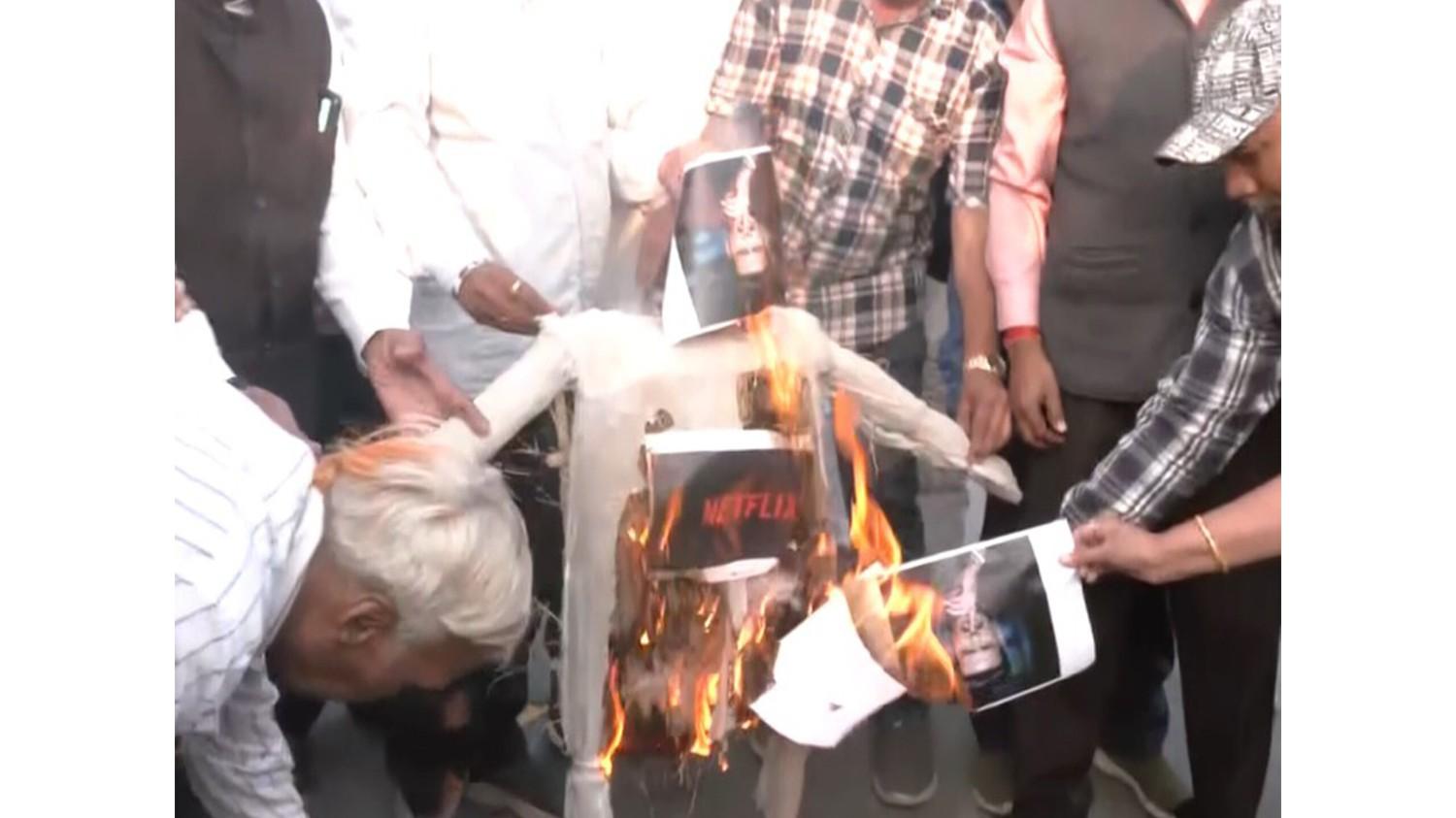यह फिल्म शार्देंदू बंद्योपाध्याय की ब्योमकेश बक्शी सीरिज की दो अलग-अलग कहानियों को मिलाकर बनाई गई है। दो कहानियों को मिलाने के चक्कर में इसमें इतनी उलझने हो गई हैं कि जबतक दर्शक एक जटिलता से जूझते हैं तब तक कहानी दूसरा मोड़ ले चुकी होती है। हालांकि इसके लिए दिबाकर की तारीफ करनी होगी कि इंटरवल से पहले कहानी तेज गति से बढ़ती है और वह दर्शकों को पूरी तरह कुर्सी से चिपकाए रखते हैं। इंटरवल के बाद कहीं न कहीं कहानी पर से दिबाकर की पकड़ छूटती है क्योंकि ध्यान से फिल्म देखने वाले दर्शकों को क्लाइमेक्स से पहले ही पता चल जाता है कि असली खलनायक कौन है।
अगर कहानी की बात करें तो फिल्म की शुरुआत 1942 के कोलकाता शहर में होती है जहां चीन के ड्रग माफिया का 500 किलो अफीम का कंसाइनमेंट उनके विरोधी गुट का माफिया डॉन हिंसक झड़प के जरिये झपट लेता है। ब्योमकेश बक्शी (सुशांत सिंह राजपूत) अभी-अभी कॉलेज से निकला युवक है जिसके पास कोई काम नहीं है और इसके कारण उसकी प्रेमिका कहीं और शादी कर रही होती है। इस तनाव से बाहर आने के लिए वह अजित बनर्जी (आनंद तिवारी) नामक एक युवक का केस लेता है जिसके पिता भुवन बनर्जी रहस्यमय हालात में गायब हो गए हैं। ब्योमकेश उस घर में पहुंचता है जहां अश्विनी बाबू कुछ और लोगों के साथ रहते हैं। कोलकाता के इस बासा के मालिक हैं एक चिकित्सक अनुकूल गुहा (नीरज काबी) जिनके साथ ब्योमकेश की मित्रता हो जाती है। बासा में भुवन बाबू के साथ कुछ और लोग भी रहते हैं जिनमें एक है कनाई देव (मियांग चेंग) जो अफीम बेचने का धंधा करता है। भुवन बाबू की तलाश के दौरान ब्योमकेश स्थानीय राजनीतिज्ञ गजानंद सिकदर की फैक्ट्री तक पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात गजानंद की रखैल और ग्लैमरस फिल्म अभिनेत्री अंगूरी (स्वस्तिका) से होती है। इसी क्रम में वह गजानंद की भांजी सत्यवती (दिव्या) और उसके महत्वाकांक्षी भांजे सुकुमार (शिवम) से भी मिलता है। इतने सारे चरित्रों के बीच उसे असली खलनायक का पता लगाना है।
अभिनय की बात करें तो मानना पड़ेगा कि सुशांत राजपूत अपनी पिछली फिल्मों से इसमें मीलों आगे बढ़े हैं और अपने चरित्र में पूरी तरह रम गए हैं। अंगूरी के किरदार को स्वस्तिका ने शानदार तरीके से निभाया है। अन्य चरित्र भी अपनी भूमिकाओं में फिट रहे हैं। इस बात के लिए दिबाकर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने फिल्म में कोई भी गीत डालने से परहेज किया है क्योंकि बॉलीवुड स्टाइल के गीत ऐसी जासूसी कहानियों की गति को धीमा कर देते हैं। दिबाकर बनर्जी 1942 के कोलकाता को भी पर्दे पर बखूबी उतारने में सफल रहे हैं। सड़कों पर चलते ट्राम और उस दौर की कारें आज की पीढ़ी का भी ज्ञानवर्धन कर सकती है। कुल मिलाकर फिल्म अपने संपूर्ण प्रस्तुतिकरण में देखने लायक है।