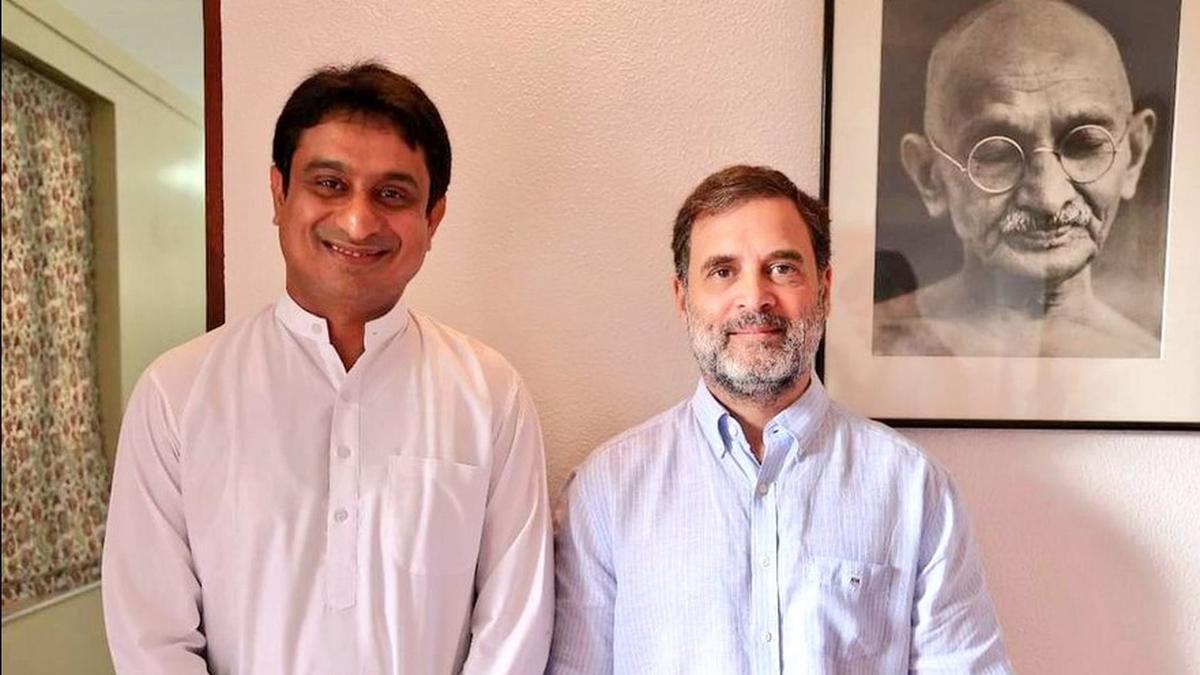हिन्दी सिनेमा में बायोपिक फ़िल्मों की परंपरा बहुत पुरानी रही है। तकनीकी नज़र से देखें तो बायोपिक फ़िल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। उन्होंने सनातन धर्म की कहानियों पर फ़िल्में बनाकर भारतीय सिनेमा की शुरुआत की। यह फ़िल्में तकनीकी दृष्टि से बायोपिक फ़िल्में ही थीं। तब से शुरू हुई बायोपिक परंपरा में राजनीति, धर्म, खेल और अपराध से जुड़े लोगों के जीवन पर बायोपिक बनाने का काम निरंतर चल रहा है। दर्शक इन फ़िल्मों को पसन्द करते हैं। उन्हें अपने प्रिय शख्सियतों के जीवन सफर को करीब से देखने का अवसर मिलता है। बायोपिक फ़िल्मों की इसी शृंखला में एक महत्वपूर्ण फ़िल्म का नाम आता है। इस शृंखला में फ़िल्म “ पान सिंह तोमर “ का नाम आता है। स्टेपलचेस दौड़ के राष्ट्रीय विजेता, फ़ौजी और बागी पान सिंह तोमर के जीवन पर आधारित फ़िल्म “ पान सिंह तोमर “ कई मायने में विशेष है। हिन्दी सिनेमा में बायोपिक बनाने की जो परंपरा रही है, उसमें लोकप्रिय और चर्चित हस्तियों को ही बायोपिक फ़िल्म के विषय के रूप में चुना जाता है। चूंकि हिन्दी सिनेमा अन्य उद्योगों की तरह की एक इंडस्ट्री है, जिसके केंद्र में कारोबार है इसलिए निर्माता निर्देशक चर्चित हस्तियों की लोकप्रियता भुनाकर पैसा कमाना चाहते हैं। यह पक्ष हमेशा उनके ज़हन में रहता है। लेकिन इसके विपरीत फ़िल्म पान सिंह तोमर का केंद्रीय किरदार पान सिंह तोमर एक गुमनाम और भुला दिया गया नायक है। लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। न वो लोकप्रिय है और न चर्चित। ऐसे व्यक्ति को लेकर बायोपिक फ़िल्म बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। न सिर्फ़ इसलिए कि उसके विषय में जानकारी जुटाना कठिन होता है बल्कि उस के ऊपर फ़िल्म बनाने के लिए निर्माता खोजने से लेकर, फ़िल्म की मार्केटिंग और फ़िल्म को थियेटर में रिलीज़ करना एक संघर्षपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। इस नाते फिल्मकार के जुनून और समर्पण की प्रशंसा लाज़िमी महसूस होती है।
फ़िल्म “ पान सिंह तोमर “ के विषय में बात करें तो इसके निर्माण की एक लंबी और संघर्षपूर्ण कहानी है। यह कहानी शुरू होती है निर्देशक शेखर कपूर की फ़िल्म “ बैंडिट क्वीन “ से। बैंडिट क्वीन डाकू और राजनेत्री फूलन देवी के जीवन पर आधारित फ़िल्म थी। इस फ़िल्म के निर्माण हेतु रिसर्च टीम का अहम हिस्सा थे तिग्मांशु धूलिया। तिग्मांशु धूलिया ने चंबल के बीहड़ में बैंडिट क्वीन के लिए रिसर्च करते हुए, बागी डाकुओं के विषय में शोध किया। तिग्मांशु ने डाकुओं के रहन सहन, पहनावे, ख़ान पान, नेतृत्व नियम, कानून, मापदंड से लेकर मानवीय पक्ष पर गहन अध्ययन किया। इसी दौरान तिग्मांशु को पहली बार पान सिंह तोमर का नाम सुनाई दिया था। लोग पान सिंह तोमर के विषय में सतही जानकारी रखते थे। लोगों की नज़र में पान सिंह बीहड़ का एक बागी था। एक आदमी, जिसने परिवारिक कलेश और सरकारी निकम्मेपन के कारण बागी होना चुन लिया था। इससे अधिक लोग नहीं जानते थे। तिग्मांशु भी चूंकि फूलन देवी और बैंडिट क्वीन में व्यस्त थे इसलिए पान सिंह तोमर के विषय में ज़्यादा तफ्तीश नहीं हुई। लेकिन कुछ तो ऐसा था पान सिंह तोमर की शख्सियत में, जो तिग्मांशु की स्मृतियों में पान सिंह तोमर रह गए।
बैंडिट क्वीन का काम पूरा हुआ। फ़िल्म रिलीज़ हुई और इसने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। यह सफलता कई मायनों में ख़ास थी। इससे पहले भी डाकुओं के जीवन पर हिंदी फ़िल्में बनी थीं। फ़िल्में जिनमें विनोद खन्ना और सुनील दत्त सरीखे रौबीले अभिनेता होते थे। यह सब फ़िल्में दर्शकों का प्यार भी हासिल करती और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे भी गाड़ती थीं। लेकिन यह फ़िल्में खालिस कमर्शियल होती थीं। इनके मूल में कारोबार होता था। यह हिन्दी सिनेमा में शायद पहली बार हो रहा था कि डाकुओं को केंद्र में रखकर एक कलात्मक फ़िल्म बनाई गई थी, जिसे देशभर में समर्थन मिल रहा था। यह नई शुरुआत थी। इस फ़िल्म ने हिन्दी सिनेमा को मनोज बाजपेई सरीखे प्रतिभावान और नैसर्गिक अभिनेता देने का काम किया। इस फ़िल्म की कामयाबी ने तिग्मांशु के विश्वास को मजबूत करने का काम किया। तिग्मांशु के गीले मन की कच्ची मिट्टी उस सांचे में ढल रही थी, जिसे आने वाले वर्षों में पान सिंह तोमर जैसी कलाकृति का सृजन करना था।
तिग्मांशु ने एक रोज़ “ संडे “ पत्रिका में पान सिंह तोमर पर लिखा गया लेख पड़ा। लेख पढ़कर स्मृतियों के आकाश में आकाशीय बिजली कड़क उठी। तिग्मांशु पान सिंह तोमर पर फ़िल्म बनाने के लिए छटपटाने लगे। यह बेचैनी और छटपटाहट ज़रूरी थी। इसके बगैर पान सिंह तोमर पर फ़िल्म बनना संभव नहीं था। तिग्मांशु पान सिंह तोमर पर फ़िल्म बनाने के विचार को लेकर संकल्प कर चुके थे। लेकिन फ़िल्म निर्माण के लिए जिस स्तर पर शोध और अन्वेषण करना था, वह अत्यधिक धन और संसाधन की मांग करता था। ज़रूरी था कि कोई प्रोडक्शन हाउस इस शोध को स्पॉन्सर करे, जिससे कि फ़िल्म की कहानी के लिए सभी आवश्यक तत्व जुटाए जा सकें। फ़िल्म बनाने से अधिक ज़रूरी यह था कि फ़िल्म प्रमाणिकता के साथ बनाई जाए। जिससे वह किसी भी कसौटी और पैमाने पर खरी उतरे। तिग्मांशु ने बहुत दौड़ भाग की लेकिन निराशा ही हाथ लगी। यह वो दौर था, जब फॉर्मूला फ़िल्मों पर पैसा लगाया जाता था। नए विचार का समर्थन करना बेवकूफी और पैसों में आग लगाना समझा जाता। तिग्मांशु के लिए यह एहसास तोड़ देने वाला था। लेकिन यह तो युद्ध था। विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने का युद्ध। तिग्मांशु ने निर्णय किया कि वह बॉलीवुड में फ़िल्में बनाकर पैसा जमा करेंगे और फिर एक दिन ज़रूर पान सिंह तोमर पर फ़िल्म बनाएंगे। समय बीतने लगा और देखते ही देखते कुछ वर्षों में तिग्मांशु धूलिया हिन्दी सिनेमा में अपनी एक जगह, एक विशेष शैली विकसित करने में कामयाब हुए। इस कामयाबी का नतीज़ा था कि तिग्मांशु को यूटीवी मोशन पिक्चर्स का साथ मिला। रोनी स्क्रूवाला ने पान सिंह तोमर के विचार को समर्थन दिया और फ़िल्म के लिए शोध और अन्वेषण कार्य शूरू हुआ। तिग्मांशु और उनकी टीम ने बीहड़ में दिन गुज़ारे। डाकुओं के जीवन पर अध्ययन किया। तिग्मांशु पान सिंह तोमर के परिवार से मिले। उनकी पत्नी और बेटे से मिले। तिग्मांशु पान सिंह तोमर के फौज़ के दिनों के साथियों से मिले। उन साथियों से भी मिले, जो पान सिंह तोमर के साथ रेस के मैदान में दौड़ लगाते थे। तिग्मांशु ने सभी से पान सिंह तोमर के बारे में उनके विचार सुने। पान सिंह तोमर से जुड़ी कहानियां सुनी। धीरे धीरे पान सिंह तोमर की शख्सियत से तिग्मांशु धूलिया की पहचान हो रही थी। तिग्मांशु ने प्रमाणिक जानकारी हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फ़िल्म के लिए भाषा, रहन सहन, अंदाज़, खान पान, कपड़े, मानवीय पक्ष, ईश्वर और प्रकृति के प्रति आस्था, मान्यताओं पर पारखी नज़र डाली गई। इस भागीरथ प्रयास के बाद तैयार हुई पान सिंह तोमर की फ़िल्म की कहानी।
फ़िल्म की कहानी को तिग्मांशु ने काबिल स्क्रीनराइटर संजय चौहान के साथ लिखा। एक एक सीन, एक एक इमोशन था। इसलिए बहुत संवेदनशील ढंग से कहानी के स्क्रीनप्ले और संवाद लिखे गए। यह इतिहास के नायक को फिर से ज़िंदा करने का एक प्रयास था। इसमें संवेदनाओं और नमी की भी उतनी ही ज़रूरत थी, जितनी ही जागरूकता और सतर्कता ज़रूरी थी। फ़िल्म की कहानी लिख लेने के बाद फ़िल्म के किरदारों की कास्टिंग की बात आई। सही कास्टिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। फिल्म निर्देशक का माध्यम है। अगर अभिनेता अयोग्य हैं तो निर्देशक और लेखक का विज़न कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि सही कलाकारों की कास्टिंग हो। तिग्मांशु जानते थे कि यह फ़िल्म बीहड़, धूल, धूप, पसीने और दौड़ भाग करते हुए शूट होनी है। इसलिए इसमें लिजलिजे कलाकार नहीं लिए जा सकते। इसमें केवल और केवल सशक्त और जुनूनी कलाकारों को शामिल किया जा सकता है। जो खून और पसीना बहाने में झिझके नहीं। इसी कड़ी में पान सिंह तोमर किरदार के लिए इरफान ख़ान को लिया गया। पान सिंह तोमर के लिए इरफान खान से योग्य और कोई नहीं था। तिग्मांशु और इरफान एक दूसरे को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दौर से जानते थे। दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। ऐसी दोस्ती कि दोनों एक दूसरे की ख़ामोशी का अर्थ बता दें। तिग्मांशु के विज़न को समझने और उसे कैमरे के आगे हुबहू अभिव्यक्त करने के इरफान ख़ान की सुपात्र थे। इसी तरह माही गिल, विपिन शर्मा, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, ज़ाकिर हुसैन, राजेन्द्र गुप्ता और रवि शाह की कास्टिंग हुई। यह लोग सुपात्र भी थे, समर्पित भी, मेहनती भी और बजट में भी थे।
कास्टिंग के बाद फ़िल्म का निमार्ण शुरू हुआ। फ़िल्म बनाते हुए दिक्कतें आईं। शारीरिक श्रम इतना अधिक था कि इरफान ख़ान के लिए यह किरदार उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य साबित हो रहा था। जितनी ट्रेनिंग और भाग दौड़ थी, उससे इरफान चोटिल हुए और बार बार घायल होकर फिर से मैदान पर लौटे। प्रमाणिक तौर पर फ़िल्म बनाने के लिए रुड़की से लेकर बीहड़ में वास्तविक जगहों पर दृश्य फिल्माए गए। यह काम कठिन था और धैर्य की मांग करता था। खैर इन सब संघर्षों में फ़िल्म का निमार्ण हुआ। अब फ़िल्म की रिलीज़ की बारी थी। फ़िल्म की रिलीज़ के लिए उपयुक्त समय बहुत ज़रूरी था। किसी भी तरह की जल्दीबाजी के कारण सारी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। यही कारण है कि जिस वर्ष तिग्मांशु पान सिंह तोमर को रिलीज़ करना चाहते थे, उस वर्ष अधिक फिल्मों के रिलीज़ होने के कारण, तिग्मांशु ने पान सिंह तोमर की रिलीज़ स्थगित कर दी। तिग्मांशु चाहते थे कि पान सिंह तोमर को उचित स्पेस मिले, जिससे दर्शक का ध्यान पूर्ण रूप से पान सिंह तोमर पर हो। पान सिंह तोमर फ़िल्म फेस्टिवल में दिखाई जा रही थी और इसे दर्शकों की अद्भुत प्रतिक्रिया मिल रही थी। इसे देखकर तिग्मांशु धूलिया का विश्वास बहुत बढ़ गया था। आख़िर 2 मार्च 2012 को वह तारीख़ आई, जब पान सिंह तोमर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई।
फ़िल्म की रिलीज़ के बाद दर्शकाें और समीक्षकों ने इसे खूब पसंद किया। पान सिंह तोमर अपने समय में अपनी तरह की इकलौती फ़िल्म थी। फिल्म की कहानी, किरदारों का अभिनय, भाषा, संगीत सब कुछ बहुत असली था। फ़िल्म की कहानी पान सिंह तोमर के शुरुआती जीवन से शुरू होती है। पान सिंह तोमर फ़ौज में भर्ती होते हैं और कई वर्षों के बाद घर लौटते हैं। घर वाले उनके जीवित होने की उम्मीद जैसे छोड़ ही चुके थे। इस आगमन से पान सिंह तोमर के जीवन और परिवार में खुशियां लौट आती हैं। परिवार का विस्तार होता है और पान सिंह पिता बनते हैं। उधर फ़ौजी ज़िंदगी में पान सिंह की ज़्यादा दिलचस्पी भोजन में होती है। लेकिन फौजियों के लिए भोजन की एक सीमा रहती है। तब पान सिंह तोमर खेलों की टफ आगे बढ़ते हैं। यह बदलाव केवल भोजन के लिए होता है। खेलों में कोई विशेष रुचि नहीं होती पान सिंह तोमर की। लेकिन जैसे जैसे जीत का, मान सम्मान का स्वाद मिलता है पान सिंह को, वैसे वैसे पान सिंह का पूरा शरीर दौड़ने लगता है। आत्मा दौड़ने लगती है। यह बहुत अहम पहलु है फ़िल्म का। पान सिंह तोमर को उसके गांव में कभी भी इज़्ज़त नहीं मिली। उसे भगौड़ा कहा गया। लेकिन अब जो वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहा था, वह उसके घायल आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की मरहम पट्टी कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर वह हुआ जो अधिकांश तौर पर भारतीय समाज और विशेष रूप से हिंदी पट्टी की कहानी है। भाई, चाचा, ताऊ के द्वारा ज़मीन हड़पने की घटनाओं का हमारे समाज में लंबा इतिहास रहा है। इससे हंसते खेलते हुए घर टूट जाते हैं। ज़िंदगियां तहस नहस हो जाती हैं। सो पान सिंह तोमर की जिंदगी भी तहस नहस हो गई। फ़ौज की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया, दौड़ना छूट गया और मां पर हुए जुल्म और प्रशासन के निक्कमेपन के बाद हाथ में आ गई बंदूक। पान सिंह तोमर बागी हो गए और निकल पड़े बीहड़ में अपने हिस्से की दुनिया जीतने, अपने हिस्से के अधिकार पाने। लेकिन यह सफर इंतकाम हासिल करने पर नहीं रुका। यह रुका पान सिंह तोमर की मौत पर।
फ़िल्म की कहानी अजीब सी टीस पैदा करती है। आप अफ़सोस से भर जाते हैं। आम तौर पर हम अपने नायक को दुनिया से लड़ते देखते हैं। यहां लेकिन ठीक उलट था। पान सिंह तोमर फ़ौज में गए, खेलों में आए, नेशनल चैंपियन बने। उन्हें फ़ौज और फील में सहयोगी मिले। किसी से ख़ास बैर या दुश्मनी नहीं रही। लेकिन घर के कलेश ने पान सिंह तोमर की खुशियों को, उनके सपनों को लील लिया। फिल्म की कहानी से पान सिंह तोमर के मानवीय पक्ष की सुंदर झलक मिलती है। ऐसे दो मुख्य प्रसंग आते हैं, जब पान सिंह महिलाओं की इज़्ज़त और आबरू के लिए उत्तेजित हो जाता है। वह अपने अफसरों की , गुरू की लाख बात मानता है लेकिन जब बात स्त्री के सम्मान की होती है तो वह अपने सपनों का त्याग भी करता है और बुलंद स्वर में आवाज़ भी उठाता है। यही अदा पान सिंह तोमर को ख़ास बनाती है। पान सिंह तोमर के संस्कार जीवित हैं। वह अंत तक दुश्मन हो चुके उसके परिवार वालों से सुलह चाहता है। भयंकर उत्पीड़न के बावजूद वह हत्या का रास्ता नहीं चुनता। बागी होने के बाद भी पान सिंह तोमर बच्चों, महिलाओं और निर्दोषों की हत्या नहीं करता। यह पान सिंह तोमर के संस्कार ही हैं।
पान सिंह तोमर की रिसर्च दिखती है, फिल्म की भाषा में, फ़िल्म के पहनावे में। फ़िल्म में जिस तरह से सभी किरदार बीहड़ की भाषा में रचे बसे दिखते हैं, वह सुख देता है। आज मेक अप और कॉस्ट्यूम से बाहरी आवरण तो तैयार हो जाया करता है लेकिन जैसे ही किरदार मुंह खोलते हैं, वैसे ही उनका नकलीपन सामने आ जाता है। यही आज हर जगह देखने को मिलता है। पान सिंह तोमर में जब आप इरफ़ान खान को देखते हैं तो आपको इरफ़ान नहीं दिखते बल्कि पान सिंह तोमर दिखता है। यह कमाल इरफ़ान की शख्सियत का तो है ही लेकिन इसमें बड़ा रोल भाषा का है। पान सिंह के अलावा रवि शाह, राजेंद्र गुप्ता, माही गिल और विपिन शर्मा भी अपनी भूमिका में बेहद ईमानदार लगते हैं। अभिनय देखते हुए एक बार यह भी महसूस होता है कि इस फ़िल्म पर शायद प्रकृति की अनुकंपा है। नहीं तो हर एक पहलु का सुंदर और सटीक होना, कठिन ही होता है।
पान सिंह तोमर फ़िल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि यह नायक की छवि सुधार के लिए बनी फ़िल्म नहीं है, जैसा कि समकालीन दौर में चलन है। इसमें जो भी है, जैसा भी आपके सामने है। आप अपने विवेक के आधार पर पान सिंह तोमर के आकर्षण में कैद हो जाते हैं। पान सिंह तोमर जैसी फिल्में रोज़ रोज़ नहीं बना करती। यह संभव ही नहीं है। लेकिन यह ज़रूर संभव है कि कला के क्षेत्र में मौजूद लोग उस स्तर को छूने का प्रयास तो करें ही, जो पान सिंह तोमर ने स्थापित किया है। लेकिन दुखद बात यही है कि पैसा कमाने की अंधी दौड़ में कला कहीं पीछे छूट गई। पान सिंह तोमर को बने हुए 10 से ज्यादा साल बीत गए हैं और हमें ऐसी कोई बड़ी फ़िल्म हिंदी सिनेमा में नहीं दिखती, जो उसी ईमानदारी से किसी गुमनाम नायक या नायिका के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई हो।