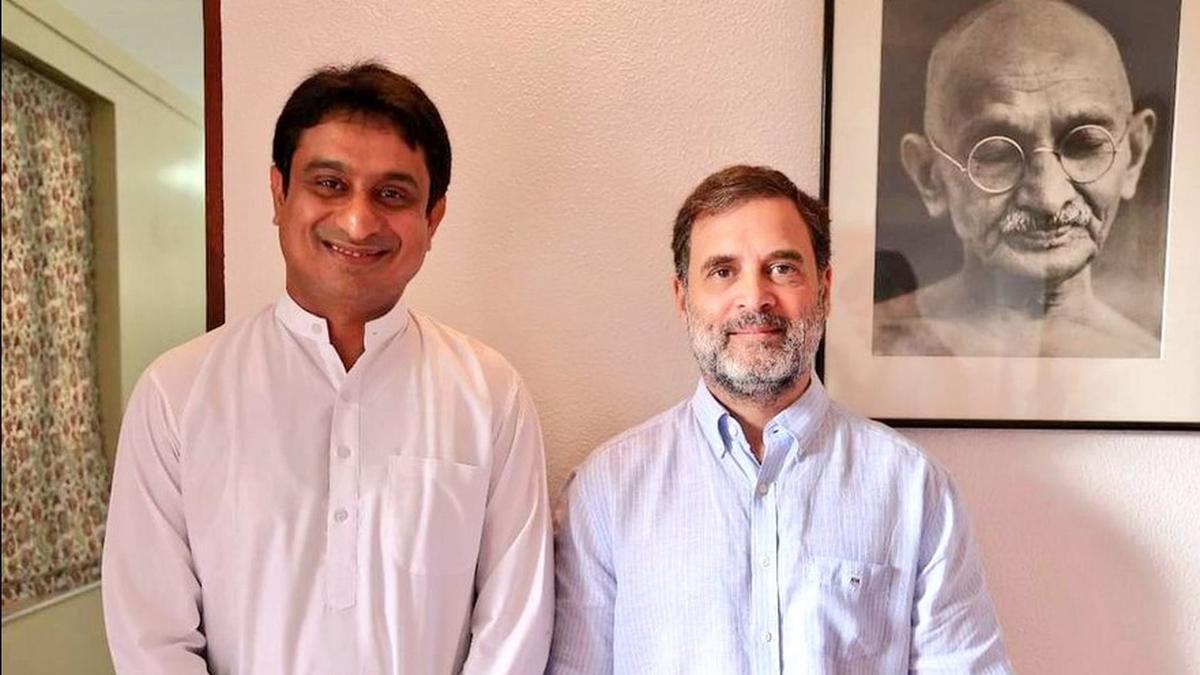भारतीय जनता पार्टी कई महीने पहले घोषित कर चुकी है कि अब उसकी सदस्य संख्या दस करोड़ से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखा जाने और गुरु दक्षिणा देने वाले स्वयंसेवकों की अनुमानित संख्या करीब साठ लाख है। उनका कोई रिकार्ड-रजिस्टर नहीं होता, लेकिन चुनाव के दौरान वे भाजपा को सत्ता दिलाने के लिए हरसंभव सहायता करते हैं। इसी तरह सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस पार्टी भी अपनी सदस्य संख्या दो-ढाई करोड़ से कम नहीं बताती। कागज पर ही सही उनके नाम का चंदा लेकर बही-खाते में दिखाया जाता है। दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के अलावा व्यक्ति केंद्रित प्रभावी क्षेत्रीय दल हैं, जिनके लाखों सदस्य और समर्थक अवसर आने पर जान न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। व्यक्ति केंद्रित पार्टी में तो 'देवी-देवता’ की तरह शीर्षस्थ नेता की पसंदगी और नाराजगी के आधार पर कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनने के अवसर मिलते हैं अथवा पार्टी की प्राथमिकताएं तय होती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक कही जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों को क्या अब संगठन के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रह गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि पार्टी के बड़े नेता भी स्पष्ट शब्दों में कहने लगे हैं कि हम चुनाव की तैयारी और उम्मीदवार के चयन के लिए निरंतर सर्वेक्षण करवा रहे हैं। मतलब लाखों का नहीं करोड़ों रुपयों का खर्च किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सर्वेक्षण करने वाले पचीसों पुरानी-नई एजेंसियां सशुल्क सेवा देने लगी हैं। कुछ एजेंसियां संबंधित पार्टियों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जुड़े लोगों ने ही बना ली। उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता भी बनी रहती है। पेशेवर एजेंसियों के लिए यह धंधा अच्छा है। वे नेताओं, दलों के लिए ही नहीं अपनी सर्वे रिपोर्ट रंग-रूप देकर विदेशी दूतावासों, निजी कंपनियों को भी बेच देती हैं।
सवाल यह है कि गांव, मोहल्ले, कस्बे, शहर, महानगर में वर्षों तक रहने वाले पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता क्या स्थानीय मुद्दों, समस्याओं, क्षेत्र में समर्पित भाव से काम करने वाले व्यक्तियों की जानकारी क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेताओं को नहीं दे सकते हैं? नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, ज्योति बसु जैसे नेताओं को लंबे सार्वजनिक जीवन में अपनी पार्टियों के लिए सर्वेक्षण की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्या उन्होंने पार्टी की सही प्राथमिकताएं तय नहीं की या सही उम्मीदवारों को नहीं चुना? कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में डॉ. शंकरदयाल शर्मा अथवा भाजपा अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे को हर प्रदेश ही नहीं जिला स्तर तक के नेताओं और समस्याओं की जानकारी कैसे मिल जाती थी? वे कार से यात्रा कर रहे हों या हेलीकॉप्टर से- चालक को सही रास्ते तक कैसे बता देते थे? इसकी वजह थी, उन्होंने वर्षों तक हर प्रदेश में जमीनी यात्रा के साथ जमीनी कार्यकर्ताओं से जीवंत संपर्क रखा। दिल्ली में रहने पर हर सुबह-शाम पचासों कार्यकर्ताओं से मिलने में उन्हें कभी हिचकिचाहट नहीं होती थी। यों नरेंद्र मोदी स्वयं संगठन पदाधिकारी के रूप में इसी तरह देश के विभिन्न राज्यों में भ्रमण करते रहे हैं और एक हद तक क्षेत्रों और लोगों की नब्ज पहचानते हैं। इसी कारण उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की कंपनी को भले ही श्रेय दे दिया और मंत्री का दर्जा देकर सरकारी तमगा लगाया लेकिन यदि नीतीश और लालू यादव का जमीनी संपर्क और अपने कार्यकर्ताओं की फौज नहीं होती तो उनकी पार्टियां बिहार में पुन: सत्ता नहीं पातीं। प्रशांत किशोर भाजपा का साथ छोड़ गए तो नई एजेंसियां आ गईं। एक नहीं चार-चार सर्वेक्षणों के ठेके एजेंसियों को दिए जा रहे हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार हो या केंद्र की भाजपा सरकार, अपनी सफलताओं का विवरण देने के लिए भी सर्वेक्षणों का उल्लेख करती हैं। यदि उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों को विकास कार्यों का लाभ मिला है तो लोगों को महसूस होगा। उन्हें कागजी आंकड़े दिखाने की क्या जरूरत है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कार्यक्रमों की जानकारी सुदूर तमिलनाडु तक पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। नाना पाटेकर ने पिछले दिनों ठीक ही कहा कि आधी-अधूरी सफलताओं के विज्ञापनों पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने वाली सरकारें सूखा प्रभावित दो राज्यों के किसानों का कर्ज माफ कर दें तो कम से कम आत्महत्याएं बंद हो जाएं और लोग मेहनत कर अगली फसल की तैयारी कर सकें। अमेरिका या यूरोप में सर्वेक्षण एजेंसियों का आकलन कुछ हद तक इसलिए ठीक हो जाता है, क्योंकि समाज का जीवन स्तर समान होता है। भारत में तो हर शहर में विभिन्न आय-वर्ग के लोगों का जीवन स्तर, सोच-विचार, आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं भिन्न हैं। परिवार के सदस्यों की राय अलग होती है। तभी तो हाल में संपन्न तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक-दो को छोडक़र अधिकांश एजेंसियों के अनुमान गलत साबित हुए। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां, पंचायत, तहसील, जिला और प्रदेश स्तर पर संगठनों को मजबूत रखेंगी और कार्यकर्ता केवल फेसबुक-ट्विटर पर गुणगान या गाली-गलौच के बजाय जनता से जुड़ेंगे तो उनकी पार्टी के साथ ही संपूर्ण समाज के हितों की रक्षा हो सकेगी।