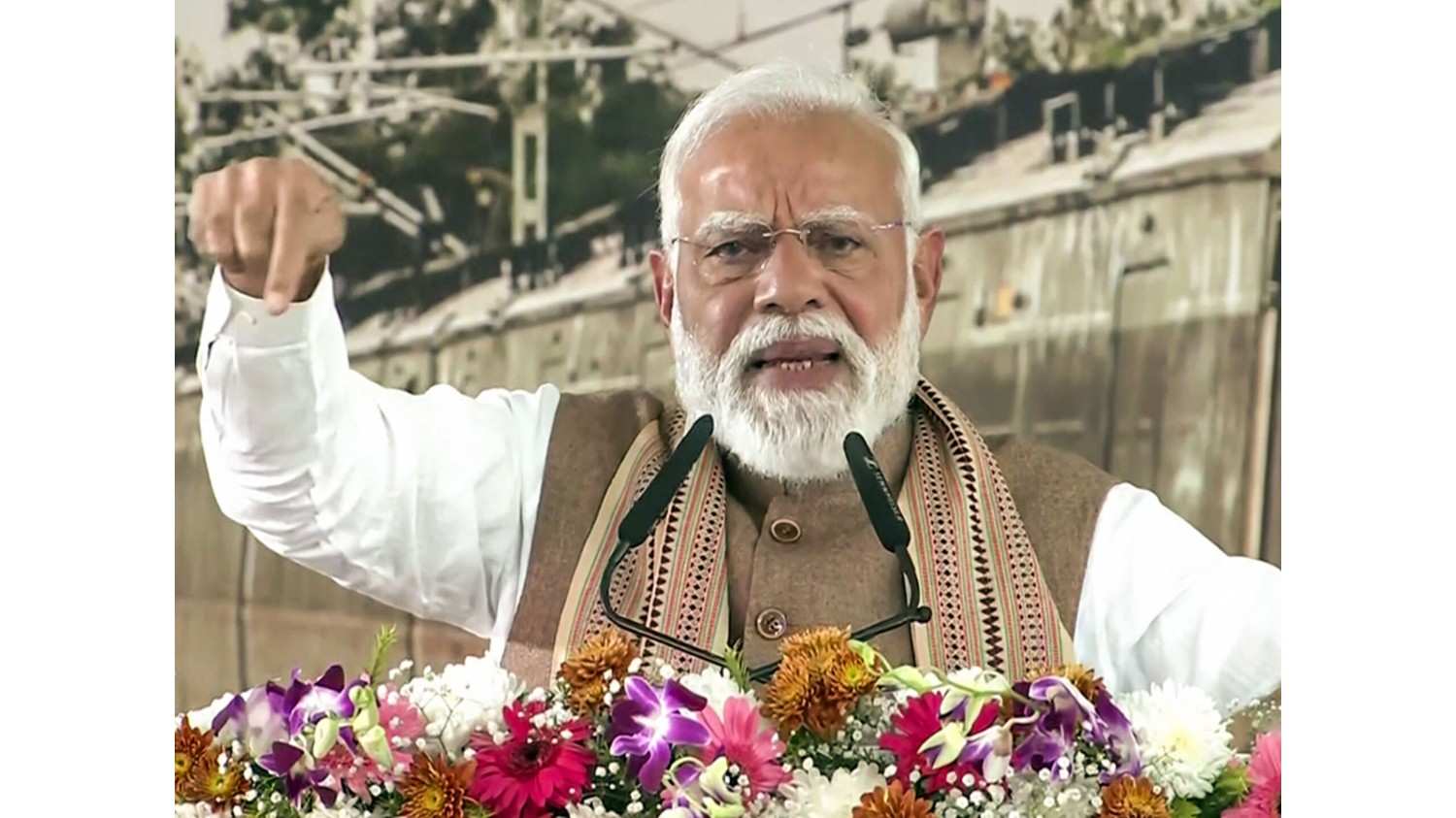उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर बहस की दरकार
बहुत पहले, इस देश के महान न्यायाधीशों में एक, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने परिभाषित किया था, ‘‘मूल सिद्घांत जमानत है, जेल नहीं, सिवाय उन मामलों के जहां न्याय-प्रक्रिया से भागने, उसे बाधित करने या बार-बार अपराध करने, गवाहों को धमकाने की कोशिशें दिखती हों।’’
आजकल, मजिस्ट्रेट या जिला अदालतें या हाइकोर्ट भी जमानत देने से इनकार करने के लगभग सभी मामलों में मूल सिद्घांत की परवाह नहीं करते हैं। इसके बजाय, मामले की समीक्षा की जाती है। इस मामले में लगता है कि हाइकोर्ट ने 3,000 पृष्ठों के आरोप पत्र और 30,000 पृष्ठों के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया दिल्ली दंगों में पूर्व-नियोजित साजिश का दोषी है, उसने भड़काऊ भाषण दिए थे और मुकदमा ‘स्वाभाविक गति’ से आगे बढ़ रहा है। यह पूरी तरह गलत न्यायिक दृष्टिकोण है।
न्यायाधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत गारंटी को नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ‘कानून की स्थापित प्रक्रिया के अलावा, किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।’
इस प्रावधान पर दिसंबर 1948 में संविधान-सभा में बड़ी बहस हुई थी। पंडित भार्गव ने इसे मैग्ना कार्टा बताया था और कहा था, ‘‘यह विधायिका की निरंकुशता पर न्यायपालिका की एकमात्र जीत है। असल में, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए दो सुरक्षा कवच चाहते हैं। एक विधायिका और दूसरी न्यायपालिका। लेकिन अगर विधायिका दलगत भावना से बहक जाए और कभी-कभी घबरा भी जाए, तो भी न्यायपालिका हमें विधायिका और कार्यपालिका के अत्याचार से बचाएगी।’’ उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की थी कि ‘‘लोकतंत्र में न्यायालय लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतिम शरणस्थली होते हैं। मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका न्याय के अपने उचित पद पर प्रतिष्ठित हो और लोग उसके संरक्षण में अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं में सुरक्षित रहें।’’
क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुईं? मुझे नहीं लगता। संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के अमल में न्यायपालिका तेजी से कार्यपालिका की ओर झुकती और लोक-विरोधी होती जा रही है। आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत भुला दिए गए हैं। जैसे, ‘‘हर आरोपी व्यक्ति तब तक निर्दोष है, जब तक अभियोजन पक्ष उसे निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से दोषी साबित नहीं कर देता है।’’ अब, इसके उलट खुद को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर डाल दिया गया है। अभियोजन पक्ष बहुत ही गोपनीय, आक्रामक, अमूमन निकम्मा और कई बार पूर्वाग्रह ग्रस्त होता है। उसके शिकार अमूमन हाशिए के और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग होते हैं।
स्वतंत्रता सेनानी, वकील, शिक्षाविद्, लेखक के.एम. मुंशी ने कहा था, ‘‘इस सदन में बार-बार यही कहा गया कि हम लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और लोकतंत्र का सार यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विधायिका में बहुमत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सेवा करने से ज्यादा सामाजिक नियंत्रण के पक्ष में होता है।’’ उन्होंने आशंका जताई थी, ‘‘दुर्भाग्य से, इस देश में, भारी बहुमत वाली विधायिकाएं गंभीर समस्याओं का सामना कर रही हैं और उनमें जल्दबाजी में कानून पारित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जो कार्यपालिका और पुलिस को व्यापक अधिकार देने की हिमायती है।’’
स्थापना के सात दशक बाद भी हमारा लोकतंत्र इन चुनौतियों से जूझ रहा है। तब मुंशी ने आगाह किया था, ‘‘इस समय हम आपात स्थिति में शायद यह भुला बैठे हैं कि अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा व्यापक नहीं करते और उसे अदालतों का संरक्षण नहीं देते, तो हम ऐसी परंपरा बना देंगे, जो अंततः देश में मौजूद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के किसी भी हिस्से को नष्ट कर देगी।’’ मौजूदा हालात गवाह हैं कि उनकी बात भविष्यवाणी जैसी साबित हुई है। हमारी स्वतंत्रताओं में बोली और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। इस मामले में प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था, ‘‘जबसे लोगों में नागरिक स्वतंत्रता की चेतना आई है, तबसे वह निरंकुश शासकों और उनके विरुद्ध लड़ने वालों का मुख्य युद्धक्षेत्र रही है... निरंकुश शासक, तानाशाह, हमेशा यही चाहता है कि जब भी वह किसी अन्य तर्क में असमर्थ हो, तो वह उन लोगों को चुप करा दे, जो उससे सहमत नहीं हैं। इसलिए, जब भी कोई व्यक्ति जरा सा भी मतभेद जाहिर करे, जरा सी भी असुविधा या शर्मिंदगी पैदा होने की संभावना पैदा करे, तो निरंकुश सत्ता ऐसे व्यक्ति को बिना किसी आरोप या मुकदमे के जेल में डाल देती है, गिरफ्तार कर लेती है या हिरासत में ले लेती है।’’
आखिर प्रोफेसर शाह को 1948 में कैसे पता था कि आज के भारत को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? मुंशी ने उसे स्पष्ट किया, “अब हमारे पास लोकतांत्रिक सरकार है, इसलिए सरकार की आलोचना और उकसावे के बीच एक रेखा खींची जानी चाहिए। आलोचना का स्वागत किया जाना चाहिए। उकसावा वह है, जो सभ्य जीवन में खलल पैदा करे या राज्य-तंत्र को उखाड़ फेंकने के इरादे से किया गया हो...असल में लोकतंत्र का मर्म सरकार की आलोचना ही है।”
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इसी समझ के अनुरूप और शांतिपूर्ण थे। लेकिन हमारे न्यायाधीश इन गारंटियों की व्यापकता को नहीं समझते। उन्हें देश के संविधान को समझने के लिए इन बहसों का गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है।
दिल्ली हाइकोर्ट पूरी तरह आंखें मूंदे हुआ लगता है, क्योंकि उसने भाजपा नेताओं के उन भड़काऊ बयानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिसमें खुलेआम भीड़ को मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया गया था। मसलन, “प्रदर्शनकारियों को अब सबक सिखाना होगा”, “देश के गद्दारों को गोली मारो”, “जहां बोली नहीं चलती, वहां गोली चलती है”, “मुसलमानों का बॉयकाट करो”, वगैरह। क्या ये सब साजिश या भड़काऊ बयान नहीं हैं? क्या इससे सामाजिक व्यवस्था और शांति भंग नहीं हुई? न्यायाधीश स्वर्ग-लोक में नहीं रहते। उन्हें पता होना चाहिए कि आज पुलिस कैसे काम कर रही है। न्यायमूर्ति ब्रेनन का प्रसिद्ध कथन सटीक है, ‘‘आदमी के दिल में सबसे गहरे अन्याय ही चुभते हैं। बीमारी हम झेल सकते हैं, लेकिन अन्याय हमें सब कुछ उखाड़ फेंकने की भावना से भर देता है। सिर्फ अमीर ही कानून का सुख संदिग्ध विलासिता की तरह ले सकें और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत वाले गरीब न पा सकें क्योंकि उसकी कीमत उनकी पहुंच से बाहर हो, तो स्वतंत्र लोकतंत्र के वजूद के लिए खतरा काल्पनिक नहीं, बल्कि एकदम असली है। दरअसल लोकतंत्र का मूल आधार न्याय तंत्र को इतना प्रभावी बनाना है कि हर नागरिकउसकी निष्पक्षता और न्याय संगत रवैए में विश्वास करे और उससे लाभान्वित हो।’’
यह बहस कई मायनों में न्यायिक प्रणाली की गंभीर समीक्षा और सुधार की मांग करती है। चाहे निचली अदालतों के न्यायाधीशों के चयन और पदोन्नति का मामला हो या हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर वकीलों और वादियों सहित सभी संबंधित पक्षों के बीच संवाद, अदालतों की रजिस्ट्री के बीच संवाद, आइआइटी और आइआइएम के साथ मिलकर केस लोड प्रबंधन सीखने और सुधारने की बात हो, सभी मामले में सुधार की दरकार है।
भारत में अन्याय सर्वत्र व्याप्त है और न्यायपालिका, कुछेक लोगों को छोड़कर या तो उसे दूर करने में सक्षम नहीं है या इच्छुक नहीं है। हमारी व्यवस्था में अमीर और ताकतवर लोग अन्याय कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। अनुच्छेद 21 का सर्वोपरि उद्देश्य किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिक्रमण को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कहा, ‘‘इस अनुच्छेद के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति को कारावास या बंदी बनाए जाने से रोका जाए।’’
देश भर में लाखों विचाराधीन कैदी अदालतों के जमानत न देने से जेलों में सड़ रहे हैं। शीघ्र सुनवाई ऐसी उम्मीद है, जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम वादों के बावजूद कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए, पांच साल के लंबे अंतराल के बाद जमानत से इनकार करना, बिना सोचे-विचारे सजा से कम नहीं है। देश में दोष सिद्धि की निराशाजनक दर को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यही अदालती रवैया है, जिस पर पुलिस और अभियोजन पक्ष फलते-फूलते हैं। इस बीच, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1979 के एक फैसले में कहा था, ‘‘दुर्भाग्य से, हमारे देश में, गरीबों को न्यायिक व्यवस्था से बाहर रखा जाता है। गरीब हमेशा कानून के स्याह पक्ष में रहे हैं। न्याय व्यवस्था कमजोर वर्गों के लिए अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है।’’
दिल्ली हाइकोर्ट, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट सहित पूरे देश की अदालतों ने उस विश्वसनीयता को पुनः प्राप्त करने और खुद को सुधारने के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं।

(सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, विचार निजी हैं)