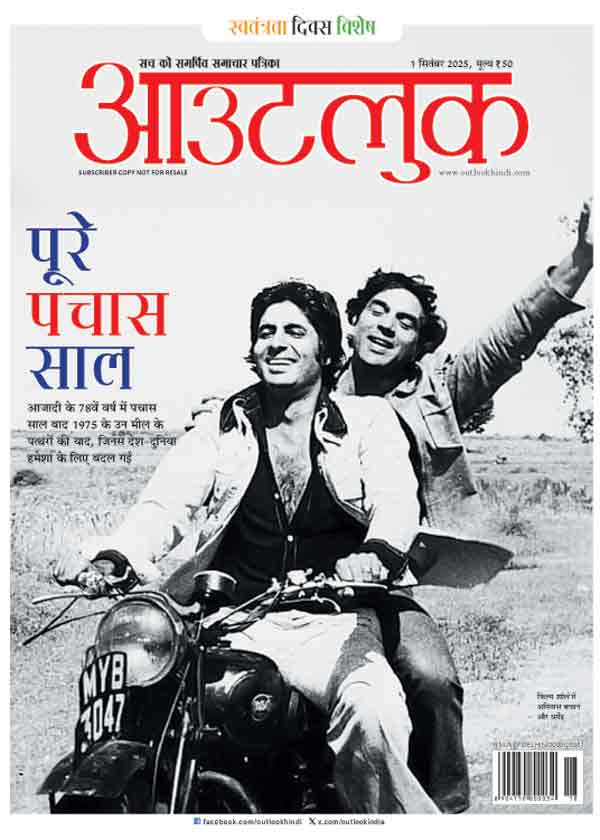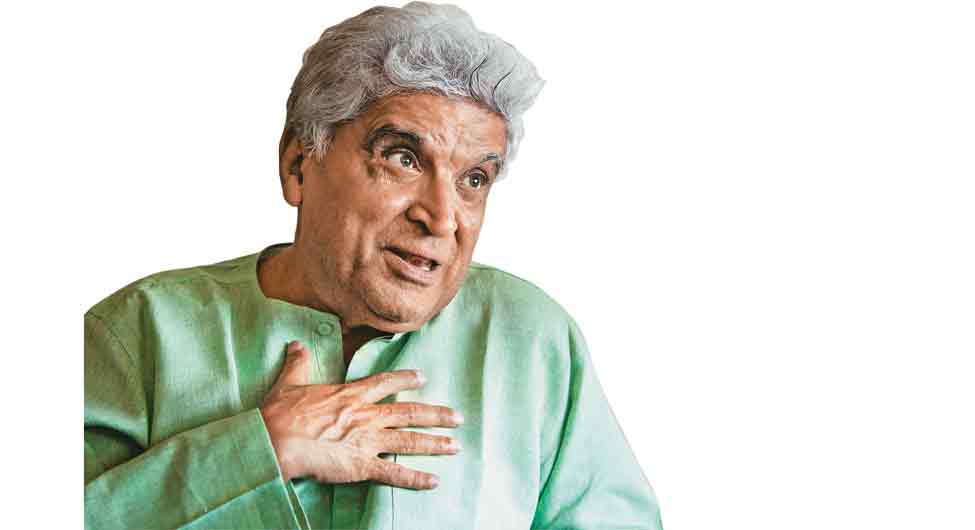शिक्षा का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। पहले जहाँ गुरुकुल में अनुभव और चरित्र निर्माण को केंद्र में रखा जाता था, वहीं औपनिवेशिक काल में शिक्षा प्रणाली किताबों और परीक्षा आधारित हो गई। आज हम फिर एक मोड़ पर खड़े हैं -जहाँ एक ओर पारंपरिक शिक्षा प्रणाली डिग्री, पाठ्यक्रम और बोर्ड परीक्षा जैसे ढाँचों पर टिकी है, वहीं दूसरी ओर स्किल-बेस्ड एजुकेशन यानी कौशल-आधारित शिक्षा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। LinkedIn की “Future of Skills” रिपोर्ट 2024 बताती है कि भारत में 75% रिक्रूटर्स अब डिग्री से अधिक स्किल्स पर ध्यान दे रहे हैं। कंपनियाँ “skills-first hiring” को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे शिक्षा की परिभाषा ही बदल रही है। अब प्रश्न यह है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इस बदलाव के लिए तैयार है?
भारत में पारंपरिक शिक्षा आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है। स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं, अंक आधारित मूल्यांकन और रट्टामार शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता है। यह व्यवस्था छात्रों को सीमित सोच और उत्तर याद करने की प्रवृत्ति में बाँध देती है। वहीं 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) ने शिक्षा को अधिक लचीला, बहुविषयक और कौशल आधारित बनाने की बात कही। लेकिन 2023 तक की UDISE रिपोर्ट के अनुसार, देश के 70% से अधिक सरकारी स्कूलों में अब भी व्यावहारिक प्रयोगशालाएँ नहीं हैं और केवल 12% शिक्षकों को स्किल-बेस्ड टीचिंग का प्रशिक्षण मिला है। इसका मतलब है कि नीति ज़रूर बनी है, पर जमीनी क्रियान्वयन अभी बहुत पीछे है। जब तक शिक्षकों और छात्रों दोनों में बदलाव नहीं लाया जाएगा, पारंपरिक ढाँचा बना रहेगा।
दूसरी ओर स्किल-बेस्ड एजुकेशन एक ऐसा मॉडल है जिसमें छात्रों को केवल किताबों से नहीं, बल्कि वास्तविक समस्याओं को हल करने के अनुभव से सिखाया जाता है। Google, IBM, और TCS जैसी कंपनियाँ अब उन छात्रों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिन्होंने Google Career Certificates, AWS Academy या Coursera जैसी प्लेटफ़ॉर्म से स्पेशलाइज्ड स्किल्स सीखी हैं। एक NASSCOM रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में 65% युवा स्नातक नौकरी के लिए तैयार नहीं होते, जबकि जिन्होंने स्किल-बेस्ड कोर्स किए हैं, उनकी नियुक्ति दर 45% अधिक रही। Skill India, PMKVY और Digital India जैसी सरकारी योजनाएँ भी इसी सोच को आगे बढ़ा रही हैं। अब शिक्षा का मतलब केवल “क्या याद है” नहीं, बल्कि “क्या कर सकते हो” होता जा रहा है।
पारंपरिक शिक्षा के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। यह बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान, अनुशासन और बौद्धिक आधार देती है। आज भी MBBS, इंजीनियरिंग, CA जैसी प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए पारंपरिक मॉडल आवश्यक है। लेकिन यह तब समस्या बनती है जब इस ढाँचे को अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। AICTE की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि हर साल लगभग 60% इंजीनियरिंग स्नातक तकनीकी रूप से अप्रासंगिक (technically unemployable) पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें केवल थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन उद्योग की ज़रूरत के अनुरूप कौशल नहीं मिलते। इसलिए पारंपरिक शिक्षा को अब कौशल आधारित ढंग से अपडेट करना अनिवार्य है।
आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में नौकरी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। WEF की Future of Jobs रिपोर्ट 2023 के अनुसार, आने वाले 5 वर्षों में 85 मिलियन नौकरियाँ समाप्त होंगी, लेकिन साथ ही 97 मिलियन नई नौकरियाँ भी पैदा होंगी -जो पूरी तरह स्किल-ड्रिवन होंगी। यह स्पष्ट संकेत है कि स्किल-बेस्ड एजुकेशन ही भविष्य का रास्ता है। इसमें छात्र “सीखो, करो और समझो” की प्रक्रिया से गुजरते हैं। प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग, टीमवर्क, और तकनीकी दक्षता उन्हें किसी भी चुनौती के लिए तैयार करती है। यह शिक्षा मॉडल न केवल नौकरियाँ दिलाता है, बल्कि उद्यमशीलता, स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि कई निजी विश्वविद्यालय अब चार वर्षीय डिग्री में स्किल मॉड्यूल को अनिवार्य बना रहे हैं।
अंततः यह स्पष्ट होता है कि न तो केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त है और न ही केवल कौशल आधारित शिक्षा। दोनों का संतुलन आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों को अब ऐसी प्रणाली अपनानी होगी जिसमें छात्र एक ओर विषय का गहराई से अध्ययन करें, तो दूसरी ओर व्यावहारिक रूप से उसे प्रयोग में लाएँ। Finland, Singapore और Germany जैसे देश इसी मिश्रित मॉडल के कारण शिक्षा में वैश्विक मानक बन चुके हैं। भारत को भी अब उसी दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जब छात्र के पास ज्ञान, सोचने की शक्ति और करने का हुनर तीनों होंगे, तभी वह ना सिर्फ़ रोज़गार पाएगा, बल्कि समाज के लिए भी मूल्यवान योगदान दे सकेगा। यही भविष्य की सच्ची शिक्षा होगी