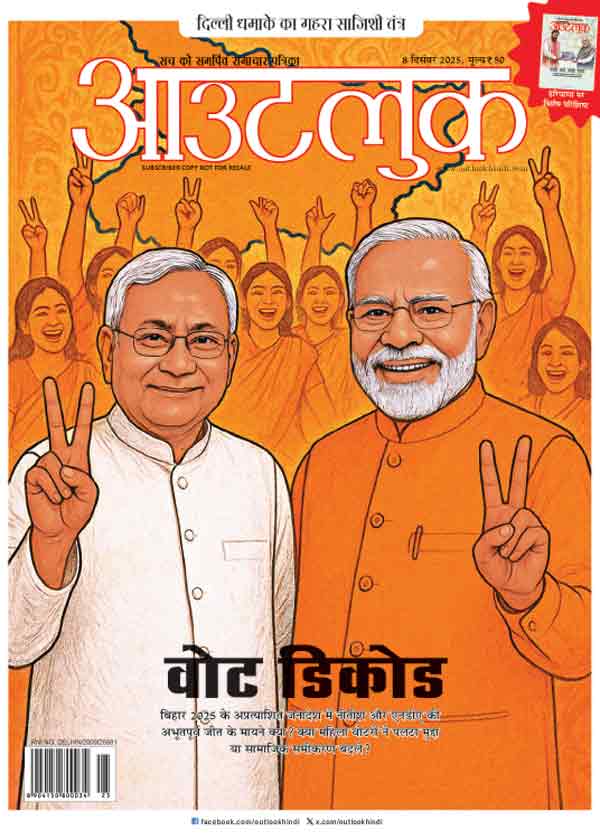राजनीति और रेल का नाता देश में जैसे गुत्थमगुत्था है। हर दौर में रेल नीतियों पर एक नजर डाल लीजिए तो उस दौर की राजनीति की खिड़कियां खुलने लगती हैं। यूं तो राजनीति से ही सब कुछ शक्ल लेता है, मगर भारतीय रेल एक विशिष्ट राजनीतिक परिघटना ऐन उसी वक्त से है जब इसकी नींव रखी गई। रेल राजनीति को देखने-समझने के लिए हम मोटे तौर पर इसे सात हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। अंग्रेजों का दौर, आजादी के आंदोलन में इसकी भूमिका, आजादी के बाद पहले दो दशकों में रेल नीति, इंदिरा गांधी का काल, जनता पार्टी का दौर, उदारीकरण का दौर और 2014 के बाद मोदी सरकार का दौर। कोई चाहे तो इसे और खांचों में बांट सकता है। यह भी है कि हर दौर और हर रेल मंत्री के काल में विविधता देखी जा सकती है। वजह यह भी है कि मंत्रालयों के बेहद केंद्रीकरण के एकाध दौर को छोड़ दें तो हर मंत्री अपने नजरिए से मंत्रालय को चलाता रहा है। आज के दौर में केंद्रीकरण ज्यादा है तो मंत्री का अपना नजरिया खास नहीं दिखता, जब तक उसे दिखाया न जाए। इन्हीं सवालों और नजरियों से यह स्पष्ट होगा कि रेल कैसे राजनीति के उलझाव में फंसी रही है और आज वह इस मुकाम पर कैसे पहुंची है।
दरअसल रेल पथ निर्माण उन्हीं गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस के दौर (1848-1856) में हुआ, जिन्होंने देश में जमीन की पैमाइश की भी योजनाएं तैयार की और उसे अमलीजामा पहनाया। उन्हीं के दौर में नए जमींदार और मोटी लगान का सिलासिला भी तेज हुआ। रेल निर्माण का शुरू में जाहिरा मकसद बंदरगाहों को जोड़ना था, ताकि माल-आसबाब और जरूरी मजदूरों की आवाजाही आसान हो। माल-आसबाब ब्रिटेन और यूरोपीय बाजारों में पहुंचाना था और गिरमिटिया मजदूरों को अपनी दूसरी कॉलोनियों में। ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दर्ज अनेक लड़ाइयां रेल की पटरियां बिछाने के वक्त की हैं, जिसमें संथाल परगना (अब झारखंड) में सिद्धू-कान्हू का आंदोलन सबसे मशहूर है। ऐसा विरोध अंग्रेजों को 1853 में बॉम्बे (अब मुंबई) से ठाणे तक 21 किमी की पहली पटरी बिछाने के दौरान ही झेलना पड़ा था, जिसका ख्याल बॉम्बे सरकार के चीफ इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क को 1843 में भांडुप दौरे के वक्त आया था। उनकी मंशा बंबई से ठाणे, कल्याण और ठाल और भोर घाटों को जोड़ने की थी, ताकि बॉम्बे बंदरगाह तक जरूरी चीजें आसानी से पहुंचाई जा सकें। आवाजाही सुचारु हो सके। इस तरह पहली रेल पटरी बंबई से ठाणे तक 1853 में साकार हो गई लेकिन तब भी स्थानीय लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। लोगों का विरोध तब वाजिब समझ से था कि इसका मकसद अंग्रेजों के साम्राज्य का विस्तार और देशी संपदा की लूट है।

घायलों के हाल लेते ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक
शायद इसी समझ का एक अक्स महात्मा गांधी के हिंद स्वराज में दिखता है। वैसे, गांधी स्थानीय सत्ता की अक्षुण्णता पर ज्यादा जोर दे रहे थे। लेकिन आजादी का आंदोलन जब देश में जोर पकड़ा तो गांधी ने एक तरह से रेल को उसका हथियार भी बनाया। वे कांग्रेस के बड़े नेताओं के बरक्स तीसरे डिब्बे में आम लोगों के साथ सवारी करने लगे और देश भर में घूम-घूम कर लोगों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने लगे। गांधी जिस अंतिम आदमी की चिंता की बात करते हैं, रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करना भी एक तरह से इस विचार को केंद्र में लाने जैसा था। फिर, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के लिए तीसरे दर्जे में यात्रा करने का चलन शुरू हो गया था। इसका संदेश और असर दोनों स्पष्ट था, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में दिखा भी।
आजादी के बाद देश-निर्माण के पहले और दूसरे दशक में भी रेल नीतियों में कमोबेंश यह विचार और दायित्व-बोध जारी रहा। कुछेक अपवाद हो सकते हैं पर ज्यादा जोर यात्री गाड़ियों में सामान्य लोगों के लिए अधिक स्थान या अधिक डिब्बे मुहैया कराने पर था। अलबत्ता, तब देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आवाजाही भी कम थी और जनसंख्या भी कम थी। उस वक्त रिजर्वेशन का चक्कर भी न के बराबर था। तीसरे दर्जे में तो बिलकुल नहीं। यही नहीं, रेल में सर्वाधिक नौकरियां और रोजगार देने पर भी जोर था और उसके लिए अलग भर्ती कमीशन भी स्थापित किया गया था। रेल को सबसे ज्यादा नौकरियां देने का तमगा तभी से हासिल हुआ। तब पटरियों के रख-रखाव पर भी ज्यादा जोर था। इसी वजह से रेलवे सुरक्षा जांच आयोग को अलग नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जिम्मे रखा गया था, ताकि उस पर रेल मंत्रालय या मंत्री का कोई जोर न चल सके। यह आयोग पटरियों की हालत से लेकर तमाम व्यवस्थाओं की निगरानी करता था और अपनी सिफारिशें देता था।
यही नहीं, राजनैतिक दायित्व-बोध भी हुआ करता था। इसी की मिसाल है कि 1956 में तूतीकोरण एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर तत्कालीन रेल मंत्री लालबहादुर शास्त्री ने इस्तीफा सौंप दिया था, जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में दायित्व-बोध का यह दबाव माधव राव सिंधिया, नीतीश कुमार जैसे रेल मंत्रियों में भी दिखा, जिन्होंने बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बाद इस्तीफा सौंप दिया, चाहे मन या बेमन से। यहां तक कि हाल के दशक में लगातार दो दुर्घटनाओं के बाद सुरेश प्रभु को भी हटना पड़ा था। लेकिन आज तो ओडिशा के बालेश्वर में इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद दलील यह दी जा रही है कि इन इस्तीफों से क्या सुधरा है। मानो सुधार के लिए हर दायित्व-बोध को परे रखना जरूरी है। वैसे भी, आज के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजनीति नहीं, अफसरशाही में रहे हैं।

वजहें और चुस्तीः प्रधानमंत्री मोदी को दुर्घटना की जानकारी
अब फिर लौटते हैं, ताकि रेल और राजनीति के रिश्ते को समझा जा सके। आजादी के बाद के दो दशकों के बाद इंदिरा गांधी के काल में उच्च और मध्यवर्गीय आकांक्षाओं को बल मिलने लगा। हालांकि नारा तो उनका गरीबी हटाओ था लेकिन जैसे उन्हीं के दौर में छोटी कार मारुति का कारखाना लगाने की प्राथमिकता बढ़ी, उसी तरह रेलगाडि़यों में भी सुविधाएं सामान्य यात्रियों के डिब्बे की बनिस्बत पहले, दूसरे दर्जे में ज्यादा दिखाई देने लगी। उन्हीं के दौर में जॉर्ज फर्नांडिस की अगुआई में सबसे बड़ी रेल हड़ताल भी हुई थी।
इसी के मद्देनजर 1977 में जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की अगुआई में सरकार बनी तो रेल नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन शुरू हुआ। दूसरा दर्जा खत्म कर दिया गया। पहले दर्जे के डिब्बे सीमित हो गए और सामान्य दर्जे के डिब्बे बढ़ा दिए गए। कई जनता एक्सप्रेस चलाई गईं, जिसमें सिर्फ सामान्य श्रेणी के डिब्बे हुआ करते थे। सामान्य श्रेणी का किराया भी बहुत कम रखा जाता था।फिर 1980 के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में लौटीं। उसके बाद और राजीव गांधी के दौर में स्लीपर क्लास में आरक्षणों का सिलसिला शुरू होता है और सामान्य श्रेणी के डिब्बे घटने शुरू हो जाते हैं। 1991 में पी.वी. नरसिंह राव की सरकार आते ही वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की उदारीकरण की नीतियों के तहत फोकस बदलना शुरू हो जाता है। रेल सहित हर मामले में सब्सिडी घटाने और वाणिज्यिक दृष्टि से देखने का सिलसिला शुरू होने लगा। जहां तक संभव हो निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाने लगा। यह सिलसिला एनडीए-1 की अटलबिहारी वाजपेयी के दौर और यूपीए के दौर में जारी रहा। 2014 के बाद केंद्र में आए नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि सरकार को कारोबार से कोई लेनादेना नहीं, यह उसी नजरिए की बुलंदी जैसा है, जो नब्बे के दशक में बाजार समर्थक कुछ हकलाहट के साथ जाहिर किया करते थे। लिहाजा, नेशनल कैरियर या राष्ट्रीय परिवहन का आधार बताई जाने वाली रेल भी बाजार और कारोबारी नजरिए से देखी जाने लगी।

पटरी खुलवाते रेल मंत्री
लेकिन यूपीए के दौर तक नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी जैसे रेल मंत्रियों का नजरिया बहुत हद तक रेल को नेशनल कैरियर और सर्वाधिक रोजगार मुहैया कराने के साधन की तरह मानने वाला ही रहा। यह भी कि तब तक मंत्रियों की नीतियों में कमोबेश चलती थी। इन सभी रेल मंत्रियों ने रेल का यात्री किराया लगभग नहीं बढ़ने दिया और रेल की आय बढ़ाने के लिए दूसरे मदों और उपायों पर जोर दिया। लालू यादव ने तो रेल किराया एक रुपए घटाकर काफी प्रसिद्घि हासिल की। लालू ने और भी कई प्रयोग किए। मसलन, मालगाड़ियों में बोझ वहन का प्रतिशत बढ़ाकर आमदनी बढ़ाने की कोशिश की और स्लीपर क्लास में अतिरिक्त बेड डालकर यात्रियों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की। लालू यादव के इस प्रबंधकीय कौशल की चर्चा भी हुई। लेकिन इस दौर में भी वातानुकूलन पर जोर था। लालू ने वातानुकूलित गरीब रथ भी चलवाया।
उनके बाद ममता बनर्जी के दौर में भी ये नीतियां जारी रहीं और मनमोहन सरकार के दबाव के बावजूद उन्होंने न किराया बढ़ने दिया, न निजी निवेश की ओर ज्यादा ध्यान दिया। अलबत्ता, 2012 में उनके दौर में रेल में पीपीपी मॉडल लाने का एक पर्चा जरूर तैयार हुआ, जिसमें बाकायदा निजी निवेश को बढ़ावा देने की रूपरेखा तैयार की गई थी। लेकिन बंगाल चुनाव जीतने के बाद उनकी जगह उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सरकार की नीतियों की तरह किराए में बड़ी बढ़ोतरी की तो ममता नाराज हो गईं और उनसे इस्तीफा देने को कह दिया। उनके बाद मुकुल रॉय तो ममता के निर्देश पर चलते रहे। 2014 के बाद त्रिवेदी और मुकुल रॉय दोनों भाजपा में शामिल हो गए। अब मुकुल रॉय फिर तृणमूल में लौट आए हैं।
रेल नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन 2014 के बाद शुरू होता है। रेल बजट को पहली बार आम बजट में शुमार कर दिया गया। यानी रेल की जो विशेष व्यवस्था थी, वह खत्म कर दी गई। टाटा की अगुआई में एक कायाकल्प समिति बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट 2015 में आई। उस रिपोर्ट का क्या हुआ, पता नहीं। शायद पीपीपी मॉडल के जरिए निजीकरण को प्रशस्त करने के लिए ही एनडीए-2 सरकार में पहले रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की जगह सुरेश प्रभु लाए गए। वे निजीकरण की दिशा में ही काम कर रहे थे लेकिन लगातार दो रेल दुर्घटनाओं के कारण उन्हें हटना पड़ा। उनके बाद आए पीयूष गोयल के दौर में 2017 में बाकायदा निजीकरण के लिए प्रस्ताव लाया गया। उसी नीति पर काम चल रहा है। अब अश्विनी वैष्णव उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वैष्णव ने यह जरूर किया कि निजी निवेश की पहल धीमी करके ध्यान रेल को चुस्त-दुरुस्त करने और उसकी चमक-दमक बढ़ाने पर दिया। लिहाजा, वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई और कुछेक स्टेशनों को नया लुक दिया जा सका।
इसका फर्क शायद यह पड़ा कि रेल में भर्तियां रुक गईं। अभी 3.5 लाख पद खाली बताए जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सिग्नलिंग सिस्टम में ही हैं। कवच का प्रचार तो हुआ लेकिन अभी तक तकरीबन 68,000 किमी रेल नेटवर्क में 14,000 किमी के आसपास ही लगाया जा सका है। मतलब यह है कि रेल उसी राजनीति-रोग का शिकार है, जिसका दंश समूचे देश में दिखता है।
मंत्रियों के रुझान
लालबहादुर शास्त्रीः आजादी के बाद 1956 में पहली बड़ी रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया
लालू प्रसाद यादवः रेल का किराया एक रु. घटाया और कई तरह के प्रयोगों से प्रबंधन कौशल दिखाया
नीतीश कुमारः किराया कम बनाए रखने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए चर्चित। दुर्घटना के बाद इस्तीफा
माधव राव सिंधियाः बड़ी रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा। नया प्रबंधन
ममता बनर्जीः किराया नहीं बढ़ने दिया और बाद में अपनी पार्टी के रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी से किराए बढ़ाने पर इस्तीफा दिलवा दिया। पीपीपी मॉडल के लिए प्रस्ताव
सुरेश प्रभुः निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए मगर लगातार दो रेल दुर्घटनाओं के बाद हटा दिए गए