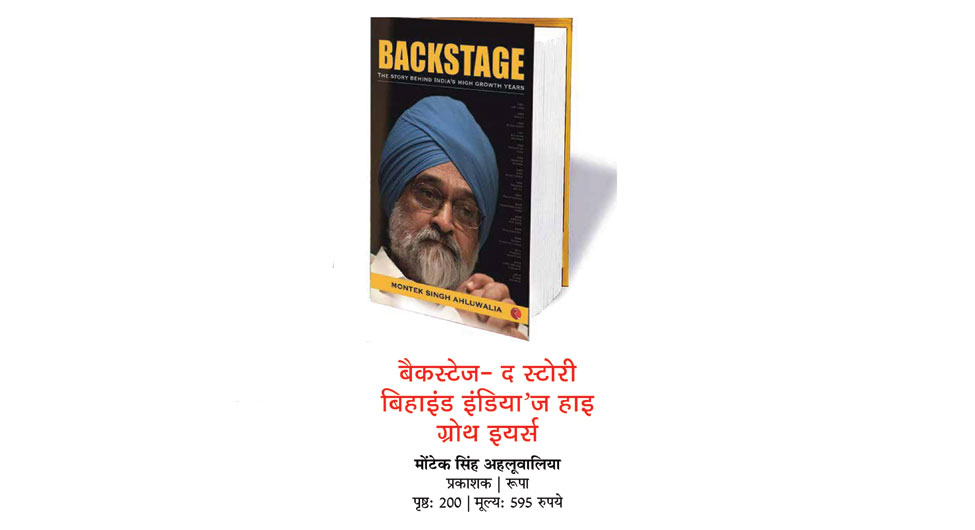विद्या भूषण अरोरा
भारत की आर्थिक नीतियों में 1991 में जो बड़ा बदलाव आया उसकी नींव अस्सी के दशक में ही पड़ चुकी थी। मोंटेक सिंह अहलूवालिया उसी समय से भारत सरकार के आर्थिक-प्रशासनिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। पुस्तक में अहलूवालिया ने आर्थिक सुधारों की इसी प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से बताया है। यह किताब देश के आर्थिक इतिहास में रुचि रखने वाले अध्येताओं के साथ-साथ नीति-निर्धारकों के लिए भी उपयोगी होगी। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता (जिसे एक समीक्षक ने कमी के तौर पर भी गिनाया है) यह है कि अहलूवालिया ने आर्थिक बदलावों में अहम भूमिका निभाने और इन दशकों में आर्थिक क्षेत्र में हुई बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं के गवाह होने के बावजूद स्वयं को किताब के केंद्र में रखने का न प्रयास किया न सनसनीखेज खुलासे किए। अहलूवालिया सहज ढंग से ऐसी बातें बताते हैं जो प्रायः पहले मालूम नहीं थीं।
अहलूवालिया ईमानदारी से उन आर्थिक सुधारों की कहानी बताते हैं, जिसकी सुगबुगाहट इंदिरा गांधी की दूसरी पारी यानी अस्सी के दशक में शुरू हो गई थी। जुलाई 1980 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई, जिसने अहलूवालिया के अनुसार, चाहे कोई खास नए अवसर न दिए हों लेकिन फिर भी इससे सरकारी नियंत्रणों में कुछ लचीलापन आया। वह याद दिलाते हैं कि जापान की सुजुकी के साथ संयुक्त उपक्रम में मारुति कार का आना अच्छा संकेत था। उस समय घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के नाम पर कुछ सरकारी नियंत्रण कैसे हास्यास्पद ढंग से काम करते थे और कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे।
आर्थिक सुधारों की खुलकर चर्चा राजीव गांधी के शासन के शुरुआती वर्षों में तब हुई जब भारत का मध्यमवर्ग बड़ा हो रहा था और उसे अच्छे फ्रिज, टीवी, स्कूटर, छोटी कार और ऐसे अन्य आरामदायक सामानों की इच्छा होने लगी थी। राजीव इस वर्ग की बढ़ती इच्छाओं के प्रति सचेत तो थे लेिकन उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह कांग्रेस की दशकों पुरानी नीतियों को एक झटके में पलट देते। राजीव गांधी के पीएमओ में अपर सचिव अहलूवालिया उनको देश का पहला ऐसा नेता बताते हैं, जिसने भारत को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करने की जरूरत पर बल दिया था। राजीव देश की अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के महत्व को अच्छी तरह समझते थे और साथ ही वह सरकारी व्यवस्था के बेहद धीमेपन और उसके भ्रष्ट होने से निराश भी थे। लेखक स्मरण कराते हैं कि राजीव ने सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए कुछ प्रशासनिक सुधार भी शुरू किए और कर-ढांचे में सुधारों की शुरुआत उनके समय में ही हो गई थी। राजीव ने शहरीकरण की जरूरत को भी समय से पहले ही पहचान लिया था और उनके समय में ही रेंट-कंट्रोल एक्ट और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट जैसे कानून के उन्मूलन की प्रस्तावना तैयार हो गई थी। हालांकि उन पर अमल कुछ बरस बाद हुआ। भारत में टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत भी राजीव गांधी ने ही की थी। अहलूवालिया बताते हैं कि बोफोर्स स्कैंडल के प्रकाश में आने के बाद राजीव सरकार की प्राथमिकताएं बदल गईं और उसके बाद कोई खास आर्थिक सुधार नहीं हो सके।
राजीव गांधी के शासन के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर की चंद महीनों की सरकारों के कार्यकाल की भी लेखक ने अच्छे से विवेचना की है और बताया है कि कैसे अर्थव्यवस्था ऐसी हालत में थी कि इन दोनों को अपने छोटे कार्यकाल में भी आर्थिक सुधार करने की दिशा में कुछ न कुछ आगे बढ़ना पड़ा। उनके विचार में वीपी सिंह अर्थशास्त्रीय बारीकियों को बखूबी समझते थे लेकिन अपनी सरकार चलाने के लिए उन्हें राजनीतिक दांव-पेचों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था। चंद्रशेखर सरकार का जिक्र करते हुए लेखक ने स्मरण कराया कि उनके पद ग्रहण करते ही देश में विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग समाप्त हो गया था और भुगतान का संकट मुंह बाए खड़ा था। उधर चुनावों की घोषणा हो गई थी लेकिन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर किसी तरह विदेशी बैंकों से कर्ज लेकर इस संकट से देश को उबारा था। अहलूवालिया लिखते हैं कि चाहे इसके लिए चंद्रशेखर सरकार की आलोचना हुई कि उसे सोना गिरवी रखना पड़ा, लेकिन असल में यह साहसिक कदम था जिसने देश को गंभीर
भुगतान संकट से बचा लिया और आने वाली सरकार को दीर्घकालीन उपाय करने के लिए समय मिल गया।
1991 की नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधारों को अलग ही दिशा दी। इस पुस्तक में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों की पृष्ठभूमि बताई गई है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नए आयाम दे दिए। लेखक का कहना है कि नरसिम्हा राव वैसे तो पुरानी पीढ़ी के कांग्रेसी थे और आर्थिक सुधारों को लेकर वह बहुत सतर्क थे लेकिन देश के सामने खड़ी गंभीर आर्थिक चुनौतियों को वह भली प्रकार से पहचानते थे, इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना वित्तमंत्री चुना। राव सरकार न केवल अल्पमत में थी बल्कि कांग्रेस के भीतर भी राव सर्व-स्वीकार्य नेता नहीं थे। आर्थिक सुधारों के लिए कांग्रेसी तैयार नहीं थे। मनमोहन सिंह ने जब 1991-92 का बजट पेश किया, तो जहां अर्थशािस्त्रयों के एक बड़े वर्ग ने उसका स्वागत किया, वहीं वाम दलों ने उसकी जमकर आलोचना की। अहलूवालिया बताते हैं कि उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठकों में संसद सदस्यों ने बजट के कई पहलुओं पर वित्तमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर खिंचाई की थी।
आर्थिक सुधारों की इस यात्रा के अलग-अलग पड़ावों के बारे में बताने के साथ-साथ मोंटेक पुस्तक में जानकारी भी देते चलते हैं कि 1991 से बाद के वर्षों में देश की जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, विदेशी पूंजी निवेश, विदेश व्यापार आदि में किस तरह की वृद्धि होती चली गई। गरीबी उन्मूलन की दर भी आर्थिक सुधारों की वजह बहुत अच्छी रही और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए।
जब हम पुस्तक में इन उपलब्धियों के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इस पर जाता है कि आर्थिक सुधारों को तेजी से शुरू हुए भी लगभग तीन दशक हो चले हैं लेकिन फिर भी असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूर अभी भी इतने गरीब हैं कि उनके पास दो-चार दिन भी बिना कमाए खाने के पैसे नहीं होते। क्या हम स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को देश के सीमांत वर्गों तक पहुंचा पाए हैं? सच तो ये है कि शिक्षा के मामले में तो उत्तर भारत के राज्य पहले से भी बदतर हो गए लगते हैं। स्वास्थ्य में भी कमोबेश यही स्थिति है कि सरकारें, चाहे वो यूपीए की हों या एनडीए की, स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र के हवाले करने को ही उत्सुक लगती हैं। पुस्तक की एक बड़ी कमी के रूप में इस बात को देखा जाना चाहिए कि लेखक ने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की कि आर्थिक सुधार जिन्हें वह रामबाण की तरह पेश करते हैं, ऐसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी क्यों रहे?
इन अनुत्तरित सवालों के बावजूद ये पुस्तक उपयोगी है। पुस्तक नीति-निर्धारकों से लेकर स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों तक, सभी को बहुत कुछ ऐसा देगी जो उनके लिए नया होगा, जिसका इस्तेमाल वह अपनी भविष्य की प्लानिंग में कर सकेंगे।
बैकस्टेज– द स्टोरी बिहाइंड इंडिया’ज हाइ ग्रोथ इयर्स
मोंटेक सिंह अहलूवालिया
प्रकाशक | रूपा
पृष्ठः 200 | मूल्यः 595 रुपये
---------------------------------------------
इतिहास पर नजर
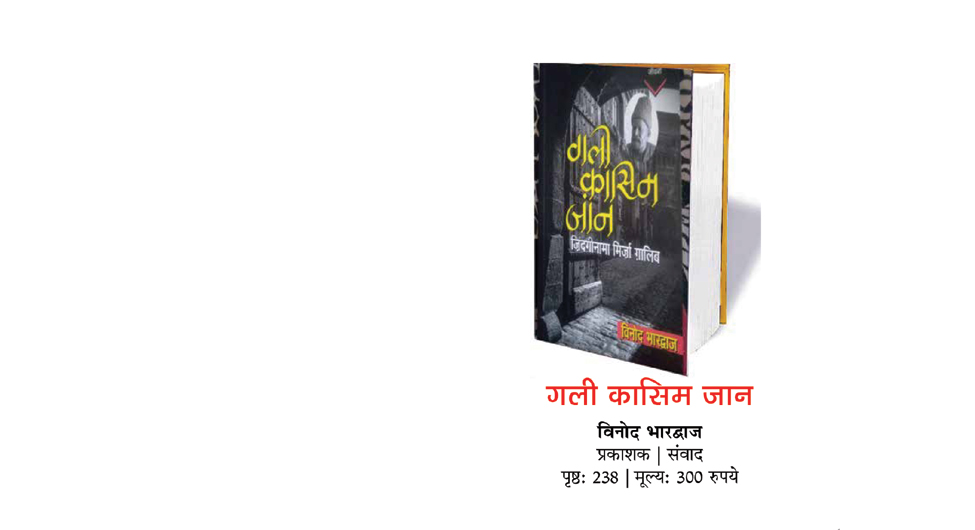
पुरानी दिल्ली की आम सी गली है, गली कासिम जान। जिस नुक्कड़ पर बल्लीमारान से गली कासिम जान मिलती है, वहीं हकीम शरीफ खां की हवेली के नजदीक एक कोयले और लकड़ी की टाल हुआ करती थी। टाल वाली इसी हवेली में मिर्जा गालिब ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा समय गुजारा। इसी गली में मिर्जा गालिब का जीवन बिखरा पड़ा है। यह जीवनी गालिब की शायरी का मूल्यांकन नहीं करती, बल्कि उनके इर्द-गिर्द जो कुछ हो रहा था, उसे बयान करती है। यह किताब गालिब की प्रासंगिकता पर बात करती है। अपने ही एक शेर में गालिब ने कहा था, ‘हूं गर्मी-ए निशाते तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंदलीबे गुलशने ना आफरीदा हूं।’ यानी मैं अपनी कल्पनाओं की उष्मा से, उसकी गर्मी से नग्में गा रहा हूं, मैं ऐसी दुनिया का हूं जो अभी वजूद में आई ही नहीं है, जिसका अभी अस्तित्व ही नहीं है। यानी गालिब खुद यह जानते थे कि जिस बेहतर दुनिया की वह कल्पना कर रहे हैं, वह अभी बनी नहीं है। पीछे मुड़कर गालिब को दोबारा देखना उस काल खंड को देखना है, जब हिंदुस्तान की तारीख एक अहम तूफान से गुजर रही थी, जब मुगल सल्तनत आखिरी सांसें गिन रही थी। ऐसे वक्त में यह शायर अंग्रेजों के जरिए पश्चिमी सोच और अंग्रेजों के सूरज को मुल्क में उभरते देख रहा था।
यह जीवनी गालिब की जिंदगी की गुरबतों, मजबूरियों, खुदा से उनके रिश्तों और तकलीफों की लंबी दास्तान ही नहीं, बल्कि गालिब की संवेदनशीलता और मानवीयता के कई पहलुओं को उजागर करती है। यह जीवनी बेतरतीब सी भी है, ठीक उसी तरह जैसे गालिब का जीवन था। इसका आगाज गालिब के इंतकाल से होता है। इसके बाद सफे दर सफे उनकी जिंदगी खुलती जाती है। 9 अगस्त 1810 को तेरह बरस की उम्र में गालिब का निकाह उमराव बेगम से हुआ। दिल्ली में उनका आना-जाना पहले भी था लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि शायरी में नामवरी के लिए दिल्ली रहना जरूरी है। गालिब, मीर तकी मीर से कभी नहीं मिल पाए। बाद में उन्होंने मीर पर शेर कहा था, ‘रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था।’ गालिब दिल्ली आए लेकिन यहां भी मुश्किलों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वह यहां भी अपनी पेंशन के लिए जद्दोजहद करते रहे। इसी सिलसिले में उन्होंने कलकत्ता (कोलकाता) जाने का फैसला किया। वह बनारस, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद भी घूमने गए। बनारस के बारे में गालिब ने कहा था कि मेरी नजर में बनारस को काबा-ए-हिंदुस्तान का दर्जा रखने वाला शहर माना जाना जाना चाहिए। इन यात्राओं पर उनके यादगार अनुभव इस किताब में दर्ज हैं। गालिब अपनी जिंदगी के, उनके इर्द-गिर्द जो कुछ हो रहा था उसे ही अपनी शायरी में दर्ज कर रहे थे। खराब आर्थिक हालात ने उन्हें अपने घर पर जुआ खिलवाने के लिए प्रेरित किया, उन्हें बादशाहों के लिए शेर भी कहने पड़े। दुश्वारियां कितनी दिलचस्प हो सकती हैं, यह इस जीवनी से पता चलता है। गालिब की जिंदगी के साथ गली कासिम जान में उस काल खंड का इतिहास भी दिखाई पड़ता है कि कैसे मुगलों का साम्राज्य लाल किले तक महदूद हो गया था। यह गालिब के दुखों का दस्तावेज है, लेकिन वह अपने दुखों को निजी दुखों के रूप में दर्ज न कर समाज के दुखों के रूप में दर्ज करते हैं। 1869 की फरवरी में गालिब का इंतकाल हुआ और उन्हें निजामुद्दीन के करीब लोहारू कब्रिस्तान में दफनाया गया।
सुधांशु गुप्त