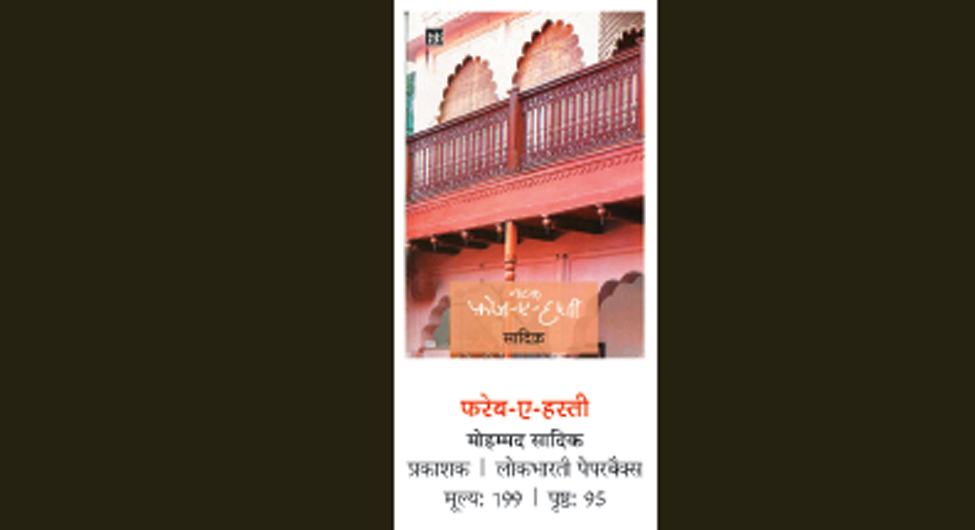मोहम्मद सादिक का नया नाटक ‘फरेब-ए-हस्ती’ 19वीं सदी के रूत्ब-ए-बुलंद शाइर मिर्जा गालिब के मौजूदा नए वक्तों में बिना तुमतुराक (शानो शौकत) दिल्ली में एक फेंटेसी के जरिए होने और मंजर-मंजर सरबसर घूमने की सरगश्तगी को समेटती एक दिलचस्प कहानी है। इस नाटक का कोई-कोई सिरा उनके पिछले ड्रामे ‘इस शक्ल से गुजरी गालिब’ में भी दर्ज है। जहां, 72 साल की जिंदगी में शोहरत और बदनामियां साथ-साथ कमाने वाले इस वली शायर की खानदानी पेंशन बंद होने की दास्तां, उमराव बेगम की उपस्थिति में इस खाकसार की गमअंगेज दुनिया और घर-बाहर की ना-उम्मीदों की तामीर की गई है। इसे उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में रंगमंच पर निर्देशक अभिषेक मुद्गल ने पेश किया था। गालिब की भूमिका में समाए प्रांजल उपाध्याय बेहतरीन अदाकार अमिताभ श्रीवास्तव और टॉम ऑल्टर की याद दिलाते हैं। पर इस नए नाटक में माजरा मिर्जा के माजी से जुदा है। नाटककार ने इस नए दौर की पेचीदगियों में ही उसकी मकबूलियत और बेबाकी को भी नए सिरे से तराशा है।
“मेरा अपना जुदा मुआमला है
और के लेन-देन से क्या काम”
नाटक की आधुनिक प्रस्तुति के बीच तीन अहम किरदारों की गुफ्तगू में असद अचानक केंद्र में उपस्थिति दर्ज कराते हुए सहज नजर आते हैं और आखिर तक अंदाजे-बयां वही रहता है। कभी-कभार बातचीत के मर्कज में न रहकर दूसरों की दिलचस्पियों में भी मौजूद हैं। बिला-शक, वे उनके नक्काद ही क्यों न हों। यह बड़ी बात है। अच्छा यह भी है कि नाटककार की कलम ने दस्तावेजीकरण नहीं होने दिया।
नाटक में गालिब के साथ एक खुलेपन का बर्ताव है। इसी खुलेपन के स्पेस में गालिब के जीवन के कुछ संदर्भ पलट कर देखे गए हैं, बुने भी गए हैं और उन्हें एक ख्याल की मानिंद रखते हुए, काफी नजदीकी से नए जमाने की नजर में जानने की कड़ी कोशिश की गई है। प्रथम पात्र विष्णु प्रसाद की फरियाद में फेरबदल महेश की प्रिय छाया की मानसिक बुनावट के कारण है। प्लांचेट माध्यम से मूलतः कबीर के बजाय गालिब की रंगमंच पर औचक उपस्थिति दृश्य के कौतुक को बदलने के लिए भी है, क्योंकि मूलतः नाटक में असद जैसे उलमा की ही कहानी है।
इस ताजादम नाटक के पढ़ जाने से पहले की जमीनें याद आती हैं। उनमें ‘कैद-ए-हयात’ भी शुमार है। मीर के सौ साल के औसाफ ओसारे के बाद जो औज अपने समकालीनों में नुक्ता मुकामे दारद जौक, मोमिन के रहते गालिब को हासिल है, उसका जादू आज तक बना हुआ है। इसे सुरेंद्र वर्मा के नाटक में भी छोड़ दिया गया है। जाती जिंदगी ही वहां भी अहम है। सुरेंद्र वर्मा ने उनको दस्तावेजों में समेटा है (जबकि नए वक्त के दो उपन्यासों ‘मुझे चांद चाहिए’ और ‘दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता’ का जो खुलापन उनकी शैली को हासिल है, उसकी आजमाइश वहां जैसे कतई हो ही नहीं)। सुरेंद्र वर्मा की मंचीय प्रस्तुति ‘कैद-ए-हयात’ की आईनागीरी से बेहतर नहीं। पर यहां भी सादिक साहब के सामने कुछ दिक्कतें हैं, जो ‘इस शक्ल से गुजरी गालिब’ नाटक में भी पेश आई होंगी। एक शहर की मुश्किलें, हयात और तकदीर की कारगुजारियां फकत नाटक के शुरुआती किरदारों महेश, छाया और रिटायर्ड अफसर विष्णु प्रसाद के संवादों को छूकर जाहिर नहीं हो सकती थी।
आखिर गालिब की हस्ती का निचोड़ उसी ख्याल की सूरत सामने आता है, जो असल में फरेब ही तो है हमारी जिंदगी का। यह नाटकीय अंत वाकई खूबसूरत बन पड़ा है। खासकर यह संवाद भी “ख्वाब से जागने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अब भी ख्वाब में ही हूं।” कायनात को समंदर और खुद को कतरा कहने की बातें यकीनन सूफीयाना ही हैं। ताबे-गम में (रहने वालों को) सहने वालों की दुनिया है। उससे राह तो नहीं निकलती। पर दोजहां में एक नक्शों-निगार तो बनता ही है। शायरों की यही फरेब-सिद्धि नाटक के नाम को जरूर सार्थक करती है और एक नया नजरिया देती है।
फरेब-ए-हस्ती
मोहम्मद सादिक
प्रकाशक | लोकभारती पेपरबैक्स
मूल्य: 199 | पृष्ठ: 95