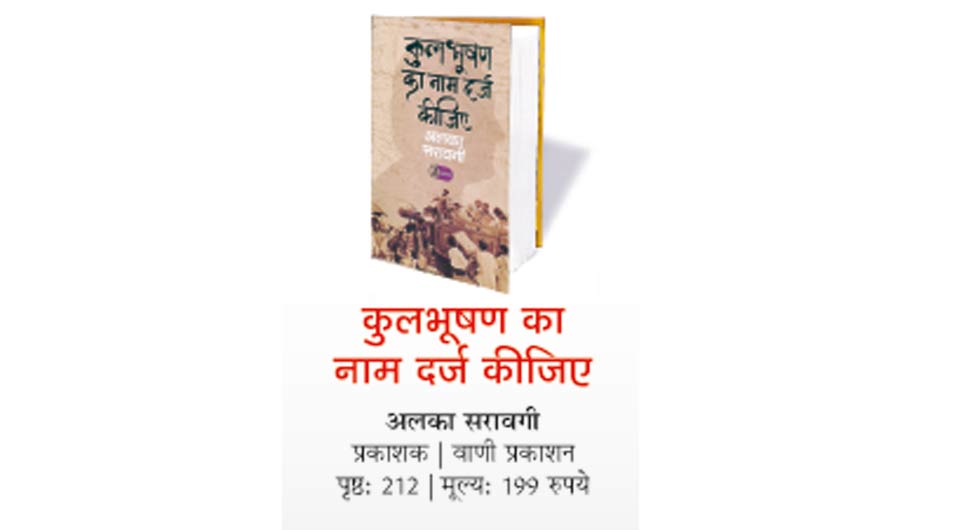अलका सरावगी के लेखन में एक तरह की सघनता होती है, वे पूरे परिदृश्य को कुछ इस सूक्ष्मता से बुनती हैं कि कई बार कथा-प्रवाह कभी कुछ अटकता और कभी कुछ भटकता भी लगता है। लेकिन यह अनुभव बना रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, वह मूल्यवान है और यह वर्तुलाकार संरचना कथा को संपूर्णता देने वाली है।
उनका नया उपन्यास कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए ऐसे समय आया है, जब भारतीय उपमहाद्वीप में पहचान की राजनीति नफरत के चरम पर जा पहुंची है और भारतीय राष्ट्र-राज्य के भीतर नागरिकता के प्रश्न को सांप्रदायिक आधार पर पुनर्परिभाषित करने की साजिश चल रही है। इत्तेफाक से अलका सरावगी के उपन्यास में दोहरे विभाजन की स्मृति है। कहानी कोलकाता से शुरू होती है, लेकिन कहानी है, दरअसल बांग्लादेश के कुष्टिया जिले की, जहां से पहले 1947 में और फिर 1971 में हिंदू परिवार भाग कर कोलकाता आ रहे हैं। लेकिन अलका सरावगी एक पल भी यह भ्रम नहीं रहने देतीं कि यह उपन्यास हिंदुओं के विस्थापन या उत्पीड़न पर है, बल्कि उनकी सधी और संवेदनशील दृष्टि बहुत स्पष्टता से विभाजन और विस्थापन से जुड़े राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की शिनाख्त करती है।
जिस समग्रता और सघनता के जिक्र के साथ इस टिप्पणी की शुरुआत हुई थी, उसका नतीजा यह है कि उपन्यास सिर्फ बंटवारे की राजनीति की कहानी नहीं कहता बल्कि वह परिवारों के भीतर के बंटवारे की, लोगों के भीतर की दरारों की दास्तान भी कहता है। उपन्यास के केंद्र में कुलभूषण नाम का किरदार है, जिसका परिवार मूलतः कुष्टिया का व्यापारी परिवार था। जब हालात बिगड़े तो पिता ने बड़े भाइयों को कोलकाता भेज दिया, जबकि कुलभूषण अरसे तक पिता के साथ रहा। जब सब कुछ लुटा कर उसे कोलकाता आना पड़ा, तो वह अपने ही घर शरणार्थी हो गया। अपने ही घर में उसकी उपेक्षा होने लगी, उस पर चोरी के इल्जाम लगाए गए। कई बार, उससे नौकरों की तरह काम लिया जाता। बेशक, घर के कुछ सदस्य हैं, जो उससे सहानुभूति रखते हैं और आने वाले वर्षों में उसकी भी मदद करते हैं।
कुष्टिया में, व्यापार और सौदे में बहुत होशियार माना जाने वाला कुलभूषण कोलकाता आकर जैसे बिखर जाता है। वह कई तरह के काम करता है, बस में कंडक्टरी भी। पकड़े जाने पर घरवालों से दुत्कारा जाता है। लेकिन अपनी नियति को कुलभूषण ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेता, वह घर छोड़कर कोलकाता के ही दूसरे हिस्से में एक बंगाली लड़की से विवाह कर दूसरी बंगाली-पहचान के साथ बस जाता है। यहां उसका नाम अलग है, उसकी सामाजिक सक्रियता अलग तरह की है और उसका जीवन बिल्कुल अलग है। दो पहचानों के इस द्वंद्व के बीच उसकी जिंदगी बहुत सारी विडंबनाओं पर भी उंगली रख जाती है।
वैसे उपन्यासकार की नजर जितनी बांटने वाले यथार्थ पर है, उतनी ही जोड़ने वाली सच्चाइयों पर भी। उपन्यास में कई उपकथाएं भी हैं। एक कहानी कुलभूषण के बचपन के दोस्त श्यामा धोबी की है, जिसे एक दिन पता चलता है कि वह न हिंदू है न मुसलमान, उसे तो कुष्टिया के लालन फकीर ने पिता के हाथ सौंपा है। वह दंगों में मारे गए एक मुस्लिम दोस्त अली की गर्भवती पत्नी अमला को फिर से पत्नी की तरह अपने घर में जगह और पूरा सम्मान देता है। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम जैसे इस छोटे से परिवार पर थोप दिया जाता है। श्यामा के पिता गोबिंदो धोबी को पश्चिमी पाकिस्तान के सिपाहियों ने मार डाला है। वे कुष्टिया और दूसरी जगहों पर लगातार खून-खराबा कर रहे हैं। अंततः श्यामा और अमला भी इसकी भेंट चढ़ते हैं। दोनों के बीच खामोश रिश्ते की मानवीय काव्यात्मकता। अमला का एक भावनात्मक धागा कुलभूषण से भी बंधा हुआ था। बरसों बाद श्यामा और अमला की बेटी मल्ली यानी मालविका कुलभूषण के पास लौटती है।
लेकिन असल में इस उपन्यास की जान, त्रासदी की उसी कथा में बसी है जिसे हम बेदखली या बंटवारे की राजनीतिक प्रक्रिया मान झटक देते हैं। दंगों ने इंसान को इंसान नहीं रहने दिया है। कुष्टिया के संभ्रांत अनिल मुखर्जी का परिवार एक विवाह में गया है, इस भरोसे से लैस कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वे वहां अरसे से हैं, सबके काम आते हैं, सबकी रोजी-रोटी उन्हीं से चलती है। लेकिन वहां कोई काम नहीं आता। कत्लो-गारत, लूटपाट और बलात्कार की यह वीभत्स कहानी तकलीफदेह है।
बांग्लादेश युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना का अत्याचार कुष्टिया के लड़कों को जैसे बदल देता है। जो श्यामा बचपन में एक चिड़िया नहीं मार पाता था, वह मुक्ति संग्राम के दिनों में बंदूक उठाता है। यह लड़ाई धार्मिक नहीं है। डॉ. कासिम पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस लड़ाई के अगुआ हैं। उपन्यास में इस मुक्ति संग्राम के एक अंश की कहानी बहुत जीवंत ढंग से दर्ज है। अनिल मुखर्जी की तलाश में कुलभूषण दंडकारण्य तक चला जाता है। इस यात्रा में उसे कई लोग मिलते हैं, जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, खुद को भी और अब वे जीवन भर अपने बसने का खुरदरा सपना देख रहे होते हैं। कुलभूषण को यहीं यह मालूम होता है कि जिसे हम विस्थापन कहते हैं, उसकी कथा तो खत्म हुई ही नहीं है। वह 1947 और 1971 तक ही सीमित नहीं है, अब तक जारी है। दुनिया ऐसे ही विस्थापितों और शरणार्थियों का देश नहीं बन गई है।
जिस समय घनघोर सांप्रदायिकता और बजबजाती घृणा को हमारे समाज में पूरी बेशर्मी से एक मूल्य में बदला जा रहा है, तब अलका सरावगी का यह उपन्यास बताता है कि यह सांप्रदायिकता कितनी छिछली होती है, कितनी खोखली होती है और अंततः वह किस तरह व्यक्ति और समाज को पीढ़ियों तक तोड़ डालती है। कुलभूषण जैन गोपाल चंद्र दास बन कर एक पूरी उम्र जी लेता है और डरता रहता है कि उसकी मूल पहचान नष्ट न हो जाए। जिस पत्रकार को वह अपनी कहानी सुनाता है, उसे बार-बार कहता है, “वह याद रखे, उसका नाम कुलभूषण है।”
अपने हर उपन्यास में अलका सरावगी जैसे एक अलग शिल्प चुनती हैं। लेकिन सबमें एक बात समान होती है, वर्तमान और अतीत के बीच वह आवाजाही जिसमें जीवन और समाज को संपूर्णता में देखने का जतन होता है।
इस उपन्यास से गुजरना इतिहास और राजनीति के एक बड़े द्वंद्व से गुजरना है और यह याद करना है कि अंततः यह क्षत-विक्षत मनुष्यता ही है, जिसमें हमारे जीने का मोल बचा रहता है।
कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए
अलका सरावगी
प्रकाशक | वाणी प्रकाशन
पृष्ठः 212 | मूल्यः 199 रुपये