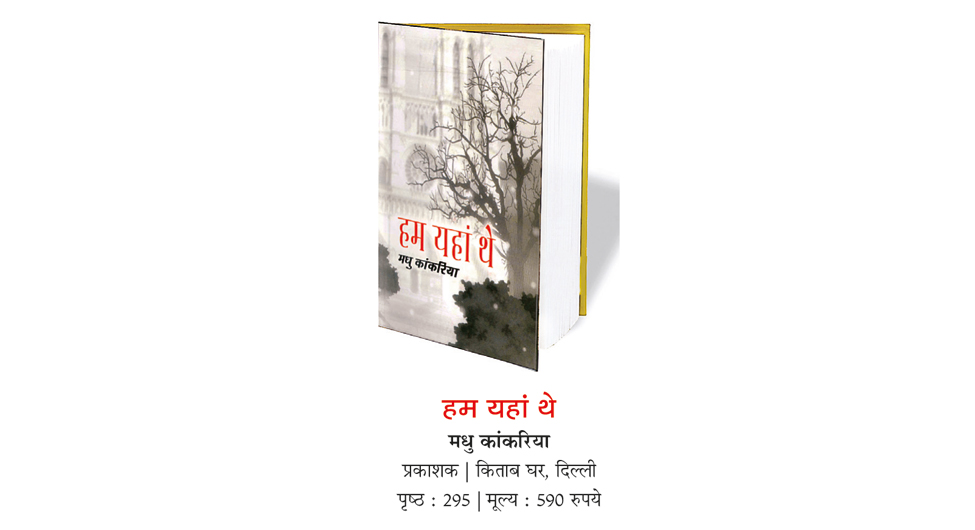मधु कांकरिया अपनी कहानियों और उपन्यासों में सामाजिक विमर्श के फलक को अधिक विस्तृत बनाने की कोशिश करती दिखती रही हैं। लेकिन यह समय कुछ ज्यादा ही ‘कातिल और चुप्पा’ है इसलिए मानो उन्हें उद्घोष करना पड़ा कि, हम यहां थे। यह उपन्यास पढ़ते हुए पाठक के सामने आज के राजनैतिक हालात की अनेक छवियां झिलमिलाने लगती हैं। इन पंक्तियों पर गौर कीजिए, “आसन्न चुनाव की अधिकांश फंडिंग इसी प्रोजेक्ट से आने वाली थी। आगे भी सिलसिला जारी रहने की भरपूर उम्मीद थी इसलिए दहशत और गुंडागर्दी के बल पर लगभग दस हजार एकड़ जमीन कंपनी के नाम रजिस्टर हो चुकी थी। प्रोजेक्ट वाले पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई थी। स्टेट पुलिस तैनात थी। बाहर वालों को, पत्रकारों को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, शोधकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सभी को फेंसिंग के भीतर जाने से रोक दिया गया था।”
यूं तो यह मंजर कई घटनाओं की याद दिला देगा। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता के प्रोजेक्ट की भी याद दिला सकता है, जहां हाल ही में प्रदूषणकारी उद्योग को हटाने के लिए प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलाई, कई लोग मारे गए लेकिन वह प्रोजेक्ट नहीं हटा।
उपन्यास की कथा भूमि झारखंड को बनाया गया है, जहां आदिवासी भी हैं और माओवादी भी। वहां एक कंपनी के प्रोजेक्ट की खातिर 24 गांवों की जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार की ओर से और अपनी जमीन बचाने के लिए आदिवासियों की ओर से संघर्ष चल रहा है। वहां “कहीं जोर-जबरदस्ती, खून, हत्या और बलात्कार के डर से तो कहीं उधारी-कर्ज से दबे, तो कहीं डिफॉल्टर होने के चलेते कोर्ट के वारंट से थरथराते... कानून की पहुंच के बाहर खड़े अधिकांश गांव वालों ने जमीन बेचने के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।” लेकिन “फसाद की जड़” एक फुलवा थी जिसके दस एकड़ जमीन का मामला फंसा हुआ था। उसकी अंधी बूढ़ी मां की एक ही गुहार थी, “जिंदगी इहीं गुजार दिहा, अब पराई जमीन पर न मरब। कुछ भी होई जाए अपने जीयतब हम इ आपन घर न छोड़ब। आपन आदमी के हाथों लगावा जामुन और पीपर के पेड़ के नीचे मरब।”
आखिर वही हुआ। एक दिन अखबार में छपा फुलवा “पुलिस मुठभेड़ में मारी गई।” उसके बदन पर माओवादी वर्दी थी और कई हथियार। इसमें आप हाल के दौर की कई कथाएं झारखंड ही नहीं, छत्तीसगढ़ और दूसरे आदिवासी अंचलों में तलाश सकते हैं। यहां आपको सोनी सोरी की छवि भी याद आ सकती है।
लेकिन उपन्यास का फलक और विस्तृत करती है इसकी नायिका दीपशिखा। वह कोलकाता के किसी अच्छे-खासे परिवार की है, जो पहले आदिवासी अंचलों पर अध्ययन और फिर नायक जंगल कुमार के साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ने वहां पहुंच जाती है। कोई चाहे तो नायिका में सत्तर-अस्सी के दशक में ब्रिटिश लेखिका मेरी टेलर की छवि देख सकता है, जो अपने प्रेमी एक नक्सल लड़के के साथ झारखंड और उससे लगे बंगाल के आदिवासी अंचलों में जाती है और फिर जो हुआ, वह उनकी किताब में दर्ज है।
आपको यहां विनायक सेन की छवि भी दिख सकती है। नायिका दीपशिखा इस कथा में नारीवादी विमर्श को भी लेकर आती है और बेमानी विवाहों के विमर्श को भी नए मुकाम पर ले जाती है। इस विमर्श में पाठक को शहरी, मध्यवर्गीय आदमी की विशुद्ध उपभोक्तावादी, संवेदनहीन जिंदगी का भी खाका मिलता है। यही वह वर्ग है जो विकास के नाम पर हर अन्याय को जायज ठहराता चलता है।
यह उपन्यास आज की राजनीति का वह कुत्सित चेहरा सामने लाता है जिसे विकास और संसदीय लोकतंत्र जैसे कई आवरणों में छुपाया जाता है। भाषा को लेकर नए प्रयोग भी हैं। ये प्रयोग ही इस उपन्यास को पठनीय बनाते हैं। स्थानीय बोली की कुछ असंगतियां हैं लेकिन यह बहुत गौण है। उपन्यास गंभीर रिपोर्ताज की तरह सच्चाइयों को उद्घाटित करता है, यही इस रचना को महत्व देता है। यह उपन्यास आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा।