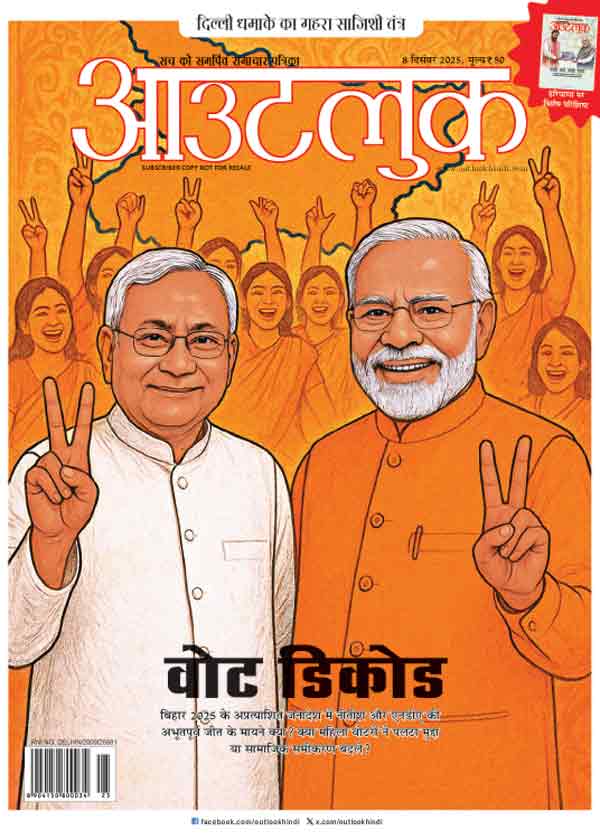हाल में जयंत चौधरी राज्यसभा के लिए चुने गए तो अपनी प्राथमिकताओं में दो बातों का जिक्र किया। एक, जाति जनगणना और दूसरे, किसानों की समस्याएं। हालांकि राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) अध्यक्ष आरक्षण या जाति की बातें कम ही करते आए हैं, बल्कि खुद को किसानों का पैरोकार ही कहलाना पसंद करते हैं। पिछड़ी जातियों और आरक्षण के वाजिब दायरे की मांग के प्रबल दावेदारों के बीच क्या जयंत की भी पहली प्राथमिकता विपक्षी राजनीति के किसी नए नैरेटिव की ओर इशारा करती है? क्या जाति जनगणना का मुद्दा मौजूदा सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान के कथित बहुसंख्यकवादी और हिंदुत्ववादी नैरेटिव के बरअक्स तगड़ी जमीन मुहैया करा सकता है? बेशक, मुद्दा पुराना है और मौजूदा सत्ता बिरादरी के लिए सियासी परेशानी का सबब भी बन सकता है, क्योंकि उसकी सोशल इंजीनियरिंग की योजना में सामाजिक न्याय कम है, बल्कि यथास्थिति बनाए रखकर समाज में नई गोलबंदी करना है। शायद इसी लिए जातियों से जुड़े किसी मुद्दे का खुलकर विरोध नहीं दिखता, लेकिन उनसे ध्यान हटाकर नई पहचान की धारा में सबको एक रंग करने की कोशिश दिखती है। इसलिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में आखिरी क्षण में जाने से पहले प्रदेश भाजपा ने यह अजीब स्पष्टीकरण जाहिर किया कि वह सिर्फ दो जातियां जानती है- गरीब और अमीर। जाहिर है, इस बयान का मतलब यह तो नहीं हो सकता कि भाजपा वामपंथ की ओर झुकने लगी है। इसका मतलब तो जातियों के मुद्दे छेड़ने से परहेज हो सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या सामाजिक न्याय की राजनीति की धारा इस कदर प्रवाहमान बनी हुई है कि उससे नया नैरेटिव तैयार हो सकता है।
जाति जनगणना की नई बहस के विंदुओं पर गौर करने से इसके मौजूदा सियासी निहितार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। हाल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जो मुद्दे मजबूत विपक्ष की बानगी बने थे, उनमें जाति जनगणना एक सशक्त मुद्दा बना था। चुनावों के कई महीने पहले समाजवादी पार्टी (सपा) के अखिलेश यादव ने कुछ पिछड़े नेताओं को अपने साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मजबूत चुनौती देने की फिजा तैयार की थी। अलबत्ता, उसमें किसान आंदोलन और सरकार विरोधी रुझानों की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन चुनौती इतनी बड़ी नहीं हो पाई कि जीत दिला सके या कहें कि जीत को हाथ से फिसलने न दे, क्योंकि भाजपा के 3.80 करोड़ वोटों के मुकाबले सपा गठजोड़ को 3 करोड़ वोट मिले थे। मतलब यह कि जाति जनगणना का मुद्दा लोगों को छू तो सकता है, लेकिन शायद उसकी अपील को जोरदार बनाने की दरकार होगी।

सत्ता समीकरणः राजद नेता तेजस्वी यादव और मनोज झा
यह जोरदार तभी बन सकता है जब आरक्षण की संभावनाएं बढ़ें और उसके लाभ के सिकुड़ते दायरे भी विस्तृत हों। यही वजह है कि देश की तमाम पिछड़ी और दलित जातियों के नेता ही नहीं, बल्कि लगभग सभी विपक्षी पार्टियां निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग कर रही हैं क्योंकि सरकारी क्षेत्र का दायरा लगातार सिकुड़ रहा है और केंद्र की मौजूदा सरकार की घोषित नीति भी निजीकरण को प्रश्रय देने की है। इसलिए निजीकरण का विरोध भी इस राजनीति का एक अहम हिस्सा है। अलबत्ता, कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों के निजीकरण के विरोध में भी शायद उस नैरेटिव की तलाश है, जो मौजूदा सत्ता के हिंदुत्व के अफसाने की काट दिला सके।
लेकिन यह कोई अबूझ पहेली नहीं है कि भाजपा को जाति जनगणना से क्यों परहेज है। उसके लिए दक्षिणपंथी और नव-पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति अपने रुझान से बड़ी उलझन ऊंची जातियों की है, जो उसका मूल आधार बनी हुई हैं। कई जानकारों का मानना है कि 1990 में वी.पी. सिंह की सरकार के मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के फैसले के बाद देश के कई हिस्सों में आरक्षण विरोधी आंदोलन को भाजपा की शह थी और उसी की काट के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, जो अयोध्या में राम मंदिर के लिए थी। उसी यात्रा के बाद से देश में सांप्रदायिक तनाव और मोटे तौर पर बहुसंख्यकवादी राजनीति का जोर बढ़ा, जिसका 2014 के बाद से दबदबा बढ़ता जा रहा है। जाहिर है, पिछड़ी जातियों के संख्याबल के हिसाब से आरक्षण मिलने लगा तो सामान्य कोटे का दायरा सिकुड़ेगा। ऊंची जातियों और जाट, पटेल, मराठा, कम्मा जैसी दबदबे वाली जातियों की आशंकाओं और मांग को शांत करने के लिए ही मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। कई जानकारों का मानना है कि भाजपा और संघ परिवार ने अपने प्रचार-तंत्र के जरिए ऊंची जातियों में यह संदेश पहुंचाया है कि पिछड़े और दलितों को वे उन पर हावी नहीं होने देंगे। इसके संकेत इससे भी मिल सकते हैं कि 2017 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में पिछड़े नेताओं को आगे करके जीत हासिल करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी गई और 2021 में तमाम अंतर्विरोधों के बाद भी उन्हें ही गद्दी मिली। इसके अलावा संघ परिवार का हिंदुत्व का बड़ा एजेंडा तो है ही।
हालांकि भाजपा यह जानती है कि पिछड़े और दलित-आदिवासियों के एक बड़े वर्ग के वोट के बिना उसे सत्ता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए 2014 के चुनावों में उसने जाति जनगणना पर हामी भर दी थी और 2019 में भी नरेंद्र मोदी को पिछड़े नेता के रूप में पेश किया गया। लेकिन सितंबर 2021 में उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना करना संभव नहीं है क्योंकि यह प्रशासनिक तौर पर मुश्किल और पेचीदा है। उसने यह जवाब महाराष्ट्र सरकार की याचिका के जवाब में दाखिल किया था, जिसमें मांग की गई थी कि 2021 की जनगणना में ग्रामीण भारत में पिछड़े वर्गों के लोगों के आंकड़े केंद्र सरकार जुटाए। याचिका में 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आंकड़े भी जारी करने की मांग की गई थी। इसे भी केंद्र ने अपूर्ण और उलझन भरा बताकर जारी करने से मना कर दिया। सरकार ने यह माना कि ये आंकड़े सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास पांच साल से हैं, लेकिन आंकड़ों में गड़बड़ियों के कारण उस पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया की अगुआई में एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। लेकिन समिति के दूसरे सदस्य तय नहीं हो पाए तो उसकी एक भी बैठक नहीं हो पाई। दरअसल गड़बड़ी की आशंका की वजहें यह बताई जाती हैं कि 2011 की गणना के पहले जातियों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। मसलन, 1931 की आखिरी जाति जनगणना में राष्ट्रीय स्तर पर 4,147 जातियां दर्ज हैं जबकि 2011 की सामाजिक-आर्थिक गणना में 46 लाख विभिन्न जातियों का जिक्र है। सरकार की दलील है कि संख्या बेहिसाब है इसलिए गड़बड़ियों की भारी आशंका है। फिलहाल केंद्र की सूची में 2,479 ओबीसी जातियां हैं और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 3,150 ओबीसी जातियां हैं।

सुशील मोदी
केंद्र की दलील यह भी थी कि यह नीतिगत मामला है इसलिए अदालती समीक्षा के दायरे से बाहर है। 2011 में केंद्र की यूपीए सरकार ने अपने सहयोगी दलों के दबाव में यह गणना कराई थी, लेकिन इसके आंकड़े जाहिर नहीं किए गए। जाहिर है, उन सहयोगियों में राजद, सपा, जनता दल के धड़े, वामपंथी पार्टियां, द्रमुक वगैरह सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले कई दल थे। हालांकि जाति जनगणना की जरूरत देश में गैर-बराबरी की चौड़ी होती खाई से भी महसूस की जा सकती है। 2020 की ऑक्सफाम की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऊपरी पायदान के 10 प्रतिशत लोगों के पास 74.3 प्रतिशत संपत्ति है जबकि मध्यम पायदान के 40 प्रतिशत लोगों के पास 22.9 प्रतिशत और निचले पायदान की 50 प्रतिशत आबादी के पास सिर्फ 2.8 प्रतिशत है।
इसी तरह की गैर-बराबरी और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने की आवाज आजादी के आंदोलन से ही उठने लगी थी, जिसका समाधान सकारात्मक भेदभाव यानी आरक्षण व्यवस्था में तलाशा गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था संविधान से ही तय हो गई। अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण की सिफारिश के लिए 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग की सिफारिशों में प्रमुख विंदु थेः 1961 में जातिवार जनगणना की जाए, सभी स्त्रियों को पिछड़ा माना जाए, सभी तकनीकी तथा पेशेवर शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों के लिए 70 प्रतिशत आरक्षण हो, सरकारी महकमे में क्लास 1 में 25 प्रतिशत, क्लास 2 में 33 प्रतिशत और क्लास 3-4 में 40 प्रतिशत आरक्षण हो। लेकिन कुछ असहमतियों के कारण सरकार ने आयोग की रिपोर्ट खारिज कर दी।
उसके बाद 1979 में जनता पार्टी की मोरारजी सरकार ने देश में शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और सिफारिशों के लिए बी.पी. मंडल की अगुआई में आयोग का गठन किया। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1931 की जनगणना के आधार पर देश में पिछड़ी जातियों की आबादी 52 प्रतिशत है, जिसके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई। इस पर 1990 में वी.पी. सिंह सरकार ने अमल करने का फैसला किया। बाद में इंदिरा साहनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षण किसी भी हालत में 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता। अनुसूचित जातियों-जनजातियों के करीब 22 प्रतिशत को मिलाकर कुल आरक्षण 49 प्रतिशत बैठता है।
लेकिन पिछड़े नेता हमेशा मांग करते रहे हैं कि आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए जातिवार जनगणना जरूरी है। काशीराम का तो नारा ही था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी हिस्सेदारी। विडंबना यह भी है कि आरक्षण के इतने दिनों बाद भी सरकारी महकमों में अनुसूचित जातियों-जनजातियों और ओबीसी की हिस्सेदारी बमुश्किल 3-4 प्रतिशत हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट इधर अपने कई फैसलों में कह चुका है कि उपयुक्त गणना के अभाव में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के तर्क बेमानी हैं। जो भी हो, पेच कई हैं और सियासी पेच सबसे बड़ा है।