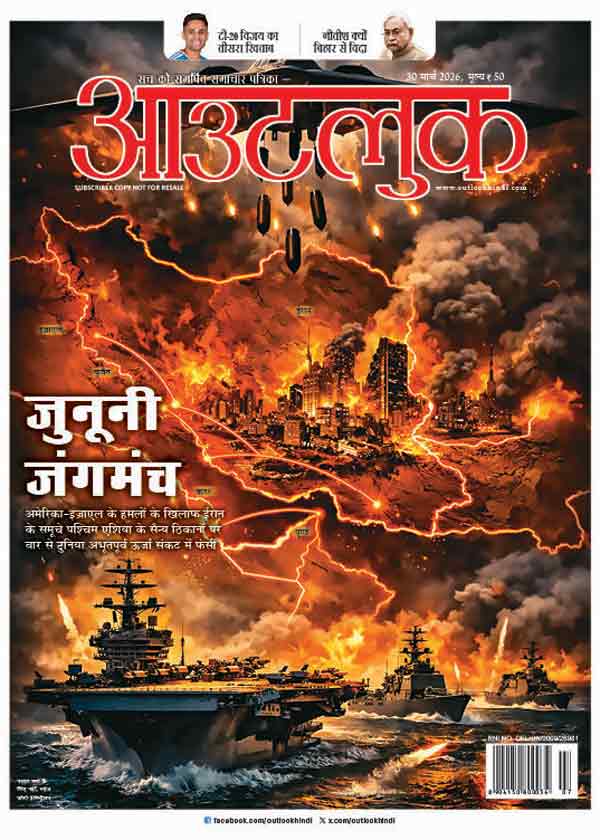भारत में लोग हर तरह की आजादी को अपना नैसर्गिक अधिकार मानते हैं। उन्हें किसी का हुक्म बजाना पसंद नहीं। आजादी का खयाल भारतवासियों के मानसपटल पर बहुत गहराई से अंकित है। चाहे वह अपने लिए कोई धर्म चुनना हो या फिर किसी बाबा या गुरु का चेला बनना या फिर अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करना, लोग ज्यादातर अपने मन की ही करते हैं। यहां तक कि वोट डालने के मामले में भी यह आम बात है कि लोग पैसा किसी पार्टी से लेकर, वोट अपने मन की पार्टी को डाल देते हैं। देश के इतिहास में ऐसा एक भी दार्शनिक नहीं हुआ, जिसने आजादी के बारे में कुछ कहा हो। आजादी क्यों जरूरी है, उसका क्या मूल्य है, उसकी क्यों रक्षा करनी चाहिए जैसे सवाल यहां बेमानी रहे हैं। चर्चा का झंझट हमने यूरोप के दार्शनिकों के लिए छोड़ा है। वहां आजादी वाकई एक दुर्लभ वस्तु थी, सो वे उसके बारे में सोचते भी ज्यादा थे।
जितना परहेज भारतवासियों को आदेश लेने में है, उतना ही परहेज भारत में सरकारों को आदेश देने में रहा है। यह जरूर है कि अंग्रेज सरकार ने समाज बदलने की थोड़ी-सी कोशिश जरूर की थी, पर जब 1857 में ऊंची जाति के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने गदर किया, तो अंग्रेजों ने समाज में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। उसके बाद, अंग्रेजों ने अपना राज केवल टैक्स इकट्ठा करने तक सीमित रखा। फौज में भारतीयों की भर्ती खुले दिल से जारी रही। फौज का इस्तेमाल देश में अपनी तानाशाही बरकरार रखने के लिए भी खूब किया। पर जो भी ब्रिटिश फौज में भर्ती हुआ, अपनी मर्जी से हुआ। यहां तक कि 1942 में प्रसिद्ध सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने फौज के चक्कर में, ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में भाग लेने से ही इनकार कर दिया। उनके मुताबिक सिखों को ब्रिटिश फौज में शामिल होने और जंग पर जाने से लाभ होता था। नतीजतन, 1941 के सत्याग्रह आंदोलन की तरह 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी, पंजाब में बेअसर रहा।
आजादी के बाद, 1950 और 1960 के दशक के समाजवादी रुझान के तहत केंद्र सरकार ने एक बार फिर बदलाव लाने की कोशिश की। भारत को आधुनिक युग, औद्योगिक क्रांति और विकास की तरफ खींचने की यह कोशिश भी 1970 के दशक तक नाकाम हो गई। समाजवाद में अंतर्निहित स्टेट कंट्रोल लोगों को नहीं भाए। कई लोगों ने सिस्टम को उल्लू बनाने के तरीके ढूंढ़ निकाले। इस कार्य प्रणाली को लोगों ने नाम दिया ‘भ्रष्टाचार’। “सौ में से निन्यानब्बे बेईमान, फिर भी मेरा देश महान” का नारा लगाते हुए लोगों ने इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया।
वैसे तो भारतवासी अपनी परवाह नहीं करते हुए भी ताकतवर से ताकतवर शक्ति को चुनौती देने में हिचकते नहीं हैं। एक निर्दोष अंग्रेज की हत्या करने के बाद 21 साल के भगत सिंह ने संसद में बम फेंका और खुद ही अपने को गिरफ्तारी के लिए शासन के हवाले कर दिया। इस तरह की वीरता भारत में आम बात है। भारतीयों को अगर परेशानी है तो सिस्टम से बंध कर काम करने में।
यह माना जाता है कि भारत में जाति ही ऐसी प्रणाली है जो कई हजार साल से समाज को किसी सिस्टम में बांधे रखी है, पर ये महज खयाल है। असलियत में जाति-प्रथा केवल एक-दूसरे को नीचा दिखाने तक सीमित है। यह तथाकथित प्रथा अपने को दूसरों से बड़ा समझने पर आधारित है। प्रथा का तो सिर्फ बहाना है। इसकी आड़ में धनी और ताकतवर लोग अपने से कमजोर लोगों को नीचा दिखाते हैं।
बहन मायावती के सामने अजीत सिंह जैसे कद्दावर जाट नेता का जूता उतार कर नमन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मायावती से पहले, ज्योतिरादित्य शिंदे (शिंदे का ‘सिंधिया’ नामकरण तो अंग्रेजों की करनी है) के पूर्वज और महान शिवाजी जाति की सीमाएं तोड़ चुके थे। आज भी आए दिन हजारों लड़के-लड़कियां अपने माता-पिता और समाज को दो टूक जवाब देते हुए, अपने से छोटी जाति वालों के साथ मनमर्जी शादी करते हैं।
दो हजार साल पहले, गौतम बुद्ध के जन्म की कहानियों में, अनेक बार बताया जाता है कि आम जनता ने अन्याय के खिलाफ बगावत की, और हथियार उठाए। कई जातक कथाओं में ऐसे भी वाकये हैं जहां अत्याचारी राजा को मौत के घाट उतारा गया।
अगर लोगों को शासन और शासकीय व्यवस्था कबूल नहीं थी, तो अक्सर वे राज्य छोड़ कर चले जाते थे। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। पश्चिम भारत में, वर्ष 1669 में, समकालीन अंग्रेज फैक्ट्री रिकॉर्ड्स में जिक्र है कि व्यापारियों ने विरोध के तौर पर सूरत शहर का बहिष्कार किया। इस वाकये की वजह थी, एक व्यापारी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाना। दरअसल, काजी ने बहाना बनाया कि उस व्यापारी ने कुछ साल पहले काजी के साथ तरबूज खाया था; इसी लिए उसे अब इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। इस पर व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद जब उसी काजी ने एक अन्य व्यापारी, तुलसीदास पारेख के भतीजे को इस्लाम धर्म कबूलने के लिए मजबूर किया, तो लगभग 8,000 व्यापारियों ने अंग्रेज शासित बॉम्बे में शरण लेने के लिए सूरत शहर को छोड़ दिया।
गेराल्ड औंगियर सूरत फैक्ट्री के अध्यक्ष और बॉम्बे के गवर्नर भी थे। उन्होंने व्यापारियों को शरण देने से मना कर दिया। गेराल्ड औंगियर को शायद औरंगजेब के कहर का डर था। बीच का रास्ता चुनते हुए उन्होंने व्यापारियों को सलाह दी कि वे अहमदाबाद जाएं और अपने राजा से न्याय की गुहार करें। काजी भड़क गया। उसने हिंदू मंदिरों को गिराने की धमकी दी। यह भी धमकी दी कि हिंदू व्यापारियों का खतना किया जाएगा। व्यापारियों ने उसे भाव नहीं दिया। काजी ने तब सूरत के गवर्नर से हस्तक्षेप करने की अपील की। गवर्नर ने इसमें अपनी लाचारी जताई। इस बीच व्यापारी अपनी पत्नियों और बच्चों को पीछे छोड़ भड़ूच में बस गए। जो पीछे रह गए, उन्होंने भी अपनी दुकानें बंद कर दीं। अहमदाबाद के गवर्नर ने व्यापारियों को शहर में आने और बसने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आखिरकार, व्यापारी तभी सूरत लौटे जब गवर्नर ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा वाकया और जुल्म फिर कभी नहीं होगा।
भारत के इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां कस्बों और गांव के लोग अपने अधिकारों को राजा से लिखवा कर अपना हक प्रदर्शित करते थे। छठी सदी ईस्वी में गुजरात क्षेत्र में, लोहात गांव के व्यापारियों ने सामंत विष्णुसेन से अपने अधिकारों को एक आचार-स्थिति-पत्र में लिखवाया और इसे एक ताम्र पत्र पर उकेरा। इसे ‘लोक-संग्रह-अनुग्रह-अर्थम’ भी कहा गया है।
इस अभिलेख में कई प्रकार के टैक्स की दर, सीमा शुल्क, कानूनी प्रक्रियाएं, विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माना और शोषण से सुरक्षा के लिए प्रचलित रिवायतों की एक लंबी सूची है। टैक्स की दर बयान करते हुए यह भी बताया गया है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर रियायती दर से टैक्स लगाया जाएगा। जब किसी की भी बेवारिस मौत हो तो उसकी जायदाद राजा जब्त नहीं कर सकता, उसकी जायदाद का फैसला स्थानीय रीति-रिवाजों के हिसाब से होगा। राजा के अधिकारियों के जबरन घरों में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। जब वे गांव का दौरा करते, तो इस पत्रक के अनुसार, गांववासियों को अधिकारियों के रहने और खाने का बंदोबस्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। यज्ञों/बलिदानों या विवाह समारोहों में व्यस्त लोगों को अदालत में तलब नहीं किया जा सकता था। लेन-देन और ऋण के मामले में अगर आरोपी प्रतिभु या सेक्योरिटी देने में सक्षम हो, तो उसकी जमानत होगी और उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। दूसरे जिलों से आए व्यापारियों को महज इस संदेह में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था कि वे स्थानीय नहीं हैं।
यदि आपने यूरोपीय और ब्रिटिश इतिहास का अध्ययन किया है, तो आपको याद होगा कि राजा के निरंकुश अधिकार को सीमित करने के लिए इस तरह का एक चार्टर 600 साल बाद, 12वीं शताब्दी में, इंग्लैंड में बनाया गया था। यह मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लैंड में लोकतंत्र का पहला कदम कहा गया है। पर इसमें तो सिर्फ ताकतवर सामंतों की राजा से रक्षा की बात कही गई थी। अंग्रेज व्यापारी और जनता तो राजा की निरंकुशता के शिकार बने रहे।भारत में परिस्थिति अलग थी। यहां समाज में आम जनता द्वारा हक प्रदर्शन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मालाबार क्षेत्र में 17वीं सदी के अंत में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा को एक ऐसा समझौता करने पर मजबूर किया, जिसके तहत भारतीय व्यापारियों और किसानों को बाजार से सस्ते दामों पर कंपनी को काली मिर्च बेचनी पड़ती। लेकिन डच इसे लागू कराने में कभी सफल नहीं हो पाए। काली मिर्च ज्यादातर बाजार भाव पर ही बेची गई। 1735 से 1743 तक मालाबार में डच कंपनी के प्रभारी गवर्नर जूलियस वैलेंटीजन स्टीन वैन गोलेसी ने लौटकर अपने संस्मरण में लिखा, “(भारत में) जनता राजा की आज्ञा तभी तक मानती है, जब तक वह मर्यादा के भीतर रहे। अगर राजा पूरे समाज के हित को चोट पहुंचाने वाला आदेश जारी करे, तो उसका आदेश कभी नहीं माना जाएगा।” जो लोग भारतीय संस्कृति के डीएनए से परिचित नहीं हैं, वे ही भारत में आजादी की कमी की बातें करते हैं। ऐसे लोग यूरोप के इतिहास को ही ध्यान में रखकर भारत में भी एक ताकतवर दक्षिणपंथी, यानी राइट विंग, शासन की कल्पना करते हैं। दक्षिणपंथी या वामपंथी होने से पहले कोई शासकीय व्यवस्था तो होनी चाहिए। बात यह है कि भारत में शासन-व्यवस्था भेड़िया कम और भेड़ ज्यादा मालूम पड़ती है।
आधुनिक राज्यों में सिर्फ कानून बता सकता है कि नागरिकता का क्या आधार है, नागरिकों के क्या हक हैं, वगैरह। भारत ही शायद ऐसा देश है जिसमें लोग कानून को यह हक भी नहीं देना चाहते। हजारों साल में जिस देश में लोगों पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहा हो उसमें इस तरह की प्रवृत्ति का होना सामान्य है। एक समय था जब राजा के अधिकार मर्यादित थे और लोग-बाग अपने इलाके में अपने पारंपरिक कानून मानने के आदी हो चुके थे। स्वतंत्र भारत में लोगों को भारत के संविधान के अनुसार काम करना पड़ा। संविधान तो राजनेताओं ने बड़े जोश से बना लिया, पर जब लोगों पर उसे लागू करने की बात आई, तो वे कतराने लगे। आलोचक इसे ‘अपीजमेंट की राजनीति’ कहने लगे।
भारत की मौजूदा सरकार राजकाज की एक ऐसी नई प्रणाली स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिसकी भारतीय इतिहास या परंपरा में कोई मिसाल नहीं है। लोग समय पर टैक्स दें, टैक्स चोरी न करें, गलत काम करने वालों को सजा मिले, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाए, जनता को जनता का हक मिले, न कि उसे बिचौलियों के भरोसे जीना पड़े। इतना थोड़ा-सा भी करने पर लोग सरकार पर असहनशील होने का आरोप लगाते हैं। असहनशील भारत का ऐसा नारा है, जो जन अधिकारों के हनन का जिक्र कम और शासन की इस नई परिभाषा पर गुस्सा ज्यादा दर्शाता है।
भारत में राज्य को चुनौती देने को प्रतिबद्ध असंतोष के कई रूप बेहद दिलचस्प हैं। उदाहरण के तौर पर, माकपा (माओवादी) ने राज्य को चुनौती देने की रणनीति गढ़ने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया, जिसमें देश में क्रांति लाने के लिए छात्रों, कर्मचारियों, महिलाओं, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को कठपुतली बनाने की अनुशंसा की गई। कहा गया कि अलग-अलग समुदायों को उनके भावनात्मक मुद्दों पर बांट कर, दंगों तथा हिंसा को भड़काने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय संविधान नागरिकों को आजादी से अपनी बात कहने का अधिकार देता है और उस अधिकार में असहमति जताने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन इस अधिकार में एक बंधन यह है कि लोगों के बीच झगड़ा न कराएं, झगड़े को न उकसाएं, नफरत से भरे भाषण न करें।
इस साल अप्रैल में जब चुनाव आयोग ने नेताओं के ऐसे भड़काने वाले भाषणों पर रोक लगाने में अपनी लाचारी जताई, तो उसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ी। उसके बाद 15 अप्रैल को चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ, बहन मायावती, आज़म खान और मेनका गांधी को 48 से 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया।
जब किसी ताकतवर को उसके गलत और बेहूदा रवैए के लिए फटकारा जाता है, तो हम खुश होते हैं। इसी तरह, जब साधारण लोग गड़बड़ी पैदा करने के लिए संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगें, तो उन्हें लताड़ लगाया जाना भी स्वाभाविक है। लेकिन शासन का बिलावजह सिर्फ लताड़ मारने के लिए लताड़ मारना कोई नैतिक बात नहीं हो सकती है।
(लेखक पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हैं)