एक गृहिणी रसोईघर से फुर्सत पाकर कुछ पंक्तियां लिखती है और उसे फेसबुक पर पोस्ट कर देती है। सोलह साल का युवक, जो सॉफ्टवेयर या संगीत सीखता है, अपनी उधेड़बुन की ताजा कविताएं ब्लॉग पर शाया करता है। दूसरा ब्लॉगर उन पर प्रशस्ति-परक टिप्पणी लिखता है। अधेड़ कवि किसी युवती के नाम से नव-शृंगारिक कविताएं लिख डालता है और उन्हें चर्चित करा ले जाता है। एक फेसबुकिया कवि को कविता या लघुकथा के लिए शाम होते-होते डेढ़-दो सौ ‘लाइक्स’ मिल जाते हैं तो वह घोषणा करता है, “मुझे आलोचकों की परवाह नहीं।” एक प्रकाशक फेसबुक खंगालता है और एक सौ या दो सौ ‘फेसबुक कवि’ नाम की किताब प्रकाशित करके एक नवोदित काव्य विधा पर मुहर लगा देता है। एक महिला कवि का रचना संसार सोशल मीडिया तक सिमटा हुआ है और उसे किताब प्रकाशित कराने से सरोकार नहीं है।
यहां वे सभी प्रतिमान, जो साहित्य-आलोचना की कसौटी माने जाते थे, ढहे हुए दिखते हैं (जब समाज में ही आलोचना की जगह सिकुड़ गई हो तो कविता में वह कैसे बची रह सकती है?) मैथिलीशरण गुप्त की राम-कथा के संदर्भ में कही बात आज और भी सच है, ‘कोई कवि बन जाए, सहज संभाव्य है।’ सतह पर अकविता, विचार कविता, युयुत्सु कविता, साठोत्तरी कविता, भूखी कविता, नई कहानी, सन साठ के बाद की कहानी, अकहानी, समान्तर कहानी जैसे आंदोलन नहीं हैं, लेकिन साहित्य का कैनवस विस्तृत हो गया है। उस पर कई रंग और रूप बन, बिगड़ और उभर रहे हैं। सोशल मीडिया, ब्लॉग, फेसबुक, मोबाइल जैसे मंचों-माध्यमों की गहमागहमी ने उसे पहले से कहीं अधिक लोकतांत्रिक बना दिया है और उसकी ‘विशिष्टता’, ‘अद्वितीयता’ खत्म कर दी है। इस हलचल के बीच वह कविता भी है जिसके रचनाकार इक्कीसवीं सदी की कविता का व्यक्तित्व निर्मित कर रहे हैं। इनमें महिलाएं बड़ी तादाद में हैं।
आज की कविता और कहानी पहले से कहीं ज्यादा मध्यवर्गीयता की चपेट में है। उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता काफी छीज गई है, सामाजिक सरोकार कुछ धुंधला गए हैं और कथ्य में आत्मगत प्रतिक्रियाओं ने बहुत जगह घेर ली है। अच्छी रचना के लिए जो गहरे आत्मसंघर्ष अनिवार्य होते हैं और जो अनुभूतियों के संसार को रचनात्मक अनुभवों में बदलते हैं, उनका अभाव दीखता है। इस साहित्य में अभी तक न खोजे गए इलाके प्रकट नहीं हुए हैं और दूसरी तरफ, रचना के शिल्प और स्थापत्य को लेकर उदासीनता नजर आती है। सुनने को मिलता है कि नई पीढ़ी को यह बोध कम है कि रचना सिर्फ ‘अभिव्यक्ति’ नहीं बल्कि ‘निर्मिति’ भी होती है। कई लोग इसकी वजह पूर्ववर्ती साहित्य से नई पीढ़ी की संवादहीनता और अलगाव में भी देखते हैं। दरअसल साहित्य में पिछली संरचनाओं को तोड़कर ही नई जमीन पाई जा सकती है और दुनिया भर में साहित्य और कलाओं में नए आंदोलन इन्हीं प्रक्रियाओं से उभर कर आए। मसलन, पश्चिमी कला में जब दादावाद के चित्रकारों ने घोषणा की थी कि ‘हम क्यूबिस्ट कलाकारों के वायलिनों को तोड़ देंगे’ (क्यूबिस्ट कला में वायलिन बहुत चित्रित हुए थे) तो हिंदी में अकवितावादियों का कहना था कि हमसे पहले के कवि उन अनुभवों को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे जिन्हें हमने किया। नई पीढ़ी में यह टकराव कम दीखता है और कुछ सरलीकरण का जोखिम उठाते हुए भी यह डरावनी बात कही जा सकती है कि वह सिर्फ अपने जीवितों को पहचानती और याद रखती है, उसके पास अपने मृतकों की स्मृति लगभग नहीं है। एक अनुमान बताता है कि नए लोग अब निराला, महादेवी, शमशेर, त्रिलोचन, अज्ञेय, विजयदेव नारायण साही, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण आदि को कम पढ़ते हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल शायद कुछ पढ़े जाते हैं और मुक्तिबोध इसलिए कि उनकी लंबी कविता ‘अंधेरे में’ कविता के उत्तर-जीवन का प्रतिमान बन चुकी है। लेकिन आज का कौन कवि ऐसा अभावग्रस्त और संतापित जीवन जीना चाहेगा जैसा इन कवियों ने जिया?
क्या यह भूमंडलीकरण, वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति, बाजारवाद और उसके साथ आने वाली फौरी कामयाबियों की सुख-भ्रांति का असर है? ये तीनों दुर्दम ताकतें लगातार स्मृति पर आक्रमण करती हैं, हमें पिछले उत्पाद, पिछले अनुभव, पिछले मूल्य और पिछले स्वप्न भूल जाने और उन राजमार्गों पर दौड़ने के लिए सहमत करती हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी निर्मित कर रही है। दरअसल हमारा विराट मध्यवर्ग जीवंत अनुभवों के अभाव से ग्रस्त है और अमेरिकी उपभोक्ता संस्कृति की निर्द्वंद्व नकल करना और धन कमाना ही उसके जीवन का मकसद रह गया है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि समाज में एक साथ मूर्ति-पूजा और मुद्रा-पूजा भीषण रफ्तार से बढ़ती रही हैं। मध्यवर्ग की मौजूदगी पहले भी अहम थी, लेकिन तब वह इस कदर नकलची और खुदगर्ज नहीं हुआ था। सन 1960 से 1980 के बीच दो दशकों के दौरान उसके भीतर बड़ी रचनात्मक बेचैनी और बदलाव की जद्दोजहद नजर आती थी। भूमंडलीकरण ने उसे ‘मैं, मेरा, मुझे, मेरे लिए’ जैसे प्रलोभनों के दुश्चक्र में डाल दिया है।
इसके बावजूद कविता के नक्शे पर आदिवासी, दलित और महिलाएं कुछ नए ज्वलंत क्षेत्र हैं क्योंकि तीनों अपने दारुण अनुभवों के रक्त, अपनी ऐतिहासिक स्मृति के अंधेरों और प्रतिरोध के औजारों के साथ अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उनकी रचनाओं में कई ऐसे पहलू दिख रहे हैं जिनसे पूर्ववर्ती कविता वंचित थी और जिनमें वर्गीय चेतना की नई लड़ाइयां झलकती हैं। आदिवासी संवेदना की आधुनिक कविता में पहला नाम निर्मला पुतुल का लिया जाना चाहिए, वे मूलतः संथाली में लिखती रही हैं और उनके हिंदी अनुवाद ही चर्चा में रहे हैं। युवा कवि अनुज लुगुन की एक कविता हाल ही में सामने आई है जो स्कूल जाना शुरू करने वाली एक आदिवासी बच्ची की ड्रेस के बारे में है, ‘हजारों साल की यातनाओं का दर्द उभारता है तुम्हारा स्कूल ड्रेस/ दुर्ग की मजबूत दीवारों में कैद नहीं थी किताबें/ पोथियां कैद नहीं रह सकती किसी कैदखाने में/ वह तो हमारी जाति थी जिसके लिए दुर्ग की मजबूत दीवारें थीं/ बुर्ज पर प्रहरी थे और उनके खतरे की घंटी हमारे खिलाफ बजती थी/ आज जब तुम स्कूल जाती हो/ तो लगता है यातनाओं का दर्द कम हो रहा है/ आसुंओं की नमी अब कुछ पतली हो चली है/ तुम घर की चौखट से ऐसे निकलती हो/ जैसे सूरज का रथ निकल रहा हो अंधेरे के खिलाफ/ तुम न सिर्फ चौका-बर्तन धो जाती हो/ बल्कि उन अंधेरे कमरों को भी बुहार जाती हो/ जो हमारे ही घरों में पुरुषों की सोच में कहीं टंगा होता है।’
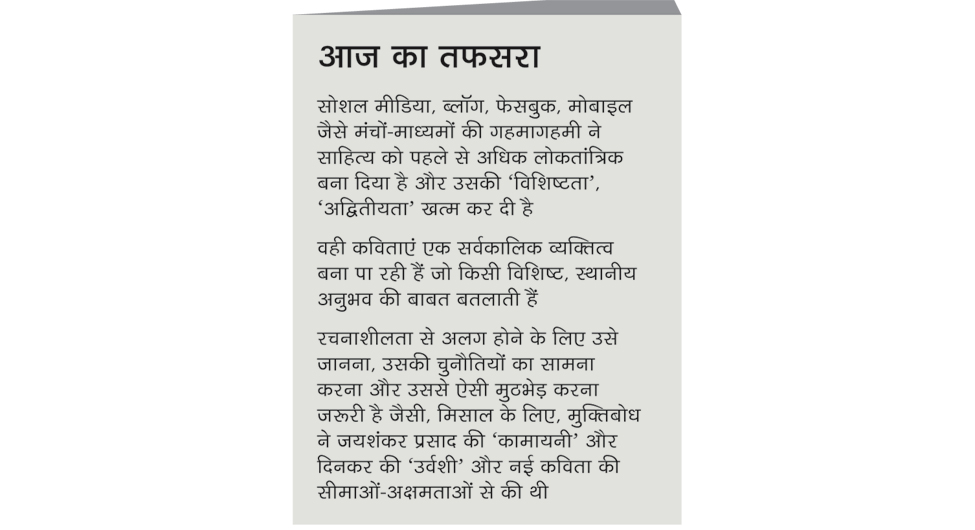
एक और आदिवासी युवा कवि जसिंता केरकेट्टा की कविताएं इन दिनों हिंदी ही नहीं, यूरोप की भी कुछ भाषाओं में चर्चित हैं। ये कविताएं बहुराष्ट्रीय निगमों की परियोजनाओं और विकास के नाम पर उजाड़े जाते आदिवासी इलाकों, कटते हुए जंगलों, खत्म होते हुए पानी और खोदे जाते पहाड़ों और उनके खनिजों की चिंता और सरकारी साहबों के अत्याचार का शिद्दत से प्रतिरोध करती हैं- ‘भूख की आग पर/ पकती हुई गुनगुनाती है/ और उठने लगती है एक साथ/ कई घरों की आग।’ एक और कविता में वे चुनौती देती हैं, ‘साहेब! एक दिन/ जंगल की कोई लड़की/ कर देगी तुम्हारी व्याख्याओं को/ अपने सच से नंगा/ लिख देगी अपनी कविता में/ कैसे तुम्हारे जंगल के रखवालों ने/ ‘तलाशी’ के नाम पर/ खींचे उसके कपड़े/ कैसे दरवाजे तोड़कर/ घुस आती है/ तुम्हारी फौज उनके घरों में/ कैसे बच्चे थामने लगते हैं/ गुल्ली–डंडे की जगह बंदूकें/ और कैसे भर आता है/ उसके कलेजे में बारूद/ साहेब! एक दिन/ जंगल की हर लड़की/ लिखेगी कविता/ क्या कहकर खारिज करोगे उन्हें?/ क्या कहोगे साहेब?/ यही न....कि यह कविता नहीं/ “समाचार” है!’
दलित कविता भी बेबाक और बेलौस ढंग से सवर्ण समाज को चुनौती देती है कि ‘दो-चार दिन के वास्ते अछूत बनके देख।’ नई दलित चेतना को युवा कवि-आलोचक कौशल पंवार में इस तरह देखा जा सकता है, ‘व्यवस्था के ठेकेदारो/ देखो-देखो वे आ रही हैं/ भंगी महिलाएं/ हाथ में झाड़ू की जगह/ कलम उठाए हुए।’ उनकी एक और कविता सवाल करती है, ‘बलात्कार की शिकार/ तुम्हारी बहन की भाषा कैसी होगी/ कैसे होंगे गुलामी की जिंदगी जीने वाले/ तुम्हारे बाप के विचार/ ठाकुर की हवेली में दम तोड़ती/ तुम्हारी मां के शब्द/ क्या वे सुंदर होंगे?’ दलित कविता बार-बार सवर्ण मिथकों की चीरफाड़ करती है, ‘जब तुम राम का नाम लेते हो/ मुझे शंबूक का/ कटा सिर दिखने लगता है/ जब तुम हनुमान का नाम लेते हो/ मुझे गुलामी का दर्द सताने लगता है/ तुम्हें अपने घृणित अतीत पर गर्व है/ मैं तुम्हारे अतीत पर थूकता हूं।’
इस परिदृश्य में महिलाओं की उपस्थिति अलग से दिखाई देती है। खास तौर से कविता में अब उनका घर पहले जैसा, मसलन छायावाद या नई कविता के दौर की तरह, अधबना और वीरान नहीं रह गया है और उसके बाशिंदों की संख्या काफी बड़ी है। कात्यायनी, शुभा, निर्मला गर्ग, अनामिका, सविता सिंह, अनीता वर्मा आदि के बाद उभर कर आई स्त्रियां अपने बाहरी और आतंरिक संसारों को व्यक्त करने के साथ-साथ पुरुषवाद से आजादी की आवाजों में शायद ज्यादा निश्चयात्मक लगती हैं। उनमें से कई कवि फेसबुक या ब्लॉग आदि माध्यमों से उभर कर आई हैं। लीना मल्होत्रा राव, लवली गोस्वामी, रश्मि भारद्वाज, बाबुशा कोहली, सुजाता, विपिन चौधरी, पूनम अरोड़ा (नामों का उल्लेख अधूरा इसलिए फिजूल होगा) आदि सोशल मीडिया में सक्रिय रही हैं। लीना मल्होत्रा एक कविता में भीमबेटका के आदिम गुफा चित्रों को देखते हुए महाभारत में जुआ खेलने के प्रसंग तक जाती हैं और देखते ही देखते राजसभा में द्रौपदी को खींच कर लाने और चीरहरण के दृश्य चित्रित कर देती हैं। युवा महिलाओं की ऐसी कविताएं आश्वस्त करती हैं।
नए लोगों से हमें ऐसी आश्वस्ति और उम्मीदें क्यों रखनी चाहिए? शायद इसलिए कि समाज के संकट और सवाल आज पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गए हैं और सत्ता-राजनीति अपने सबसे निकृष्ट, भ्रष्ट, हिंसक और सांप्रदायिक रूपों में समाज को तोड़ने-बांटने में लगी है। शिक्षा, कला और संस्कृति की संस्थाएं भी हमलों की जद में हैं। यह सही है कि हिंदी साहित्य आम तौर पर प्रतिबद्ध और यथास्थिति विरोधी रहा है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में लेखकों-कवियों से कहीं ज्यादा और कारगर हस्तक्षेप की अपेक्षा की जानी चाहिए। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब राजनीति द्वारा नष्ट किए जा रहे जीवन-मूल्यों को बचाने का दायित्व लेखकों को उठाना पड़ता है। यूरोप, स्पेन और कई लातिन अमेरिकी देशों में कवियों-लेखकों ने अनुकरणीय मिसाल पेश की हैं। कई बड़े लेखक अपने समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं के कठोर आलोचक रहे हैं। ब्रिटिश नाटककार हारोल्ड पिंटर ने तो इराक पर हमले में अमेरिका का साथ देने के लिए तब के प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर को गिरफ्तार करने की मांग की थी और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जर्मन उपन्यासकार ग्युन्टर ग्रास का यह कथन भी प्रसिद्ध है कि ‘किसी देश की नियति को सिर्फ राजनीतिक नेताओं के भरोसे छोड़ना खतरनाक है।’ फासिस्ट जर्मनी की याद दिलाने वाले दौर की तरफ बढ़ते हमारे देश में यह हस्तक्षेप का क्षण है और एक ज्यादा बड़ी, गहरी प्रतिबद्धता ही प्रतिरोध का सच्चा साहित्य पैदा करेगी।
उम्मीद की एक दूसरी वजह यह है कि आज नई पीढ़ी को प्रकाशन की अधिक सुविधाएं हासिल हैं जैसी पहले नहीं थीं। न छप पाना अब कोई समस्या नहीं है। पुरस्कारों की तादाद भी बढ़ गई है। यह सुखद है, लेकिन आशंका भी होती है कि प्रकाशन की आसानियां और पुरस्कारों की बहुतायत रचनाशीलता की धार कुंद तो नहीं कर रही हैं। पुरस्कार तात्कालिक और अस्थायी होते हैं, लेकिन कुछ स्थायी किस्म की संतुष्टियों को जन्म दे सकते हैं। इक्कीसवीं सदी की रचना कामयाबियों के रसातल से सावधान रहते हुए जोखिम उठाकर ही संभव होगी।
(लेखक वरिष्ठ कवि, पत्रकार, अनुवादक और स्तंभकार हैं। पहाड़ पर लालटेन, नए युग में शत्रु, एक बार आयोवा उनकी चर्चित कृतियां हैं)








