आज भारतीय समाज गैर-मामूली संकटों से घिरा है और इससे उबरने के लिए उसे जिस राजनीतिक या सामाजिक नेतृत्व की दरकार है, वह कहीं दिखता नहीं। अवाम के बड़े हिस्से का मनोबल गिरा हुआ है। विपक्ष लगभग गायब होता जा रहा है। उसके लिए लोकतंत्र जीवन-मृत्यु का प्रश्न नहीं, शतरंज की बाजी है। जब नरसंहार के दोषी मानवद्रोही विकास-पुरुष बनकर उभरें, जब संदिग्ध किस्म की समाजसेवी संस्थाओं के ऑपरेटर साधारण जन के उद्धारक की तरह देखे जाने लगें, कुछ सस्ते ठग, राष्ट्रीय महत्व के संत राजनेताओं में बदलकर ‘विकल्प’ की तरह खड़े दिखाई दें, जब पक्ष और विपक्ष का निर्माण, यथास्थिति और उसका विकल्प दोनों ही सत्ताधारियों के ही हाथ में आ जाएं, तो रघुवीर सहाय की कविता ‘आपकी हंसी’ सहज ही आज के समय का केंद्रीय वक्तव्य बन जाती है—
निर्धन जनता का शोषण है
कह कर आप हंसे
लोकतंत्र का अंतिम क्षण है
कह कर आप हंसे
सबके सब हैं भ्रष्टाचारी
कह कर आप हंसे
चारों ओर बड़ी लाचारी
कह कर आप हंसे
कितने आप सुरक्षित होंगे
मैं सोचने लगा
सहसा मुझे अकेला पा कर
फिर से आप हंसे
पैंतालीस साल पहले लिखी गईं ये पंक्तियां भारतीय मध्यवर्ग के भीतर फासिज्म की बढ़ती चाहत को जाहिर करती हैं। आज सांप्रदायिक फासीवाद काफी हद तक लोकप्रिय विचार का रूप ले चुका है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। राज्य और उसके संस्थानों पर उसका औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण बढ़ता गया है। वह सत्ता में रहकर भी प्रतिरोध के स्वर में बोलता है। विपक्ष की जगह भी उसने हथिया ली है। संगठित दुष्प्रचार, सांप्रदायिकता, भीड़तंत्र, राज्य-समर्थित हिंसा, बहुमतवाद यानी हिंदुत्ववाद इसके प्रमुख औजार हैं। आज का ज़ालिम अपने को हरदम उत्पीड़ित दिखाता रहता है और अक्सर फरियादी वेश में हाजिर होता है।
भारत की जनता इतनी अधिकारहीन पहले कभी न थी। खासकर आदिवासी और मुसलमान जन, भूमिहीन लोग, और दलितजन का बहुलांश। गर्वीले, आत्मविश्वास से भरे मजदूर अब दीखते नहीं। कृषि क्षेत्र और किसानों का हाल किसी से छिपा नहीं है। सफेदपोश उद्यमों में भी ट्रेड यूनियनिज्म की मजबूत परंपरा बिखर चुकी है, शिक्षकों की कोई ताकत ही नहीं रह गई है। निजीकरण, कॉन्ट्रैक्ट और दमनकारी कानूनसाजी के माध्यम से नए भारत के विधाता सबको अधिकारहीन करते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ भी सब स्तरों पर दलालों की एक फौज खड़ी करना ही है। मूल रूप से तो हम एक दमनकारी पुलिस राज और सैन्यीकृत राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
यह भ्रम है कि राजनेता और जनप्रतिनिधि के हाथ में ताकत और निर्णय का अधिकार बचा है। दिनोदिन ये हृदयहीन, खूनी निजाम की कठपुतलियों की तरह नजर आते हैं। ये उसी हद तक ताकतवर हैं जिस हद तक लूट में और अधिकारों के हनन में हिस्सेदारी रखते हैं। इन्होंने स्थानीय और सार्वदेशिक पूंजी और वैश्विक स्तर पर अन्यायी शक्तियों के सामने हथियार डाल दिए हैं। वे जनमत से नहीं, दलाली से शक्ति अर्जित करते हैं। इन्हीं शक्तियों से ही चुनाव लड़ते हैं और इन्हीं को पार्टियां टिकट देती हैं।
दरअसल बरसों से भारत का सरमायेदार तबका, अपने फरमाबरदार बुद्धिजीवियों और सैद्धांतिकों की मदद से लोकतंत्र की परिभाषा बदलने में लगा है। वह लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रति लोगों में कड़वाहट, हताशा और विश्वासहीनता पैदा करने और उसे दोगुना-चौगुना करने में दिलचस्पी रखता है। पहले पूंजी उन संस्थानों पर अपना कब्जा मजबूत करती है जो लोकतांत्रिक परिवर्तन के कारण अस्तित्व में आए, जिनसे लोकतंत्र की दिनचर्या बनती है : संसद, संविधान और कानून, मीडिया, न्यायपालिका, नौकरशाही, चुनाव और मताधिकार, न्यायिक बराबरी, नागरिक अधिकार आदि। दूसरी तरफ आम जनता भी अपनी आजादी और अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहती है जिन्हें कुरबानी देकर हासिल किया गया था। सरमायेदार तबके प्रबुद्ध वर्गों की मदद से इन्हीं संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने में लग जाते हैं। वह न केवल व्यवस्था के प्रति वितृष्णा और राजनीति मात्र से नफरत का भाव पैदा करते रहते हैं, बल्कि जोशो-खरोश से कल्याणकारी नीतियों को समाप्त करने की अपील करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण के नए-नए औचित्य ढूंढ़ते रहते हैं। लोकतंत्र की सार वस्तु नष्ट कर दी जाती है, बस खोखला ढांचा बचा रह जाता है जिस पर पूंजी के कारकुन तैनात रहते हैं। अंत में सिर्फ एक चीज रह जाती है, वोट, जिसे आप चाहें इस मोदी को दें या उस मोदी को।
आज हिंदुस्तान में जो भी ताकतवर हैं, उद्योगपति, धनपति, कारपोरेट प्रबंधक, दलाल राजनेता और नौकरशाह लगभग सब राजनीतिक तंत्र और समाज-व्यवस्था का फासीवादी पुनर्गठन करना चाहते हैं। पच्चीसेक साल पहले तक, यह असंभव लगता था, पर अब यह सामान्य सच्चाई है। सरमायेदार, दलाल और क्राइम सेक्टर का कब्जा हर जगह बढ़ गया है। यह सिलसिला वैसे तो इमरजेंसी के समय से ही शुरू हो गया था, पर बाद में आई सरकारों और अंतरराष्ट्रीय पूंजी के चहेते नेताओं के शासनकाल में परिपक्व होते हुए और रफ्तार पकड़ते हुए अब एक ‘क्रिटिकल मास’ अर्जित कर चुका है। भारतीय लोकतंत्र के नृशंस पुनर्गठन में अब पुराने और नए मीडिया घराने और नई पूंजी साथ दे रही है। अखबार, टेलीविजन और सिनेमा के माध्यम से लोकतांत्रिक तहजीब के विरुद्ध आक्रामक अभियान काफी समय से जारी है। हर स्टूडियो में घोर अलोकतांत्रिक टीवी एंकर बैठे हैं और उसके पीछे मीडिया मालिकों का हाथ है।
अवाम लोकतंत्र को अपने हक में, एक स्वाधीन, दासताहीन, सुरक्षित समाज और कल्याणकारी भविष्य के निर्माण के औजार में न बदल सके, इसके लिए सरमायेदार तबका विभाजनकारी हथकंडे अपनाता है। वह सांप्रदायिकीकरण, गुंडाराज, दुष्प्रचार, राजकीय आतंक, भ्रष्टाचार, अंधराष्ट्रवाद, सैन्यीकरण, युद्ध, तानाशाही, फासिज्म इन सब चीजों का रास्ता खोल देता है। मोटे तौर पर पूंजीवाद का यही इतिहास रहा है। इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आजाद हिंदुस्तान की जनता ने इन वर्षों में न देखा हो और आज मुल्क के किसी न किसी हिस्से में हरदम न झेल रही हो। लगातार होने वाले नरसंहार, हर तरह का दमन, उत्पीड़न, शोषण, भूख, बीमारी और कुपोषण, बेरोजगारी, विस्थापन, विषमता, अन्याय से ‘संसार के विशालतम लोकतंत्र’ का जिस्म दागदार है।
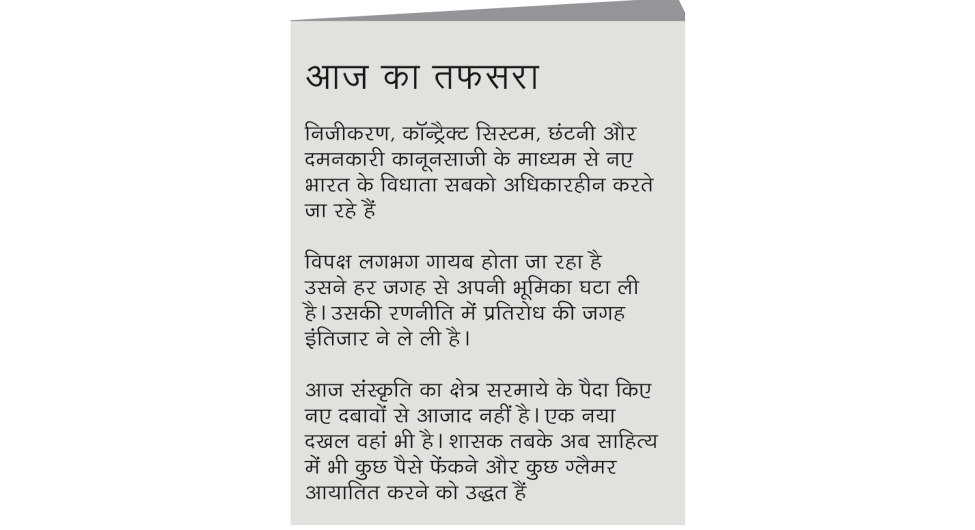
पूंजी के अपने वृहत्तर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब राज्य और उसकी संस्थाएं काफी नहीं हैं; उसे अनिवार्यतः अपराधियों की और अपराधतंत्र की मदद चाहिए। यह काम जरायमपेशा छुटभैयों की सामर्थ्य और महत्वाकांक्षा से परे है। उसे बड़े आपराधिक तंत्र को खड़ा करने, विकसित करने, हर तरफ फैला देने की दरकार है। पुलिस और सरकारी मशीनरी अपनी हद के भीतर ही काम कर सकती है, भले ही वह हदें तोड़ती रहती है पर वहां भी हद है। आपराधिक तंत्र का काम उस हद के बाद शुरू होता है। सबसे पहले इसका लक्ष्य होता है नागरिकों के प्रतिरोध को तोड़ना, और ऐसी दशा ले आना कि ज्यादातर लोग नियति की तरह इसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लें।
आज जबकि समाचार और प्रचारतंत्र और ‘सार्वजनिक बुद्धि’ पूरी तरह से आवारा पूंजी के हाथ में हैं और राष्ट्रीय जीवन में अराजनैतिकीकरण का मुख्य औजार हैं, हर स्वाधीनचेता नागरिक, बुद्धिजीवी और लेखक-कलाकार की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह लोकतंत्र में राजनीति की केंद्रीयता और राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहे। वह हर सार्वजनिक मंच पर निडरता के साथ हस्तक्षेप करे। आम जनता के संपर्क में आने, उनसे धैर्य से बात करने से न कतराए। मास मीडिया नामक पूंजी के कारखानों में खबरें जिस तरह बनती हैं, चर्चा और विचार के विषय जैसे तय किए जाते हैं, जिस तरह की मैनपॉवर संपादकों, संवाददाताओं, कॉलम लेखकों, एंकरों, संयोजकों के रूप में भर्ती और तैनात की जाती है, फिर जिन तरकीबों से वे पेशेवर बुद्धिजीवी वर्ग की मदद से ‘नए भारत’ की तस्वीर बनाते हैं और ‘नया ज्ञान’ हम तक पहुंचाते हैं, इस पर गौर करने और लोगों को समझाने की जरूरत है। यह बताने की जरूरत है कि आप निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं, सक्रिय नागरिक हैं। जो जनता अपनी ताकत में विश्वास खो चुकी हो और जो यह मानने को तैयार हो कि अब सुप्रीम कोर्ट, भगवान, कोई चमत्कारी पुरुष, फौजी शासन या फासीवाद ही देश को बचा सकता है, उसी जनता से बुद्धिजीवी या कलाकार को जिरह करनी है।
जिस तरह की राजनीतिक शक्तियां सत्ता पर काबिज हैं वे ऐतिहासिक संरचना, सामाजिक बुनावट और सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने को कटिबद्ध हैं, कला केंद्रों के स्वरूप को बिगाड़ने से भी बाज नहीं आएंगी। शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो फेरबदल हो रहे हैं और संस्थाओं के साथ जो असाधारण छेड़छाड़ की जा रही है, वह साबित करता है कि लोकतंत्र बल्कि मानव-विरोधी शक्तियों का साया हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर पड़ रहा है।
यह सही है कि लेखक, कलाकार अपने कलाकर्म के बूते राजनीतिक शून्य और सामाजिक शून्य को नहीं भर सकते लेकिन किसी भी संस्कृतिकर्मी और लेखक को हर हाल में अपना काम करने और नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। महान कलाकार मकबूल फ़िदा हुसेन का निर्वासन और परदेस में उनकी मौत इसका ज्वलंत उदाहरण है। उनकी लाश को उनका परिवार इसलिए भारत लाकर दफना नहीं सका क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अपने देश में उन्हें कब्र में भी चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। दाभोलकर, पनसारे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश की हत्या की घटनाएं इतनी पुरानी नहीं कि भुलाई जा सकें। लेखक-कलाकारों द्वारा पुरस्कार वापसी का कदम बढ़ते फासीवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम था जिसका व्यापक असर भी हुआ। लेकिन दैनिक स्तर पर संस्कृतिकर्म की चुनौती वही है जो बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में विश्व भर में साहित्यकारों और कलाकारों ने, भारतीय साहित्य-कला के अग्रणी रचयिताओं ने आगे बढ़कर स्वीकार की थीं। यानी अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार और अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक सरोकारों से गहरा लगाव।
आज संस्कृति का क्षेत्र सरमाये के पैदा किए नए दबावों से आजाद नहीं है। शासक तबके अब साहित्य में भी कुछ पैसे फेंकने और कुछ ग्लैमर आयातित करने को उद्धत हैं। जगह-जगह जो ‘लिटफेस्ट’ होते रहते हैं, वहां लोग मासूम भूखे पशुओं औरे कीट-पतंगों की तरह, इकट्ठे हो जाते हैं। इन आयोजनों को उसी तरह की आवारा पूंजी का सहयोग और समर्थन प्राप्त है जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। प्रलोभनकारी हस्तक्षेप की पुरानी विधियों तो अपनी जगह हैं ही। पर उम्मीद का एक इलाका है जहां कलाकार की स्वायत्तता और प्रतिबद्धता उसके हाथ में होती है, वैयक्तिक नैतिकता का इलाका। साहित्य और अनेक कलाओं में रचना का काम निजी मूलतः और प्रथमतः निजी स्तर पर होता है, इसलिए कलाकर्म में प्रतिक्रियावादी पूंजी का दखल लेखक या कलाकार की दहलीज से आगे, बिना उसकी अनुमति के कभी नहीं हो सकता।
(लेखक वरिष्ठ कवि और टिप्पणीकार हैं। संस्कृति सम्मान से सम्मानित। बहनें और अन्य कविताएं, कविता का जीवन, सामान की तलाश उनकी चर्चित कृतियां हैं)








