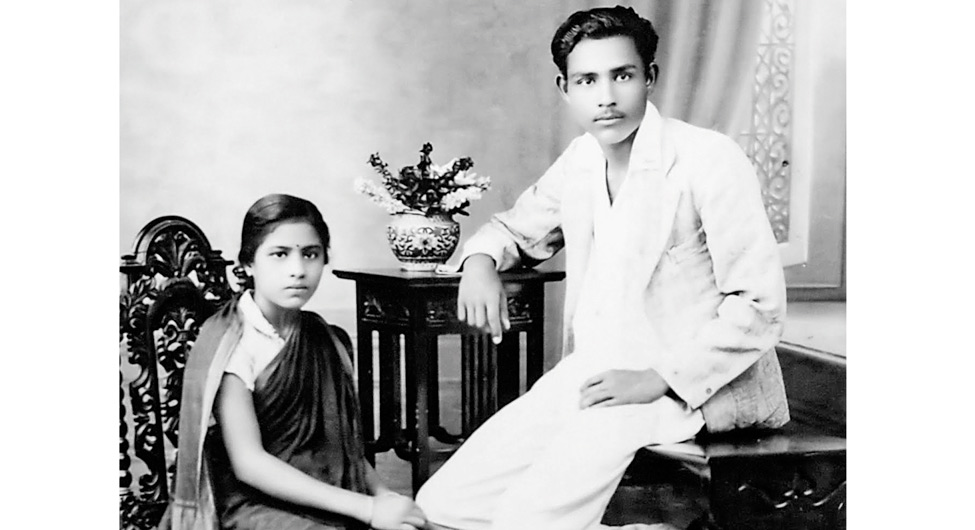लेखक और कवि वक्त के साथ पुराने पड़ जाते हैं। उनकी रचनाएं समय-बद्ध हो जाती हैं, भविष्य में जाने की बजाय पीछे जाने लगती हैं और एक काल-खंड की साहित्यिक विशेषताएं बन कर रह जाती हैं। लेकिन गजानन माधव मुक्तिबोध उन थोड़े से कृती लेखकों में हैं जिनकी रचनाएं अपने समय से होकर आने वाले समय में स्थानांतरण करती गई हैं और उनकी अनेक कविताएं, कहानियां, आलोचनात्मक लेखन और डायरी सिर्फ धरोहर न बनकर आज भी परमाणु समूहों की तरह सक्रिय और जीवंत हैं। 1964 में मुक्तिबोध के असामयिक निधन के बाद प्रकाशित हुए उनके पहले कविता संग्रह की मार्मिक भूमिका में शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा था, "एकाएक क्यों ’64 के मध्य में गजानन माधव मुक्तिबोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो उठे? धर्मयुग, ज्ञानोदय, लहर, नवभारत टाइम्स साप्ताहिक, मासिक और दैनिक उनका परिचय देने लगे और दिल्ली की साहित्यिक हिंदी दुनिया में एक हलचल-सी आ गई? इसलिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध एकाएक हिंदी संसार की घटना बन गए। कुछ ऐसी घटना, जिसकी ओर से आंखें मूंद लेना असंभव था। उसकी एकनिष्ठ तपस्या और संघर्ष, उसकी अटूट सच्चाई, उनका पूरा जीवन, सभी एक साथ हमारी भावना के केंद्रीय मंच पर सामने आ गए।"
मुतिबोध की महान कविता 'अंधेरे में' के बारे में शमशेर ने लिखा था कि यह "देश के आधुनिक जन इतिहास का, स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से जन का एकीकरण है।" यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि मानवीय तकलीफों के सबसे बड़े कवि माने जाने वाले मुक्तिबोध के संग्रह की भूमिका प्रेम और सौंदर्य के सबसे बड़े कवि शमशेर ने लिखी। शायद इसलिए कि दोनों की संवेदना में एक गहरा अंतर्संबंध है। शायद शमशेर प्रेम की जिस पृथ्वी पर खड़े हैं, वह मुक्तिबोध सरीखी पीड़ाओं से ही निर्मित होती है।
पिछले पांच दशकों की कविता का स्वभाव जानने के लिए अगर हम किसी केंद्रीय रूपक या प्रतिनिधि पाठ की खोज करें तो वह मुक्तिबोध की कविताओं में ही मिलेगा। हमारे लोकतंत्र का अंधेरा अगर कहीं सबसे ठोस और डरावना दीखता है तो वह मुक्तिबोध की कविता में है। इस अंधेरे के और भी घनीभूत होते जाने के साथ और शायद इसी वजह से उनकी कविता की सार्थकता और प्रासंगिकता लगातार बढ़ती गई और अब जबकि मुक्तिबोध की जन्मशताब्दी का समय है और तीन साल पहले ‘अंधेरे में’ भी अपने प्रकाशन के पचास वर्ष पूरे कर चुकी है, यह देखना अप्रासंगिक नहीं होगा कि किस तरह उनकी कविता और दूसरी रचनाएं साहित्य के केंद्र में आती गईं।
मुक्तिबोध के प्रासंगिक बनते जाने की वजहें उनके यंत्रणा-बोध से भरे जीवन, अस्वस्थता और असमय निधन में नहीं हैं, बल्कि उन तत्कालीन सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनैतिक प्रक्रियाओं में हैं जो उथल-पुथल से भरी थीं और आनेवाले वक्त की शक्ल तामीर कर रही थीं। नेहरू-युग से स्वप्नभंग के उन दशकों में गैर-कांग्रेसवाद, नक्सलवाद, वियतनाम युद्ध विरोधी माहौल, अमेरिकी बीट और ब्लैक कविता, भारतीय भाषाओं में वाम राजनीति से प्रेरित कविता और मराठी में दलित पैंथर जैसे आंदोलन एक नया प्रस्थापना-परिवर्तन कर रहे थे। इस सबके बीच मुक्तिबोध की कविता समाज और मनुष्यों की यातनाओं-संघर्षों-स्वप्नों और नियति के दस्तावेज की तरह सामने आई।
‘अंधेरे में’ की पटकथा (जो बहुत फंतासीमूलक और सिनेमाई है) तो स्वाधीनता की लड़ाई, उसके अधूरे रह जाने की हताशा, उसके संकटों, फासिस्ट शक्तियों के जुलूस, मार्शल लॉ, चौराहे पर बंदूकों-टैंकों और गोलीबारी की घटनाओं और स्वाधीनता की संघर्ष-यात्रा से ही बुनी गई है। एक अंश में गांधी काव्य-नायक के हाथ में एक शिशु को थमाकर उसे संभालने-सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं जो कि हमारी आजादी का ही एक रूपक है, और जैसा कि हमारी आज़ादी के साथ हुआ, जल्दी ही यह शिशु अदृश्य हो जाता है और कंधों पर फूलों के लंबे गुच्छों की बजाय एक बंदूक आ जाती है। फिर आतताई सत्ता द्वारा हत्याओं, गिरफ्तारियों और यंत्रणा दिए जाने के बिंब हैं, जिनमें कहीं अंग्रेज साम्राज्यवादियों से जन साधारण के संघर्ष और कम्युनिस्ट पार्टी के भूमिगत आंदोलन की झलक भी मिलती है। यह पटकथा एकरैखिक नहीं, बल्कि बहुत संश्लिष्ट है और उसके भीतर से काव्य-नायक की ग्लानि बार-बार झांक उठती है: ‘मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम...’ यही ग्लानि उस दौर के संवेदनशील और यथास्थिति विरोधी लोगों, लेखकों, कवियों में भी थी और नक्सलवाद से सहानुभूति रखने वाले बहुत से नए कवियों को इन पंक्तियों में अपने समय के बिंब नजर आते थे:
‘गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूं,/ इतने में चुपचाप कोई एक/ दे जाता पर्चा,/ कोई गुप्त शक्ति/ हृदय में करने-सी लगती है चर्चा!!/ मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं /उसको!/ आश्चर्य!/ उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व/ दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव/ पीड़ाएं जगमगा रही हैं।’
मुक्तिबोध की कविता ने एक ऐतिहासिक काम यह किया कि एक पूरी पीढ़ी को अकविता की विकृत दैहिक भूलभुलैया में भटकने से रोक दिया, जिसका बाजार उन दिनों काफी सजा हुआ था और कई वरिष्ठ कवि भी भाषा में यौन कुंठा और अराजकता के परनाले बहा रहे थे। मुक्तिबोध की मार्फत जैसे इस रुग्ण क्रोध को एक सामाजिक दिशा और राजनैतिक धार मिली। इस कविता ने अगली पीढ़ी के संवेदन तंत्र में भी कुछ बदलाव किया और उसे एक ऐसा रूप दिया जो मुक्तिबोध को ही उद्धृत करें तो, ‘स्थानांतरगामी’ था। यह व्यक्ति से समाज की ओर जाने की शिक्षा देने वाली कविता थी। प्रगतिशील कविता की परंपरा और रघुवीर सहाय और कुंवर नारायण जैसे कवियों को छोड़ दें तो ज्यादातर नई कविता मानसिक प्रत्याघातों का चित्रण अधिक थी और मुक्तिबोध ने उसकी आलोचना में कहा था कि वह "भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से आगे नहीं जाती।"
मुक्तिबोध की कविता के ‘आत्म-धिक्कार’ या ‘आत्म-ग्लानि’ की काफी चर्चा हुई है और उसे अपनी और पूरे मध्यवर्ग की बुजदिली और अकर्मण्यता पर तरस खाने की कार्रवाई मानते हुए कहा जाता है कि मुक्तिबोध अपने ही वर्ग की तीखी आलोचना कर रहे हैं। यह सही है, लेकिन ग्लानि का यह बोध कहीं अधिक गहरा और राजनैतिक है-इटली के प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक अंतोनिओ ग्राम्शी के एक प्रसिद्ध कथन की तरह कि "ग्लानि-बोध एक क्रांतिकारी भावना है।" ग्राम्शी का आशय यह था कि ग्लानि का एहसास ही हमें किसी वास्तविक परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है।
मुक्तिबोध की ग्लानि इसलिए क्रांतिकारी है कि वह काव्य-नायक की चेतना को झकझोर कर, उसकी जड़ता को तोड़कर उसे एक संघर्ष-यात्रा के लिए प्रवृत्त करती है। ‘मर गया देश/जीवित रह गये तुम’ क्या एक स्तर पर निराला की ‘सरोज स्मृति’ की ग्लानि ‘धन्ये, मैं पिता निरर्थक था/तेरे हित कुछ कर न सका’ से नहीं जुड़ती? ‘धन्ये’ की जगह अगर हम ‘देश’ को रख दें तो निराला की स्वीकारोक्ति में मुक्तिबोध की चेतावनी सुनाई दे जाएगी और यही एहसास रघुवीर सहाय की एक कविता में सवाल उठाता दिखता है: ‘लेखक क्या हत्याओं के साझीदार हुए!’
मुक्तिबोध की कविताओं ने हमारी पीढ़ी को क्या सिखाया? उनकी संरचना और शिल्प की नकल शायद किसी ने नहीं की और यह संभव भी नहीं था—यहां तक कि अपने को मुक्तिबोध से सर्वाधिक प्रभावित माननेवाले कवि—विनोद कुमार शुक्ल, चंद्रकांत देवताले और विष्णु खरे आदि—भी मुक्तिबोध की संवेदना और शैली के चिह्नों पर नहीं चले। पिछले दिनों विष्णु खरे ने मुक्तिबोध को ‘सृजन-पिता’ और असद जैदी ने खुद को ‘मुक्तिबोध की काव्य-संतान’ कहा है। दरअसल, हर नया समय एक बदली हुई संवेदना की मांग करता है या उसे जन्म देता है और पूर्ववर्ती पीढ़ियां भी अपनी संवेदना से अधिक अपना जीवन-विवेक ही अगली पीढ़ी को सौंपती हैं।
लेकिन मुक्तिबोध की काव्य संवेदना के कई पहलू नई पीढ़ी तक पहुंचे और उनकी विकलता, बेचैनी, विडंबना-बोध, ग्लानि, स्थानांतरण की काव्य-प्रवृत्ति और ‘जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि’ के निषेध को बाद की बहुत सारी कविता में देखा जा सकता है। इसी के साथ उनका काव्य-विवेक—जिसमें उनकी गहरी वैचारिक प्रतिबद्धता, मार्क्सवाद में विश्वास, प्रगतिशील कविता और आलोचना की खामियों का एहसास और ‘पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?’ भी शामिल हैं—आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता रहा। इस लिहाज से बीते चार दशकों की पड़ताल करें तो यह दिखेगा कि हिंदी की श्रेष्ठ कविता पर मुक्तिबोधीय विवेक की छाया सबसे अधिक है, और उसके बाद शायद रघुवीर सहाय की। यह अकारण नहीं है कि लघु विमर्शों के खंडित दौर के बावजूद ‘अंधेरे में’ जैसी कविता का महावृत्तांत काल से होड़ ले चुका है और महाकाव्यों से रहित हमारे समय का महाकाव्य बन चुका है। ‘अंधेरे में’ का वह विकराल जुलूस, जिसमें सत्ताधारियों, व्यापारियों और डोमाजी उस्ताद से लेकर लेखक-कवि-कलाकार-बुद्धजीवी तक ‘मृत्यु-दल की शोभा-यात्रा’ की तरह चल रहे हैं, भारतीय ही नहीं, बल्कि विश्व कविता में भी ताकत और अत्याचारी व्यवस्थाओं और उनके हाथ अपनी आत्मा बेच चुके लोगों को दर्ज करने, उनका प्रतिरोध करने और उनसे हमें आगाह करने वाले महान दृश्य के रूप में अमिट है और अंश ही अपने में एक संपूर्ण कविता है।
मुक्तिबोध की जन्मशती मनाने का अर्थ यही हो सकता है कि हम हिंदी में बुरी तरह प्रचलित प्रतिमा-पूजन और कर्मकांडी आडंबर से अलग हटकर उनकी कविता और गद्य के बीहड़ और तकलीफदेह वन-प्रांतर में जाएं और यह देखें कि उसके कथ्य हमारी समकालीनता में कहां-कहां घटित हो रहे हैं।
हम उस डरावने जुलूस को फिर से देखें जिसमें डोमाजी उस्ताद से लेकर शहर के तमाम बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, कविगण शामिल हैं और जिसमें एक संतापित कवि अपनी आत्मा बेच चुके ‘लोगों को नंगा देखने के कारण’ मिलनेवाली सजा की आशंका से बुरी तरह घिरा हुआ है, और जिसका ग्लानि-बोध इतना त्रासद है कि वह गोली चलने और कर्फ्यू लगने की घटना के लिए भी अपनी ही किसी भूल को जिम्मेदार मानता है।
इसमें दो राय नहीं कि यह इसकी जांच करने का समय भी है कि क्या हमारे भीतर मुक्तिबोधीय ग्लानि का कोई अंश बचा हुआ है, क्या हम खुद को धिक्कार पा रहे हैं और शोषित-वंचित और हाशिए पर धकेले गए लोगों, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर तरह-तरह के जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्या उनमें हमारी भूमिका की भी कोई चूक दिखाई देती है? क्या समाज में हमारे ही कारण कोई ‘दुर्घट’ घटित हुआ है और क्या हमारे ‘ज्ञानात्मक संवेदन’ में यातना का वह बोध कहीं बचा है, जिसके साथ ‘अंधेरे में’ के काव्य-नायक और मुक्तिबोध की समूची कविता ने पिछले पांच दशक बिताये हैं?
(लेखक वरिष्ठ कवि, समीक्षक और पत्रकार हैं)