‘ओह! लेकिन तुम तो मुसलमान की तरह नहीं दिखती हो।’
वाकई मैं हैरान हूं कि आखिर कोई कैसे अपने धर्म जैसा दिख सकता है। कैसे किसी के लिए पगड़ी या टोपी, दाढ़ी या बुर्का जैसे बाहरी प्रतीक उसके धर्म को तात्कालिक पहचान देने वाले हो सकते हैं? फिर भी दिल्ली में पली-बढ़ी होने के नाते मैं यहां स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, नौकरियों के लिए बातचीत से लेकर दफ्तरों तक में, सामाजिक मेलजोल और आयोजनों की तो बात ही छोड़िए, ऐसी बातें लोगों को कहते सुनती रहती हूं। कुछ हैरानी जताते हैं तो कुछ हामी भरते हुए दिखते हैं। वक्त गुजरने के साथ मुझे यह समझ में आने लगा है कि सामने वाला मुझ पर तंज कस रहा होता है। मैं मुस्लिम की तरह नहीं दिखती तो ‘ठीक’ ही है न कि मैं आम धारणा के अनुरूप ‘उन’-बम फेंकने वाले, बीफ स्मगलिंग करने वाले, जेहाद की बात करने वाले मुसलमानों जैसी नहीं दिखती हूं।
सो, मैं आम धारणा के अनुरूप मुस्लिम की तरह नहीं दिखती हूं। न तो मैं दाढ़ी रखती हूं, न ही आंखों में सुरमा लगाती हूं और न ही टोपी पहनती हूं। मुझे इसके लिए शायद माफ कर दिया जाए क्योंकि मैं मर्द नहीं हूं। लेकिन मैं उन जैसी भी नहीं हूं जैसी धारणा आम मुस्लिम महिलाओं के बारे में है। मैं दिल्ली में पली-बढ़ी लड़की की तरह हूं। खासकर के दक्षिणी दिल्ली की लड़कियों की तरह नकचढ़ी। मैं अपने सामाजिक दायरे और हमउम्र महिलाओं से न तो अच्छा और न ही खराब ड्रेस पहनती हूं। मैं छोटे बाल रखती हूं, सिर हिजाब से नहीं ढंकती। थोड़े में कहूं तो मैं दिल्ली की किसी आम महिला की तरह ही हूं।
फिर भी मेरे होने का एक अलग दायरा है। इसे आप चमड़ी का अलग रंग भी कह सकते हैं और यह है मेरा मुस्लिम होना। मेरी चमड़ी का यह रंग फौरन पहचान लिया जाता है, जब मैं खालिस उर्दू बोलती हूं या मुस्लिम युवकों को ट्रेन या बस से खींचकर पीटने या मार दिए जाने पर नाराज हो उठती हूं या रोहिंग्या संकट के प्रति बेरुखी देख बेचैन हो जाती हूं या शाकाहार को अहिंसा और मांसाहार को हिंसा का पर्याय सुनकर हैरान रह जाती हूं। इसे लेकर मेरे मन में कोई द्वंद्व नहीं है। मैं एक मुस्लिम हूं और बिना किसी विशेष पदवी के एक भारतीय हूं। मैं दोनों हूं। यही नहीं, मैं इसमें शर्मिंदा या रक्षात्मक होने की कोई वजह भी नहीं देखती हूं कि कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम युवा आइएसआइएस (संयोग से उनकी संख्या गिनती की है) से जुड़ने का फैसला कर लेते हैं या कोई पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर खुशी मनाता है (ऐसा आजकल कम हो गया है पर मेरे बचपन में पाकिस्तान मैच हारता कम था और जीतता ज्यादा था)। फिर, मेरा दूसरा नाम तो यकीनन मेरे ‘मोहम्मडन’ होने का सुराग दे देता है।
अपनी पहचान छुपाने की जगह मैं भारतीय और मुस्लिम होने का जश्न मनाना चाहती हूं। ऐसा मैं केवल एक रास्ते से करना चाहती हूं, जिसे मैं जानती हूं। यह रास्ता है मेरा लेखन। इतना ही नहीं, मैं यह साफ तौर पर और अपनी पूरी ताकत से कहना चाहती हूं कि मैं अल्पसंख्यकों के बीच अल्पसंख्यक नहीं हूं। मैं उस नए मध्यवर्गीय मुस्लिम समाज की आवाज हूं जो 1947 के बंटवारे के बाद काफी कम हो गया था पर सात दशक के बाद इसकी संख्या अच्छी हो गई है। इस बड़े समुदाय को दुनिया खासकर भारत को स्वीकार करना होगा और यह सीखना होगा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इसके अलावा सभी भारतीय मुसलमानों को एक समान रवैए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्हें क्षेत्रीय और जातीय रूप में देखा जाता है पर उनके सामाजिक ढांचे, आर्थिक स्थिति और शिक्षा को नहीं देखा जाता। विविध संस्कृतियों वाले जनसमूह में बहुत सारे लोग मुसलमान हैं। उनमें धार्मिक आस्था रखने वाले भी हैं। मगर ये इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का सपना देखने वाले कट्टरपंथियों से काफी दूर हैं। मेरी सोची-समझी राय में 17.2 करोड़ की मुस्लिम आबादी का बहुमत आतंकियों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखता है। भारत को दार-उल-हरब (काफिरों का देश) से दार-उल-इस्लाम (इस्लाम का देश) में बदलने की बात मुसलमानों से अधिक दक्षिणपंथी हिंदू कट्टरपंथियों के दिमाग की उपज है।
फिल्म या दूसरे माध्यमों में मुसलमानों को जिस रूप में दिखाया गया उससे उनके अंदर अलगाव और आहत भावना ही बढ़ी। वैश्वीकरण के पूर्व भारत में फिल्म उद्योग में मुसलमानों को स्मगलर या पान खानेवाला, सुरमा लगाए पठान सूट पहने लफंगे या कव्वाली गाने वाले ऐसे ऐय्याश की तरह दिखाया गया, जिसने अपनी पत्नी को बेहद छोटी-सी बात पर तलाक दे दिया हो। उदारीकरण के बाद इन चरित्रों की जगह पश्चिम एशिया में बैठे डॉन ने ले ली जो वहीं से भारतीय शहरों को दहलाने की साजिश रच रहा होता है। इसके अलावा हाल के दिनों में उन्हें तकनीक की समझ रखने वाले, पर मजहबी मुस्लिम के रूप में दिखाया जा रहा है जो कट्टर होने के साथ खून का प्यासा भी हो गया है।
धीरे-धीरे ही सही पर निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें सामाजिक स्तर पर फैलने लगीं जिससे लोगों के बीच घृणा बढ़ी। मुस्लिम युवकों पर हिंदू लड़कियों को रणनीति के तहत प्यार के जाल में फंसाने का आरोप लगा और उसे ‘लव जेहाद’ के रूप में प्रचारित किया गया। हिंदुओं की भावना भड़काने के लिए गाय को मारने और उसका मांस खाने की बात कही गई। हर जुम्मे को मुसलमान बड़ी संख्या में जुटकर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर देते हैं और खुतबे में तमाम दकियानूसी बातें सुनते हैं, जैसे बच्चों को पोलियो ड्रॉप न पिलाना, बैंक में पैसा जमा न करना क्योंकि उससे मिलने वाला ब्याज हराम है। इसी तरह ‘वंदे मातरम्’ गाने से इनकार करने को सीधे-सीधे राष्ट्र-विरोधी बता दिया गया।
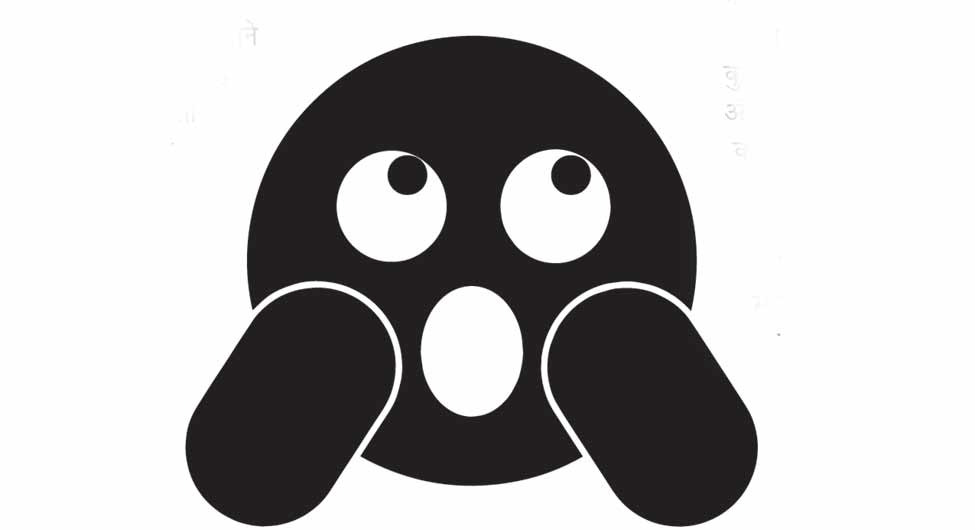
इस तरह के दुष्प्रचार का असर पूरे मुस्लिम समुदाय की छवि और उसकी अवधारणा पर पड़ा। जिस तरह की बातें कही गईं उससे संस्कृति और जीवन पद्धति पर भी असर पड़ा। उर्दू का इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है पर इसे सारे मुसलमानों से जोड़ दिया गया। ऐसा करने में इस बात तक को नकार दिया गया कि केरल का मुसलमान मलयालम बोलता है, असम में रहने वाला असमिया और दूसरे राज्य में रहने वाला वहां की बोली। लोकप्रिय संस्कृति में उर्दू कवियों और नवाबों को पुरानी यादों और करुणा में डूबे रहने वाले चरित्र या ‘मुस्लिम सामाजिक प्रतीक’ के रूप में शेरवानी पहने हीरो या घाघरा पहनी हीरोइन के रूप में दिखाया गया है। जब किसी तरह की रोक या बंधन नहीं होता तो कुछ चित्रण काफी आक्रामक होते हैं।
इनमें मुस्लिमों को आक्रमणकारी के रूप में दिखाया गया और कहा गया कि इन लोगों ने लूटपाट की और मंदिर ढहाए। इतना ही नहीं मध्यकालीन सुल्तानों को राजपूत रानियों के प्रति कामुक और वहशी के रूप में दिखाया गया। क्या यह एक गलत धारणा के लिए वास्तविकता का त्याग कर भड़काने वाले हमले की तरह नहीं है? क्या यह जानबूझकर की गई कार्रवाई, हिंसा का प्रकार नहीं है, एक हिंसा जो दिमाग और आत्मा के प्रति हो? और सांप्रदायिक हिंसा में हाल में हुई वृद्धि और बढ़ते हुए नफरत-अपराध (हेट क्राइम) का क्या होगा? गोमांस विरोधी हिस्टीरिया से जिस तरह से अतिसक्रियता बढ़ी और नियंत्रण से बाहर हो गई उसका क्या होगा?
ऐसे में, मुस्लिम खुद पर हो रही उस तरह की हिंसा का जवाब कैसे देते हैं जो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उनके खिलाफ हो रही है? वे केंद्रीय मंत्री के इस सवाल का क्या जवाब दे सकते हैं कि बूचड़खानों (मुस्लिमों द्वारा संचालित और कथित रूप से अवैध) से मिल रही आमदनी आतंकी गतिविधियां संचालित करने के लिए दी जा रही है? या जब एक निर्वाचित एमएलए का यह कहना हो कि ताज महल ‘राष्ट्र के नाम पर कलंक’ है क्योंकि इसे गद्दारों ने बनाया है? और यह चलता रहता है। भारतीय मुसलमान डरा हुआ और चुप है। खुद के चारों ओर व्याप्त हिंसा की ताकत से भयाक्रांत है। वह अपने हिंदू भाइयों से बात करने का इंतजार कर रहा है। वे कभी-कभी विरोध मार्च तो करते हैं पर यहां भी वे सहमे रहते हैं और उनके हाथ में ‘मेरे नाम पर नहीं (नॉट इन माइ नेम)’ और ‘चुप्पी तोड़ो (ब्रेक द साइलेंस)’ लिखा प्लेकार्ड होता है।
अल्लामा इकबाल ने भी खुदा को ‘शिकवा’ शीर्षक से लिखी अपनी लंबी कविता में लिखा है ‘बर्क (बिजली) गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर’। और वास्तव में ऐसा है भी। 1857 में हुई आजादी की पहली लड़ाई के क्रूर परिणाम के डेढ़ शताब्दी बीत जाने के बाद भी भारतीय मुसलमान घेराबंदी की भावना के तहत जी रहा है। उसे अपने पुरखों के पाप के लिए सताया और दंडित किया जा रहा है। इन पर चूक, अपमान, उल्लंघन के गलत आरोप लगाए जाते हैं। विभाजन के बाद के वर्षों में इनपर गद्दार होने का आरोप लगाया गया और इनकी जगह सीमा के पार बताई गई। वह सीमा जिसे बनाने में इनके पूर्वजों ने मदद की थी। इसके बाद इन्हें चुनावी राजनीति में खेल के प्यादे के रूप सीमित कर दिया गया। 2014 का चुनाव भारतीय मुसलमानों को आईना दिखाने सरीखा रहा। परिणाम से यह साबित हो गया कि यह कहना अब लफ्फाजी नहीं है कि वे अब हाशिए पर चले गए हैं और बड़ी योजनाओं के लिए कैसे अप्रभावी हो गए हैं। जब संख्याओं के खेल की बात आती है तो मुस्लिमों का वोट कोई मायने नहीं रखता है।
स्पष्ट रूप से भारतीय मुसलमानों को सामाजिक-आर्थिक अर्थों में खुद में और अधिक सुधार की जरूरत है। यह और एकीकृत और गतिशील होना चाहिए। सच्चर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जिन बिंदुओं पर वे अटकते हैं वे बहुत ही स्पष्ट हैं। देश के लिए, खासतौर पर हिंदुओं के लिए यह समान रूप से जरूरी है कि वे उस लेंस को ठीक करें जिससे वे मुस्लिमों को देखते हैं।
भारत के मुसलमानों के बीच अव्यक्त धारणा है कि वे कौन हैं या क्या हैं और उन्हें कैसा दिखना चाहिए, पड़ोसियों और साथियों से बेहतर या बुरा नहीं। ऐसे में इनसे आग्रह है कि वे यह दिखाएं कि उनके समुदाय में हिंसा के प्रति विशेष प्रवृत्ति नहीं है, न ही उनके धर्म में हिंसक प्रवृत्तियां अंतर्निहित हैं और न ही इन्हें बढ़ावा दिया जाता है।
भारतीय और विदेशी, संस्कारी और कुसंस्कारी जैसे शब्द चोट पहुंचाने वाले और गलत तो हैं ही इनकी रूढ़िवादिता को बढ़ाने वाले हैं। ये मुस्लिमों को और अधिक हाशिए पर धकेल देते हैं। हिंसा के लिए दोषी ठहराए जाने की जगह वे खुद को हिंसा के शिकार के रूप में देखते हैं। भारत को अपनी मिश्रित समाज के रूप में एकजुटता और अखंडता बनाए रखने के लिए न सिर्फ इस असंतुलन को पहचानना होगा बल्कि इसे दूर भी करना होगा।
(लेखिका आलोचक और साहित्यिक इतिहासकार हैं)








