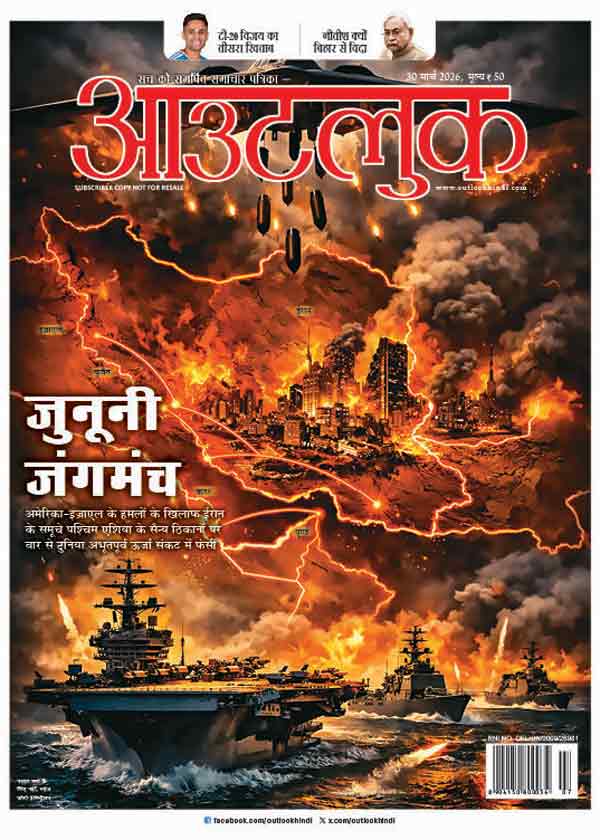क्या होता है स्त्री लेखन? या क्या होता है महिला लेखन? और क्या होता है पुरुष लेखन? जब हम पढ़ते थे, तो यह विभाजन हमें समझाया नहीं गया कि हम जब मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रहे हैं या जयशंकर प्रसाद की कविता का पाठ कर रहे हैं, तो पुरुष लेखन से गुजर रहे हैं। या जब महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं पर पहुंचते हैं और फिर आगे चलते हैं तो कहा जाता है कि यह महिला लेखन है। साहित्य जगत में इस रवैये के चलते मैं हमेशा ऊहापोह में रही हूं कि कलम एक, वर्तनी एक और कागज एक जिसके जरिये लेखक अपनी बात कहता है, यहां तक कि वह स्त्री और पुरुष के संदर्भ में अपना नजरिया पेश करता है और मानवीयता की सिफारिश करता है, तो हमें वह लेखन मनुष्यगत ही लगता है। बेशक हम ऐसे ही भाव विचारों के साथ रचनाओं को पढ़ते आए हों।
यह भी सच है कि साहित्य हो या कला ये इतिहास की तरह स्थिर नहीं, इनमें बदलाव होता रहता है और यह बदलाव अतीत की या वर्तमान की कथा ही नहीं कहता, यह भविष्य कथाओं की भी संभावना खोजता है। ऐसी खोजों के परिणामस्वरूप ही हमारे सामने आया लेखन में स्त्री और पुरुष का विभाजन! यह हमारे गले उतरे या न उतरे मगर साहित्य जगत में प्रचलित हो गया है। कुछ लेखक और लेखिकाएं इस विभाजन को संपादकों के नाम पर डालकर यह सिद्ध करना चाहती हैं कि उनके संपादन में पत्रिकाएं पाठक नहीं जुटा पा रही थीं, तब उन संपादकों ने स्त्रियों और पुरुषों के लेखन के बंटवारे का शिगूफा छोड़ा। मैं यहां किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकती क्योंकि यह बंटवारा नहीं था, अब स्त्री लेखन की उठान का समय आ गया था। स्त्री की जो कलम पहले झिझकती सी आगे बढ़ती थी मगर अपनी त्रासदियों को कहना चाहती थी, अब स्त्री की वही कलम नई धार के रूप में बेधड़क बयान करने लगी। लोगों ने कहा, स्त्री विमर्श।
स्त्रियां इस फतवे पर संतुष्ट दिखीं। नहीं देखा कि यह भी एक बंटवारा ही है। वे तो इस खुशफहमी में रहीं कि वाह अब भारतीय स्त्री मेधा को सिमोन द बउआर के पीछे-पीछे लाया जा रहा है। नहीं सोचा कि भारतीय स्त्री के जीवन-संघर्ष कठिन और अलग तरह के हैं जिनमें पुरुष बाकायदा शामिल है। अत: हमें अपना डिस्कोर्स पश्चिम की नकल पर नहीं, देश में चली आ रही रूढ़ियों, फलते-फूलते अंधविश्वासों और जानलेवा रिवाजों के खिलाफ प्रस्तुत करना है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इन बुराइयों की जड़ बहुत गहरे दबी है परिवारों में समाज में और पूरे देश में। इनके खिलाफ जो स्त्री उठती है उसको वाह-वाही तो नहीं मिलती, परिवार और समाज बेहयायी के साथ घृणित मान लेता है। तब समझ में आता है कि स्त्री विमर्श के नाम पर चलाया गया आंदोलन क्यों ठिठक गया? रूढ़िवादी रिवाजें और परंपराएं भारतीय जनमानस की सदियों की कमाई हैं, इस पुरुषवादी खजाने को स्त्रियों के विमर्श के हाथों क्या सहज लुट जाने दिया जाएगा? अत: परंपराओं के नाम पर पुराने चलन नए रूप में आने लगे जिन्होंने, शिक्षित और आधुनिक महिलाओं को गिरफ्त में ले लिया।
मैं निराशावादी नहीं हूं। हमें मालूम है कि अभी पूरे मानवीय अधिकार हाथ में नहीं आए हैं मगर स्त्री पक्ष से खींचतान शुरू होकर लगातार जारी है। यहां उम्मीद है तभी तो कुछ कानून भी औरत के पक्षों लिखे गए हैं, मगर पुरुष भी अपने पक्ष को किसी हालत में कमजोर होने देना नहीं चाहता। पिछले समय से अब तक फर्क तो यह आया है कि पुरुष स्त्री को मनमाने ढंग से पत्नी रूप में बांधकर निर्द्वंद्व नहीं रह सकता। हालांकि यह बात अभी सब जगह लागू नहीं की जा सकती मगर इन बातों की खबर तो देश के कोने-कोने में जाती है। भला हो इस वैज्ञानिक समय का कि खबरों के काफिले जगह-जगह उतार दिए क्योंकि झोंपड़ियों में भी टीवी बोल रहा है। हमारे देश की स्त्रियों ने स्त्री विमर्श का तात्पर्य समझा हो या न समझा हो लेकिन विभिन्न सूचना-साधनों से वे दुर्दशा और उत्पीड़न के मायने समझ चुकी हैं, जिसे वे अब तक पतिव्रता का कर्तव्य मानती चली आ रही थीं। यही तो बात है कि आज मजदूर स्त्री से लेकर पढ़ी-लिखी और नौकरीपेशा महिला मुक्त होने के रास्तों की तलाश में है।
यह सन उन्नीस सौ सैंतालिस नहीं जब भारत को भारतीयों ने अंग्रेजों से आजाद कराया था, यह दो हजार बाईस है, जब स्त्री स्वतंत्र भारत में अपने संवैधानिक अधिकार पाकर उनको लागू करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बेशक अभी अपने देश में औरत की जंग जारी है।

(सुप्रसिद्ध साहित्यकार और स्तंभकार)