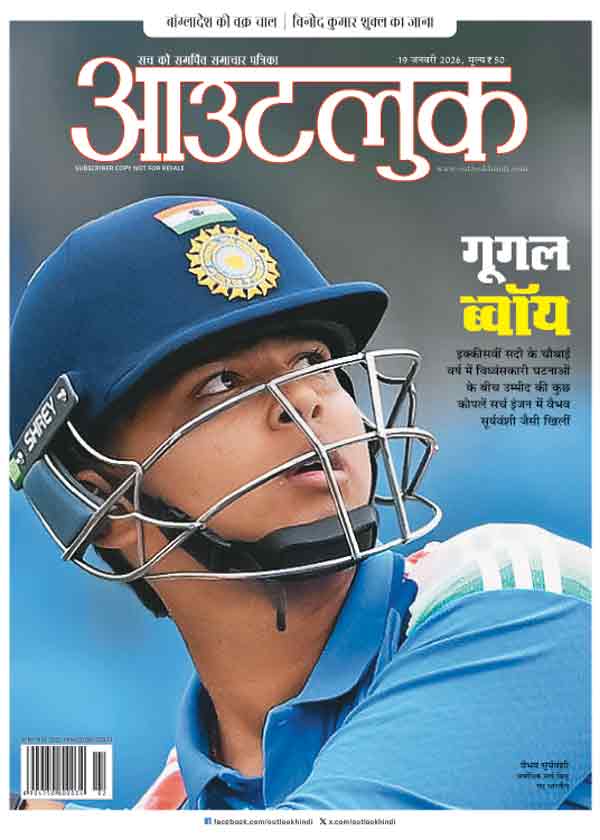भारत में जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं रह गया है। अब इसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी तेजी से उभरने लगे हैं। जलवायु संकट की बड़ी वजह औद्योगीकीकरण और अमीरों की आरामदायक जीवन-शैली वगैरह मानी जाती है, जिसकी कीमत गरीब और हाशिए पर जीने वाले लोग चुका रहे हैं। पर्यावरण के साथ की गई मनमानी का बोझ अब मजदूर वर्ग के सिर पर टूट रहा है, वही सबसे ज्यादा इसकी मार झेल रहे हैं। 2023 की ऑक्सफैम की रिपोर्ट इस बात की तसदीक करती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोग, सबसे गरीब 50 प्रतिशत लोगों की तुलना में चार गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके पीछे उनकी जीवनशैली है, जिसमें बड़ी-बड़ी एसयूवी गाड़ियां, लगातार चलने वाले एयर कंडीशनर और अनियंत्रित उपभोग के सामान शामिल हैं। इन सबने मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ाया है।
इस असमानता का एक और आयाम है सामाजिक संरचना। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम), बेंगलूरू की एक रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव न केवल आर्थिक, बल्कि जातिगत आधार पर भी असमान है। निम्न जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों को गर्मी, बाढ़ और सूखे का सामना करने के लिए अपर्याप्त संसाधनों के साथ जीना पड़ता है।
मौसम की मार
वैसे तो पूरे दक्षिण एशिया को जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बिगड़ते प्रभावों के चलते ‘रेड जोन’ में रखा गया है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में गर्मियों का मौसम समय से पहले आ गया था। देश में कई जगहों पर तापमान 50 डिग्री के पार होना अब 'सामान्य' हो गया है। विश्व मौसम संगठन की 2023 की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार, 2023 अब तक का सबसे गर्म साल था। हालांकि, सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि बाढ़ और सूखे की समस्या भी काफी तेजी से बढ़ी हैं। इससे भी धन्नासेठ नहीं, बल्कि गरीब ही प्रभावित हुए हैं।

भूस्खलनः जम्मू के डोडा में भूस्खलन, 26 जून
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले दशक में बाढ़ की घटनाओं में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2023 में असम में आई बाढ़ ने 70 लाख लोगों को विस्थापित किया और 2.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को नष्ट कर दिया। बिहार में 2024 की बाढ़ ने 12 लाख लोगों को प्रभावित किया, जिसमें से अधिकांश निम्न-आय वर्ग के थे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले समय में स्थिति और भयावह होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान से हिमालयी ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे और बाढ़ की समस्याएं और बढ़ेंगी।
जानलेवा गर्मी और बाढ़ की तरह सूखा भी जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर परिणाम है। सेंट्रल वाटर कमीशन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 21 राज्यों में सूखे की स्थिति गंभीर हो रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2019–2023 के बीच सूखे के कारण 30 प्रतिशत फसल नष्ट हुई। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ा। सूखे का प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं है। पानी की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट बढ़ रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2030 तक चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई जैसे भारत के 21 शहरों में भूजल की कमी हो जाएगी, जिससे करीब 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। 2019 के "जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक" में भारत को 'उच्च जोखिम' श्रेणी में रखा गया है।
बहरहाल, चाहे तीव्र गर्मी हो, सूखा हो या बाढ़ या जलवायु परिवर्तन का कोई भी विनाशकारी रूप, इन सभी का असर समाज के उन कथित संभ्रांत लोगों पर नहीं, बल्कि उन पर पड़ा है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं।
शहरीकरण के दुष्परिणाम
शहरों में जलवायु परिवर्तन का असर और भी भयावह है। अमीरों की सुविधाएं जैसे एयर कंडीशनर, बड़े मॉल और कंक्रीट के जंगल, शहरी तापमान को बढ़ा रहे हैं। इसे "अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट" कहा जाता है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में यह प्रभाव स्पष्ट दिखता है। द नेचर में ‘भारत में जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं’ शीर्षक से छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘भारत में एयर-कंडीशनिंग की मांग, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा से पांच गुना अधिक है।’’
इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने वाली कंपनी वोल्टास के एमडी मुकुंदन मेनन ने एक इंडस्ट्री इवेंट में कहा, “फिलहाल साल में 15 लाख एसी खरीदे जा रहे हैं। यह बिक्री पिछले चार वर्षों में ही दोगुनी हो गई है और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी ही होगी।” इस बात से यह सवाल भी उठ सकता है कि प्रति व्यक्ति लगभग 2.5 लाख रुपये सालाना आय वाले भारत में, आखिर इतने एसी खरीदेगा कौन?
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘भारत के 82 प्रतिशत पुरुष और 92 प्रतिशत महिला श्रमिक 10 हजार रुपये महीने से भी कम कमाते हैं। जिस देश में 75 करोड़ की आबादी एक दिन में केवल 250 रुपये कमाती हो, उसके लिए क्या एसी लगाना संभव है? इसका जवाब है, नहीं।
आजीविका और स्वास्थ्य पर असर
जलवायु परिवर्तन आजीविका और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. अलग-अलग शोध भी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं। परपज-लेड पब्लिशिंग की एक रिपोर्ट बताती है कि एक डिग्री तापमान बढ़ने से मजदूरों की कमाई 14 प्रतिशत तक घट जाती है। बाढ़ और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में यह नुकसान और बढ़ जाता है।
लैंसेट काउंटडाउन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में गर्मी के कारण वैश्विक स्तर पर 470 अरब श्रम घंटों का नुकसान हुआ, जिससे 39 लाख करोड़ रुपये की आय प्रभावित हुई। भारत में यह नुकसान विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ा।
ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम अब जानलेवा भी होते जा रहे हैं। 2023 में दिल्ली के गाजीपुर में एक कूड़ा बीनने वाले श्रमिक की गर्मी के कारण सड़क पर मौत हो गई। स्थानीय निवासी माजिदा बेगम ने बताया, “परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गर्मी ने उनकी जान ली, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है?”
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2000–2020 के बीच लू से 20,615 मौतें हुईं, लेकिन स्वतंत्र अध्ययनों का दावा है कि वास्तविक संख्या कहीं अधिक है। बाढ़ और सूखे से होने वाली मौतें भी इस आंकड़े में शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं रखा जाता।
नीतियां और हकीकत
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत में कई योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन इनका जमीनी प्रभाव सीमित है। अहमदाबाद ने 2010 में देश का पहला हीट एक्शन प्लान लागू किया, जिससे गर्मी से होने वाली मौतों में 27 प्रतिशत की कमी आई। इस योजना में पब्लिक कूलिंग सेंटर, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और काम के घंटों में बदलाव शामिल थे। हालांकि, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की समीक्षा बताती है कि 37 हीट एक्शन प्लानों में से अधिकांश में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन की कमी है।
बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए भी समग्र नीतियों का अभाव है। एनडीएमए की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ प्रबंधन के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण योजनाएं कागजों तक सीमित हैं।
संयुक्त राष्ट्र की माने तो ग्लोबल तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना अब अनिवार्यता है। ऐसे में समय रहते हमें सचेत रहने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन अब मात्र पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता का भी प्रतीक है। जब तक नीतियां और संसाधन इन समुदायों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक यह असमानता की खाई और गहरी होती जाएगी।