अगर सौमित्र चटर्जी ने मृणाल सेन की विचलित कर देने वाली मृत्यु के बाद के दिनों में एक बांग्ला दैनिक में अपने लेख में जिक्र नहीं किया होता तो शायद बहुत सारे लोग मृणाल सेन की बेहद कम देखी गई और उससे भी कम चर्चित 1977 की तेलुगु फिल्म ओका ऊरी कथा (बहिरागत) के बारे में सत्यजित राय की प्रशंसा से सर्वथा अनजान रह जाते। अनुवाद में चटर्जी का लिखा कुछ इस तरह पढ़ा जाएगा, ‘‘1977/78 के दिन थे। मैं मानिक दा (सत्यजित राय के घर का नाम) से मिलने उनके घर गया था। मैंने उन्हें बहुत उत्तेजित पाया। वे बोले, “जानते हो, मैंने अभी-अभी मृणाल की ओका ऊरी कथा देखी। मुझे बड़ी पसंद आई। फिल्म किसी भी डायरेक्टर के मन में ईर्ष्या जगा सकती है।”
अवाक कर देने वाली मौलिक फिल्म ओका ऊरी कथा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ‘कफन’ से ‘खोज’ निकाली गई थी। सेन इस कहानी को हिंदीभाषी हृदय प्रदेश से सुदूर तेलंगाना के अंधियारे खेत-खलिहानों में ले गए और महान कन्नड़ अभिनेता वासुदेव राव को तलाश में निकले आदिम दार्शनिक की केंद्रीय भूमिका में पेश किया। अपनी असहाय प्रजा को संपूर्ण समर्पण पर मजबूर करने के लिए सामंती भूमि-स्वामियों के अंतहीन शोषण के तौर-तरीकों की बेहद कटु, अराजक आलोचना के इस मास्टरपीस में सेन अखिल भारतीय नजरिये में चोटी पर खड़े दिखते हैं। निपट दो-टूक और बिना किसी हमदर्दी के, यह क्रूर किस्सा कुल मिलाकर एक अधेड़ बाप और जवान बेटे की छल-कपट की दास्तान है, जो जिंदगी चलाने की खातिर काम करने से तौबा कर लेते हैं क्योंकि बकौल उनके, बुरी व्यवस्था में काम करना उसे बढ़ावा देता है।

ओका ऊरी कथाः अरे वेंकैया की भूमिका में कन्नड़ अभिनेता वासुदेव राव और किष्टैया
बेटा घर में पत्नी लाता है और वह काम करने जाती है क्योंकि वह अलग सोच-समझ की उपज है, तो बाप और बेटा उसकी कमाई पीने में उड़ा देते हैं। कड़ी मेहनत और भुखमरी की शिकार जवान औरत बच्चे के जन्म के दौरान मर जाती है। दोनों मर्द उसका कफन खरीदने के लिए गांव में पैसा मांगते घूमते हैं, लेकिन भीख में मिले पैसे को पीने में उड़ा देते हैं। फिल्म देखकर दर्शकों के मन में गुस्से, उदासी का गुबार घुमड़ने लगता है और सबसे बढ़कर वह चकित कर देने वाला गहरा एहसास, कि कोई कलाकार अगर सोये हुए दर्शकों को जगाने की ठान ले, तो किस हद तक जा सकता है।
अपने उतार-चढ़ाव वाले लगभग पूरे करियर में सेन मासूम किस्सागोई से अपनी वितृष्णा की मानिंद खुद को अलग खड़ा करते हैं। सुरक्षित मनोरंजन मुहैया कराना कभी उनकी कलात्मक और बौद्धिक प्रतिभा का अंग नहीं रहा। सब कुछ खुलेआम या दबे-छुपे पाखंड को उजागर करने की उनकी टकराव मोल लेने की राजनैतिक दृष्टि पर सोचे-समझे ढंग से सामने आता क्योंकि उसके बगैर मध्य-वर्ग कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। लगता है, सेन के दिमाग में हमेशा साफ था कि उन्हें अपने दर्शक वर्ग के लिए बतौर कलाकार और नागरिक कौन-सा दायित्व उठाना चाहिए। इसी स्पष्ट नजरिये से लगभग आधी सदी तक अपने लोगों के मन में उथल-पुथल मचाने या नैतिक पहरुए की स्वयंभू भूमिका में सेन अपनी कला का जश्न मनाते रहे, बशर्ते आपको पसंद आए। अगर वे (दर्शक) हमेशा खुद से सवाल करने, या ठीक-ठीक कहें तो शर्म और पछतावे की आंच में नहीं झोंक दिए जा सकते तो उसमें डायरेक्टर की कोशिशों की गंभीरता से ज्यादा उनके वर्ग की दुर्दशा और ढीठाई ही झलकती। सौभाग्य से, कुछ आलोचकों में विवाद की खातिर विवाद पैदा करने की निंदक प्रवृत्ति को छोड़ दें, तो दूसरों ने उसे भटके हुओं को राह पर लाने और गुनहगारों के मन में कबूलनामे/पछतावे के भाव भर देने की सुविचारित संयोजना के रूप में वर्णित किया।

किष्टैया की पत्नी की भूमिका में ममता शंकर
उपलब्ध सबूतों पर गौर करें तो सेन को कभी पढ़े-लिखे, अपेक्षाकृत खुशहाल वर्ग ने उस जख्म के लिए कभी माफ नहीं किया, जिसे वे बार-बार हरा करते रहे, तब भी नहीं जब उन्होंने अपने करियर के आखिरी वर्षों में कुछ नरमी दिखाई। हालांकि वे इसी वर्ग का हिस्सा थे (इस मायने में उनका अनुभव अग्रणी मलयाली मार्क्सवादी ईएमएस नंबूदरीपाद से मिलता-जुलता था, जिन्हें तीखा विरोध सभी नहीं, तो भी अपने ही अनेक नंबूदरी ब्राह्मणों से झेलना पड़ा)। कोई आसानी से याद कर सकता है कि साठ के दशक की शुरुआत से लेकर अस्सी के दशक के मध्य तक विस्तारित दौर में जब भी सेन कोई नई फिल्म लेकर आते तो कुछ खास हलकों में वह बेचैनी पैदा कर देती, जिसमें कलकत्ता के प्रमुख अखबारों-पत्रिकाओं के पीलियाग्रस्त स्तंभ भी थे। लगता था कि कई चिड़चिड़े आलोचकों या दर्शकों में दहशत या कहें वितृष्णा हिलोरें लेने लगती कि इस बार यह विवेकवान विद्रोही क्या लेकर आएगा! हालांकि, इस संदर्भ में सेन की बात तब की बहुत-सी बेचैन जवान आत्माओं के लिए सोच-विचार का खुराक बनी, जब शहर और देहात दोनों ही आंतरिक विरोधाभासों और सरकारी दमन से पैदा बाहरी भय की आग में झुलस रहे थे। “मैं जान-बूझ कर कोई लोकप्रिय फिल्म नहीं बना सकता। भारतीय दर्शक जब सिनेमा देखने जाते हैं तो अपनी दैनिक जिंदगी से बचने की राह तलाशते हैं। मेरे विषय लोकप्रिय अपील के लिए दैनिक जीवन के बहुत ही करीब हैं। मुझे संदेश सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए कोई तरीका तलाशना है। मुझे लगता है कि दर्शकों को बेचैन कर देना ही काफी नहीं है। जरूरी है कि उकसावे के एजेंट जैसा काम किया जाए।”
सेन के काम पर गंभीर दृष्टि डालने वाले कई दर्शक इस राय के लगते हैं कि उनकी सभी फिल्में सामाजिक विवेक को झकझोरती हैं, बेशक, ओका ऊरी कथा सबसे गहरे उतरती है। फिल्म के यथार्थ और अतिरेकी-यथार्थ, मतलब कि निपट अविश्वास की हद तक, की मिलाजुली नियति से यकीनी गहरी अपील के मद्देनजर उससे सरासर बावस्ता होने से खुद को रोक पाना मुश्किल है।

एक शूट के दौरान सेन
अरे वेंकैया, बाप, किसी जंगली जानवर की तरह टूट पड़ता है, और किष्टैया, बेटा, पक्के आज्ञाकारी की तरह बाप के पीछे-पीछे, उसके बातूनी कदमों पर चल पड़ता है, असाध्य परजीवी की तरह? या मानो वे विस्फोटक विद्रोही हैं जो अपनी उन्मत्त बातों और तौर-तरीकों से भूचाल लाने पर तुले हैं? या, मानो वे कोरे आदिम बेमेल जोड़े हैं, एक परंपरा-सिद्ध समाज-व्यवस्था के जाने-बूझे परित्यक्त, जिसका फैसला है कि जिंदा रहने के लिए वेंकैया जैसे को गुलाम होने को राजी होना है, उनके श्रम का फल भू-स्वामी और उसके गुर्गों-पुरोहित, किराना दुकानदार और सूदखोर की सेवा में लगना है? शायद ये नीच पराश्रयी, जो शारीरिक श्रम की संस्था की आम समझ के लिहाज से किसी काम के नहीं, शारीरिक और मानसिक गुलामी की संस्कृति से मुक्त होने को छटपटा रहे हैं, जैसे कोई क्रोधित प्रेत, जो आधा वास्तविक, आधा मिथकीय है- मौजूदा सामाजिक नियमों और आर्थिक समीकरणों पर चलने से इनकार करता बस एक-एक पल को जीता है।
दर्शक अपने भीतर किसी कल्पना-लोक में शायद इस मोहक ‘विध्वंसक गर्जना’ के नारकीय दृश्य की ताजपोशी के विचार से मुग्ध हों, जो निपट अपने क्रोध से स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फेंकने पर तुले हैं। क्या यह वही हो सकता है, जब कवि कहता है, ‘दीवाना होने में एक शर्तिया सुख है, जो और कोई नहीं सिर्फ दीवाना ही जानता है’? शायद वह लंबी अंधियारी रात के ऐसे वंचित प्राणियों के बारे में भी सोच रहा हो, जिन्होंने शोषण करने वाले की संगठित ताकत से भिड़ने के लिए एक खास तरह की दीवानगी को बहाने, या बेहतर कहें, तो रणनीति की तरह अपना लिया है?
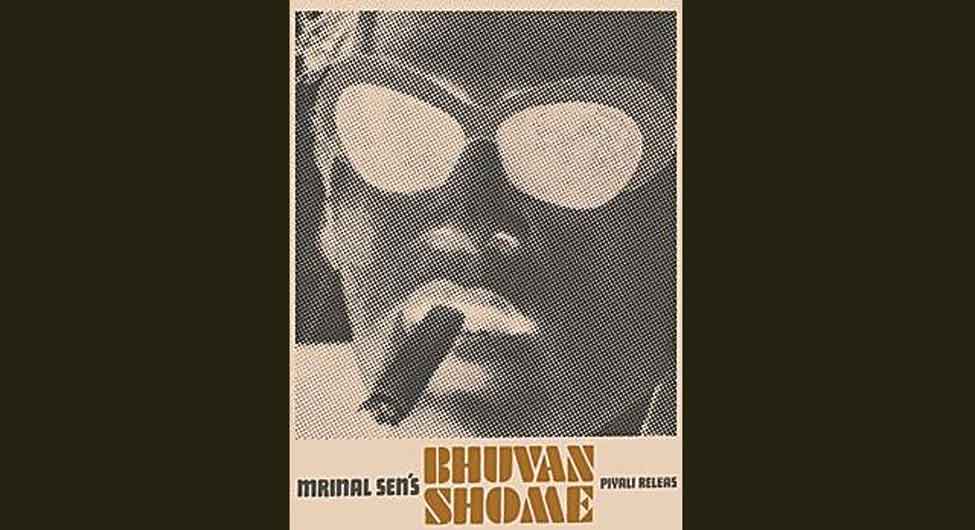
भुवन शोम का पोस्टर
प्रतिबद्ध सूत्रधार की अपनी भूमिका को सच साबित करते हुए सेन ने दोनों की ‘काम करने या न करने’ के मामले में अपनी पसंद के चयन को अनोखे, दो-टूक संदर्भों में दिखाया है। उन्होंने तय किया है कि काम तभी करेंगे जब भूख सताए, वरना अपने दुखों को सोकर काट देंगे, भीख मांगेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे। बीच-बीच में बहकी-बहकी बातें, शेखी बघारेंगे। बाप को देख वितृष्णा होती है, मगर वह अपनी ओर खींचता है, जैसे नकार का कोई बेहद बातूनी अवतार हो। दूसरे शब्दों में कहें, तो इन चोटी के रणनीतिकारों ने तय किया है कि अपनी मेहनत-पसीने से शोषण करने वालों को धनी, ताकतवर, अधिक लालची नहीं होने देंगे। बूढ़ा अपने बेटे, और गांव मेें हर उससे जो उसे सुनना चाहे, कहता है कि तुम मूर्ख हो कि काम करने जाओ, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ मालिक को मोटा करेगा, जो तुम्हारी लंगोट चुराने में एक पल को भी नहीं सोचेगा! वह अपने बेटे को चेताता है, जिसके मन में कभी-कभी संदेह उपजता है कि काम के जाल में न फंसो- “काम का प्रेत कभी तुम्हें आजाद नहीं होने देगा; अगर उस जाल में फंसे तो खो जाओगे।”
ओका ऊरी कथा में हमारा वास्ता जिससे पड़ता है, मुट्ठी भर ग्रामीणों के हाथ में धनबल जमा होने में भूमिहीन मजदूरों के अहम योगदान की विस्फोटक जांच-परख में कई जगह अतिरेक या अतिशयोक्ति का प्रयोग निहायत जरूरी, अनिवार्य था। स्वयंभू कंगाली धारण करने का यह ड्रामा स्वीकृत नियम-कायदों के अधीन काम करने की जरूरत के मामले में परंपरागत समझ की खिल्ली उड़ाता है तो जाहिर है, ऐसे कोलाहल, शोर-शराबे की दरकार थी, जिसे सेन ने बखूबी इस्तेमाल किया है, ताकि एक तरफ दो कंगाल लावारिसों और दूसरी तरफ जमींदार तथा उसके लोगों के बीच निहायत गैर-बराबरी वाली प्रतिस्पर्धा का नजारा दिखाया जा सके। विद्रोह, पतन या मृत्यु की छवियों की कटु सच्चाई लगभग सम्मोहक अंदाज में जिंदा हो उठती है, जब वासुदेव राव के अभिनय के बेहद भावुक, भड़कीले अंदाज में वह पिरोई जाती है, जो उनकी कुल शख्सियत की रहस्यमय अदाकारी में साकार हो उठी है।

मृणाल दा की फिल्म का एक दृश्य
सेन का काम की निरर्थकता का ‘संदेश’ ग्रामीण शोषण को एक हास्यास्पद प्रभावशाली मोड़ पर खड़ा कर देता है, जिससे मालिक की धन-संपदा, खुशहाली बढ़ती है जबकि मातहत की हालत दयनीय होती जाती है। ऐसा भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया, या इस मायने में बाद में भी नहीं। यह सवाल भी उठाया जा सकता है कि क्या बेहतर लोगों द्वारा नियंत्रित और कायम किए गए ग्रामीण समाज/अर्थव्यवस्था में गैर-फायदेमंद मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने का ऐसा विद्रोही यूटोपिया दुनिया भर के सिनेमा में कहीं दिखता है।
कलात्मक नजरिये से कहें तो ओका ऊरी कथा का बेचैन कर देने वाला आकर्षण विरुद्धों को अगल-बगल रखने की यादगार शैली से पैदा होता है। मानो भयानक डरावने और हंसोड़ नजारे पूरे अफसाने में साथ-साथ कदमताल कर रहे हैं। अंत में विरुद्धों का यह घालमेल अवाक कर देने वाली उदासी में बदल जाता है, मसलन, आला दर्जे का आलसी ससुर आत्मघात की हद तक ऊर्जावान बहु के खिलाफ खड़ा है, जो मानव मनोविज्ञान और मानव आचार-व्यवहार के विरोधाभासी विमर्श की अकूत संभावनाओं से भरा है।
सेन के सामाजिक दर्शन का अनूठापन और उनकी फिल्म कला की निडर प्रकृति का स्रोत उनके इन शब्दों में बखूबी रोशन होता है, “भारत में कुछेक अपवादों के अलावा, फिल्मकार शायद ही उससे आगे देखते हैं जो उनके पूर्ववर्ती हासिल कर चुके हैं। हमें अपने काम के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रयोग करने की दरकार है; ऐसे प्रयोग जो सिनेमा के नए जॉनर की आमद का प्रतीक बनें; सबसे बढ़कर ऐसे प्रयोग जो समाज परिवर्तन के औजार के नाते इस माध्यम को धारदार बनाएं।”
अपनी राजनीति या मौलिक प्रकृति में ओका ऊरी कथा भारतीय सिनेमा में दैत्यों और हत्यारों के कहने में आसान, पचने में आसान, घिसी-पिटी परंपरा से एक क्रांतिकारी बदलाव थी। फिल्म इस जरूरत पर बल देती है कि अगर आजादी और इंसाफ के मुकाम पर पहुंचना है तो हर तरह के श्रम से मीलों दूर का सफर तय करना होगा। वह मौलिक प्रयोग के मामले में उतनी ही अद्भुत थी, जिसमें डॉक्यूमेंट्री के तत्वों के साथ अतिनाटकीयता का गजब मिश्रण था। सेन व्यक्ति और समाज के विध्वंसक, हताशाजनक अफसाने को साथ जोड़कर एकदम कोरी जिंदगी के कुल अनुभव को सामने ले आए। आशा है, ओका ऊरी कथा का ‘पाठ’ जारी रहेगा, अलबत्ता धीरे-धीरे बढ़ती विशिष्ट दर्शकों की बिरादरी में, इस ‘सोची-समझी अतार्किकता’ के महाकाव्य का पाठ, जो कि यह है। सुनने में कितना ही बेतुका लगे, फिल्म की विकृत बौद्धिकता असह्य भावनाओं के साथ जुड़कर ऐसी हैसियत कायम करती है कि उसे प्यार करने से ज्यादा कला के दायरे से खारिज करने में डर लगता है।

(लेखक कोलकाता स्थित पुरस्कार प्राप्त फिल्म समालोचक और लेखक हैं)








