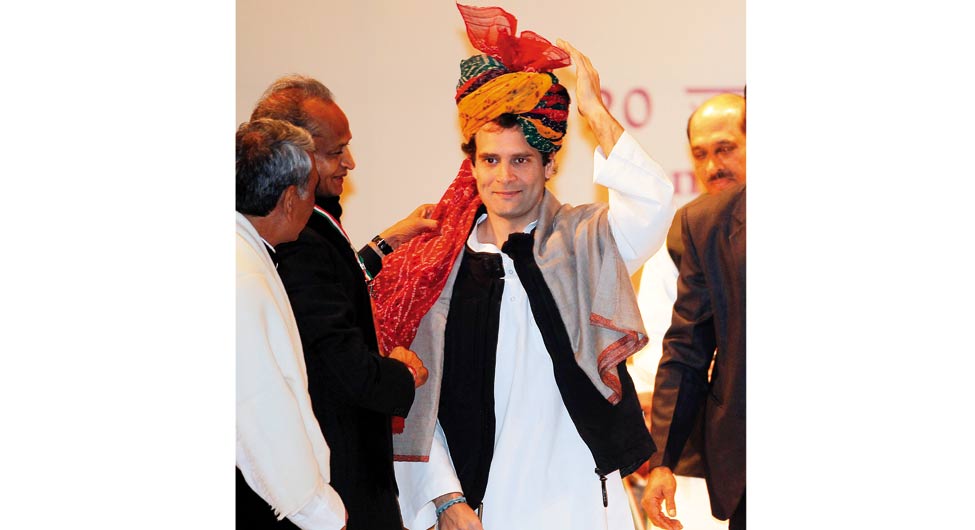कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के दो बड़े मायने हैं। एक, यह इस्तीफा नहीं, बल्कि राहुल की आत्म-स्वीकृति है। दूसरे, यह उनके सहयोगियों, विशेष रूप से वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा किए गए विश्वासघात की भी स्वीकृति है। कांग्रेस में राहुल के इस्तीफे से जिस प्रकार का संकट पैदा हुआ है, वह एक तरह से नया भी है और पिछले संकटों की पुनरावृत्ति भी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट पहली बार पैदा नहीं हुआ है।
देश की सबसे पुरानी राजनैतिक पार्टी को मैंने 1967 से कवर करना शुरू किया था। तब से लेकर 2019 के बीच कई संकटों से यह पार्टी गुजरी है। वैसे 1885 में स्थापित यह पार्टी 1947 तक कई बदलावों के शिखर और तलहटियों से गुजरती रही। लेकिन स्वतंत्र भारत में मई 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद पहली बार नेतृत्व को लेकर तात्कालिक संकट खड़ा हुआ था। उस समय पंडित जी के करीबी लालबहादुर शास्त्री थे, तो इसका समाधान तत्काल हो गया। लेकिन उसके बाद डॉ. राममनोहर लोहिया ने गैर-कांग्रेसवाद का नारा दिया। नतीजतन 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार तो नहीं हुई, लेकिन लोकसभा में सीटें बहुत कम हो गईं। कई राज्य भी उसके हाथ से फिसल गए। 1966 में इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया समझकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल जैसे खुर्राट नेताओं ने सोचा कि इंदिरा उनके इशारे पर नाचती रहेंगी और नेहरू वंश की विरासत भी जारी रहेगी। इस दोहरे लाभ को निचोड़ने के लिए तब के सिंडिकेट कांग्रेसियों ने सरकार और संगठन पर कब्जे की रणनीति अपनाई। लेकिन देखते ही देखते इंदिरा स्वतंत्र होने लगीं। खुर्राट नेताओं और नई पीढ़ी की प्रतिनिधि इंदिरा के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। 1967 में प्रधानमंत्री पद को लेकर इंदिरा और मोरारजी देसाई के बीच घमासान छिड़ा था। आखिर में मोरारजी को उप-प्रधानमंत्री बनाकर संकट का हल निकाला गया।
जब हम 1969 में आते हैं तब संगठन कांग्रेस और इंदिरा के नेतृत्व में सत्ताधारियों की कांग्रेस के बीच अंतर्विरोध तीव्र हो जाता है। इंदिरा अपने ही दल के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराने में परोक्ष भूमिका निभाती हैं और अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का नारा लगाती हैं। फलस्वरूप उनके अघोषित उम्मीदवार वी.वी. गिरि चुनाव जीत जाते हैं और संगठन के उम्मीदवार रेड्डी हारते हैं।
यहीं से कांग्रेस में संकट शुरू होता है। यह आजादी के बाद पार्टी का सबसे बड़ा संकट था। कांग्रेस विभाजित हो जाती है। इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस को इंदिरा कांग्रेस या रूलिंग कांग्रेस (कांग्रेस-आर) जबकि संगठन कांग्रेस को सिंडिकेट कांग्रेस कहा जाने लगा। दोनों के महाधिवेशन अलग-अलग जगह होते हैं। इंदिरा कांग्रेस का महाधिवेशन बंबई में और संगठन कांग्रेस का अहमदाबाद में। इसके बाद संकट और गहराता है। इंदिरा सरकार अल्पमत में आ जाती है, लेकिन समाजवादी और वाम सांसदों के समर्थन से वे सत्ता में बनी रहती हैं। वे बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजाओं का प्रिवीपर्स खत्म करती हैं। 'गरीबी हटाओ' नारा देश में गूंजता है। नतीजतन, 1971 के चुनाव में इंदिरा को जबरदस्त बहुमत मिलता है और उनकी कांग्रेस को ही असली कांग्रेस मान लिया जाता है।
सत्ता में इंदिरा गांधी की वापसी के कुछ वर्ष बाद जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हुआ। चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत जैसे कई वरिष्ठ नेता इंदिरा का साथ छोड़ जेपी के साथ हो जाते हैं। कांग्रेस में फिर एक संकट गहराता है, क्योंकि इंदिरा राजनीति की जबरदस्त खिलाड़ी थीं, उनमें एक सीमा तक अधिनायकवाद भी मौजूद था। नए संकट का समाधान जून 1975 में इमरजेंसी लगाकर करने की कोशिश की जाती है। यहीं से कांग्रेस का जमीनी ढांचा कमजोर होने लगता है। उनका दबदबा बढ़ने लगता है जो इंदिरा के करीबी और राजनैतिक परजीवी थे। उस समय के संगठन के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने 'इंदिरा इज इंडिया', 'इंडिया इज इंदिरा' का नारा दिया। लोकतंत्र में जब व्यक्ति पूजा की संस्कृति को प्रश्रय मिलता है तो परिणामस्वरूप संगठन और इसके साथ लोकतंत्र कमजोर होने लगता है।
कांग्रेस में उस समय संगठन के स्तर पर आंतरिक संकट गहरा गया था। ऊपर से सब मजबूत दिख रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि इसके परंपरागत आधार खिसकते जा रहे थे। नतीजतन, 1977 के चुनाव में इंदिरा को करारी हार मिलती है। वे रायबरेली और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं।
बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे वरिष्ठ नेता नई कांग्रेस बनाते हैं- कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इसके समानांतर पुरानी संगठन कांग्रेस भी चलती रहती है जिसमें के.सी. पंत जैसे नेता रहते हैं। इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस भी बनी रहती है। लेकिन जनता पार्टी में आंतरिक कलह की वजह से उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और जनवरी 1980 में इंदिरा की फिर वापसी होती है। अब वे कांग्रेस की सर्वेसर्वा नेता बन जाती हैं। संगठन कांग्रेस का वजूद न के बराबर रह जाता है।
कह सकते हैं कि राजीव गांधी तक कांग्रेस मजबूत रही। लेकिन 1989 में यह फिर सत्ता से बाहर हो जाती है। राजीव के कई वरिष्ठ सहयोगी- विद्याचरण शुक्ल, आरिफ खान, अरुण नेहरू जैसे नेता वी.पी. सिंह के साथ हो जाते हैं। 1989 में गठबंधन का दौर शुरू होता है जिसका नेतृत्व वी.पी. सिंह करते हैं। 1991 में मध्यावधि चुनाव में पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस वापसी करती है, लेकिन अल्पमत के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के समर्थन से सरकार चलती है।
20 मई 1991 को विस्फोट में राजीव की मौत के बाद नेहरू-इंदिरा वंश हाशिए पर चला जाता है। संगठन और सरकार, दोनों पर नरसिंह राव का आधिपत्य हो जाता है। हालांकि तब भी अनेक नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनें। लेकिन नरसिंह राव कांग्रेस को नेहरू परिवार से अलग नया नेतृत्व देना चाहते थे। यही कारण था कि 1996 में कांग्रेस की हार के बाद सीताराम केसरी अध्यक्ष बने। लेकिन नेहरू-इंदिरा वंश के समर्थक प्रणब मुखर्जी और अर्जुन सिंह जैसे कई वरिष्ठ नेता सोनिया को अध्यक्ष देखना चाहते थे। सीताराम केसरी से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। वह जबरदस्त संकट की घड़ी थी। आखिरकार सोनिया अध्यक्ष बनीं। उन्हें खांटी राजनीति का अनुभव नहीं था। उन्हें बनाने वालों के अपने मंसूबे रहे होंगे। सोनिया सर्वेसर्वा बन गई थीं। उनके सामने एकमात्र चुनौती कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने की थी। वे प्रधानमंत्री बन सकती थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन नहीं देने से ऐसा नहीं हुआ। 1996 के आम चुनाव के बाद 1998 और 1999 में अल्पावधि चुनाव हुए। इस दौरान सोनिया ने बिखरती कांग्रेस को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नतीजतन, 2004 में कांग्रेस की फिर वापसी हुई, हालांकि उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मनमोहन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। बिना उथल-पुथल के सरकार पांच साल चली। 1998 से 2014 तक कांग्रेस संगठन में कोई बखेड़ा नहीं हुआ तो इसका श्रेय सोनिया को ही जाता है।
अब 2019 में राहुल इस्तीफा देते हैं तो परिदृश्य बदला है। 2014 में नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने देश की राजनैतिक संस्कृति का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया। निस्संदेह मोदी की भाषण कला प्रभावशाली है। वे जनता के साथ खुद को प्रभावशाली ढंग से जोड़ते हैं। इस नई राजनैतिक संस्कृति का जवाब कांग्रेस नहीं दे सकी। कांग्रेस में जिस कल्पनाशील नेतृत्व की जरूरत थी, उसका अभाव रहा। 2014 से 2019 तक जिस आंदोलनात्मक भूमिका की अपेक्षा थी, वह कांग्रेस नहीं निभा सकी। इसकी बड़ी वजह यह है कि मोदी ने राजनीति की चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बदल दिया। उन्होंने नई केमिस्ट्री तैयार की। धर्म, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और कॉरपोरेट पूंजी, सबके मिश्रण ने मोदी को शिखर से नीचे तक जोड़ दिया। भाजपा या जनसंघ को मैंने कभी स्वाभाविक राजनैतिक पार्टी नहीं माना। भाजपा मूलतः आरएसएस की बैसाखी पर टिकी है। संघ का काडर हमेशा उसके समर्थन में हिमालय बन कर खड़ा रहा है। कांग्रेस कभी काडर वाली पार्टी नहीं रही। वह स्वाभाविक दल है। 1885 से अब तक यह मध्य वामपंथी और मध्य दक्षिणपंथी, सभी विचारधाराओं का आंदोलन रही है। इसे विरोधाभासों का रसायन कह सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व की विशेषता विरोधाभासों की खूबसूरती के साथ रचनात्मक परिणाम लेने की रही है।
एक बात और। आजादी के समय से लेकर राजीव गांधी तक देश में धर्मनिरपेक्षता का जो प्रोजेक्ट था, वह धीरे-धीरे चुकने लगा। राम मंदिर और मंडल आंदोलन ने इसे काफी हद तक शिथिल बना दिया। कांग्रेस उसमें नई जान नहीं फूंक सकी। नेतृत्व इसे नई चुनौतियों के मुताबिक ढालने में नाकाम रहा। इसका लाभ संघ परिवार को मिला। इसी के क्लाइमेक्स के रूप में आज हम राजनीति में मोदी-अमित शाह सिंड्रोम से मुकाबिल हैं।
आज सबकुछ बदल गया है। देश पर कॉरपोरेट पूंजी का आधिपत्य है। नेहरू युग में शुरू मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवाद 21वीं सदी के दूसरे दशक में खत्म हो चुके हैं। पूरे विश्व में दक्षिणपंथ उभार पर है, जिसके प्रतिनिधि मोदी और ट्रंप के साथ फ्रांस, तुर्की, रूस और यहां तक कि चीन के राष्ट्रपति हैं। इस परिवेश में कांग्रेस नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती विचारधारा के साथ संगठन को धरातल पर पुनर्जीवित करने, परंपरागत आधार को फिर से जोड़ने और युवा वर्ग की महत्वाकांक्षाओं का जोरदार ढंग से प्रतिनिधित्व करने की है।
मैं यहां शिद्दत से कहना चाहूंगा कि पदमुक्त होने के बाद भी राहुल को लोक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहिए। वे कांग्रेस के स्वतंत्र सिपाही के नाते संगठन को जन-जन के साथ जोड़ने का अभियान चलाएं। मेरा मत है कि राहुल और उनके युवा साथी अरुणाचल के ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग या पूर्वोत्तर की ही किसी अन्य जगह से पदयात्रा शुरू करें। वहां से असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचें। लोगों के बीच सर्वे कराएं, उनकी समस्याएं उठाएं। जनता को विश्वास में लें। सिर्फ मोदी-शाह को गाली देने और कोसते रहने से काम नहीं चलेगा।
इसके साथ ही संविधान का एक गुटखा तैयार कर जनता में वितरित करें, जिसमें संविधान की मूलभूत प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, लोकतंत्र, सूचना, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा का अधिकार जैसी जमीनी बातें शामिल हों। इस पदयात्रा का मूल मकसद जनता को लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्र के प्रति सचेत करना होना चाहिए। यह नए किस्म का जन-जागरण अभियान होगा। महात्मा गांधी ने भी राजनीति में आने से पहले भारत यात्रा की थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर से यात्रा नया अध्याय लिख सकती है। वे अब तक दक्षिण भारत को ही जोड़ते रहे हैं।
जहां तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद का सवाल है तो मेरे मत में उसका अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो आक्रामक रहे, समाज के हाशिए के वर्गों का प्रतिनिधित्व करे, साफ-सुथरा चरित्र हो, उसे संसद का अच्छा अनुभव होना चाहिए, हिंदी-अंग्रेजी के साथ किसी प्रादेशिक भाषा पर अच्छा अधिकार हो। वह मुलायम तबीयत का न हो।
पार्टी में दो कार्यकारी अध्यक्ष हों। एक युवा और दूसरा अल्पसंख्यक समाज से। नए महासचिव भी इसी तरह चुने जाएं। युवा वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। ये नेता समाज से जुड़े हों। राजीव गांधी ने कभी राज्य और जिला कोऑर्डिनेटर की परंपरा शुरू की थी। इसे दोबारा शुरू करना चाहिए। कांग्रेस विचारधारा की ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं।
देश की तमाम लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी, संविधान-प्रेमी, समाजवादी, वामपंथी शक्तियों का एकमात्र मकसद होना चाहिए संविधान की रक्षा। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के मोह से बचे क्योंकि यह संघ परिवार का विशेष अखाड़ा है। उसके दांव-पेच के सामने कांग्रेस टिकेगी नहीं। कांग्रेस नव-धर्मनिरपेक्ष और नव-बहुतलावादी पथ पर चले। भाजपा की अनुचर न दिखे। वह आक्रामक लेकिन रचनात्मक भूमिका निभाए।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस के जानकार हैं)