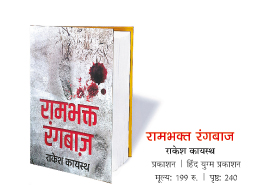राकेश कायस्थ का उपन्यास ‘रामभक्त रंगबाज’ बहुत साहस और संजीदगी से ऐसे सवाल उठाता है जिन पर बोलना इस सांप्रदायिक समय में लगभग गुनाह बना दिया गया है। उपन्यास याद दिलाता है कि आज नफरत के जो छोटे-बड़े पौधे पर्यावरण को जहरीला बना रहे हैं, उनको हवा-पानी मुहैया कराने का काम किन तत्वों और ताकतों ने किया है।
उपन्यास पर पिछले चार दशकों की छाया है, लेकिन मूल कथा साल नब्बे के एक महीने की है। उपन्यास के केंद्र में एक रामभक्त मुस्लिम किरदार है जो कपड़े सिलने की दुकान चलाता है। यह पुराने मोहल्ले का ऐंठा हुआ रंगबाज भी है, जिसकी चुटीली टिप्पणियां सबको घायल करती चलती हैं। धर्म की उसकी जानकारी के आगे खोखली धार्मिकता और खूंखार सांप्रदायिकता दोनों हारती रहती हैं।
कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब पूरे देश और शहर की तरह मोहल्ले में भी राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की लहर चल रही है। सबको लगता है कि मंदिर तो बिल्कुल बनकर रहेगा। इधर रामभक्त रंगबाज के मोहल्ले में अचानक नोटिस चला आता है कि सबके घर टूटेंगे, क्योंकि वे नाजायज कब्जे वाली जमीन पर बने हैं। बाप-दादाओं के जमाने से वहां रह रहे अल्पसंख्यक लोगों की यह गली घबराहट और अंदेशे में डूब जाती है।
यह सबके इम्तिहान की घड़ी है। सांप्रदायिक मंसूबों के खिलाफ खड़े लोगों के भी, कानून के भी और संविधान के भी। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान रामभक्त के सामने है, जो हिंदुओं में भी संदिग्ध हो चुका है और मुसलमानों में भी।
क्या इस रामभक्त का भरोसा लौटता है? क्या लोगों के घर बच पाते हैं? क्या भारतीय संविधान और कानून अपने लोगों को यह गारंटी दे पाता है कि वे तमाम साजिशों के बावजूद उखाड़े नहीं जा सकेंगे? इनके जवाब उपन्यास में मिलेंगे, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि राकेश कायस्थ ने उन जलते हुए दिनों की कहानी कुछ इस तरह लिखी है कि उसमें समकालीन राजनीति और समाज के विद्रूप बड़ी आसानी से पढ़े जाते हैं।
वैसे, राकेश कहानी जहां शुरू करते हैं, वहीं छोड़ नहीं देते। वे उसे बिल्कुल वर्तमान तक लाते हैं। इस बिखरे हुए समय में भी पुरानी यादों का एक संसार है, पुराने रिश्तों की ख़ुशबू है और वह मजबूत साझेदारी है, जो तोड़े जाने के सारे प्रयत्नों के बाद बची रहती है। इस हिस्से में पाठकों की आंख नम होने का खतरा है।
खास बात यह है कि राकेश कायस्थ ने यह कहानी अपने शहर के जाने-पहचाने मोहल्ले के कई वास्तविक चरित्रों को उपन्यास में जगह देते हुए लिखी है। बहुत सारे लोग उन दिनों को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन राकेश ने यहां लेखकीय परिपक्वता दिखाई है। दरअसल, आम तौर पर लेखक यथार्थ को जस का तस रखने के मोह में कुछ इस तरह फंसे होते हैं कि वे भूल जाते हैं कि वे ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसे सार्वभौमिक भी होना है। कभी-कभी यथार्थ के इस चित्रण से वह कहानी लिख भी ली जाती है, लेकिन कोई कथाकार अपने लक्ष्यों तक तब पहुंचता है जब वह उस यथार्थ को एक आकार देने के लिए उसमें कल्पना का जरूरी अंश मिलाता है, चरित्रों और घटनाओं को जरूरत के हिसाब से आपस में फेंटता भी जाता है।
उपन्यास के शिल्प की एक खासियत और है। राकेश मूलत: व्यंग्यकार हैं, इसलिए इस उपन्यास में स्थितियों के चित्रण में अपनी तरह का ‘विट’ है। इस ‘विट’ की वजह से उपन्यास पढ़ते हुए कभी-कभी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास ‘राग दरबारी’ की याद आ सकती है और कभी ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास ‘बारहमासी’ की। हिंदी में व्यंग्य तो बहुत लिखा जा रहा है लेकिन ऐसे व्यंग्य उपन्यास बहुत कम हैं जो अपनी मारक महीनी में समय और समाज का धागा खोल कर रख दें। ‘रामभक्त रंगबाज’ यह काम करता है।
हिंदी में सांप्रदायिकता को विषय बनाकर कई उपन्यास लिखे गए हैं। गीतांजलि श्री के ‘हमारा शहर उस बरस’ और दूधनाथ सिंह के ‘आखिरी कलाम’ की याद तत्काल आती है। राकेश ने भी हमारा शहर उस बरस ही लिखा है, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में।
उपन्यास में कई मार्मिक प्रसंग हैं, कई अर्थपूर्ण वाक्य भी। उपन्यास में नायक का बेटा अब देश छोड़ने को तैयार है। वह अपने ब्लॉग में लिखता है, "मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का मंदिर दो ढांचों को गिरा कर बनाया जा रहा है। पहला ढांचा अयोध्या में था और दूसरा दिल्ली में। पहला ढांचा मैंने देखा नहीं, उससे मेरा कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। लेकिन ‘दूसरे ढांचे’ पर मेरा वजूद टिका था। वह मेरी हिफाजत की गारंटी था। वही जब धराशायी हो रहा है तो मुझ जैसों के लिए क्या बचा?"
यह एक मार्मिक सवाल है- एक व्यक्ति का नहीं, पूरे मुल्क का। ‘प्रजातंत्र के पकौड़े’ के बाद यह राकेश कायस्थ का दूसरा उपन्यास है- बताता हुआ कि समकालीन यथार्थ की पकड़ और इतिहास की समझ उनमें पूरी है और इसे वे दिलचस्प किस्सागोई के साथ कथा में बुनने का हुनर भी जानते हैं।
रामभक्त रंगबाज
राकेश कायस्थ
प्रकाशन | हिंद युग्म प्रकाशन
मूल्य: 199 रु. | पृष्ठ: 240