ईश्वर ने कहा, ‘कामगार हों’, और कामगार तबके का जन्म हो गया। ईश्वर सबको एक आंख से देखता है, तो अपनी इंसाफ पसंदगी में उसने फिर कहा, ‘कामगारों के दुश्मन भी हों’, और इस तरह बनिये, महाजन, कॉरपोरेट और उनके रहनुमा भी पैदा हो गए। तब से लेकर अब तक दोनों पक्षों के बीच हास्यास्पद रूप से एक गैर-बराबर जंग मची हुई है।
वर्ग विभाजन से बनी इस दुनिया को इतने आसान ढंग से समझाते हुए विद्यार्थी चटर्जी जब सत्यजीत रे की महानगर से शुरू करके नौ अध्यायों के अंत में अनामिका हक्सर की फिल्माई पुरानी दिल्ली (घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूं) तक पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई सबाल्टर्न इतिहासकार समाज में बीते दशकों के दौरान बदली मजदूरों की जीवन-स्थिति पर क्रोनोलॉजी रच रहा हो।
वरिष्ठ सिने आलोचक विद्यार्थी चटर्जी की पुस्तक ‘डिस्पेयर ऐंड डिफायंस: द वर्कर इन इंडियन सिनेमा’ अपने दस अध्यायों में फिल्मों का एक महासिनेमा रचती है, जिसके किरदारों में सत्यजीत रे से लेकर मृणाल सेन, एमएस सथ्यू, सईद अख्तर मिर्जा, बुद्धदेब दासगुप्ता, मंगेश जोशी, सुमित्रा भावे, भाऊराव करहड़े और अनामिका हक्सर शामिल हैं।
इन फिल्मकारों की अलग-अलग दौर में बनाई फिल्मों के मुख्य किरदार यानी मजदूर इस पुस्तक का केंद्रीय विषय हैं। मजदूर भी वह नहीं जिसकी छवि यह शब्द सुनते ही दिमाग में आती हो। कोई बूढ़ा पेंशनर है जो झुग्गियों में रहता है। कोई बस का खलासी है तो कोई गराज मिस्त्री। एक आदमी लेथ मशीन पर काम करता है तो दूसरा मध्यवर्ग का कामगार है जो शहर में पैदा हुए अलगाव से परेशान है। यहां महिला श्रमिक हैं, तो ग्रामीण मजदूर भी हैं। और इन सब की परिणति ऐसे गरीब मजदूरों में भी होती है जो व्यवस्था में मजदूरी या कहें काम करने की बुनियादी अवधारणा पर ही सवाल उठा देते हैं।
विद्यार्थी चटर्जी पुस्तक के परिचय में बताते हैं कि भारतीय सिनेमा में मजदूरों के चित्रण में उनकी दिलचस्पी कैसे जगी। जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में रहते हुए उनकी पढ़ाई जिस अंग्रेजी स्कूल में हुई, वहां पहली बार उनकी जिज्ञासा जगी कि लोयोला स्कूल के सभागार में उन्हें जो फिल्में दिखाई जाती हैं उनमें मजदूर क्यों नहीं होते जबकि चारों ओर धुआं उगलती चिमनियां और कारखाने मौजूद थे। वे लिखते हैं, “मैं हमेशा इस बात पर अचरज करता था कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे पोंगा, पगार या नागा से मैं जुड़ क्यों नहीं पाता हूं। शनिवार को जो फिल्में दिखाई जाती हैं उनमें मजदूर वर्ग की कहानियां क्यों नहीं होती हैं?”

मृणाल सेन की फिल्म ओका ऊरी कथा का दृश्य
बाद में विद्यार्थी चटर्जी ने लगातार फिल्मों में श्रमिकों के जीवन के चित्रण पर लिखा। वे बताते हैं कि फिल्मकार सैकत भट्टाचार्य ने सबसे पहले इन लेखों को पुस्तकाकार करने का सुझाव उन्हें दिया। थीमा, कोलकाता द्वारा जमशेदपुर के सेलुलॉयड चैप्टर के साथ मिलकर प्रकाशित की गई चटर्जी की यह पुस्तक श्रमिक जीवन की विभिन्न छवियों को तो साथ लाती ही है, साथ में यह समझने में भी मदद करती है कि समाज में मजदूरों की स्थिति समय के साथ कैसे बदली है।
मसलन, जब वे एमएस सथ्यू की बनाई गरम हवा में आगरा के जूता श्रमिकों पर बात करते हैं, तो फिल्म के अंत को सकारात्मक बताते हुए लिखते हैं कि इस फिल्म ने न केवल मजदूर वर्ग की तमाम सच्चाइयों को पहचाना है बल्कि यह भी बताया है “कि इनसे पैदा होने वाली दिक्कतों का सामना सम्मान और साहस के साथ कैसे किया जा सकता है।” सईद मिर्जा की मोहन जोशी हाजिर हों तक दिखने वाला यह आत्मसम्मान और साहस बदलते हुए समय में कैसा विद्रूप हो जाएगा, वह अरविंद देसाई की अजीब दास्तान (सईद मिर्जा) में दिखता है जहां एक मध्यवर्गीय कामगार शहरी जीवन से उपजे अलगाव के चलते अपनी जान लेना चाहता है लेकिन उसे कायदे से खुदकुशी करना भी नहीं आता।
ऐसा लगता है कि लेखक सईद मिर्जा की फिल्मकारी से बहुत प्रभावित है लेकिन उनकी फिल्मों को वह उतने पन्ने नहीं दे पाया है जितनी जरूरत थी। मिर्जा की कम से कम चार फिल्मों को चटर्जी ने एक ही अध्याय में समेट लिया है। पुस्तक में हिंदी के अलावा बांग्ला और मराठी फिल्मों पर अध्याय हैं। मंगेश जोशी की फिल्म लेथ जोशी का जिक्र वर्तमान संदर्भों में बहुत मौजूं है जिसमें विजय जोशी को लोग लेथ जोशी के नाम से पुकारते हैं क्योंकि वह लेथ मशीन पर काम करता है। कैसे एक मजदूर का काम ही उसकी पहचान और संज्ञा बना दिया जाता है, यह फिल्म इस पर एक टिप्पणी है। उत्तराखंड में इकतालीस मजदूरों को बचाने वाले बारह मजदूरों को लगातार रैटहोल माइनर कहा जाना इस बात की पुष्टि करता है कि आज बरसों बाद भी काम ही मनुष्य की पहचान बना हुआ है और किसी को लेथ या अंग्रेजी में चूहे की तरह खोदने वाला कहने में सभ्य समाज की जबान नहीं कटती।
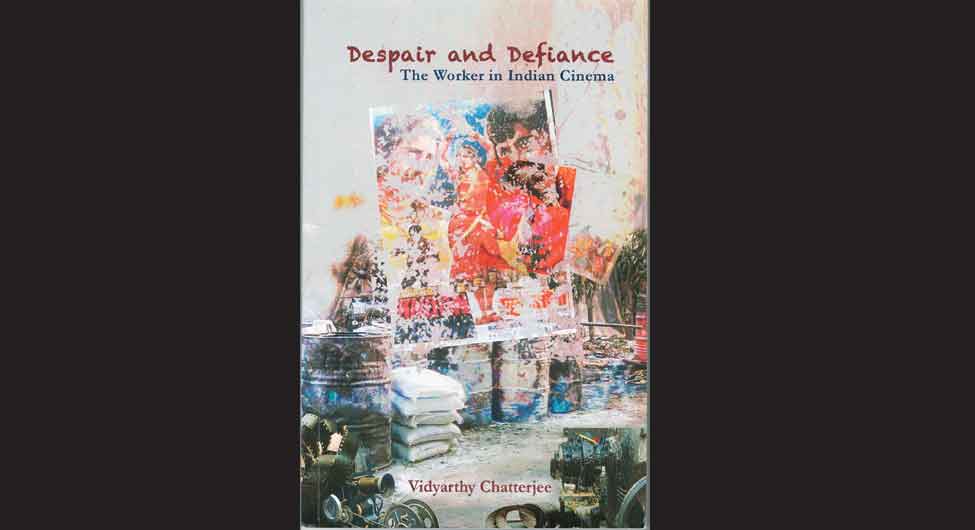
पुस्तक का आवरण
सुमित्रा भावे की एक कप चाय, भाऊराव करहड़े की ख्वाड़ा, मृणाल सेन की ओका ऊरी कथा और बुद्धदेब दासगुप्ता की दूरत्व पर किताब में अलग-अलग अध्याय सम्मिलित हैं। सभी पठनीय हैं और मजदूर जीवन की भिन्न छवियां दिखाते हैं। इनमें मृणाल सेन की ओका ऊरी कथा का जिक्र अलग से करना बहुत जरूरी है जहां सेन ने प्रेमचंद की कहानी 'कफन' को प्रेरणा बनाकर एक बुनियादी सवाल उठा दिया है। 1977 में तेलुगु में बनी यह फिल्म सेन की सबसे कम चर्चित कृति है।
सेन ने यहां 'काम' की व्यर्थता को रेखांकित किया है, खासकर ऐसे काम को जो मालिक का खजाना भरने के काम आता है लेकिन कामगार को लगातार वंचित करते जाता है। फिल्म में मौजूद राजनीति भारतीय सिनेमा की ठस कथानक परंपरा से एक ऐतिहासिक विक्षेप है, जहां शोषित नायक विरोध या विद्रोह नहीं करता, न ही आत्मसमर्पण करता है या आत्मघात की सोचता है, बल्कि काम की बुनियादी अवधारणा पर सवाल उठाते हुए खुद को अपने ही हाथों वंचना के लिए अभिशप्त कर लेता है और परंपरागत सोच के हिसाब से अनैतिक हो जाता है। वर्ग समाज के भीतर यह एक ऐसा विद्रोह है जो भारत में ऊपर से दिखाई नहीं देता, लिहाजा अपने काल से बहुत आगे की चीज बन जाता है।
इस किस्म के कामगार का अपने काम के प्रति संवेदनहीन या संज्ञाशून्य हो जाना एक और परिणति है। यह वह मोड़ है जहां मजदूर को अपने वर्गीय हितों का ही खयाल नहीं रह जाता है। गोया वह वर्गीय चेतना से ऊपर उठकर अपने हित के खिलाफ फैसले ले रहा हो। आजकल इस विषय पर काफी काम हो रहा है। विवेक छिब्बर ने “द क्लास मैट्रिक्स” में इस विषय पर काफी विचार किया है कि आखिर आज का मजदूर अपनी वर्ग चेतना से अलग होकर क्यों जी रहा है और संगठित क्यों नहीं हो पा रहा। पुरानी दिल्ली की गलियों में सात साल तक आम जीवन का अनुभव लेने के बाद अनामिका हक्सर की बनाई फिल्म घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूं ऐसे ही आधुनिक मजदूरों की बात करती है। चटर्जी की पुस्तक भी इसी पर केंद्रित आलेख से समाप्त होती है, जैसे यह मजदूर और उनके मालिकान के बीच चल रहे सतत संघर्ष की परिणति हो।
विद्यार्थी चटर्जी इन्हें “आवारा सर्वहारा” कहते हैं। वे लिखते हैं, “इतिहास (पढ़ें बाजार) की गति ऐसी रही है कि एक ‘सामान्य’ कामगार अब गायब हो चुका है। आज का ‘असामान्य’ कामगार वह है जो अपना पेट चलाने के लिए दूसरे की जेब काटने को बाध्य है। इतिहास ने ही उसे अपना काम चुनने का हक दिया है। धरती के ऐसे तमाम अभिशप्त किसी जमाने के मशहूर शाहजहांनाबाद के सड़ांध भरे अंधेरे सीवरों में चूहों की तरह रहने को मजबूर हैं।”
दिल्ली और यूपी के जिन रैटहोल माइनर मजदूरों का जश्न आज देश मना रहा है, उसकी तुलना विद्यार्थी चटर्जी ने बहुत उपयुक्त ही “सड़ांध भरे अंधेरे सीवरों में चूहों” से की है। यह संयोग नहीं है। मजदूर साहित्य के इतिहास में फ्रांस से लेकर रूस तक शहरी मजदूरों की तुलना चूहे से की जाती रही है। इस लिहाज से रैटहोल शब्द अपने आप में अपमानजनक है।
चटर्जी लिखते हैं, “इस फिल्म में जितने किस्म के आवारा सर्वहारा दिखाए गए हैं, वे अपने उत्पीड़कों के प्रति अवमानना का भाव रखते हुए उसके बरअक्स उम्मीद और कॉमरेडशिप की एक संस्कृति निर्मित करते हैं और चैपलिन की प्रसिद्ध उक्ति की याद दिलाते हैं कि, 'इस धूर्त जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है- हमारे कष्ट भी नहीं!’”
सत्तर के दशक के अरविंद देसाई से लेकर आज के आवारा सर्वहारा पतरू और छदामी तक पहुंच चुकी भारतीय सिने चेतना इस बात को रेखांकित करती है कि लगातार नाउम्मीद होती जाती दुनिया में उम्मीद, और बस उम्मीद ही एक कामगार की घड़ी को टिकटिक करते हुए चलने की प्रेरणा दे सकती है। शायद यही वह उम्मीद थी जिसने सत्रह दिनों तक उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाया। यही वह उम्मीद थी जिसके चलते उनके बारह भाई उन्हें बिना किसी अपेक्षा के बचाने के लिए भीतर गए और कामयाब लौटे।
डिस्पेयर ऐंड डिफायंस
विद्यार्थी चटर्जी
प्रकाशक | थीमा
पृष्ठः 96 | मूल्यः 250








