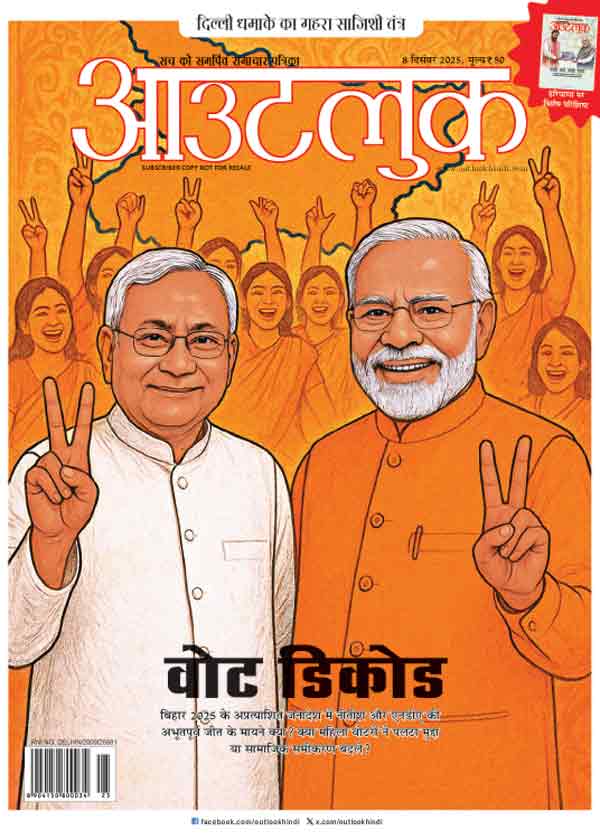शहरों की चमचमाती रौशनी के पीछे एक स्याह साया है, जो हर शाम ढलते ही किसी खिड़की में उदासी बनकर टिक जाता है। यह साया किसी बुज़ुर्ग का है जो रिटायरमेंट के बाद, जीवन की उस अवस्था में पहुँचा है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा संवाद, साथ और सम्मान की ज़रूरत होती है। लेकिन इन महानगरों में, जहाँ वक़्त की क़ीमत दौड़ से तय होती है, वहाँ उम्रदराज़ लोग अक्सर एक कोने में छूट जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद का अकेलापन केवल एक भावनात्मक पीड़ा नहीं, बल्कि एक गहराता हुआ सामाजिक संकट है, जिसमें बुज़ुर्गों को उनका ही घर धीरे-धीरे एक ऐसी जेल में बदलता दिखता है, जहाँ दीवारें बोलती नहीं, और लोग सुनते नहीं।
संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के उदय ने बुज़ुर्गों के जीवन में गहरी दरारें डाल दी हैं। एक समय था जब दादी-नानी की कहानियाँ केवल बच्चों के मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि रिश्तों की जड़ों को सींचने वाली संवेदनाएँ थीं। अब वही बुज़ुर्ग एक कमरे में टीवी के सामने अकेले बैठते हैं, जिन्हें केवल दवाइयों की समय-सीमा याद रखी जाती है, बाक़ी किसी संवाद की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। शहरी जीवन की आपाधापी में बच्चे करियर, ट्रैफिक और प्रतिस्पर्धा में इतने उलझ गए हैं कि उन्हें अपने माता-पिता की आँखों में उगते सन्नाटे दिखाई ही नहीं देते। यह अकेलापन धीरे-धीरे अवसाद में बदलता है, फिर चुप्पी में, और अंततः — कभी-कभी — एक अनकहे अंत में।
भारत जैसे देश में, जहाँ ‘मातृ-पितृ देवो भव’ जैसी पंक्तियाँ संस्कृति का हिस्सा रही हैं, वहाँ रिटायरमेंट के बाद बुज़ुर्गों के जीवन की विडंबना और भी कटु हो जाती है। शहरों में बुज़ुर्गों के लिए न सार्वजनिक स्थल हैं, न सामुदायिक संवाद के मंच, और न ही कोई ऐसा तंत्र जो उन्हें जीवन के इस नए चरण में सक्रियता और सम्मान के साथ जीने का अवसर दे। उनकी सारी भूमिका केवल घर की रखवाली, दवाइयों की सूची और कभी-कभार बच्चों की देखभाल तक सीमित रह जाती है। धीरे-धीरे वे अपने ही घर में ‘अतिरिक्त’ महसूस करने लगते हैं। कुछ बुज़ुर्ग स्वयं वृद्धाश्रम की शरण लेते हैं, क्योंकि वहाँ कम से कम कोई उनकी बात तो सुनता है।
मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक गंभीर चुनौती है। बुज़ुर्गों में डिप्रेशन, चिंता, भूलने की बीमारी (Dementia), और नींद की समस्याएँ आम होती जा रही हैं। खासकर रिटायरमेंट के बाद, जब उनका दिनचर्या, पहचान और सामाजिक भूमिका अचानक ख़त्म हो जाती है, तो वे स्वयं को व्यर्थ महसूस करने लगते हैं। यह स्थिति केवल भावनात्मक नहीं, शारीरिक रूप से भी उन्हें कमजोर बनाती है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि जो बुज़ुर्ग सामाजिक रूप से कटे रहते हैं, उनमें बीमारियाँ अधिक होती हैं और उनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है।
इस अकेलेपन की रोकथाम के लिए सबसे पहले समाज को यह समझना होगा कि बुज़ुर्ग ‘निष्क्रिय’ नहीं होते — उन्हें केवल एक नई भूमिका, एक नई पहचान की आवश्यकता होती है। रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी, अगर सही रूप से पुनर्गठित की जाए, तो यह ‘आत्म-संवर्धन’ और ‘सामाजिक मार्गदर्शन’ का काल बन सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि परिवार अपने बुज़ुर्गों को सिर्फ सहानुभूति से नहीं, बल्कि सहभागिता से देखें। उन्हें घर के निर्णयों में शामिल करें, उनके अनुभव को सम्मान दें, और उन्हें संवाद का अवसर दें।
समाज स्तर पर बुज़ुर्गों के लिए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण होना चाहिए जहाँ वे अपनी रुचियों, जैसे संगीत, लेखन, बागवानी या योग के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ सकें। ऐसे समूह बुज़ुर्गों को उद्देश्य देते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त करते हैं। कुछ स्थानों पर ‘इंटरजनरेशनल संवाद’ की पहल की जा रही है, जहाँ बुज़ुर्ग स्कूल या कॉलेज जाकर अपने अनुभव साझा करते हैं। यह मॉडल बच्चों और बुज़ुर्गों के बीच संवाद का सेतु बनाता है।
सरकार की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आज भारत में ‘राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति’ (National Policy for Senior Citizens) है, लेकिन यह ज़मीनी स्तर पर बहुत सीमित प्रभाव छोड़ पाई है। सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक शहर में बुज़ुर्गों के लिए ‘डे-केयर सेंटर्स’, ‘सामाजिक सहभागिता केंद्र’, और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्रों की स्थापना करे। बुज़ुर्गों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, ट्रांसपोर्ट में रियायत जैसे उपाय तो ज़रूरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है — उन्हें फिर से ‘समाज का हिस्सा’ महसूस कराना।
दूसरे देशों के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जापान में बुज़ुर्गों के लिए ‘इकिगाई’ की अवधारणा है, जिसमें उन्हें जीवन के किसी उद्देश्य से जोड़ा जाता है — चाहे वह सामुदायिक सेवा हो, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या स्थानीय स्वच्छता अभियानों में भाग लेना। स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में बुज़ुर्गों के लिए रिटायरमेंट के बाद ‘सक्रिय नागरिकता’ (active citizenship) कार्यक्रम चलते हैं, जिनमें वे सामुदायिक निर्णयों में भाग लेते हैं और स्थानीय सरकार के साथ सहयोग करते हैं। कनाडा में कई बुज़ुर्गों को पार्ट-टाइम वॉलंटियरिंग या प्रोफेशनल मेंटरशिप में शामिल किया जाता है। ये सारे मॉडल दिखाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है — बशर्ते समाज और सरकार दोनों इसकी ज़िम्मेदारी लें।
शायद अब समय आ गया है कि हम बुज़ुर्गों को किसी जिम्मेदारी से मुक्त व्यक्ति नहीं, बल्कि स्मृतियों और अनुभवों की जीवित पुस्तक मानें — जिसे पढ़ने, सुनने और समझने की आवश्यकता है। वे कोई बोझ नहीं हैं, बल्कि हमारे भविष्य की नींव रखने वाले हाथ हैं। अगर हम उनकी ख़ामोशी को नहीं सुन पाए, उनके अकेलेपन को नहीं देख पाए, तो यह हमारी संवेदनशीलता की नहीं, हमारी सभ्यता की हार होगी। जिस समाज की नींव अपने बुज़ुर्गों को अकेला छोड़ने पर टिकी हो, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए यदि हमें भविष्य सुरक्षित करना है, तो हमें अपने अतीत — अपने बुज़ुर्गों — को अपनाना ही होगा। यह सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि उस मानवता की पहचान है, जिसके बिना कोई भी समाज समाज नहीं कहलाता।