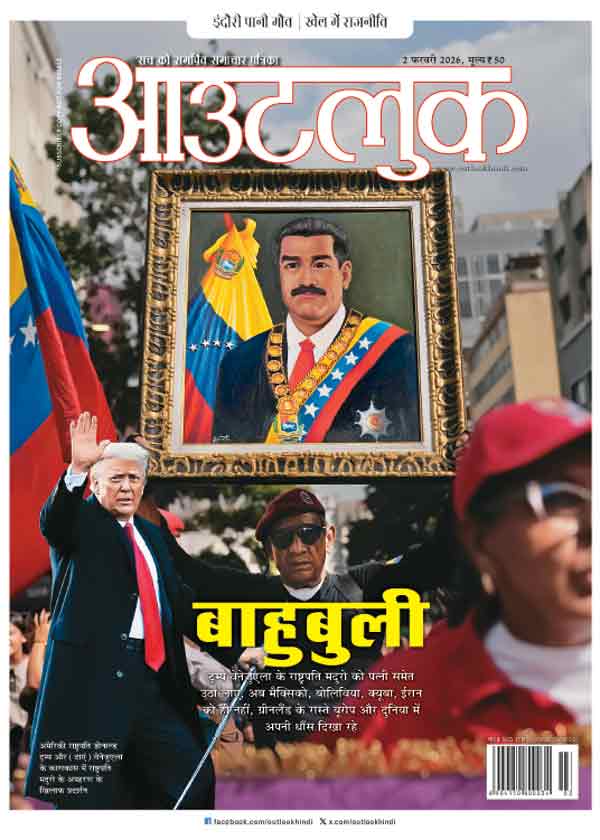भारतीय लोकतंत्र में चुनावों के दौरान जनता को लुभाने के लिए की जाने वाली घोषणाएँ अब एक परंपरा सी बन गई हैं। हर चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने-अपने घोषणापत्र में मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा देते हैं—कोई कहता है कि हम महिलाओं को हर महीने ₹1000 देंगे, कोई युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करता है, तो कोई फ्री बिजली, पानी, बस यात्रा, राशन, गैस सिलेंडर या स्कूटी देने की बात करता है। इन सबका एकमात्र उद्देश्य होता है मतदाताओं को प्रभावित करना और वोट बटोरना। लोकतंत्र में वादों का महत्व है, लेकिन जब ये वादे मुफ्तखोरी की संस्कृति को जन्म दें और सरकार की आर्थिक स्थिति पर बोझ बनें, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। देश में लोक-लुभावन वादों का चलन कोई नया नहीं है, लेकिन 2011 के बाद से जब चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं का असर स्पष्ट दिखाई देने लगा, तब से इसे ‘रेवड़ियों की राजनीति’ कहा जाने लगा। इस पर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह देश की आर्थिक रीढ़ को कमजोर करने वाला चलन है, जिससे बचा जाना चाहिए।
तमिलनाडु वह राज्य रहा जहाँ इस संस्कृति की नींव पड़ी। 2006 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने चुनाव जीतने के बाद मतदाताओं को रंगीन टीवी बाँटे। इसके बाद अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने अपने शासन में मिक्सी, ग्राइंडर और फ्री लैपटॉप बाँटने का अभियान चलाया। धीरे-धीरे यह चलन उत्तर भारत की राजनीति में भी प्रवेश कर गया। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बिजली-पानी मुफ्त करने, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा देने, मोहल्ला क्लीनिक जैसी योजनाओं को मुख्य मुद्दा बनाया और बहुमत से सत्ता में लौट आई। इसके बाद पंजाब में भी आप ने यही रणनीति अपनाई और सफल रही। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी अब मुफ्त योजनाएँ किसी भी चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। गुजरात में 2022 के चुनावों में कांग्रेस और आप, दोनों ने महिलाओं को हर महीने ₹1000 देने का वादा किया। सवाल यह है कि क्या इससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है या केवल मतदाता को लुभाया जाता है? मतदाताओं के लिए यह तय करना कठिन हो गया है कि कौन-सी योजना कल्याणकारी है और कौन-सी केवल राजनीतिक लालच।
अगर इन योजनाओं के असर को जनता के जीवन पर देखें तो यह बहस दो हिस्सों में बँट जाती है। एक पक्ष कहता है कि गरीबों और वंचितों के लिए ये योजनाएँ आवश्यक हैं, क्योंकि वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें राहत दे। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली सरकार द्वारा बिजली और पानी पर दी गई सब्सिडी से लगभग 80% उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। इसी तरह केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले। लेकिन दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि हर चुनाव में केवल मुफ्त की वस्तुएँ देकर वोट बटोरे जाएँगे, तो जनता अपनी समस्याओं की गंभीरता को समझना छोड़ देगी और एक उपभोक्ता भर बनकर रह जाएगी। साथ ही यह आदत आत्मनिर्भरता की भावना को भी कमजोर करती है। जब हर चीज़ सरकार से मुफ्त मिलने लगे, तो मेहनत, उद्यम और स्वयं प्रयास की भावना समाज में घटने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए खतरनाक मानी जाती है।
मुफ्त योजनाओं का असर केवल समाज पर ही नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा पड़ता है। किसी भी योजना के लिए बजट की आवश्यकता होती है, और अगर राज्य सरकारें अपने राजस्व से अधिक मुफ्त योजनाओं में खर्च करेंगी, तो उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का कुल ऋण जीएसडीपी (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद) के 40% से भी अधिक हो चुका है, जो चिंताजनक है। पंजाब में 2023 तक राज्य सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था, जबकि राज्य की आमदनी उसका आधा भी नहीं थी। यह स्थिति केवल जनता को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आर्थिक बोझ में धकेल देती है। जब सरकारें मुफ्त की घोषणाएँ कर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर देती हैं, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों में निवेश कम हो जाता है। भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भी इस पर चिंता जताई है कि कुछ राज्य अपने बजट का 40% तक मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। यह राजकोषीय अनुशासन के विरुद्ध है और दीर्घकालिक विकास के लिए खतरनाक संकेत है।
इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए 2022 में कहा था कि मुफ्त रेवड़ियों की संस्कृति लोकतंत्र को क्षति पहुँचा सकती है और इसके लिए स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस पर दिशानिर्देश जारी करने चाहिए ताकि मतदाताओं को भ्रमित करने वाली घोषणाओं पर लगाम लग सके। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। आयोग का तर्क है कि वह केवल आदर्श आचार संहिता को देख सकता है, और वादों पर रोक लगाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके चलते राजनीतिक दलों को पूरी छूट मिल जाती है कि वे जो चाहें, वादा कर सकते हैं। चुनाव आयोग की इस निष्क्रियता को लेकर जनहित याचिकाएँ भी दाखिल हुईं, परन्तु अब तक कोई सख्त नीति सामने नहीं आई है। इसके साथ ही, मुख्यधारा की मीडिया भी इस विषय पर बहुत अधिक सवाल नहीं उठाती, क्योंकि मुफ्त योजनाएँ जनता के बीच लोकप्रिय होती हैं और विरोध करने वाले राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहते।
इस पूरी बहस का निष्कर्ष यही है कि जनता को मुफ्त चीज़ों की नहीं, बल्कि सस्ती, टिकाऊ और न्यायोचित योजनाओं की आवश्यकता है। कल्याणकारी योजनाओं में और लोकलुभावन वादों में फर्क किया जाना चाहिए। अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवेलपमेंट और रोजगार पर निवेश करे तो जनता खुद सक्षम बन सकती है। लंबे समय तक मुफ्त बाँटना न तो विकास की गारंटी है और न ही गरीबी मिटाने का तरीका। इसके साथ ही यह जरूरी है कि राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में वित्तीय स्रोतों का स्पष्ट उल्लेख करें, जिससे पता चले कि वे पैसे कहाँ से लाएँगे। अंततः, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। केवल मुफ्त चीज़ों के लालच में वोट देना किसी भी देश की लोकतांत्रिक चेतना को कमजोर करता है। अगर हम देश के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत, और समाज को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो हमें रेवड़ियों की राजनीति पर पुनर्विचार करना ही होगा।
(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं। विचार निजी हैं)

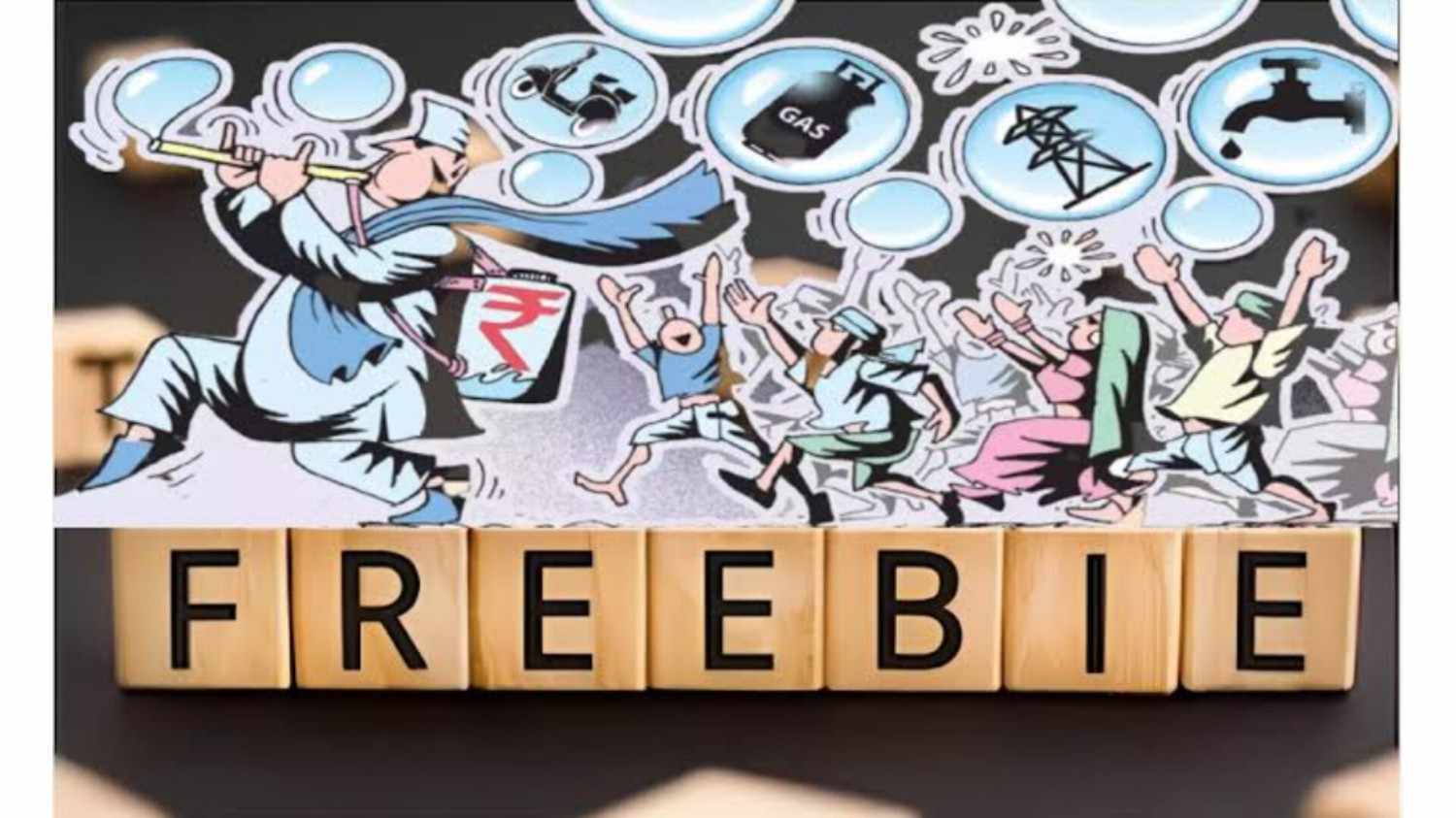


.jpg)