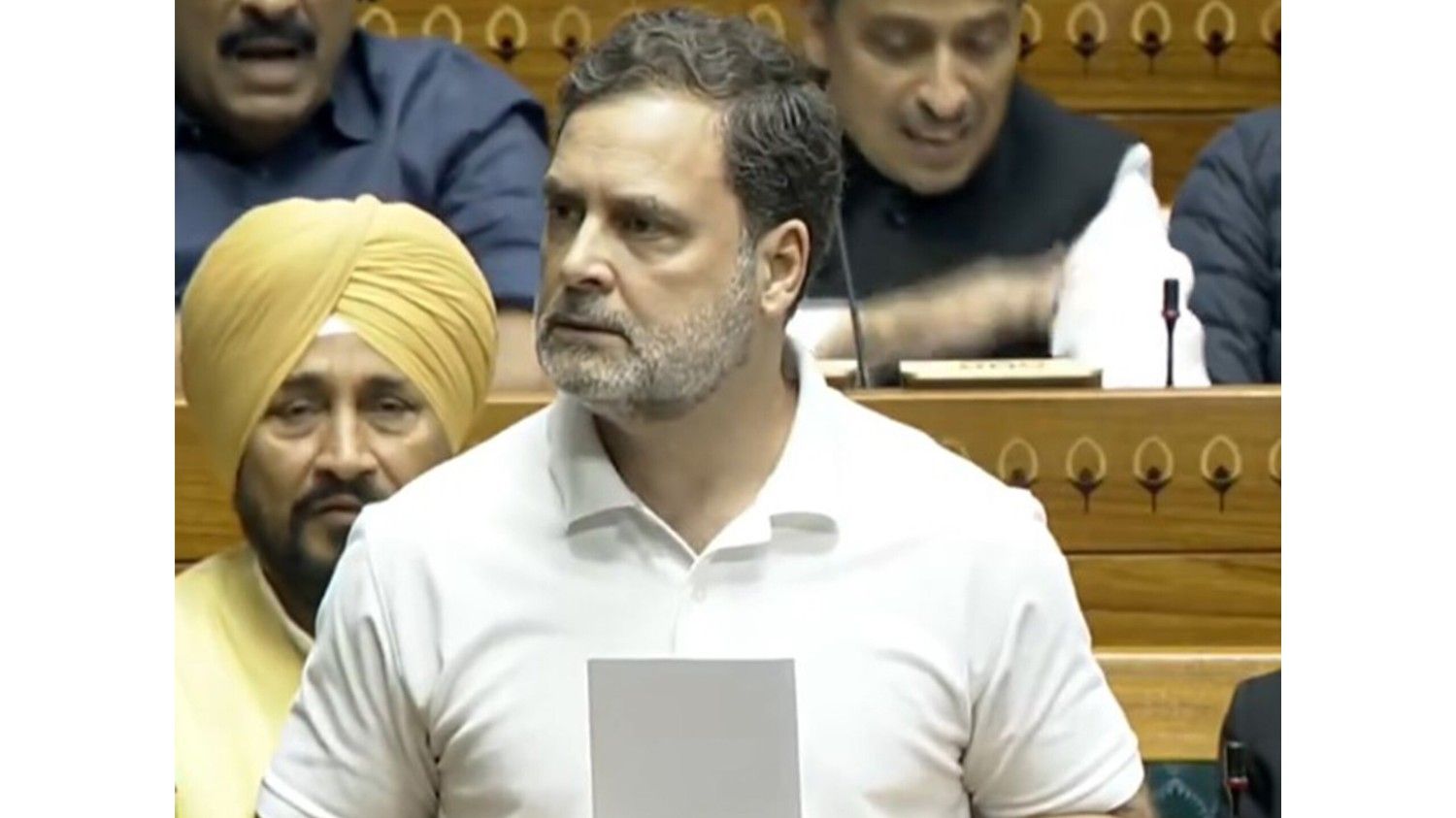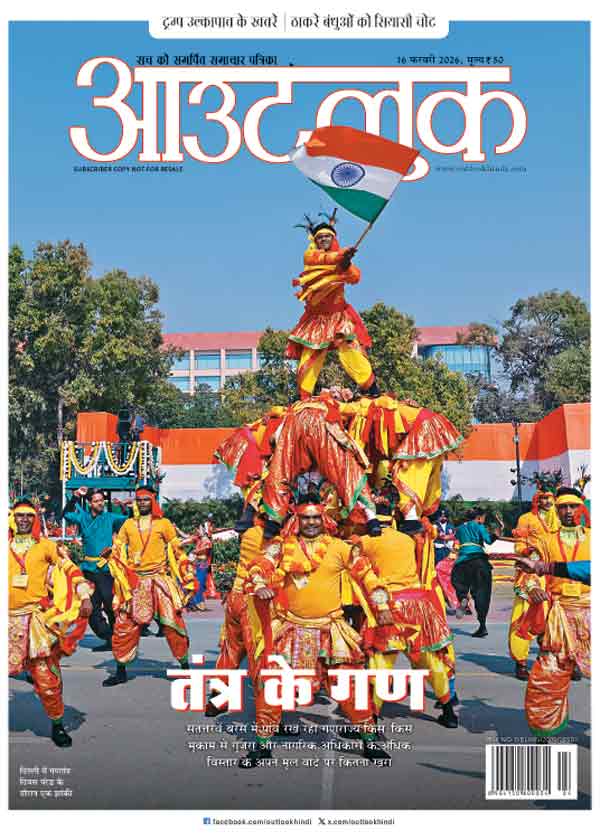वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) सिर्फ उस सीमा तक स्वागत योग्य है, जहां तक यह कोविड-19 के सामाजिक खतरे के कारण गरीब परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा। इसमें टैक्स से जुड़ी राहतें भी हैं। आरबीआइ ने भी ब्याज दरें घटाने के साथ बैंकों को टर्म लोन की किस्तें स्थगित करने की अनुमति दी है। सरकार और इसकी संस्थाओं की इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। वित्त मंत्री की 26 मार्च 2020 की घोषणा के अनुसार, भविष्य में निश्चित ही ऐसे और उपाय किए जाएंगे। यह और भी उपयुक्त होता अगर सरकार ने टैक्स, गरीबों, औपचारिक और अनौपचारिक कर्मियों, उद्योगों और व्यापार खासकर एमएसएमई और स्वास्थ्य संसाधनों के लिए एक ही बार में व्यापक उपाय किए होते, क्योंकि ये सभी एक-दूसरे से जुड़े हैं। आरबीआइ भी इसके समानांतर वित्तीय उपाय पेश कर सकता था।
पीरियॉडिक लेबर फोर्स के 2017-18 के सर्वे अनुसार, गैर कृषि क्षेत्र में नियमित मजदूरी/वेतन वाले 72.8% श्रमिकों के पास औपचारिक रोजगार कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इनमें से लगभग 53% को सवैतनिक छुट्टी नहीं मिलती और इनमें से 48% के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। यह जान लेना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लगभग 85% (4.77 करोड़ श्रमिक), नॉन-मैन्युफैक्चरिंग के लगभग 95% (इसमें भवन निर्माण की हिस्सेदारी लगभग 93% है, जिनमें ज्यादातर अनौपचारिक श्रमिक हैं) और सेवा क्षेत्र के लगभग 79% श्रमिक अनौपचारिक हैं। शहरों में भवन निर्माण क्षेत्र के 70.4% श्रमिक अनियमित हैं। संगठित फैक्टरी क्षेत्र में कुल कामगारों में से आधिकारिक रूप से 35% ठेका श्रमिक हैं।
इस तरह, हम देख सकते हैं कि अनौपचारिकता व्यापक पैमाने पर है और कुल गैर-कृषि श्रमिकों में से बड़ी संख्या में ऐसे हैं, जिनके पास किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। शहरों में फेरी लगाने वाले अनौपचारिक कामगारों का एक और बड़ा वर्ग है। इसके अलावा लाखों लोग ऐसे हैं जो महामारी के जोखिम, राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन और क्षेत्रीय सीमाओं और प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हैं। विडंबना यह है कि ये वे लोग हैं जिन्हें काम और आय की जरूरत है, इसलिए इन पर वायरस का खतरा अधिक है। हालांकि, केंद्र और कई राज्य सरकारों ने निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से अपने कामगारों को नौकरी से न निकालने और उनका वेतन नहीं काटने की अपील की है, लेकिन यह नैतिक आग्रह मात्र है। गैर कृषि क्षेत्र के बहुत कम श्रमिकों को इसका लाभ मिल पाएगा।
वित्त मंत्री ने जो राहत पैकेज की घोषणा की है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो क्षेत्रीय रूप से पसंद की जाने वाली दाल शामिल है। सरकार का अनुमान है कि इससे 80 करोड़ लोगों को मदद मिलेगी। यह दुनिया में संभवतः अपनी तरह की सबसे साहसिक और सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा है, लेकिन इसकी सफलता इसे लागू करने में समाहित है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली नहीं है। इस उपाय में अनौपचारिक कामगार भी शामिल होंगे, क्योंकि उनमें ज्यादातर गरीब हैं और खाद्य सुरक्षा के दायरे में आते हैं।
पीएमजीकेपी में बिना किसी आधार के कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों की नौकरी जाने का खतरा है जो 100 कर्मचारियों से कम को रोजगार देने वाले संस्थानों में काम करते हैं और जिनका वेतन 15,000 रुपये महीना तक है। इसी तर्क के आधार पर इसमें कर्मचारी (15,000 से कम आय वाले) और नियोक्ता दोनों के हिस्से के ईपीएफ अंशदान का भुगतान करने का प्रस्ताव है। यानी सरकार तीन महीने तक उनके वेतन के 24% के बराबर राशि उनके पीएफ खाते में जमा कराएगी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। सरकार का दावा है कि इस उपाय से कामगारों की नौकरी बचाने में मदद मिलेगी। सरकार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के चैप्टर V-बी और ईपीएफ एक्ट 1952 के बीच स्पष्ट रूप से उलझ गई है। पहला कानून 99 से अधिक कर्मचारियों वाली केवल पंजीकृत फैक्टरियों, खदानों और बागानों में लगातार एक साल काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है। इन फर्मों को श्रमिकों की छंटनी और उन्हें निकालने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। ईपीएफ एक्ट के तहत 15 हजार रुपये महीने से कम आय वाले कर्मी नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के अंशदान के लिए पात्र होते हैं। अगर सरकार 15 हजार रुपये से कम आय और 100 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों में ईपीएफ अंशदान का भुगतान करती है, तो नौकरी जाने के खतरे से मिलने वाली सुरक्षा बहुत मामूली होगी।
छठवें आर्थिक जनगणना, 2016 के अनुसार 4.53 करोड़ प्रतिष्ठानों में से सिर्फ 0.08 फीसदी में 100 या अधिक कर्मचारी हैं। इन प्रतिष्ठानों में से 99.35 फीसदी में तो काम करने वालों की संख्या 20 से भी कम है। सरकार का तर्क है कि अगर कॉस्ट टू कंपनी (सीटीसी), जिसमें नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला ईपीएफ अंशदान शामिल है, सरकारी छूट के कारण घटती है तो 100 लोगों से कम को रोजगार देने वाले नियोक्ता (जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के दायरे से बाहर होंगे) कर्मचारियों की छंटनी पर कम जोर देंगे। यहां महत्वपूर्ण है कि सरकार यह मान रही है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के चैप्टर V-बी के तहत नहीं आने वाले कामगारों के सामने ‘नौकरी जाने का खतरा है’। इसलिए यह उपाय भ्रमित करता है। इसके लिए रखी गई 5,000 करोड़ रुपये की रकम बहुत ज्यादा हो सकती है, हालांकि संभव है कि सरकार ने अपने पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ऐसा किया हो। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए कोलेटरल फ्री लोन की सीमा बढ़ाना एक आकर्षक उपाय है। लेकिन अभी यह निश्चित नहीं है कि आर्थिक सुस्ती को देखते हुए वे कर्ज लेना चाहेंगे। ब्याज में छूट के साथ ही कर्ज की सीमा में बढ़ोतरी उन्हें आर्थिक सुस्ती के बावजूद कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन इसे सही मायने में राहत उपाय नहीं कहा जा सकता है।
पीएफ खाताधारक अपने ईपीएफ एकाउंट से शादी, शिक्षा, बीमारी, घर खरीदने और बेरोजगारी (हर मद में रकम निकालने की सीमा अलग है) की अवस्था में सेवानिवृत्ति से पहले या सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब एडवांस ले सकते हैं। अब सरकार ने महामारी को भी एक कारण के रूप में जोड़ दिया है। ईपीएफ अंशधारक अपने खाते में जमा कुल राशि का 75% या तीन महीने के वेतन के बराबर, दोनों में जो भी कम हो, बतौर एडवांस ले सकते हैं। यह रकम उन्हें दोबारा जमा नहीं करनी पड़ेगी। यह कामगारों के अदूरदर्शी कदम को प्रोत्साहित करता है। बल्कि सरकार तो हाल के कुछ वर्षों में इसे प्रोत्साहित करती रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की नौकरी बचाना चाहती है तो उसे नियोक्ताओं, खासकर एमएसएमई को वेतन की मदद या ले-ऑफ सब्सिडी देनी चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम वेतन से कम आय वाले कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पूरक राशि देनी चाहिए।
गैर-कृषि क्षेत्र में काम करने वाले अनेक श्रमिकों को इस राहत पैकेज का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें ठेका कर्मचारी, आकस्मिक और अस्थायी श्रमिक और सालों से प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं, जिनका ईपीएफ खाता होने की संभावना बेहद कम है। अगर उनके ईपीएफ खाते हुए भी तो उनमें रकम बहुत कम होगी। इसलिए बिना ईपीएफ/ईएसआई कवर वाले कामगारों के लिए सरकार को टेम्पररी यूनिवर्सल नॉन-फार्म अनएंप्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम (अस्थायी सार्वभौमिक गैर-कृषि बेरोजगारी भत्ता योजना) तैयार करनी चाहिए थी, जिसके लिए धन का इंतजाम टैक्स से होना चाहिए। ईपीएफ/ईएसआइ कवरेज वालों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना लानी चाहिए थी। इसके साथ ही शहरों में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें फेरी वालों और दूसरे गरीब स्वरोजगार वालों को भी शामिल करना चाहिए। लेकिन सरकार ने सिर्फ चार श्रेणियों के लिए कैश ट्रांसफर की घोषणा की है- महिला जनधन खाताधारक, वरिष्ठ नागरिक, विधवा व दिव्यांग और किसान। इस तरह उसने बड़ी संख्या में शहरी अनौपचारिक कामगारों को छोड़ दिया है।
सरकार ने कंस्ट्रक्शन कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपकर कोष (सेस फंड) के इस्तेमाल की बात कही है। इसे भी राहत पैकेज की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कामगार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर स्कीम के तहत पंजीकृत हैं तो वे फंड से ‘अपने धन का ही’ इस्तेमाल करेंगे। यह इस कोष के सदुपयोग का अच्छा मौका है, लेकिन इसे किसी भी तरह से राहत उपाय नहीं कह सकते। कई राज्य सरकारों ने भी इन श्रमिकों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है, लेकिन वहां भी रजिस्ट्रेशन की शर्त है।
वैसे यह अच्छा है कि सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वालों की दिहाड़ी 20 रुपये बढ़ा दी है, लेकिन बढ़ने के बाद भी दिहाड़ी 202 रुपये है। यह सबको पता है कि कृषि मजदूरों की तुलना में मनरेगा में काम करने वालों की दिहाड़ी बहुत कम है। सी-कैटेगरी के शहरों में कृषि मजदूरों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये है। मनरेगा और कृषि मजदूरों की मजदूरी के बीच समानता की मांग पुरानी है, फिर भी इस पर अमल नहीं किया गया है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि हर परिवार को मनरेगा के तहत औसतन 45-50 दिनों का ही काम मिलता है। पिछले चार वर्षों से यही औसत बना हुआ है, हालांकि राज्यों के आधार पर इसमें अंतर हो सकता है। सरकार की ही रिपोर्ट बताती है कि 2019-20 के दौरान 7.77 करोड़ लोगों और 5.41 परिवारों को इस योजना के तहत काम मिला।
भारत का श्रम बाजार जिस तरह बंटा हुआ और अनौपचारिक है, उसे देखते हुए वित्त मंत्री के राहत पैकेज से लोगों को बेहद सीमित सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी। बेशक, राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राहत उपाय लेकर आ रही हैं। ये राष्ट्रीय योजना के पूरक के रूप में काम करेंगे।
(लेखक एक्सएलआरआइ, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर में प्रोफेसर हैं)
पैकेज सबके लिए नहींः कंस्ट्रक्शन सेक्टर के सिर्फ रजिस्टर्ड कर्मचारियों को मिल पाएगी मदद