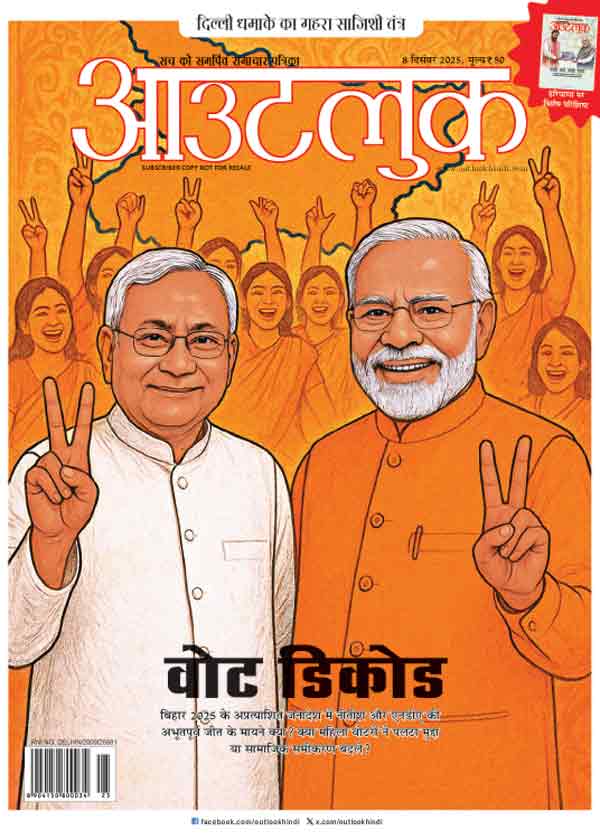मानव जीवन की सबसे भयावह त्रासदी तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने अस्तित्व से हार मान लेता है। भारत में आत्महत्या केवल व्यक्तिगत संकट नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में भारत में 1,71,765 लोगों ने आत्महत्या की, जो प्रतिदिन औसतन 470 आत्महत्याएँ दर्शाता है। इनमें सबसे ज़्यादा मामले 18 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं में पाए गए — जो देश की सबसे सक्रिय और उत्पादक जनसंख्या है। आर्थिक संकट, परीक्षा में असफलता, पारिवारिक कलह, बेरोज़गारी, अवसाद, और प्रेम में असफलता इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। आत्महत्या अक्सर एकाएक नहीं होती, यह मानसिक पीड़ा का एक क्रमिक परिणाम है, जिसे समाज अक्सर ‘कमज़ोरी’ मानकर नज़रंदाज़ कर देता है।
पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्याओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। NCRB के आँकड़े बताते हैं कि 2019 में 1.39 लाख, 2020 में 1.53 लाख और 2022 में 1.64 लाख आत्महत्याएँ हुईं, जो लगातार बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। विशेष चिंता का विषय यह है कि छात्रों और किसानों में आत्महत्या की दर बढ़ रही है। 2022 में करीब 13,000 छात्रों और 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। कोरोना महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की कमी, डिजिटल अवसाद, सोशल मीडिया का दबाव, और आर्थिक असुरक्षा जैसे नए कारक उभरकर सामने आए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के बोझ और शहरी युवाओं में प्रतिस्पर्धा की दौड़, आत्ममूल्य की भावना को तोड़ देती है। मानसिक स्वास्थ्य अब केवल अस्पतालों का विषय नहीं, बल्कि नीति निर्माण का केंद्रीय मुद्दा बन चुका है।
समस्या की जड़ में केवल व्यक्तिगत परिस्थितियाँ नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा वातावरण भी है जो व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि वह सुना नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, और किसी भी सामाजिक सहारे से वंचित है। आत्महत्या को रोकने के लिए सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य पर कलंक (stigma) हटाना आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों में भावनात्मक साक्षरता (emotional literacy) को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, आत्महत्या रोकने के लिए समय रहते परामर्श और चिकित्सकीय हस्तक्षेप सबसे कारगर हैं। हेल्पलाइन जैसे ‘iCall’, ‘AASRA’, और सरकार की ‘KIRAN’ जैसी सेवाओं का विस्तार ज़रूरी है। मीडिया को भी आत्महत्या की खबरों को सनसनीखेज़ ढंग से पेश करने से बचना चाहिए। परिवार और समुदाय की सतत निगरानी, संवाद और समर्थन ही वह दीवार बन सकती है जो एक व्यक्ति को उस आखिरी कदम से रोक सके।
समाज की भी भूमिका आत्महत्या की रोकथाम में निर्णायक है। जब कोई युवा, महिला, बुज़ुर्ग या छात्र आत्महत्या करता है, तो कहीं-न-कहीं समाज की असंवेदनशीलता भी उसके पीछे होती है। हम अक्सर संघर्षशील व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को ‘कमज़ोरी’ या ‘ड्रामा’ मानकर उसकी उपेक्षा करते हैं। पितृसत्ता, जातीय भेदभाव, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, या LGBTQ समुदाय के प्रति अस्वीकार — ये सब सामाजिक कुचक्र उस अकेलेपन को जन्म देते हैं, जो आत्महत्या की ज़मीन बनता है। यदि समाज सहानुभूति, स्वीकार्यता और संवाद की संस्कृति को बढ़ावा दे, तो यह आत्मघाती प्रवृत्तियों को कम कर सकता है। हर व्यक्ति को यह महसूस कराना कि उसकी उपस्थिति महत्त्वपूर्ण है, एक शक्तिशाली सामाजिक दवा बन सकता है।
सरकार की जिम्मेदारी केवल हेल्पलाइन चलाने या मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय को आत्महत्या को राष्ट्रीय संकट घोषित कर, इसे स्वास्थ्य बजट का एक प्रमुख हिस्सा बनाना चाहिए। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य बजट का मात्र 1.3% खर्च होता है, जो वैश्विक औसत (5%) से बहुत कम है। मानसिक चिकित्सकों की भारी कमी (1 लाख की जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक) और समर्पित संस्थानों की कमी, इस संकट को और गहरा करती है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) को ज़मीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। सरकार को ऐसे ‘सुसाइड क्लस्टर्स’ की पहचान करनी चाहिए जहाँ बार-बार आत्महत्याएँ होती हैं, और वहाँ विशेष हस्तक्षेप करने चाहिए।
दुनिया के कई देशों ने आत्महत्या रोकथाम के प्रभावी मॉडल तैयार किए हैं। जापान में रेलवे स्टेशनों पर नीली लाइट्स लगाई गईं क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से तनाव कम करने में सहायक पाई गईं। ऑस्ट्रेलिया ने ‘HEADSPACE’ नामक राष्ट्रीय युवा मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की है, जिसमें 12-25 वर्ष के युवाओं के लिए नि:शुल्क काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाती है। यूके ने ‘सैमेरिटन्स’ नामक हेल्पलाइन को सुदृढ़ बनाया, और स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य किया गया। फ़िनलैंड में ‘Zero Suicide’ नामक रणनीति अपनाई गई, जिसके तहत हर आत्महत्या की पृष्ठभूमि की जाँच और विश्लेषण होता है ताकि भविष्य में उसे रोका जा सके। भारत को भी इन उदाहरणों से सीखकर अपने सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में आत्महत्या निरोधी नीति तैयार करनी चाहिए।