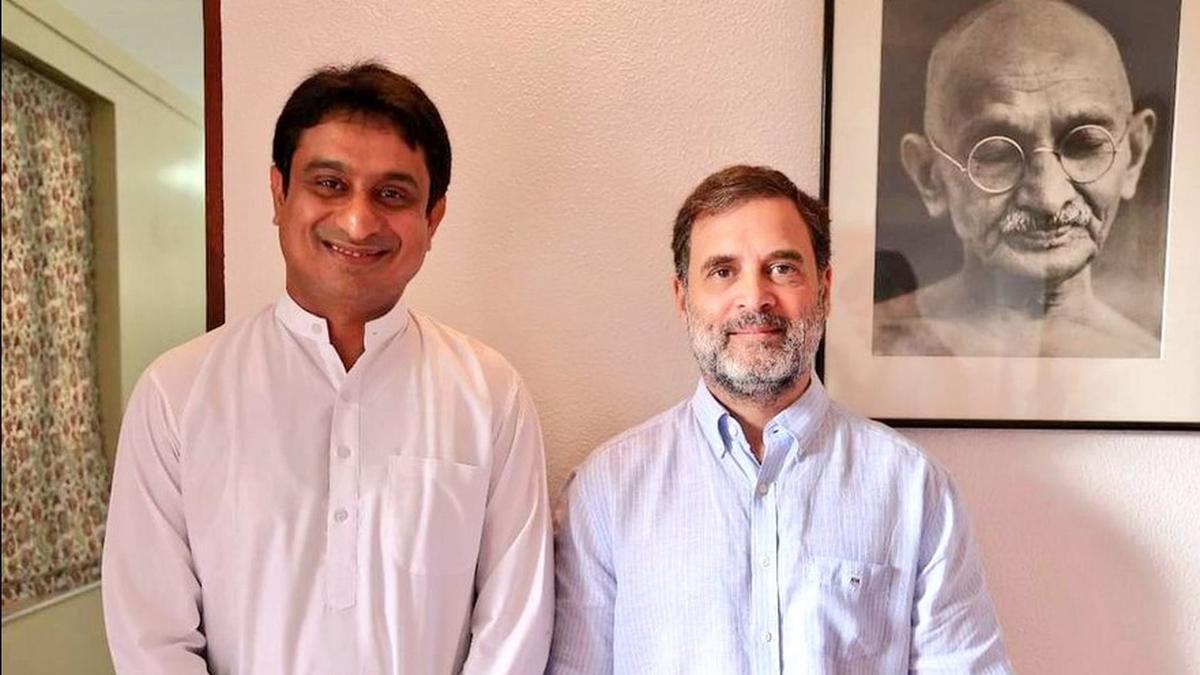दीवार हिंदी
निर्देशश: यश चोपड़ा
वर्ष: 1975
कलाकार: अमिताभ बच्चन, शशि कपूर,
परवीन बॉबी, निरूपा रॉय, मदन पुरी
सन 1955 में आई फिल्म श्री 420 में राज कपूर रोजी-रोटी की खातिर इलाहाबाद से मुंबई आता है। सीधा-साधा राज मायानगरी में माया (नादिरा) के मायाजाल में फंसकर चार सौ बीसी से संपत्ति जरूर अर्जित कर लेता है लेकिन उसका जमीर उसे भटके हुए रास्ते की याद दिलाता है। अंत में राज कपूर विद्या (नर्गिस) के साथ सादगीपूर्ण जिंदगी की ओर लौट जाता है। स्वतंत्रता के 28 साल बाद 1975 में राज कपूर वाला यह रोमांटिसिज्म खत्म हो चुका था। एक बड़ा वर्ग बेइंसाफ व्यवस्था का शिकार था। इस प्रचलित व्यवस्था की दीवार से टकराने का साहस कुछ ही लोगों में था और इसके लिए अनुचित मार्ग अपनाने से भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। 24 जनवरी 1975 को इसी मनोवृत्ति को दशाने वाली फिल्म दीवार रिलीज हुई। आलोचक इस फिल्म को अलग-अलग परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। मेरी राय में सलीम-जावेद साहब ने यह फिल्म विजय (अमिताभ बच्चन) के नजरिये से लिखी है। विजय के हाथ पर लिखा है, 'मेरा बाप चोर है।’ यह विजय के मन में विद्रोह का पहला बीज है। वहीं से वह जिंदगी को अलग तरह देखता है और ईमानदार इंस्पेक्टर भाई रवि (शशि कपूर) की परवाह नहीं करता। 'मैं आज भी फेंके हुए हुए पैसे नहीं उठाता’ या मंदिर में भगवान को 'खुश तो बहुत होंगे तुम’ विजय के विद्रोही तेवर को बढ़ाते हैं। इसी साल देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। इसी से समझा जा सकता है कि दीवार में व्यवस्था से सीधा टकराने वाला और उसे खारिज करने वाला अमिताभ बच्चन का किरदार उन दिनों के समाज का कैसा चित्रण दिखाता था।
केतन जोशी
पल्प फिक्शन अंग्रेजी
निर्देशक: क्वेटिन टेरंटिनो
वर्ष: 1994
कलाकार: जॉन ट्रेवोल्टा, उमा तुरमैन, ब्रूस विलिस,
सैमुएल एल जैक्सन, हार्वे कीटल, क्रिस्टोफर वाकेन
पेशेवर हत्यारे विंसेंट (जॉन ट्रेवोल्टा) को एक शाम अपने नशे के कारोबारी बॉस मार्सेलस वालेस की पत्नी मिया का मनोरंजन करना है। दोनों बार में बैठे हैं और टल्ली हैं। ऐसे में वह उसे अपने पति की कहानी सुनाती है जो सबको पता है कि कैसे उसके पति ने एक लडक़े को इस आरोप में अपने घर की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया था कि वह मिया को फुट मसाज दे रहा था जबकि वह सिर्फ हाथ मिला रहा था। उसी समय विश्व प्रसिद्ध ब्लैक रैबिट स्लिक्वस ट्विस्ट कॉन्टेस्ट की घोषणा होती है। एमसी भागीदारों के बारे में पूछता है और मिया कहती है 'यहां हैं।’ विंसेंट का मुंह फक पड़ जाता है मगर मिया उसे डांस फ्लोर पर खींच ले जाती है। अगले पांच मिनट जो होता है उसे पूर्णत: जादू कह सकते हैं। थुरमैन और ट्रेवोल्टा (उन्होंने सैटरडे नाइट फीवर के कुछ बचे हुए डांस स्टेप यहां दिखाए हैं) दोनों ने शानदार ट्विस्ट नंबर पेशकर यह ट्राफी जीत ली। निर्देशक टेरंटिनो ने एक इंटरव्यू में माना कि यह दृश्य फिल्माने की प्रेरणा उन्हें अन्ना केरनीना की बैंड अ पार्ट से मिली। पल्प फिक्शन ऐसे दृश्यों से भरा है और यह टेरंटिनो का कमाल है कि यह सभी लड़ियां खूबसूरती से अंत में जुड़ती हैं। इस फिल्म को बने दो दशक हो चुके हैं मगर आज भी सियोल से साउ पाउलो तक हर फिल्मकार इसके जादू के सामने नतमस्तक हैं।
गोपी गायन बाघा बायन बांग्ला
निर्देशक: सत्यजित रे
वर्ष: 1969
कलाकार: रबि घोष, तपन चटर्जी
एक महान फिल्मकार बच्चों की दुनिया को कैसे संवेदनशील ढंग से टटोलते हैं, इसकी बेमिसाल नजीर है-सत्यजित रे की ऐतिहासिक फिल्म गोपी गायन, बाघा बायन। यह फिल्म 1969 में सत्यजित रे ने बनाकर एक जबर्दस्त प्रयोग किया था, जिसे जनता ने बेहद सराहा था। इस फिल्म को मैं शायद इसलिए कभी नहीं भूल सकती क्योंकि इसमें बेहद सहज ढंग से, बिना उपदेशात्मक हुए यह बताया, 1. इनसान में अगर चाह हो, तो वाकई राह मिलती है, 2. हर व्यक्ति में हुनर होता है और वह किसी भी सूरत में बेकार नहीं जाता, 3. जीवन में खाने, घूमने और गाने-बजाने के सुख से वंचित नहीं होना चाहिए, खासतौर से एक कलाकार को। बच्चों के मन को टटोलने वाली यह फिल्म दिमाग में बसी रहती है, अपने संगीतमय ताने-बाने के साथ। सहज, सरल जीवन को परदों में उतारने में महारथी सत्यजित रे की यह फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ऐसे दो व्यक्तियों -गोपी और बाघा की कहानी है, जिन्हें गाने और ढोल बजाने की शौक था, लेकिन वे बेहद बेसुरे थे और राजा ने उन्हें खराब गाने और बजाने की सजा सुनाई और जंगल भेज दिया। जंगल में उनके हुनर पर भूतों का राजा प्रसन्न हो गया। वरदान दे डाला और इसने उनकी जिंदगी बदल दी। गाना और संगीत बजाना सिर्फ इनसानों की दुनिया को ही मोहित नहीं करती, बल्कि जानवरों-भूतों की दुनिया को प्रभावित करती है, युद्ध को पलटती है। इसके गाने भी लोट-पोट कर देते हैं। फिल्म देखते हुए बच्चे हों या बूढ़े किसी को नहीं लगता कि यह कल्पना की दुनिया है। ये संसार सत्यजित रे की दूसरी फिल्मों से अलग है, लेकिन इसमें भी किरदार असली जिंदगी वाले लगते हैं।
भाषा सिंह

बंदिनी हिंदी
निर्देशक: बिमल रॉय
वर्ष: 1963
कलाकार: अशोक कुमार, नूतन, धर्मेंद्र
यदि किसी पुरुष का प्रेम स्त्री को ताकत देता है तो उसी पुरुष का धोखा उसे हत्यारिन भी बना सकता है। बंदिनी इसी प्रेम और गलतफहमी की कहानी है। अपने पुराने प्रेमी को वह शादीशुदा मर्द के रूप में देखती है। वह उस औरत की तीमारदारी करती है और जब जानती है कि वह उसके सुख-संसार पर बैठी है तो उसे जहर दे देती है। बिमल रॉय इसे सिर्फ एक दृश्य से दिखा देते हैं। कल्याणी स्टोव में पंप करती हुई हवा भर रही है। पुरानी बातें उसके आसपास घूम रही हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा स्टोव में हवा भरने की तेजी से पता चलता है और यही गुस्सा उसे बंदिनी यानी कैदी बना देता है। बिमल रॉय की नायिका को इसका कोई मलाल नहीं है। यही उस स्त्री का सशक्तीकरण है। वह अपने काम और व्यवहार से जेल में सभी का दिल जीतती है यह उसका प्रायश्चित है। एक स्त्री अपनी पूरी शक्ति के साथ कैसे दुनिया की हो जाती है, कैसे दुनिया को अपना बना लेती है यह इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। बिमल रॉय ने इनसानी मनोवृत्ति की इतनी परतों पर काम किया है कि हर व्यक्ति उन किरदारों को कहीं न कहीं से जोड़ लेता है। जो स्त्री किसी की हत्या के जुर्म में सजा काट चुकी है, वही छूत की बीमारी से ग्रसित एक स्त्री की सेवा को तैयार है। आखिर में वह अपने प्रेमी की मजबूरी जान कर वह सब कुछ छोड़ उसके साथ चल देती है। बिमल रॉय ने फिल्म को एक कविता की तरह परदे पर रचा है।
आकांक्षा पारे काशिव
द गॉडफादर अंग्रेजी
निर्देशक: फ्रांसिस फोर्ड कोपोला
वर्ष : 1972
कलाकार: मार्लन ब्रांडो, अल पचिनो
क्या आपको पता है कि आज संगठित अपराध की हर घटना को माफिया नाम से पुकारना संभव नहीं होता यदि दुनिया में एक किताब और उस पर बनी फिल्म न होती। मारियो पूजो ने अमेरिका में सिसिलियन माफिया की काल्पनिक कहानी को इतनी शिद्दत से कागज पर गॉडफादर की शक्ल में उतारा कि पूरी दुनिया में संगठित अपराध की हर टोली को ही लोग माफिया कह कर पुकारने लगे। इतनी प्रसिद्ध रचना को जब पर्दे पर उतारने का सवाल हो तो जाहिर है कि इसके लिए हर चीज उत्कृष्ट ही होनी चाहिए। हॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों मार्लन ब्रांडो और अल पचिनो से सजी 1972 की द गॉडफादर ने इस मामले में लोगों को निराश नहीं किया और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पर्दे पर अपराध की काली दुनिया का नया शाहाकार रच दिया। सिर्फ एक-दो दृश्य ही नहीं, पूरी फिल्म इतनी शानदार बनी कि पूरी दुनिया में इससे प्रभावित होकर सैकड़ों फिल्में बनीं। इटली के छोटे से इलाके सिसली से भागकर सपनों के देश अमेरिका पहुंचे एक आम इनसान के संगठित अपराध की दुनिया का बादशाह बनने और फिर उसका कारोबार संभालने के अनिच्छुक उसके सबसे छोटे बेटे के एक क्रूर माफिया बॉस बनने की कहानी ने सफलता का ऐसा अध्याय रचा कि महज 70 लाख डॉलर में बनी इस फिल्म ने पूरी दुनिया में करीब 28 करोड़ डॉलर की कमाई कर डाली। रिलीज के 43 साल बाद भी संगठित अपराध पर बनी कोई भी फिल्म देखें तो उसमें गॉडफादर की छाप जरूर दिखेगी।
सुमन कुमार

चुपके चुपके हिंदी
निर्देशक: ऋषिकेश मुखर्जी
वर्ष: 1975
कलाकार: धर्मेंद्र, जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर
ऋषिकेश मुखर्जी यानी ऋषि दा फिल्में बना कर हंसाते नहीं बल्कि गुदगुदाते थे। उनके पात्र परदे पर अदायगी करने के बजाय सामने बैठकर दर्शकों से बतियाते थे और परिवार के सदस्य की तरह ही लगते थे। जिस साल शोले रिलीज हुई थी उसी साल जय और वीरू, परिमल त्रिपाठी और सुकुमार सिन्हा बने थे। एक फिल्म में दोनों छटे हुए बदमाश, सडक़छाप के रूप में दर्शकों को लुभा रहे थे तो वहीं ऋषि दा ने दोनों को इतनी विश्वसनीयता से पेश किया कि लगा ही नहीं कि ये दोनों गुंडे प्रोफेसर के रूप में यहां विशुद्ध हास्य रच सकते हैं। शरारत में शर्मिला टैगोर ने भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। जया प्रदा का खिलंदडपन उतना ही ताजा रहा जितना गुड्डी में था। खुद को होशियार समझने वाले जीजा जैसा किरदार इतना सहज था कि केंद्र में रहकर हर पात्र को उसने बांधे रखा। 'अबके बरस सावन में आग लगेगी बदन में’ जैसे गाने ने उस शरारत को और शोख कर दिया जो ऋषि दा ने परदे पर रची थी। वसुधा जब प्रेम में डूबी तो सुकुमार का बॉटनी ज्ञान कितना 'खतरनाक’ हो गया यह दर्शकों को आज भी गुदगुदाता है। पूरी फिल्म में मीठी सी गफलत है। कोई यहां, कोई वहां और सब एक साथ। ऋषिकेश मुखर्जी परिवार के लिए फिल्म बनाने में माहिर थे। उनकी फिल्म पारिवारिक होती थी और परिवार को बांधे रखने के हुनर के साथ रहती थी। उनकी फिल्मों में न नाटकीय संवाद होते थे, न बेकार का ड्रामा। फिर भी आज भी उनकी फिल्में सबके चेहरे पर मुस्कराहट ले आती हैं।
आकांक्षा पारे काशिव
ड्रेस्ड टू किल अंग्रेजी
निर्देशक: ब्रायन डी पामा
वर्ष: 1980
कलाकार: एंजी डिकिंसन, नैंसी एलेन, माइकल केन
सन 1980 में जब तक ब्रायन डी पामा ने ड्रेस्ड टू किल नहीं बना ली थी तब तक उन्हें अल पचीनो को लेकर बनाई गई अपनी प्रसिद्ध फिल्म स्कारफेस और द मास्टर ऑफ मैकाब्रे के लिए अल्फ्रेड हिचकॉक को आदरांजलि देने वाला फिल्मकार ही माना जाता था। निर्देशक का खुद का मानना था कि एंजी डिकिंसन का हत्या का सीन उनके द्वारा फिल्माया सबसे अच्छा सीन था। डी पामा चाहते थे यह भूमिका लिव उल्लमैन निभाएं। लेकिन इस सीन की हिंसा देख कर उन्होंने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया। सीन कॉनेरी खुद इसमें भूमिका निभाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके कुछ दूसरे वादे थे जिनकी वजह से वह इस फिल्म से नहीं जुड़ पाए। हालांकि बाद में पामा के साथ द अनटचेबल्स में उनके साथ किया था। यह फिल्म एक सिरे से सूत्र में बंधी कहानी के बजाय अलग-अलग सीन की कहानी थी जो अपने आप में एक कहानी की तरह अनूठा था। जैसे-कभी न भुलाया जानेवाला पूरे दस मिनट का संग्रहालय का सीन और सीन में पागल बना देने वाले संवाद। यह फिल्म के अनुभव को पक्के तौर पर दर्शक के जेहन में बसा देती है। माइकल केन ने इस फिल्म में दोहरे व्यक्तित्व वाले परेशान चरित्र को विश्वसनीयता से परदे पर उतारा था। जिसे पटकथा ने और ज्यादा असली बना दिया था। ड्रेस्ड टू किल रोलर कोस्टर की तरह दर्शकों को बांधे रखती है और पामा को बार-बार दाद देने को उकसाती है।
कंटेंप्ट फ्रेंच
निर्देशक: ज्यां ल्यूक गोदार
वर्ष: 1963
कलाकार: ब्रिजित बार्डोट, मिशेल पिकोली
ज्यां ल्यूक गोदार की कंटेंप्ट उनकी महान फिल्मों से से एक है। महान दोनों संदर्भों में- इसके निर्माण और इसके बनाने के दौरान आने वाली परेशानियों के संदर्भ में भी। गोदार ऐसे निर्देशक थे, जिन्होंने सिनेमा माध्यम को कुशलता से चलाया। ब्रिजित बार्डोट की देहयष्टि को इतनी खूबसूरती से गोदार ही दिखा सकते थे। उनकी नग्न देह को गोदार के कैमरे ने कई सीन में इस्तेमाल किया। उनका लक्ष्य एक स्त्री की नग्नता को दिखाने से ज्यादा यह दिखाना था कि क्यों एक फ्रेंच महिला अपने प्रेम करने वाले पति से नफरत पाल लेती है, जो इटली में फिल्मों की पटकथा लिखकर ढेर सारा पैसा कमा रहा है। अल्बर्टो मोराविया के उपन्यास पर आधारित कंटेंप्ट में विवाहित जोड़े के बीच पैदा होती कड़वाहट और उनकी वैवाहिक धुन के बिगडऩे की कहानी है। यह पति-पत्नी के बीच की दुरूह दास्तान है जिसमें वाक् युद्ध और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के साथ ही एक-दूसरे के साथ रहते और अंदर कहीं न कहीं प्यार होने को दिखाया है। कहानी में फिल्म का सेट है जिसमें पत्नी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि निर्माता और उसके पति के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। एक अपार्टमेंट में पति-पत्नी की दिनचर्या को फिल्माते हुए गोदार ने इंडोर शूटिंग का बेहतरीन नमूना पेश किया है। दोनों पति-पत्नी नहा रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, एक साथ हैं लेकिन फिर भी अलग-अलग हैं। यह बहस फिल्म के सेट तक भी पहुंचती है और वहां पत्नी कहती है कि उससे घृणा करती है और उसे छोडऩे का निर्णय उसने ले लिया है। गोदार ने रोचक तरीके से फ्रेंच, इटैलियन और अंग्रेजी के संवाद का प्रयोग किया है। एक दुरूह रिश्ते की गलियों से गुजरते हुए कंटेंप्ट रोचक अंत तक पहुंचती है।
अमर अकबर एंथनी हिंदी
निर्देशक: मनमोहन देसाई
वर्ष: 1977
कलाकार: अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, प्राण
एक परिवार के बिछडऩे और अंत में मिलने की बेहद आम-सी कहानी पर निर्माता-निर्देशक मनमोहन देसाई ने ऐसी फिल्म गढ़ दी थी जो आज तक याद की जाती है। सन 1977 में जब अमर अकबर एंथनी आई थी तो लोग परिवार सहित इस फिल्म को देखने गए थे। फिल्मी भाषा में कहें तो इस फिल्म में सारे मसाले थे। बरसों कहानी का यह 'प्लॉट’ बाकी फिल्मों में कॉपी होता रहा। इस फिल्म में तीन किरदार और तीन धर्म का फॉर्मूला भी बहुत हिट हुआ। इस वजह से मनमोहन तीन अलग-अलग स्वभावों को बखूबी परदे पर दिखा पाए। पुलिस वाला सख्त (विनोद खन्ना), अनाथालय में पला थोड़ा नासमझ (अमिताभ बच्चन) जिसने दर्शकों को खूब हंसाया और एक लडक़ी के पिता को मनाने वाला थोड़ा व्यावहारिक (ऋषि कपूर)। परिवार के सदस्यों के बिछडऩे के बाद जो नाटकीयता शुरू होती है वह इस फिल्म की खासियत थी। पैसा वसूल यह फिल्म अब भी टेलीविजन के चार्ट में सबसे ऊपर रहती है। फिल्म में बचपन में बिछड़े तीन भाई हैं जिनकी पवरिश अलग-अलग माहौल के साथ ही अलग धर्मों में होती है। जहां बड़ा भाई एक हिंदू परिवार में पलकर ईमानदार और निष्ठावान निडर पुलिस अधिकारी बनता है तो दूसरा चर्च की सीढिय़ों पर पहुंचकर एक अनाथ ईसाई युवक के तौर पर बड़ा होता है, जो छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े और हेराफेरी करता है। वहीं तीसरा और छोटा भाई इस्लामिक माहौल में परवरिश पाकर एक मुसलमान दर्जी बन जाता हो जो मिजाज से शायर भी होता है और आशिक मिजाज भी। फिल्म का यह पक्ष उसे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करने वाली फिल्म भी बनाता है।
आसिफ सुलेमान खान
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिंदी
निर्देशक: आदित्य चोपड़ा
वर्ष: 1995
कलाकार: शाहरुख खान, काजोल
उन दिनों जवां दिलों की जुबान पर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे (डीडीएलजे) का एक ही गीत रहता था, 'तुझे देखा तो यह जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।’ पंजाब में सरसों के पीले फूलों के बीच शाहरुख खान और काजोल पर फिल्माया यह गीत भारतीय फिल्मों के रोमांस का एक बेहतरीन दृश्य है। इश्क में डूबा हर लडक़ा खुद को राज और लडक़ी सिरमन समझती थी। डीडीएलजे सन 1995 में बनी। फिल्म का निर्देशन निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने किया। शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, फरीदा जलाल ने फिल्म में मुख्य किरदार निभाए। डीडीएलजे के नाम सबसे ज्यादा चलने का रेकॉर्ड है। यह मुंबई के मराठा मंदिर में लगातार लगभग तेरह साल से ज्यादा चली। फिल्म की लोकप्रियता की वजह यह रही कि इसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। पीली सरसों सिल्वर स्क्रीन पर प्रेम के इजहार का सूचक बन गई। करवा चौथ, मेहंदी की रस्म सब ऐसे दृश्य थे जैसे किसी भी पंजाबी परिवार की शादी में होते हैं। सबसे अहम था, फिल्म के 'बाऊ जी।’ हर प्रेम करने वाले जोड़े को वह अपने बाऊ जी लगते थे। फिल्म में जिस प्रकार सिमरन का एनआरआई परिवार पंजाब के गांव में आकर शादी की तैयारियां करता है वह इतना वास्तविक था जैसे असली शादी की तैयारियां। फिल्म का दूसरा गीत 'मेहंदी लगा के रखना’ अरसे तक मेहंदी की रस्म में डीजे पर बजने वाला गीत रहा। गीत ही नहीं, फिल्म के डायलॉग भी अरसे तक दर्शकों की जुबान पर रहे। आखिरी सीन में अमरीश पुरी काजोल का हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, 'जा सिरमन जा, जी ले अपनी जिंदगी’ ने आज तक अपनी ताजगी नहीं खोई है।
मनीषा भल्ला
फार्गो अंग्रेजी
निर्देशक: जोएल कोएन, एथन कोएन
वर्ष: 1996
कलाकार: फ्रांसिस मेकडोरमेंट, विलियम एच मैसी
जोएल एवं इथान कोएन बंधु ने घर के अंदर हत्या की कहानी पर आधारित फार्गो का ताना-बाना बुना और विषय के विपरीत आनन-फानन में इसे बना डाला। इस फिल्म की थकाऊ यात्रा की जमीन अमेरिकी मिडवेस्ट है जहां के विशाल हिस्से और सडक़ों के बीचो बीच घर जैसे माहौल में लोक संगीत चलता रहता है। थोड़ी हास्यपूर्ण इस फिल्म में एक कार सेल्समैन फिरौती के लिए अपनी पत्नी का अपहरण करा देता है। उसे लगता है कि उसके ससुर सर्दियों में हुई बर्फबारी से अटी जमीन के जरिये जल्द ही फिरौती की राशि गिरा देंगे। लेकिन इस घटनाक्रम में एक के बाद एक छोटी-छोटी घटनाएं प्रतिकूल होती जाती हैं जिस कारण दूसरे छोर पर मौजूद अपहर्ताओं, हठी लेकिन कमजोर इच्छाशक्ति वाले सेल्समैन तथा अडिय़ल ससुर के लिए स्थितियां बिगड़ती जाती हैं। ज्यादातर दर्शक और प्रशंसक और जो लोग बीच में फार्गो के रोचक तूफानी मिजाज को पसंद नहीं करते, लेकिन पूरी फिल्म में शांत रहते हैं, वे भी इसे फ्रांसेस मैकडोर्मंड के अभिनय के रूप में याद करते हैं। इसमें फ्रांसेस एक गर्भवती पुलिस प्रमुख की भूमिका में हैं और अपहर्ताओं का पीछा करना नहीं छोड़ती। जब यह मामला सुलझ जाता है तो पति के साथ इस खुशी का वह साझा करना चाहती है लेकिन पति यह जानने की भी कोशिश नहीं करते कि वह ठीक तो है। इस चिड़चिड़े व्यक्ति की चिड़िया की पेंटिंग को अमेरिकी डाक टिकट के लिए चुना गया है लेकिन यह जानकर निराश हो जाता है कि उसकी पेंटिंग तीन सेंट के टिकट के लिए ही चुनी गई है और उसे ज्यादा मूल्य भी नहीं मिला। फ्रांसेस उसे दिलासा देती है और उसे अपने होने वाले बच्चे की याद दिलाती है।
लगे रहो मुन्नाभाई हिंदी
निर्देशक: राजकुमार हिरानी
वर्ष: 2006
कलाकार: संजय दत्त, विद्या बालन, अरशद वारसी, बोमन ईरानी
भरपूर मनोरंजन वाली इस सीक्वल फिल्म में निर्माता विधु विनोद चोपड़ा और निर्देशक राजकुमार हिरानी ने नए अंदाज में गांधीगीरी को पेश किया। यह संभवत: पहली ऐसी सफल फिल्म थी जिसमें हास्य और भावनाओं का बेहतरीन संतुलन देखा गया। एक दशक बीत जाने के बाद भी इस फिल्म के दृश्य और संवाद दर्शकों के जेहन में आज भी कैद हैं। टपोरियों की भाषा में गांधीगीरी का संदेश देना और फिर इससे सामने वाले को प्रभावित करना ही इस फिल्म की खासियत है। संजय दत्त ने मुन्नाभाई और अरशद वारसी ने सर्किट की सशक्त भूमिका में जता दिया है कि गांधीजी के सिद्धांतों पर अमल करते हुए देश की हर समस्या का हल संभव है। हालांकि 2006 में आई इस फिल्म पर गांधीवादी बुद्धिजीवियों ने आपत्ति भी उठाई थी लेकिन फिल्म की अपार सफलता ने 'गांधीगीरी’ को इतना मशहूर बना दिया कि देश-दुनिया के मीडिया में भी यह शब्द स्थापित हो गया। वृद्धाश्रम की जमीन हड़पने वाले लकी सिंह (बोमन ईरानी) से मुन्नाभाई और सर्किट ने जिस अंदाज में जमीन वापस लेने की कोशिश की है वह खत्म होते जा रहे गांधीजी के सिद्धांतों, विचारों और मूल्यों को एक बार फिर प्रासंगिक बनाती है। इक्कीसवीं सदी के युवाओं के बीच गांधीजी की तस्वीर या तो धुंधली पड़ चुकी थी या उनके सिद्धांतों को हास्यास्पद मान लिया गया था लेकिन इसकी 'जादू की झप्पी’ ने एक बार फिर इन युवाओं को यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि लगे रहो मुन्नाभाई। फिल्म का संदेश भी यही था कि हर इनसान के अंदर गांधीगीरी है, बशर्ते कि वह गांधी की आवाज सुन सके।
राजेश रंजन
नायकन तमिल
निर्देशक: मणि रत्नम
वर्ष: 1987
कलाकार: कमल हासन, शरण्या, जनगराज
पूरी दुनिया में द गॉडफादर से प्रेरित होकर जो फिल्में बनीं उनमें 1987 में तमिल भाषा में बनी मणिरत्नम निर्देशित और कमल हासन अभिनीत नायकन सबसे अलग है। यूं तो बॉम्बे में अपराध की दुनिया पर दीवार जैसी सफल फिल्म पहले बन चुकी थी मगर नायकन ने अपराध की असली दुनिया से लोगों का परिचय कराया। नायकन को बॉम्बे के एक समय के डॉन वरदराजन मुदलियार की कहानी भी बताया जाता है। यह फिल्म सिर्फ अपने कथानक की वजह से ही नहीं बल्कि इलैयाराजा के मधुर संगीत की वजह से भी सफलता के कई पायदान चढ़ गई। इसकी सफलता से प्रेरित होकर फिरोज खान ने विनोद खन्ना को मुख्य भूमिका में लेकर हिंदी में इसे दयावान के नाम से बनाया। दोनों फिल्मों की भाषा भले ही अलग थी मगर कहानी में कोई बदलाव नहीं किया गया था। दाऊद इब्राहिम और उसके बाद की पीढ़ी के अंडरवर्ल्ड दादाओं से परिचित हमारी आज की युवा पीढ़ी को यह जरूर जानना चाहिए कि आखिर मुंबई अपराध की इतनी बड़ी राजधानी कैसे बनी थी। इसके लिए यह फिल्म 2016 में देखने के लिए आपकी लिस्ट में होनी ही चाहिए।
सुमन कुमार
जागते रहो हिंदी
निर्देशक: अमित मित्र, शंभु मित्र
वर्ष: 1956
कलाकार: राजकपूर, डेजी ईरानी, नरगिस
साल 1956 में आई हिंदी फिल्म जागते रहो सामाजिक व्यंग्य है। इस फिल्म ने सभ्य समाज के परदे के पीछे छिपे काले सच को उजागर किया। फिल्म के 60 साल पूरे होने के बाद आज भी यह प्रासंगिक बनी हुई है। फिल्म में राज कपूर ने एक भोले-भाले मजदूर का किरदार निभाया है, जो काम की तलाश में अपने गांव की ताजगी और मासूमियत छोडक़र महानगर में आने को मजबूर है। नायक शहर पहुंचते ही बड़ी गाडिय़ों और ऊंचे-ऊंचे मकानों में रहने वाले लोगों की शक्ल में भेडिय़ों को देखता है। धीरे-धीरे शहर की असलियत उसके सामने आनी शुरू हो जाती है। यह फिल्म एक रात की कहानी है। रात के साथ फिल्म की कहानी शुरू होती है और सुबह की किरण के साथ ही खत्म हो जाती है। एक ही रात में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, जमाखोरी और अपराध और एक-दूसरे के प्रति तेजी से घट रही संवेदनशीलता फिल्म में आती है। फिल्म का प्लॉट बड़े शहर की बड़ी इमारत है जिसमें गांव से नौकरी की तलाश में आया एक भूखा-प्यासा गरीब बेनाम आदमी चौकीदारों के डर से घुस जाता है। नायक इमारत में रहने वाले लोगों के काले कारनामे देख पाने का मौका अनायास पाता है। वहां अवैध शराब बनाने वाले से लेकर नकली नोट छापने वाले सफेदपोश सेठ रहते हैं। नायक न चाहते हुए भी इमारत में रहने वाले लोगों की काली करतूतों का गवाह बनता है। फिल्म में उसे चोर समझकर रात भर लोग उसकी तलाश करते हैं और वह उन्हीं के बीच मौजूद रहता है। खुद बेपर्दा हो जाने के डर से लोग चुप लगा जाते हैं। लोगों की अपनी कमजोरियां ही रात भर उसका बचाव करती हैं। एक मजबूर शख्स की एक रात की लुकाछिपी की जिंदगी कई बड़े दिलचस्प किरदार सामने लाती है। फिल्म का निर्देशन इप्टा के शंभू और अमित मित्र ने किया था। राज कपूर में कथानक को समझने की विलक्षण प्रतिभा थी। इसी वजह से उन्होंने न सिर्फ इस अनूठी फिल्म में काम किया बल्कि इसका निर्माण भी किया था। फिल्म में राज कपूर की मुश्किल से दो संवाद पाने वाली भूमिका उनके अभिनय जीवन की अविस्मरणीय भूमिका है।
आसिफ सुलेमान खान
साहिब बीबी और गुलाम हिंदी
निर्देशक: अबरार अल्वी
वर्ष: 1962
कलाकार: गुरु दत्त, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, रहमान
एक फिल्म जो शादीशुदा महिलाओं की सेंसुएलिटी, बेवफा पति को साधने की तड़प और तेजी से ढहते सांमती ढांचे को एक साथ बांधकर सतरंगी अमर वितान रचती है तो वह है साहब बीबी और गुलाम। इसमें छोटी बहू का जगमग रूप, शराब के नशे से चूर उनकी गुलाबी आंखों का जादू, मीना कुमारी के तमाम किरदारों पर भारी-सा पड़ता है। इसमें एक तरफ मांग में लाल चटक सिंदूर भरती, घुंघराले बालों को संवारती मीना कुमारी हैं, जो कोठों पर बैठने के शौकीन अपने पति (रहमान) को अपने पहलू में बांधने को सारे जतन करने को तैयार नजर आती हैं, दूसरी तरफ चमड़े के चमर-चमर जूते पहने आंखें फाड़े भूतनाथ (गुरुदत्त) और उस पर फिदा जबा (वहीदा रहमान) नजर आती हैं। सारे किरदार बेहतरीन अदाकारी से एक जटिल समाज की भावनात्मक कहानी को जिस सहजता से निभाते हैं, वह इस फिल्म को सदाबहार फिल्म बनाती है। डगमग चाल से हाथ में शराब का गिलास लिए मीना कुमारी पर जब यह गाना फिल्माया जाता है, न जाओ सईंया छुड़ाकर बइयां तब फिल्म भारतीय स्त्री की एक बिल्कुल अलग छवि को निर्भीक ढंग से सामने रखती है। महिला की सेंसुएलिटी के बारीक धागों की जबर्दस्त पकड़ गुरुदत्त की खासियत है, जो इस फिल्म में छाई हुई है। इसमें एक महिला की चाह, उसका स्वतंत्र अस्तित्व और पति के अलावा किसी पराए पुरुष से अपनी व्यथा कहना किस तरह उसकी हत्या का कारण बनता है, इसे बहुत सशक्त ढंग से बड़े परदे पर उतारा गया है। निर्माता गुरुदत्त और निदेशक अबरार अल्वी के बीच मंझी हुई साझेदारी और बेमिसाल गानों ने इस फिल्म को बहुत मानीखेज बनाया।
भाषा सिंह